डिजिटल युग की रोशनी जितनी तेज है, उतना ही गहरा उसका अंधकार भी है। हम अब एक ऐसे दौर में जी रहे हैं, जहां हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह इंटरनेट पर निर्भर हो चुकी है। हमारे निजी विचार, पसंद-नापसंद, आदतें, संबंध, स्वास्थ्य, बैंक खाते, पहचान-पत्र, कार्यालयी दस्तावेज, सब कुछ डिजिटल हो चुका है। लेकिन इस सुविधा की कीमत भी हमें चुकानी पड़ रही है। कुछ ही दिन पहले जो चौंकाने वाला खुलासा सामने आया, वह यही संकेत करता है कि हम जिन सेवाओं पर आंख मूंदकर भरोसा करते आए हैं, वही अब हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी हैं। साइबर सुरक्षा शोधकर्ताओं ने एक ऐसे डेटा लीक का पर्दाफाश किया है, जिसे तकनीकी इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा साइबर अपराध बताया गया है। 16 अरब से अधिक लॉगइन क्रेडेंशियल्स, जिसमें पासवर्ड, ईमेल, फोन नंबर, सोशल मीडिया आईडी, यहां तक कि पते और कार्यस्थल तक की जानकारी शामिल है, लीक हो चुकी है और डार्क वेब पर बिक रही है। यह कोई साइंस फिक्शन नहीं बल्कि 2025 की एक भयावह वैश्विक सच्चाई है।
यह घटना केवल एक सामान्य डेटा चोरी का मामला नहीं बल्कि एक सुनियोजित, वैश्विक साइबर हमला है, जो महीनों या शायद वर्षों तक चलता रहा और अब जाकर इसका विस्फोट हुआ। इस लीक से गूगल, एपल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, गिटहब जैसे वैश्विक प्लेटफॉर्म्स ही नहीं, कई सरकारी पोर्टल्स और डवलपर प्लेटफॉर्म्स भी प्रभावित हुए हैं। खास बात यह है कि यह डेटा पुराना नहीं बल्कि ताजा है, जिसका अर्थ है कि इस पर कार्रवाई की संभावना भी अत्यधिक सीमित हो चुकी है क्योंकि अपराधी पहले ही इसका इस्तेमाल कर चुके होंगे या कर रहे हैं। डेटा लीक की यह भयावहता केवल संख्या में नहीं है बल्कि इसमें छिपे उस खतरे में है, जो यह हर व्यक्ति, संस्था और समाज पर मंडरा रहा है। एक आम नागरिक सोचता है कि उसका डेटा का कोई क्या करेगा, अब उसकी यह सोच ही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है क्योंकि जब एक व्यक्ति का डेटा चोरी होता है तो उसका पूरा डिजिटल व्यवहार सामने आ जाता है। वह किससे बात करता है, कहां जाता है, किससे खरीदारी करता है, कब अस्पताल जाता है, कौनसी बीमारियों का इलाज ले रहा है, किस बैंक का ग्राहक है, किन वेबसाइट्स पर लॉगइन करता है, कौनसी सामाजिक या राजनीतिक राय रखता है, डेटा चोरी होने के बाद यह सब एक अपराधी के हाथ में हो सकता है।
यह डेटा चोरी ‘इंफोस्टीलर’ नामक मैलवेयर द्वारा की गई है, जो किसी गेम लिंक, फर्जी वेबसाइट, स्पैम ईमेल या पॉपअप के जरिए हमारे फोन, लैपटॉप या टैबलेट में घुसपैठ करता है और वहां से ब्राउजर में सेव पासवर्ड, कुकीज, चैट्स, ईमेल, वॉलेट जानकारी, फॉर्म डिटेल्स और लोकेशन डेटा चुरा लेता है। इसके बाद इस जानकारी को एक खास फॉर्मेट में व्यवस्थित कर डार्क वेब के जरिए बेचा जाता है, ठीक वैसे, जैसे किसी बाजार में सामान बिकता है। शोधकर्ताओं ने पाया कि ऐसे कम से कम 30 डेटासेट हैं, जिनमें से हर एक में औसतन 3.5 अरब रिकॉर्ड्स हैं यानी यह चोरी किसी एक या दो लहर की नहीं बल्कि लगातार बहते एक डिजिटल अपराध के समुद्र की तरह है। इस लीक की सबसे खतरनाक बात यह है कि इसमें शामिल जानकारियों की गुणवत्ता और व्यापकता पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा है। यह केवल ईमेल या पासवर्ड तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें यूजर्स के नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, घर का पता, ऑफिस की जानकारी, मेडिकल रिकॉर्ड्स, लोकेशन हिस्ट्री और यहां तक कि बैंकिंग डेटा भी शामिल है। यह सोचकर ही रूह कांप जाती है कि किसी अनजान अपराधी के पास अब किसी सामान्य नागरिक के जीवन की पूरी जानकारी मौजूद हो सकती है और वह उसका इस्तेमाल धमकाने, ब्लैकमेल करने, फेक प्रोफाइल बनाने, फाइनेंशियल फ्रॉड करने या पहचान बदलने तक में कर सकता है।
साइबर विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में इस लीक का असर और भी गहरा हो सकता है क्योंकि यहां डिजिटल साक्षरता सीमित है, साइबर कानूनों का पालन ढ़ीला है और यूजर्स की सावधानी अपेक्षाकृत कम है। अधिकांश लोग बिना पढ़े किसी भी लिंक पर क्लिक कर देते हैं, बिना जांचे अनजान ऐप डाउनलोड कर लेते हैं और एक ही पासवर्ड कई जगह इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारत की बड़ी आबादी पहले ही इस लीक की चपेट में आ चुकी है, बस उन्हें अभी इसका अहसास नहीं हुआ है। देश में साइबर फ्रॉड की घटनाएं पहले से ही बढ़ रही थी और अब यह लीक उस आग में घी डालने का काम करेगा। ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई ट्रांजेक्शन, आधार लिंक सर्विस, ऑनलाइन हैल्थ रिपोर्ट, सब कुछ अब अपराधियों की जद में हो सकती हैं।
इस डेटा लीक के सामाजिक प्रभाव भी कम भयावह नहीं हैं। एक लड़की, जिसकी निजी तस्वीरें चोरी होकर किसी फेक प्रोफाइल पर पोस्ट हो जाती हैं, एक पत्रकार जिसकी लोकेशन डेटा अपराधियों के पास पहुंच जाती है, एक अफसर, जिसकी निर्णय लेने की गोपनीयता खत्म हो जाती है, एक सेलिब्रिटी, जिसे उसकी निजी चैट्स के जरिए ब्लैकमेल किया जाता है, ये सब अब केवल कल्पनाएं नहीं, वास्तविक उदाहरण हैं, जिनका असर उनके कैरियर, मानसिक स्वास्थ्य और जीवन पर गहरा पड़ता है। यहां तक कि छोटे व्यापारी, स्टार्टअप संस्थान और आम छात्र भी इस खतरे की परिधि में हैं क्योंकि कोई भी अकाउंट, जो इंटरनेट से जुड़ा है, अब सुरक्षित नहीं है। हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े पैमाने पर हुए डेटा लीक के बाद भी किसी देश की सरकार ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। जिन कंपनियों के प्लेटफॉर्म्स से यह डेटा चुराया गया, वे केवल सलाह देने तक सीमित रह गई हैं, ‘पासवर्ड बदलें’, टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करें, ‘पासकी अपनाएं’, ‘सावधानी बरतें’। लेकिन क्या यह पर्याप्त है? क्या ये कंपनियां जिम्मेदार नहीं, जिन्होंने अरबों लोगों का डेटा एकत्र किया और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पाई? क्या कोई ऐसा ठोस तंत्र नहीं होना चाहिए, जिससे यूजर्स को कम से कम यह पता चल सके कि उनका डेटा लीक हुआ या नहीं? विडंबना यह है कि हम जिन सेवाओं को उपयोग करते हैं, उनके लापरवाह ढांचे की वजह से हमारी निजता तार-तार हो रही है और फिर वही कंपनियां हमें कहती हैं कि हम खुद को बचाएं।
इसका समाधान केवल व्यक्तिगत स्तर पर एहतियात बरतने से नहीं होगा। यह वैश्विक डिजिटल संकट है, जिसका समाधान भी वैश्विक होना चाहिए। भारत जैसे देशों को अब कठोर डेटा संरक्षण कानून की आवश्यकता है, जिसमें कंपनियों को जवाबदेह बनाया जाए, डेटा लीक की स्थिति में अनिवार्य रूप से सूचना साझा करनी पड़े, पीड़ितों को मुआवजा मिले और डार्क वेब मॉनिटरिंग के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी हो। साथ ही, साइबर सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूलों से लेकर सरकारी कार्यालयों तक, एक अनिवार्य प्रशिक्षण प्रणाली होनी चाहिए। तकनीकी कंपनियों को भी पारदर्शिता अपनानी चाहिए, यूजर डेटा कैसे प्रोसेस हो रहा है, कहां स्टोर हो रहा है, किसके साथ शेयर हो रहा है, इन सभी सूचनाओं को आम और स्पष्ट भाषा में उपलब्ध कराना अनिवार्य होना चाहिए। लेकिन तब तक, जब तक यह संरचनात्मक सुधार नहीं होता, हमें स्वयं अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी उठानी होगी।
हर यूजर को चाहिए कि वह अपने सभी खातों के पासवर्ड तुरंत बदले, हर सेवा के लिए अलग-अलग मजबूत पासवर्ड बनाए, टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू रखे, पासवर्ड मैनेजर का उपयोग करे और हर संदिग्ध लिंक या अज्ञात संदेश से बचकर रहे। यदि किसी अकाउंट में असामान्य गतिविधि दिखे तो तुरंत उसकी रिपोर्ट करें, लॉगिन डिवाइस हटाएं और रीसेट करें। यह समय चेतने का है। यह केवल तकनीकी चेतावनी नहीं, सामाजिक और मानवीय चेतावनी है। 16 अरब डेटा लॉग का लीक केवल एक आंकड़ा नहीं, यह पूरी मानवता की डिजिटल छवि का क्षरण है। हम एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं, जहां आपकी निजता अब एक उत्पाद बन चुकी है, जिसे खरीदा-बेचा जा सकता है। इससे लड़ाई केवल तकनीक से नहीं जीती जा सकती, इसके लिए नागरिक चेतना, नीतिगत सख्ती और वैश्विक सहयोग आवश्यक है। यदि आज हमने सजगता नहीं दिखाई तो कल इस डिजिटल गुलामी से निकल पाना लगभग असंभव होगा।

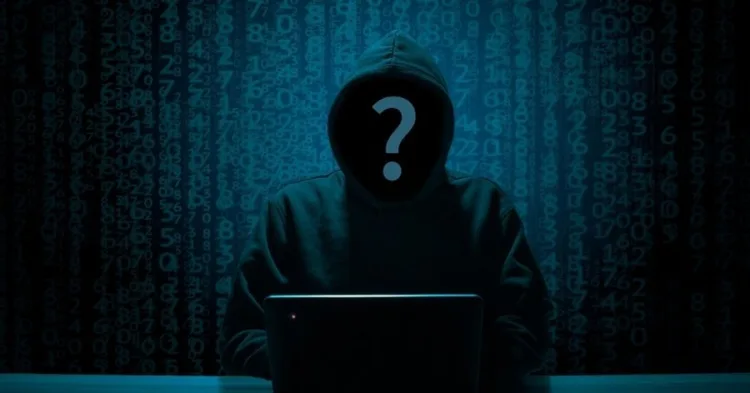
















टिप्पणियाँ