1925 में डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार ने जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नींव रखी थी, तब उन्होंने केवल एक संगठन की नहीं, बल्कि एक विचार यात्रा की शुरुआत की थी— ऐसी यात्रा, जो भारत की सांस्कृतिक चेतना को पुनः जाग्रत करने का स्वप्न लिए आगे बढ़ी। आज, जब संघ अपने शताब्दी वर्ष की दहलीज पर खड़ा है, यह ज़रूरी हो जा भारत की सांस्कृतिक चेतना ता है कि हम उसे केवल सत्ता या राजनीति के चश्मे से नहीं, बल्कि उसके सामाजिक-सांस्कृतिक योगदान के आलोक में देखें।

वाल्टर के. एंडरसन और श्रीधर दामले जैसे अंतरराष्ट्रीय शोधकर्ताओं ने भी यह महसूस किया है कि संघ को समझना भारत की आत्मा को समझने की चाबी हो सकता है। उनकी पुस्तक ‘The Brotherhood in Saffron’ इसका एक प्रमाण है। तो ऐसे में क्या कुछ कारक या कहिए कुछ ऐसी खिड़कियां हो सकती हैं जिनमें झांकने पर संघ के अलग-अलग आयामों से गुजरते हुए उसका एक बड़ा चित्र हम समझ सकें! आइए प्रयास करते हैं –
शाखा : मौन निर्माण का जीवंत मंच
सुबह की पहली किरण के साथ जब किसी मैदान में कुछ स्वयंसेवक खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, तो यह सिर्फ एक औपचारिक जमावड़ा नहीं होता—यह एक अनुशासित, संकल्पित और विचारशील भारत के निर्माण की चुपचाप चल रही प्रक्रिया का हिस्सा होता है। शाखा वह जगह है, जहां बिना किसी प्रचार के व्यक्ति के भीतर राष्ट्र और समाज के प्रति समर्पण के बीज रोपे जाते हैं।
यहां सिर्फ व्यक्तियों की ‘कसरत’ नहीं होती, विचारों को भी राष्ट्रीय भाव में रमने, जड़ों से जुड़ने का वैचारिक आलम्बन मिलता है। गीतों में देशप्रेम झलकता है, खेलों में टीम भावना और चर्चाओं में सामाजिक जागरूकता। शाखा, दरअसल एक ऐसी कार्यशाला है, जहां ‘मैं’ धीरे-धीरे ‘हम’ में परिवर्तित हो जाता है।
गांवों की ओर लौटना : विकास का भारतीय मार्ग
संघ की ग्रामोन्मुख दृष्टि केवल योजनाओं या रूखे डाटा के पहाड़ों तक सीमित नहीं है। वह एक भावनात्मक जुड़ाव है—भारत की आत्मा से। जब कोई स्वयंसेवक किसी सुदूर गांव में शिक्षा केंद्र चलाता है या पानी की व्यवस्था करता है, तो वह केवल सेवा नहीं कर रहा होता, वह भारत को फिर से ‘स्वावलंबी’ बना रहा होता है।
महात्मा गांधी का ‘ग्राम स्वराज’ और पं. दीनदयाल उपाध्याय का ‘एकात्म मानववाद’—इन दोनों विचारधाराओं का जीवंत मिश्रण हमें दीनदयाल शोध केंद्र, विवेकानंद केंद्र या ग्रामोदय ट्रस्ट जैसे प्रयासों में दिखता है। यह ‘विकास’ नहीं, ‘पुनरुत्थान’ है—भारतीयता के मूल स्वर का।
शिक्षा में संस्कृति की सांस
विद्या भारती के स्कूलों में जब प्रार्थना होती है, तो बच्चे सिर्फ शब्द नहीं दोहराते, वे अपने भीतर एक संस्कार रोपते हैं। इन विद्यालयों में शिक्षा के साथ-साथ जीवनमूल्य भी पढ़ाए जाते हैं—संस्कार, योग, मातृभाषा, लोककला और परंपरा। शिक्षा यहां केवल परीक्षा पास करने का माध्यम नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण की प्रक्रिया है।
शक्ति की सच्ची अभिव्यक्ति
राष्ट्रीय सेविका समिति की सेविकाएं जब किसी बस्ती में जाती हैं, तो वे सिर्फ कार्यकर्ता नहीं होतीं—वे प्रेरणा होती हैं। उनका प्रशिक्षण, उनकी प्रतिबद्धता और उनका व्यवहार यह दर्शाता है कि भारतीय स्त्री शक्ति इस समाज में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह उस कुटुंब व्यवस्था का आधार है जो समाज और राष्ट्र के संस्कारित ‘निर्माण’ की क्षमता रखता है। यह संगठन महिलाओं को ‘भूमिका’ नहीं, ‘उद्देश्य’ देता है—राष्ट्र निर्माण में बराबरी का।
सेवा : प्रचार से दूर, आवश्यकता के निकट
कोई आपदा हो, महामारी या प्राकृतिक संकट—संघ का स्वयंसेवक अक्सर वहां पहले पहुंचता है, जहां सरकारें देर से पहुंचती हैं। बिना पहचान पूछे, बिना श्रेय चाहे—वह सेवा करता है। शायद यही संघ की सबसे मानवीय पहचान है—’नर सेवा, नारायण सेवा’।
दवा से आगे, संवेदना तक : आरोग्य की अलख
सक्षम, नेशनल मेडिकोज आर्गेनाइजेशन ( NMO) और आरोग्य भारती जैसे संगठन जब ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचते हैं, तो केवल औषधि नहीं, आश्वासन भी लेकर आते हैं। दिव्यांगजन जब ‘सक्षम’ के माध्यम से समाज में आत्मविश्वास से लौटते हैं या जब कोई दूरस्थ गांव में NMO की स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करता है—तो वह केवल ‘चिकित्सा’ नहीं, समकक्षता और ‘सम्मान’ अनुभव करता है।
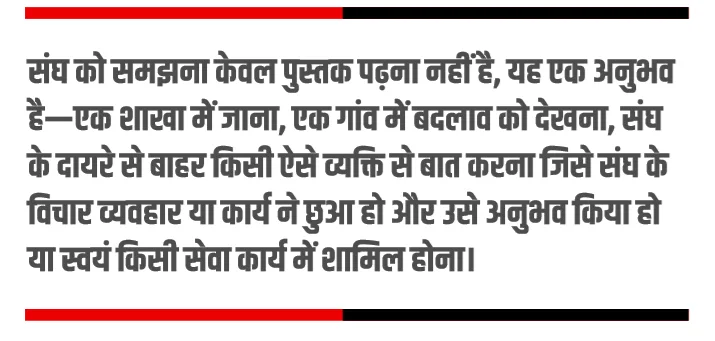
जनजातीय सशक्तिकरण : विविधता का सम्मान, साझी पहचान
वनवासी कल्याण आश्रम का कार्य केवल शिक्षा या हॉस्टल का नहीं—यह पहचान की रक्षा और गौरव की पुनर्स्थापना का अभियान है। यह जनजातीय युवाओं से कहता है, ‘तुम जैसे हो, वैसे ही भारत की आत्मा हो। बदलो मत—जुड़ो।’ यह संगठन कन्वर्जन रोकने का काम भी करता है, पर डर या विरोध से नहीं—सम्मान और अपनत्व से।
श्रमिकों की आवाज : ठेंगड़ी का संतुलित दृष्टिकोण
भारतीय मजदूर संघ ( BMS) जब किसी मजदूर के अधिकार की बात करता है, तो वह केवल ‘हक’ की भाषा नहीं बोलता, वह ‘कर्तव्य’ की भाषा भी बोलता है। यह संगठन दिखाता है कि राष्ट्रवाद और श्रमिक कल्याण परस्पर विरोधी नहीं, पूरक हो सकते हैं।
‘जो कमाएगा, सो खाएगा’ की अहंकार और टकरावपूर्ण भाषा बोलने की बजाय ‘जो कमाएगा, वह खिलाएगा’ का मंत्र लेकर बढ़ने वाले श्रमजीवियों का यह अभियान ऐसा है, जिसके मन में समन्वय का भाव है और राष्ट्र सर्वोपरि का लक्ष्य।
स्वदेशी : अर्थनीति में आत्मा का समावेश
स्वदेशी जागरण मंच (SJM) केवल आर्थिक नीतियों की समीक्षा नहीं करता, वह भारतीय परंपरा को अर्थव्यवस्था में स्थान दिलाने की कोशिश करता है। यहां खादी सिर्फ वस्त्र नहीं, विचार है। हस्तशिल्प सिर्फ कला नहीं, आत्मनिर्भरता का स्वर है। यहां कौशल केवल परंपरा नहीं, आने वाली पीढि़यों का क्षमता विकास भी है।
भारत की बात, भारत के तरीके से
रा. स्व. संघ के भाव से प्रेरित ‘हिंदू स्वयंसेवक संघ’ विदेशों में अपने माध्यम से भारतीय संस्कृति, सेवा भावना और भारतीय दृष्टिकोण का विस्तार कर रहा है। यह संगठन बताता है कि भारत की विचारधारा भी वैश्विक हो सकती है—बिना जड़ें छोड़े।
विचार से परे, अनुभव तक पहुंचना होगा
संघ को समझना केवल पुस्तक पढ़ना नहीं है, यह एक अनुभव है—एक शाखा में जाना, एक गांव में बदलाव को देखना, संघ के दायरे से बाहर किसी ऐसे व्यक्ति से बात करना, जिसे संघ के विचार व्यवहार या कार्य ने छुआ हो और उसे अनुभव किया हो या स्वयं किसी सेवा कार्य में शामिल होना। यह एक विचारधारा नहीं, एक जीवन शैली है। जिस तरह किसी पुस्तक को बिना पन्ने पलटे उसकी समीक्षा का दम भरना गलत है, उसी तरह बिना संघ और संघ कार्य का अनुभव किए संघ को जानने का दावा करना भी गलत है।
शताब्दी वर्ष संघ के समारोह आयोजित करने का समय नहीं है, बल्कि यह आत्ममंथन का समय है, उनके लिए जो कहते हैं कि वे संघ को जानते हैं, किंतु संघ को कतई नहीं जानते।
X@hiteshshankar

















टिप्पणियाँ