पिछले लगभग एक दशक से दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है कि बहुसंख्यक शासन में मनमानी है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता नहीं बची है, सरकार न्यायपालिका के कामकाज में हस्तक्षेप कर रही है वगैरह-वगैरह। हमें इस प्रकार के तथ्यात्मक रूप से गलत प्रचार का कानूनी तर्क के साथ सामना करना होगा। आपातकाल यानी 1975 से 1977 का दौर निश्चित रूप से स्वतंत्रता के बाद के इतिहास का सबसे काला दौर था। हालांकि यह सिर्फ चरमोत्कर्ष था। संविधान का दुरुपयोग सिर्फ आपातकाल के दौरान नहीं हुआ, बल्कि यह बहुत पहले शुरू हो गया था। इस बारे में हमें स्पष्ट होना चाहिए।

भारत के सॉलिसिटर जनरल
जब कोई देश स्वतंत्र होता है, तो इसकी प्रक्रिया क्या होती है? ऐसा तो नहीं होता कि लॉर्ड माउंटबेटन कह दें कि कल सुबह मेरी फ्लाइट है तो नेहरू कल से कमान संभाल लें। देश को स्वतंत्रता इस तरह से नहीं मिली। यह सब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम-1947 नामक एक अधिनियम के माध्यम से हुआ, जिसे ब्रिटिश संसद ने पारित किया था। हालांकि यह वर्तमान उद्देश्य के लिए यह प्रासंगिक नहीं है। लेकिन प्रासंगिक बात यह है कि उस अधिनियम में यह प्रावधान था कि एक संविधान सभा होगी, जो संविधान बनाएगी। संविधान सभा ने देश की 16 प्रतिशत जनसंख्या का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन वे प्रतिभाशाली दिमाग वाले थे और देश के बेहतरीन दिमागों में से एक थे। उन्होंने ऐसा संविधान बनाया, जो तब तक कायम रहेगा जब तक कि इसमें कोई छेड़छाड़ न की जाए। लेकिन कोशिश यह हुई कि संविधान कैसा हो, इस मंसूबे के साथ छेड़छाड़ की गई।
पहला हमला नेहरू का अभी संविधान कई हिस्सों में है, पर आपातकाल से संबंधित केवल तीन हिस्से हैं- प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और संविधान में संशोधन की शक्ति। प्रस्तावना के बारे में तो सभी जानते हैं कि भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य है और हमने यह संविधान स्वयं को दिया है। इसलिए इस पर और चर्चा की आवश्यकता नहीं है। संविधान का भाग तीन उन मौलिक अधिकारों का प्रावधान करता है, जिनका मैं उपयोग करता हूं, जिनका आप उपयोग करते हैं, एक सामान्य लोग और आर्थिक पदानुक्रम के सबसे निचले स्तर के किसान भी उसी संविधान का उपयोग करते हैं।
पहला प्रावधान है, संविधान का अनुच्छेद-13, जो कानून को पारिभाषित करता है। संविधान के संदर्भ में यहां कानून का मतलब केवल संसद या विधानसभा द्वारा बनाया गया कानून नहीं है। इसमें नियम, विनियम और उपनियम शामिल हो सकते हैं। इसमें प्रथा और उपयोग भी शामिल हो सकते हैं। संविधान निर्माता चाहते थे कि ऐसा कोई कानून न हो, जो नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे। लेकिन उस समय की सरकार ने कानून शब्द की परिभाषा को बदलने के लिए हर प्रयास किए।
देश में पहला चुनाव 1951 में हुआ। तब तक भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अनुसार संविधान सभा देश की संसद के रूप में जारी रही। लेकिन 1951 में पहली संसद का गठन होता, उससे पहले ही संविधान में पहला संशोधन कर दिया गया। इस पहले संविधान संशोधन में अनुच्छेद-31ए जोड़ा गया, जिसमें प्रावधान किया गया कि संसद यदि कृषि सुधारों, कृषि समुदाय या कृषि भूमि के संबंध में कोई कानून बनाती है, तो उसे किसी भी अदालत में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। दूसरी बात यह कि जब संविधान बना था, तब इसमें 395 अनुच्छेद और आठ अनुसूचियां थीं। लेकिन पहली बार अनुच्छेद-31बी में एक प्रावधान के साथ अनुसूची-9 नाम से एक नई अनुसूची जोड़ी गई कि यदि संसद कोई कानून बनाती है और उसे अनुच्छेद-9 में रखती है, तो यह मौलिक अधिकारों के आधार पर चुनौती से मुक्त होगा। यानी यदि संसद कोई कानून बनाकर उसे अनुसूची-9 में डाल देती है, तो भले ही वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो, उसे किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
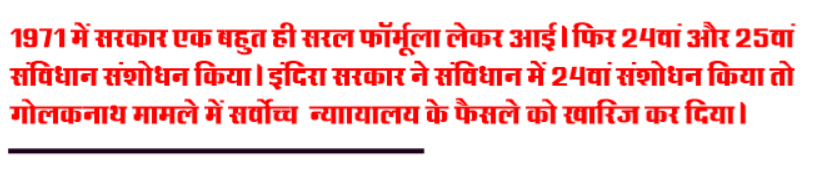
मौलिक अधिकारों का उल्लंघन
बहरहाल, इसे विभिन्न उच्च न्यायालयों, मुख्य रूप से पटना उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। एक उच्च न्यायालय ने संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर दिया, जबकि अन्य अदालतों ने इसे बरकरार रखा। अंतत: शंकरी प्रसाद मामले के रूप में यह पहली बार सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आया। इसमें मूल प्रश्न यह था कि कानून क्या है? जब संसद ने संविधान में ही संशोधन किया है, तो क्या उस संशोधन अधिनियम को कानून कहा जा सकता है? यहां अंतर देखिए। संसद द्वारा जमीन को लेकर कानून बनाना एक बात है। लेकिन यहां संसद संविधान में बदलाव कर रही है और उस शक्ति का स्रोत संविधान ही है।
मूल प्रश्न यह था कि क्या संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह संशोधन स्वयं मेरे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे? खैर, यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में पांच जजों की पीठ के पास गया। पीठ ने परीक्षण के बाद कहा कि अधिनियम द्वारा संविधान में जो संशोधन किया गया है, वह अनुच्छेद-13 के अर्थ में कोई कानून नहीं है। इसलिए भले ही यह आपके किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता हो, यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है। इसी के साथ अदालत ने यथास्थिति बनाए रखी, जो 14 वर्ष तक जारी रही। यानी 14 वर्ष तक सरकार कानून बनाती रही और उसे अनुसूची-9 में डालती रही और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर भी कुछ नहीं किया जा सका। उस समय तक अनुसूची-9 में 30 अधिनियम शामिल थे, जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकते थे।
मान लीजिए मेरी जमीन छीन ली गई। लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि जमीन कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना ली गई है, इसलिए यह अनुच्छेद-14 का उल्लंघन है। चूंकि मेरे पास अनुच्छेद-14 का संरक्षण नहीं है। लिहाजा, मैं नहीं कह सकता कि यह भेदभाव है। मेरे पड़ोसी की जमीन नहीं ली गई और मेरी जमीन ले ली गई, यह स्पष्ट भेदभाव है। लेकिन कुछ भी नहीं किया जा सकता है।

मौलिक अधिकारों पर बहस
इसके बाद 1965 में सज्जन सिंह का मामला आया, तो यह सवाल फिर खड़ा हो गया कि क्या संसद द्वारा कोई कानून बनाना संविधान में संशोधन करने और संशोधन अधिनियम बनाने से भिन्न है? फिर से मामला पांच जजों की पीठ के पास गया। पीठ ने संविधान में संशोधन की संसद की शक्ति को बरकरार रखते हुए कहा कि संशोधन वैध होगा, भले ही यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीन ले। हालांकि पांच जजों की पीठ का निर्णय सर्वसम्मत नहीं था। तीन जज इस निर्णय के पक्ष में थे, जबकि दो इसके विरोध में थे। न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला और न्यायमूर्ति मुधोलकर इस फैसले से असहमत थे, लेकिन वे अल्पमत में थे। न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला ने कानून शब्द के व्याकरणिक अर्थ की बजाए अपनी आत्मा की सुनी और कहा कि यदि अनुच्छेद-13 की भावना यह है कि संसद द्वारा निर्मित कोई भी कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो वह शून्य है, वह अति-विरोधी है, वह गैर-कानूनी है।
दिलचस्प बात यह है कि सज्जन सिंह मामले में न्यायमूर्ति मुधोलकर ने पहली बार अपनी असहमति में ‘बुनियादी संरचना’ शब्द का इस्तेमाल किया था। बाद में केशवानंद भारती मामले में बुनियादी संरचना सिद्धांत पर लंबी बहस हुई थी। न्यायमूर्ति मुधोलकर का कहना था कि संसद ऐसा संशोधन नहीं कर सकती, जो संविधान की मूल संरचना को नष्ट कर दे।
इंदिरा ने भी किया संविधान का दुरुपयोग
1966 में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनीं। इंदिरा सरकार ने आपातकाल के दौरान संविधान ही नहीं, नागरिकों के मौलिक अधिकारों के साथ भी खिलवाड़ किया था। 1966 में सत्ता परिवर्तन इस अर्थ में हुआ कि नेता बदला गया। इस पर चर्चा और बहस चल रही थी कि यदि संसद को संविधान में बदलाव करने की अनुमति दे दी जाए और नागरिकों को उपचार-विहीन कर दिया जाए तो क्या होगा। आखिरकार 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 11 जजों की पीठ ने 6 और 5 के बेहद मामूली बहुमत से निर्णय दिया। 6 जजों ने कहा कि संसद नागरिकों के मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकती। अनुच्छेद-3 के तहत कानून में संविधान में संशोधन भी शामिल है। भले ही निर्णय 6 और 5 में बंटा था, लेकिन यह संविधान पीठ का अब तक का सबसे बड़ा फैसला है। इस पर सरकार की ओर से तत्काल प्रतिक्रिया हुई। कानून बनाकर शीर्ष अदालत के फैसले को डंप कर दिया गया।
पहली बात, हम जब भी कानून कहते हैं, तो उसमें संविधान संशोधन शामिल नहीं होता है। इसका मतलब यह संविधान संशोधन से से इतर है। इसी तरह, अनुच्छेद-31 में संशोधन कर उसमें 31सी जोड़ा गया। इसमें कहा गया कि अनुच्छेद-31बी और सी के तहत पारित कोई भी कानून, जो राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत हैं, को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के तहत न अदालत में चुनौती दी जा सकती है और न ही उसकी समीक्षा की जा सकती है। इसका मतलब यह है कि राज्य, संसद ऐसा कोई भी कानून बना सकती है, जो मौलिक अधिकारों को छीन सकता है। दूसरी बात, उन्होंने (कांग्रेस सरकार) बताया कि जो काम वर्जित था, उसे करने का बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही सही तरीका है। इसका कारण कानूनी सरलता है। राजनीतिक रूप से यह सबसे बुरी चीज है, लेकिन कानूनी तौर पर कहें तो सरकार का यह एक उपयुक्त कदम था।
सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय पलटा
1971 में सरकार एक बहुत सरल फॉर्मूला लेकर आई। उसने 24वां और 25वां संविधान संशोधन किया। इंदिरा सरकार ने 24वां संशोधन किया तो गोलकनाथ मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को खारिज कर दिया। फिर यह मुद्दा 1973 में केशवानंद भारती मामले में 13 जजों की पीठ के समक्ष आया।
अब दिलचस्प इतिहास शुरू होता है। अदालत ने मौलिक अधिकारों और संसद की कानून बनाने की शक्ति के बीच संतुलन बनाना शुरू किया। केशवानंद भारती मामले का नेतृत्व नानी पालकीवाला कर रहे थे। उस समय जज भी बंटे हुए थे। कुछ सरकार समर्थक, तो कुछ नागरिक समर्थक थे। लिहाजा, बहस में पालकीवाला के सामने सवालों की झड़ी लग जाती थी कि आखिरकार संसद ही संविधान की रचना क्यों है? यदि संविधान उसमें संशोधन की अनुमति देता है तो उसे इसकी अनुमति क्यों नहीं दी जानी चाहिए? अंतत: यह लोगों की इच्छा है, जो संसद में प्रतिबिंबित होती है। यह बड़ा आकर्षक तर्क था कि भारत का संविधान एक दस्तावेज है, जो संसद बनाता है। यह अनुच्छेद-368 का प्रावधान करता है, जो कहता है कि संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। यह प्रक्रिया दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत, आधे राज्यों द्वारा अनुसमर्थन आदि के लिए प्रदान की जाती है, ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता है?
इस पर पालकीवाला ने कहा था, श्रीमान्, बाकी सब भूल जाइए। प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य है। संप्रभुता का अर्थ है, संप्रभुता देश की जनता के पास होती है। अब कल को संसद संविधान में संशोधन करना चाहे कि हम इस चुनाव, प्रधानमंत्री और सरकार के कैबिनेट स्वरूप आदि को जारी रखेंगे, लेकिन संप्रभुता इंग्लैंड की रानी को स्थानांतरित कर दी जाए तो क्या होगा। अदालत का कहना था कि तकनीकी रूप से पालकीवाला का तर्क सही है कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। संविधान में वर्णित लोकतांत्रिक गणराज्य का अर्थ है कि 1947 तक प्रत्येक वयस्क भारतीय को वोट देने का अधिकार नहीं था। केवल कुछ लोगों को ही वोट देने का अधिकार था। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता तय की गई थी। हमें छोटी-छोटी बातों से कोई सरोकार नहीं है। इस पर पालकीवाला ने एक उदाहरण।
उन्होंने कहा कि संसद संविधान में कुछ संशोधन कर एक कानून लाए, जिसमें कहा जाए कि अब से केवल करदाता ही मतदाता होंगे या स्नातक ही मतदाता होंगे या एक खास समुदाय ही वोट कर सकेगा। फिर आप क्या करेंगे? यह लोकतंत्र को नष्ट करने वाला होगा। आपको यह कहना होगा कि भारत के संविधान की मूल विशेषता है लोकतंत्र। हम एक गणतंत्र हैं। कोई कह सकता है कि हमें कोई चिंता नहीं है। हमें सरकार के गणतांत्रिक स्वरूप में कोई दिलचस्पी नहीं है और हम गणतांत्रिक सरकार के स्वरूप को खत्म कर सकते हैं। हम कोई अन्य सरकार अपनाएंगे। ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता? उनके इस तर्क ने जजों को झकझोर कर रख दिया और उन्हें कहना पड़ा कि तर्क में दम है। फिर जजों ने दो तर्क दिए। पहला, अनुच्छेद-368 में संशोधन की शक्ति सरकार के पास रहेगी। लेकिन उसे संसद में एक निहित प्रतिबंध पढ़ना होगा कि ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा, जिसकी परिकल्पना संविधान निमार्ताओं ने कभी नहीं की थी। दूसरा, भले ही संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति हो, पर वह ऐसा नहीं कर सकती। वह संविधान की मूल विशेषता को छेड़े बिना ऐसा कर सकती है। लेकिन फैसले के बाद उस दिन की सरकार की क्या प्रतिक्रिया थी?
सरकार की मनमानी
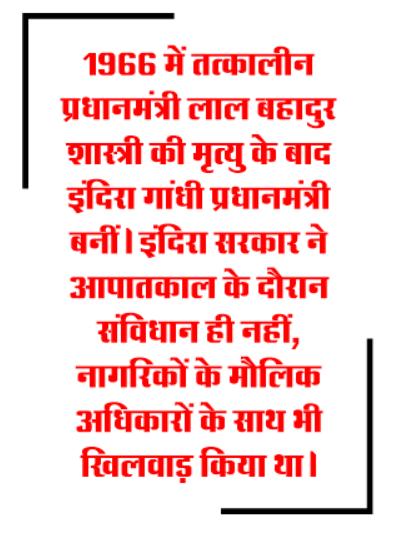 इसी तरह, 1973 का केशवानंद भारती मामला भी दिलचस्प है। इस मामले में 24 अप्रैल, 1973 को फैसला सुनाया गया था। उस दिन भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सीकरी सेवानिवृत्त होने वाले थे। परंपरा यह है कि मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति से 30 दिन पहले सरकार अगले वरिष्ठतम न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अधिसूचित करती है। लेकिन तब सरकार ने कोई नाम अधिसूचित नहीं किया था। न्यायमूर्ति सीकरी के बाद तीन वरिष्ठ न्यायाधीश थे- न्यायमूर्ति शैलज, न्यायमूर्ति हेगड़े और न्यायमूर्ति ग्रोवर। 24 अप्रैल की सुबह तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई और तीनों वरिष्ठतम न्यायाधीशों को पद से हटाने का निर्णय लिया गया। वरिष्ठता में पांचवें क्रम के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजीत नाथ रे को भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। आल इंडिया रेडियो पर जब न्यायमूर्ति हेगड़े ने यह खबर सुनी तो चौंक गए। वे मुख्य न्यायाधीश से मिले, पर वह कुछ नहीं कर सके, क्योंकि यह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था।
इसी तरह, 1973 का केशवानंद भारती मामला भी दिलचस्प है। इस मामले में 24 अप्रैल, 1973 को फैसला सुनाया गया था। उस दिन भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सीकरी सेवानिवृत्त होने वाले थे। परंपरा यह है कि मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति से 30 दिन पहले सरकार अगले वरिष्ठतम न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अधिसूचित करती है। लेकिन तब सरकार ने कोई नाम अधिसूचित नहीं किया था। न्यायमूर्ति सीकरी के बाद तीन वरिष्ठ न्यायाधीश थे- न्यायमूर्ति शैलज, न्यायमूर्ति हेगड़े और न्यायमूर्ति ग्रोवर। 24 अप्रैल की सुबह तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई और तीनों वरिष्ठतम न्यायाधीशों को पद से हटाने का निर्णय लिया गया। वरिष्ठता में पांचवें क्रम के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजीत नाथ रे को भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। आल इंडिया रेडियो पर जब न्यायमूर्ति हेगड़े ने यह खबर सुनी तो चौंक गए। वे मुख्य न्यायाधीश से मिले, पर वह कुछ नहीं कर सके, क्योंकि यह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था।
उस दिन जो लेख प्रकाशित हुए थे, उनके अनुसार सब कुछ पूर्व नियोजित था। न्यायमूर्ति जगनमोहन रेड्डी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि 25 अप्रैल, 1973 से एक या दो हफ्ते पहले एक आधिकारिक रात्रिभोज हुआ था, जिसमें तत्कालीन कानून मंत्री कुमार मंगलम ने न्यायमूर्ति रे को बधाई देते हुए कहा था, ‘बधाई हो जस्टिस, दो हफ्ते बाद…।’ तब किसी को समझ में नहीं आया था कि पांचवें नंबर के जज को बधाई क्यों दी जा रही है। यह पहले से ही तय था कि न्यायमूर्ति रे सरकार के पक्ष में फैसला देंगे। बाकी जजों ने सरकार के पक्ष में फैसला नहीं दिया, बल्कि यह माना कि सरकार संविधान में ऐसा संशोधन नहीं कर सकती, जिससे कि संविधान का मूल ढांचा नष्ट होता हो।
1977 में आपातकाल के बाद चुनाव में कांग्रेस हार गई। जनता सरकार सत्ता में आई, तो हलचल हुई। एडीएम जबलपुर बनाम शशिकांत शुक्ला मामले में फैसले के बारे में सभी जानते हैं। उस फैसले में कहा गया था कि यदि कानून के अनुसार किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता छीन ली जाती है, तो उसे भारत के संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत कोई सुरक्षा नहीं है। न्यायमूर्ति खन्ना ने इस फैसले पर असहमति जताई थी। दरअसल, मोरारजी देसाई की सरकार के दौरान यह कदम उठाया गया था कि जिन जजों ने एडीएम जबलपुर के फैसले पर हस्ताक्षर किए थे, उन्हें भी हटा दिया जाना चाहिए। अब देखिए सरकार की ताकत। जब कोई न्यायपालिका में हस्तक्षेप आदि की बात करता है, तो यह नहीं देखता कि न्यायमूर्ति रे के भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालते ही अचानक 10 नवंबर, 1974 को केशवानंद भारती मामले की समीक्षा के लिए 13 न्यायाधीशों की पीठ फिर से गठित की गई थी। तब न तो किसी ने समीक्षा की न ही किसी ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी।
मतलब यह कि आपातकाल के दौरान जब लोकतंत्र और न्यायपालिका की स्वतंत्रता खतरे में थी, तब वकील, न्यायाधीश, न्यायपालिका, पत्रकार, शिक्षाविद् और आम आदमी एक साथ आए और देश को इस अंधेरे दौर से बाहर निकाला।
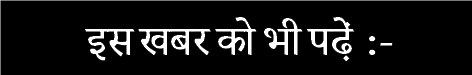
क्यों लगा आपातकाल ?
कांग्रेस की मनोवृत्ति तानाशाही

नि:सन्देह आपातकाल के दिनों में अनगिनत जुल्म ढाए गए। अत्याचार की ऐसी घटनाएं घटीं जैसी कभी नहीं घटी थीं। आपातकाल के बाद जब माननीय बालासाहब ने देश भर का दौरा किया तो उन्होंने हम सबसे यही कहा कि जो कुछ हुआ, उसे भूल जाओ। और हम सचमुच भूल गए। तब से आज तक इसको लेकर कभी किसी कोई अभिव्यक्ति नहीं की। जब आपातकाल लगा, मैं कानपुर संभाग का प्रचारक था। मैं अपने भाई, जो पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी थे, के घर पर था, वहीं मुझे यह समाचार मिला। बालासाहब का फिरोजाबाद में एक कार्यक्रम था। वापसी में जब वे नागपुर जा रहे थे तो उन्हें ट्रेन से उतारकर गिरफ्तार कर लिया गया। हम लोग समझ चुके थे कि हमें भूमिगत होकर ही काम करना पड़ेगा। हम सभी भूमिगत हो गए। हमने सोच लिया था कि सम्पर्क बनाए रखेंगे, किसी भी कीमत पर संगठन बिखरने नहीं देना है।
 कांग्रेस ने अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए न केवल तानाशाही भरे कदम उठाए, बल्कि न्यायालय के आदेश की भी धज्जियां उड़ा दीं। जब आपातकाल लगा तब मैंने यही सोचा था कि जिस तरह पानी का मार्ग रोका नहीं जा सकता, उसी तरह इंदिरा गांधी भले ही कितनी कोशिश करें, वे जन आक्रोश का सामना नहीं कर पाएंगी और जनता उन्हें सत्ता से हटा ही देगी। और वैसा ही हुआ। एक बात बहुत महत्त्वपूर्ण है कि पूरे संघर्ष के दौरान संघ के कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी से बचने के लिए सरकार से माफी मांगी हो या कोई सरकार का मुखबिर बन गया हो, ऐसी घटना पूरे देश में शायद ही कोई हुई हो। संघ में हम जो चरित्र निर्माण करते हैं यह उसी का परिणाम है।
कांग्रेस ने अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए न केवल तानाशाही भरे कदम उठाए, बल्कि न्यायालय के आदेश की भी धज्जियां उड़ा दीं। जब आपातकाल लगा तब मैंने यही सोचा था कि जिस तरह पानी का मार्ग रोका नहीं जा सकता, उसी तरह इंदिरा गांधी भले ही कितनी कोशिश करें, वे जन आक्रोश का सामना नहीं कर पाएंगी और जनता उन्हें सत्ता से हटा ही देगी। और वैसा ही हुआ। एक बात बहुत महत्त्वपूर्ण है कि पूरे संघर्ष के दौरान संघ के कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी से बचने के लिए सरकार से माफी मांगी हो या कोई सरकार का मुखबिर बन गया हो, ऐसी घटना पूरे देश में शायद ही कोई हुई हो। संघ में हम जो चरित्र निर्माण करते हैं यह उसी का परिणाम है।
(विहिप के तत्कालीन महामंत्री अशोक सिंहल से बातचीत पर आधारित है)
पाञ्चजन्य के अंक (25 जून,1995) से संपादित अंश
आपातकाल और बर्बरता

आपातकाल के दौरान सत्ता का क्रूर चेहरा सामने आया। सत्याग्रहियों को जेल में ठूंस दिया गया। यातनाएं दी गर्इं। गभर्वती महिलाओं तक को बेड़ियों में रखा गया। कैदियों की नाभि में कीड़े बांध दिए जाते थे। मोमबत्ती से जलाया जाता था। स्वतंत्र भारत में जनता को ऐसी बर्बरता की उम्मीद नहीं थी। पुलिस लॉकअप में स्वयंसेवकों को यातनाएं दी जाती थीं। भूमिगत तरीके से आपातकाल के विरोध में पर्चे छापे जाते थे। इस संबंध में जब स्वयंसेवकों से पूछा जाता था तो भयंकर यातनाएं देने के बाद भी वे अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकालते थे। इसलिए उन्हें और अधिक यातनाएं दी जाती थीं।
जेल भेजने से पहले पुलिस लॉकअप में क्रूरता की जाती थी। उस समय आंध्रप्रदेश (आज तेलंगाना) के एक कार्यकर्ता के शरीर को मोमबत्ती से लगभग सौ जगह जलाया गया था। लॉकअप में कई दिनों तक अत्याचार सहने के बाद जो लोग जेल में आते थे उनकी मालिश करने जैसे काम स्वयंसेवक करते थे ताकि वह खड़े हो सकें, चल सकें। मैंने भी ये सब काम किए। इन अमानवीय अत्याचारों से कुछ लोग जीवनभर के लिए अपंग हो गए। कुछ लोगों को जीवनभर के लिए किसी न किसी प्रकार की व्याधि हो गई। बेंगलुरु में गायित्री नाम की एक महिला थीं।
 आपातकाल के विरोध में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वह गर्भवती थीं, उन्हें प्रसव वेदना हुई तो हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल में में डिलीवरी के समय उनके दोनों पैरों को जंजीर से बांधकर रखा गया था। उन बातों को आज याद करने से अपने मन में अनावश्यक वेदना होती है। आपातकाल में जो हुआ वह घोर अमानवीय और मानवाधिकार के विरुद्ध इतिहास के पन्नों पर एक काला धब्बा है।
आपातकाल के विरोध में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वह गर्भवती थीं, उन्हें प्रसव वेदना हुई तो हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल में में डिलीवरी के समय उनके दोनों पैरों को जंजीर से बांधकर रखा गया था। उन बातों को आज याद करने से अपने मन में अनावश्यक वेदना होती है। आपातकाल में जो हुआ वह घोर अमानवीय और मानवाधिकार के विरुद्ध इतिहास के पन्नों पर एक काला धब्बा है।
(रा. स्व. संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले के एक साक्षात्कार से लिया गया अंश)


















टिप्पणियाँ