इक्कीसवीं सदी में वैश्विक भू-राजनीतिक परिदृश्य एक गहरे संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। इसका सबसे स्पष्ट प्रभाव रक्षा व्यापार क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। पिछले दशकों में रक्षा क्षेत्र की राजनीति, अर्थव्यवस्था और तकनीक जिस तेजी से बदली है, उसने पारंपरिक शक्तियों के प्रभुत्व को चुनौती दी है और कई नए खिलाड़ियों को वैश्विक मंच पर आने का अवसर दिया है। एक समय अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे देश रक्षा आपूर्ति के पर्याय माने जाते थे। अब तुर्किये, दक्षिण कोरिया, इस्राएल व भारत जैसे देश अपने उत्पादों और तकनीकी नवाचारों के दम पर वैश्विक बाजार में मजबूती से स्थापित हो रहे हैं। साथ ही, वैश्विक दक्षिण के देश, जो कभी रक्षा उद्योग में केवल ‘ग्राहक’ थे, अब ‘रणनीतिक साझेदार’ के रूप में स्वयं को पुनः परिभाषित कर रहे हैं।
एकध्रुवीयता बनाम बहुध्रुवीयता

राज्यपाल, मिजोरम एवं
पूर्व सेनाध्यक्ष
1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका विश्व राजनीति और सैन्य प्रभाव का केंद्र बन गया। इसे एकध्रुवीय व्यवस्था कहा गया, जहां अमेरिका की आर्थिक, सैन्य और तकनीकी शक्ति निर्विवाद थी। इस दौरान अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने रक्षा व्यापार पर प्रभुत्व बना लिया। नाटो के सदस्य देश छोटे और विकासशील देशों को ‘सुरक्षा सहायता’ के नाम पर राजनीतिक प्रभाव में ले आए। हथियारों की बिक्री के साथ राजनीतिक और रणनीतिक नियंत्रण भी सुनिश्चित किया गया।
21वीं सदी के दूसरे दशक से धीरे-धीरे एक बहुध्रुवीय विश्व की झलक मिलनी शुरू हुई। चीन की आर्थिक और सैन्य ताकत का बढ़ना, भारत का वैश्विक मंच पर उदय, रूस की आक्रामक रणनीति, तुर्किये की क्षेत्रीय आकांक्षाएं और वैश्विक दक्षिण की आत्मनिर्भरता की ओर रुझान ने स्पष्ट किया कि अब अमेरिका अकेला निर्णायक नहीं है। इसके परिणामस्वरूप सुरक्षा साझेदारियों की विविधता बढ़ी। ग्राहक देश अब अपनी जरूरतों के अनुसार आपूर्तिकर्ता चुनने में अधिक स्वतंत्र हो गए। रक्षा व्यापार केवल सामरिक दबाव के आधार पर नहीं, बल्कि तकनीकी, आर्थिक और रणनीतिक लाभ के आधार पर तय होने लगा।
पारंपरिक आपूर्तिकर्ताओं की बदलती भूमिका
अमेरिका अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा निर्यातक है। उसके प्रमुख उत्पादों में एफ-35 पेट्रायट मिसाइल सिस्टम और अत्याधुनिक ड्रोन शामिल हैं। परंतु अमेरिका की रक्षा बिक्री अक्सर राजनीतिक शर्तों से जुड़ी होती हैं, जैसे-मानवाधिकार, गठबंधनों की वफादारी व रणनीतिक संरेखण की शर्तें। भारत जैसे देशों को सीएएटीएसए (प्रतिबंधों के माध्यम से अमेरिका के विरोधियों का मुकाबला करने का अधिनियम) जैसे अमेरिकी कानून से चुनौती मिलती है, जो रूस से खरीद पर प्रतिबंध की धमकी देता है।
भारत, वियतनाम, सीरिया और कई अफ्रीकी देशों का दशकों से रूस पर निर्भर रहना इसकी ताकत रही है। हालांकि यूक्रेन युद्ध ने रूस की छवि को नुकसान पहुंचाया है।
आपूर्ति में देरी, तकनीकी प्रतिबंध और युद्धक प्रभावशीलता पर सवाल उठे हैं। फिर भी रूस कम लागत वाले सैन्य प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, जो कई विकासशील देशों के लिए आकर्षक है। वहीं, राफेल विमान, स्कॉर्पीन पनडुब्बी और वायु रक्षा प्रणाली जैसे उत्पादों के माध्यम से फ्रांस उच्च गुणवत्ता वाला आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। भारत के साथ फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी (तकनीकी स्थानांतरण, सह-उत्पादन व लॉजिस्टिक सहयोग) एक नया मॉडल प्रस्तुत करती है। परंतु फ्रांस की कीमतें अपेक्षाकृत अधिक होती हैं, जो हर देश की पसंद नहीं बन सकता।
नए आपूर्तिकर्ताओं का उदय
बायकर टीबी-2 द्वारा निर्मित ड्रोन ने दुनिया भर में तुर्किये की तकनीकी क्षमता को सिद्ध किया है। इसने सोमालिया, अजरबैजान, यूक्रेन व लीबिया में अपनी सैन्य क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। अब वह कई अफ्रीकी और एशियाई देशों को किफायती और प्रभावी सैन्य विकल्प प्रदान कर रहा है। वहीं, के-9 वज्र होवित्जर, टी-50 ट्रेनर/लाइट फाइटर जेट और पनडुब्बियों ने दक्षिण कोरिया को एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता बना दिया है। पोलैंड के साथ 15 अरब डॉलर का रक्षा सौदा दक्षिण कोरिया की वैश्विक क्षमताओं को दर्शाता है।
इस्राएल रक्षा क्षेत्र में नवाचार का पर्याय बन गया है, विशेषकर मिसाइल डिफेंस (आयरन डोम), ड्रोन्स, निगरानी सिस्टम और साइबर युद्ध तकनीक में। उसकी बिक्री का एक बड़ा हिस्सा भारत और अमेरिका के सहयोग से पूरा होता है। ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ पहल ने भारत को एक उभरते रक्षा उत्पादक के रूप में उभारा है। तेजस, ब्रह्मोस, आकाश, पिनाका और डीआरडीओ आधारित अन्य परियोजनाएं वैश्विक मंच पर भारत की उपस्थिति मजबूत कर रहे हैं। भारत अब अफ्रीका, दक्षिण-पूर्व एशिया और लातिनी अमेरिका को हथियार निर्यात कर रहा है।
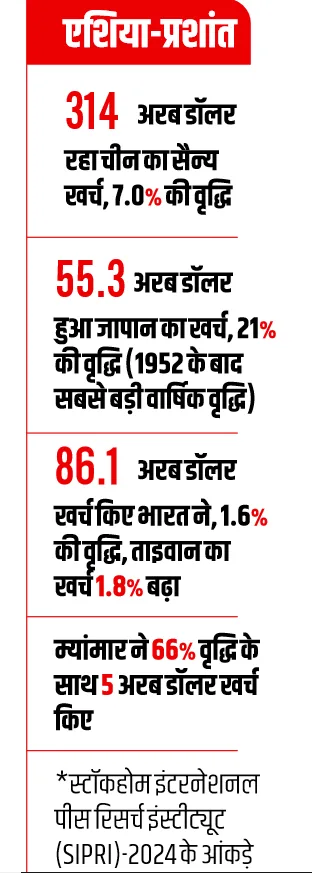 पहले वैश्विक दक्षिण के देश केवल ‘ग्राहक’ थे, उन्हें हथियार मिलते थे, लेकिन रणनीतिक या तकनीकी भागीदारी नहीं। अब वही देश तकनीक हस्तांतरण, सह-निर्माण, प्रशिक्षण और लॉजिस्टिक साझेदारी की मांग कर रहे हैं। रक्षा व्यापार से परे रणनीतिक साझेदारी। भारत-ब्राज़ील, भारत-अफ्रीका, तुर्किये-अजरबैजान और चीन-पाकिस्तान जैसे संबंध अब केवल रक्षा सौदों तक सीमित नहीं हैं। इनमें प्रशिक्षण, सैन्य अभ्यास, रक्षा उद्योगों के संयुक्त निवेश और भू-राजनीतिक समन्वय भी शामिल हैं। तकनीकी संप्रभुता की आकांक्षा बढ़ी है। वैश्विक दक्षिण के देश अब केवल हथियार नहीं चाहते, वे तकनीक और उत्पादन क्षमता भी चाहते हैं। यह बदलाव उन्हें पश्चिमी दबाव से स्वतंत्र बना रहा है।
पहले वैश्विक दक्षिण के देश केवल ‘ग्राहक’ थे, उन्हें हथियार मिलते थे, लेकिन रणनीतिक या तकनीकी भागीदारी नहीं। अब वही देश तकनीक हस्तांतरण, सह-निर्माण, प्रशिक्षण और लॉजिस्टिक साझेदारी की मांग कर रहे हैं। रक्षा व्यापार से परे रणनीतिक साझेदारी। भारत-ब्राज़ील, भारत-अफ्रीका, तुर्किये-अजरबैजान और चीन-पाकिस्तान जैसे संबंध अब केवल रक्षा सौदों तक सीमित नहीं हैं। इनमें प्रशिक्षण, सैन्य अभ्यास, रक्षा उद्योगों के संयुक्त निवेश और भू-राजनीतिक समन्वय भी शामिल हैं। तकनीकी संप्रभुता की आकांक्षा बढ़ी है। वैश्विक दक्षिण के देश अब केवल हथियार नहीं चाहते, वे तकनीक और उत्पादन क्षमता भी चाहते हैं। यह बदलाव उन्हें पश्चिमी दबाव से स्वतंत्र बना रहा है।
आज का वैश्विक रक्षा व्यापार केवल युद्धक प्रणालियों की खरीद-बिक्री तक सीमित नहीं रहा। यह एक व्यापक रणनीतिक, तकनीकी और कूटनीतिक प्रक्रिया बन चुका है। एकध्रुवीय दुनिया का युग अब अतीत होता जा रहा है और बहुध्रुवीय शक्ति संतुलन के दौर में पारंपरिक आपूर्तिकर्ताओं की भूमिका पुनर्परिभाषित हो रही है। वहीं तुर्किये, इस्राएल, दक्षिण कोरिया और भारत जैसे देश वैश्विक स्तर पर रक्षा व्यापार के नए ध्रुव बनते जा रहे हैं। ऐसे में आने वाले वर्षों में रक्षा व्यापार का स्वरूप और अधिक बहुआयामी, सहयोग आधारित और तकनीक-केंद्रित होता जाएगा।
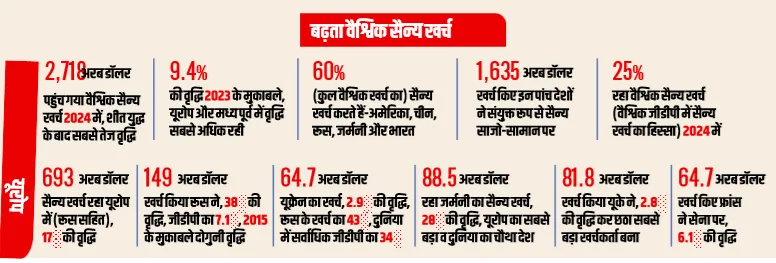

चुनौतियां
- भू-राजनीतिक तनाव : अमेरिका-चीन प्रतिद्वंद्विता, रूस-नाटो संघर्ष आदि से रक्षा आपूर्ति प्रभावित हो सकती है।
- तकनीकी निर्भरता : कुछ देशों के पास अब भी मूलभूत तकनीकी क्षमता की कमी है।
- साइबर खतरे : रक्षा नेटवर्क अब साइबर हमलों का प्राथमिक लक्ष्य है।
अवसर
- रक्षा से रोजगार और नवाचार : स्वदेशी रक्षा उद्योग स्थानीय रोजगार, तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देता है।
- रणनीतिक स्वायत्तता : विविधता आधारित रक्षा साझेदारियां देशों को स्वतंत्र नीति अपनाने में सक्षम बनाती हैं।
- दक्षिण-दक्षिण सहयोग : समान चुनौतियों का सामना करने वाले देश अब मिलकर समाधान खोज रहे हैं।
रक्षा व्यापार की नई प्रवृत्तियां

- मल्टी-डोमेन रक्षा : पारंपरिक हथियारों से इतर साइबर, अंतरिक्ष, एआई और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में तेजी से निवेश हो रहा है। अब युद्ध भूमि केवल भौगोलिक नहीं, बल्कि डिजिटल भी है।
- लो-कॉस्ट, हाई-इम्पैक्ट सिस्टम्स : ड्रोन, पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, सटीक निर्देशित मिसाइलें-कम लागत में अधिक प्रभाव वाले हथियारों की मांग बढ़ रही है।
- सह-निर्माण और सह-विकास के मॉडल : भारत और रूस की ब्रह्मोस परियोजना, भारत-फ्रांस की स्कॉर्पीन परियोजना, या दक्षिण कोरिया और यूएई के बीच यूएवी सहयोग-ये सभी द्विपक्षीय रक्षा संबंधों के उदाहरण हैं
















टिप्पणियाँ