पाकिस्तान में पल रहे जिहाद के विरुद्ध हुआ ऑपरेशन सिंदूर एक निर्णायक लड़ाई नहीं थी, लेकिन इसका सांकेतिक महत्व जरूर है, बशर्ते पाकिस्तान के नेता उसे समझें। चार दिन के ‘संक्षिप्त-युद्ध’ से बहुत ज्यादा निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते हैं, पर कुछ तो निकाले ही जा सकते हैं। मसलन, इससे भारत की वैश्विक-प्रतिष्ठा बढ़ी है, घटी नहीं। पाकिस्तान में दहशत बढ़ी है, भले ही वे अभिनय किसी दूसरे किस्म का करें। तीसरी दुनिया के देशों ने भारत के इस रूप को भी देख लिया, जिसकी बहुतों ने कल्पना नहीं की थी। भारत की सेना और रक्षा तकनीक ने अपनी श्रेष्ठता और प्रभुत्व को भी स्थापित किया है।

वरिष्ठ पत्रकार
‘ऑपरेशन सिंदूर’ के सैनिक, राजनयिक और राजनीतिक निहितार्थ भी हैं। मोटी बात है कि भारत ने पहलगाम की परिघटना का बहुत ‘संयमित और सीमित प्रतिशोध’ लिया है। काफी लोगों की राय है कि इस बार लड़ाई ‘आर-पार’ के इरादे से लड़ना चाहिए था। ऐसा वही सोच सकते हैं, जो डिप्लोमेसी की जटिलताओं से परिचित नहीं हैं। अंततः हमें आर्थिक विकास की लड़ाई लड़नी है, जिसमें पाकिस्तान को पहले ही काफी पीछे छोड़ दिया है।
हमारी ताकत ही कमजोरी भी है। हम दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और 2030 तक हम अमेरिका और चीन के बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। यदि हम युद्ध ज्यादा लंबा खींचेंगे, तो विकास और सुधारों की अनदेखी होने लगेगी। पाकिस्तान के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। यह कारक हमें ‘स्वस्थ युद्धविराम’ को स्वीकार करने को प्रेरित करता है। पाकिस्तान अधिक्रांत जम्मू-कश्मीर को तुरंत अपने कब्जे में लेने की मांग करना फिलहाल आत्यंतिक परिकल्पना है। उसके व्यावहारिक पहलू भी हैं। उसका भी समय आएगा।
ढाई मोर्चे की लड़ाई
भारत को पाकिस्तान और चीन, दो मोर्चों के अलावा अपने भीतर मौजूद आधे मोर्चे की भी चिंता करनी होगी और उससे निपटना होगा। युद्ध की एक नई शैली ‘हाइब्रिड-युद्ध’ के रूप में विकसित हो रही है, जिसमें शत्रु, परोक्ष रूप से सोशल मीडिया और राजनीति में अपने हितैषियों को तैयार करता है। इस्लामिक स्टेट ने भारत में सोशल मीडिया के मार्फत बाकायदा भर्ती की थी। 26 जनवरी को लालकिले में जो हिंसा हुई थी, उसे हम कैसे भूल सकते हैं?
सोशल मीडिया पर कुछ समय पहले अमेरिकी पत्रकार जोशुआ फिलिप का वीडियो वायरल हुआ था। उन्होंने कहा था कि चीन तीन रणनीतियों का सहारा लेता है-मानसिक, सांविधानिक और मीडिया। यह ‘तीन युद्ध’ रणनीति है। वह अपने प्रतिस्पर्धी देशों को उनके ही आदर्शों की रस्सी से बांधता है। आपके वाणी वाणी की स्वतंत्रता है, तो वह व्यवस्था विरोधी आंदोलनों को हवा देगा। आपकी न्याय व्यवस्था का सहारा लेकर आपको कठघरे में खड़ा किया जाएगा। आपके मीडिया की मदद लेगा।
पाकिस्तानी राजनेता और जनरल फिलहाल अपनी अवाम को यह बताने की कोशिश जरूर करेंगे कि अमेरिका अब कश्मीर पर मध्यस्थता करेगा। हालांकि भारत ने इसकी संभावना से इनकार किया है, पर वे अमेरिकी राष्ट्रपति डोलाल्ड ट्रंप के किसी बयान से बहुत खुश हैं, तो उन्हें रोका तो नहीं जा सकता। भारत अपने मूल राष्ट्रीय हितों पर किसी भी तरह की मध्यस्थता को कभी स्वीकार नहीं करेगा।

‘आतंकिस्तान’ की नाभि
इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान की ‘एटमी धमकी’ की हवा ही नहीं निकाली, बल्कि वैश्विक मीडिया में खबरें हैं कि भारतीय मिसाइलों ने ‘आतंकिस्तान’ के नाभिकीय भंडारों के काफी करीब भी हमला किया। 10 मई की सुबह जब भारत ने पाकिस्तानी वायुसेना के नूर खान एयरबेस पर हमला किया, तब रावलपिंडी में खतरे की घंटी बजी। वह एयरबेस पाकिस्तान की नेशनल कमांड अथॉरिटी के स्ट्रैटेजिक प्लांस डिवीजन से कुछ किलोमीटर के फासले पर ही है, जो देश के नाभिकीय शस्त्रागार की कमान और नियंत्रण का काम करता है।
इस प्रहार के बाद पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस (डीजीएमओ) ने भारत के डीजीएमओ से हॉटलाइन पर बात की और हमले रोकने की गुहार लगाई। उसके बाद के कई किस्से हैं, जिनमें से कुछ को ट्रंप बार-बार दोहरा रहे हैं। इस बार की मार काफी गहरी थी। भारत नहीं, पाकिस्तान चाहता था कि उसे बचाया जाए। संघर्ष एक और दिन तक जारी रहता, तो पता नहीं क्या होता। शायद पाकिस्तान ने भारत की ऐसी कठोर, तीखी व त्वरित प्रतिक्रिया का अनुमान लगाया नहीं था। सवाल है कि इस झन्नाटेदार तमाचे से पाकिस्तान का दिमाग सही हुआ या नहीं? अगली बार पहलगाम जैसा कदम उठाने के पहले वह एक बार सोचेगा या नहीं वगैरह-वगैरह?
मेक इन इंडिया
‘ऑपरेशन सिंदूर’ की सफलता को भारत की सैन्य आत्मनिर्भरता की दिशा में मील का पत्थर माना जाएगा, जिसे ‘मेक इन इंडिया’ पहल द्वारा संचालित किया जाता है। ‘ऑपरेशन सिंदूर’ सिर्फ एक सैन्य सफलता ही नहीं, बल्कि भारत की रक्षा तकनीकों का प्रदर्शन भी था, जिनमें से कई तकनीकें स्वदेशी हैं। यह डीआरडीओ, इसरो और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जैसे अन्य संगठनों पर वर्षों के निवेश और शोध का परिणाम है। भारत ने अपने लक्ष्यों को सटीकता से मारा, जिनमें से कई पाकिस्तान के अंदर स्थित थे। यह न केवल आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के सैन्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण था, बल्कि इसने दुनिया में यह भी स्थापित किया कि भारत जिम्मेदारी से व्यवहार कर रहा था और असैनिक क्षति को कम करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था।
भारत की स्वदेशी नौवहन और मार्गदर्शन प्रणाली, ‘नाविक’ उपग्रह प्रणाली पर निर्भर करती है, जिसे हाई-रिज़ॉल्यूशन वाले पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों की एक शृंखला द्वारा पूरित किया जाता है। कार्टोसैट, रिसैट व ईओएस शृंखला के उपग्रह उपमहाद्वीप पर चौबीसों घंटे नजर रखते हैं और सेना के लिए उपयोगी महत्वपूर्ण जानकारी और तस्वीरें प्रदान करते हैं।
इनमें से कुछ उपग्रह 25 से 30 सेमी आकार की छोटी वस्तुओं की पहचान या उनमें अंतर कर सकते हैं। कहा जाता है कि नाविक 10 से 20 सेमी की स्थिति सटीकता प्राप्त करता है। इससे लक्ष्य पर निशाना लगाना संभव हो जाता है, जो ऑपरेशन के दौरान दिखा। भारतीय वैज्ञानिक इन क्षमताओं को और बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। जून 2023 में डीआरडीओ के अनुसंधान चिंतन शिविर के बाद पहचाने गए 75 प्रौद्योगिकी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक ‘मार्गदर्शन और नेविगेशन’ था।
सबसे घातक जवाब
‘ऑपरेशन सिंदूर’ की सफलता के मूल में कम से कम तीन उत्कृष्ट शस्त्र प्रणालियां रहीं- ब्रह्मोस, सुखोई-30एमकेआई और आकाशतीर वायु रक्षा प्रणाली। इनके अलावा दूसरे स्वदेशी प्लेटफॉर्म भी महत्वपूर्ण साबित हुए। दूसरी तरफ पाकिस्तान की चीन निर्मित एचक्यू-9 व एचक्यू-16 प्रणालियां और तुर्की के ड्रोन अपेक्षित परिणाम देने में विफल रहे।
2019 के बालाकोट हवाई हमलों के बाद पाकिस्तानी सेना में शामिल किए गए सिस्टम को विमान, क्रूज मिसाइलों, यूएवी और सामरिक बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें एचक्यू-9बी वैरिएंट की रेंज 300 किमी तक है। इन विशिष्टताओं के बावजूद, एचक्यू-9 व एचक्यू-16 भारतीय हमलों का पता लगाने या उन्हें रोकने में विफल रहे। पाकिस्तान ने भारतीय सैन्य व नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाते हुए मिसाइलों और ड्रोन-स्वार्म की बौछार की, जिसका समापन 9-10 मई की रात को प्रतिक्रिया स्वरूप भारत के सबसे घातक हमले में हुआ।

ब्रह्मोस
ब्रह्मोस मिसाइल भारत के आक्रमण की अगुआ रही। 10 मई को ब्रह्मोस के हवा और जमीन से लॉन्च किए जाने वाले दोनों संस्करणों ने पाकिस्तान के प्रमुख एयरबेस पर अचूक हमले किए। इस मिसाइल ने एक मीटर के करीब एक सर्कुलर एरर प्रोबैबिलिटी हासिल की, जो पहले की आधिकारिक रेटिंग से कहीं बेहतर है। इन हमलों ने रनवे, बंकर और हैंगर जैसे महत्वपूर्ण सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया, जिसमें भारी किलेबंदी वाला नूर खान एयरबेस भी शामिल है। ब्रह्मोस की बहुमुखी प्रतिभा इसकी ताकत को कई गुना बढ़ा देती है। इसे भूमि, समुद्र, पनडुब्बी और युद्धक विमानों से, विशेष रूप से सुखोई-30एमकेआई जेट से प्रक्षेपित किया जा सकता है, जिससे दुश्मन की सुरक्षा को क्षति पहुंचाते हुए दूर तक मार करने की क्षमता प्राप्त होती है।
सुखोई-30एमकेआई
वायुसेना के सुखोई-30एमकेआई जेट विमानों ने, जिन्हें हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने घरेलू स्तर पर बनाया है, ब्रह्मोस के लिए डिलीवरी प्लेटफॉर्म के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
सुखोई-30एमकेआई ने ऑपरेशन के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल के लिए प्राथमिक हवाई लॉन्च प्लेटफॉर्म के रूप में काम किया, जिससे पाकिस्तानी क्षेत्र में अंदर तक सटीक हमले करना संभव हो गया।
ऑपरेशन के दौरान ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस सुखोई-30एमकेआई ने भारी सुरक्षा वाले नूर खान और सरगोधा सहित महत्वपूर्ण पाकिस्तानी वायुसेना अड्डों को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। मिसाइल की कम ऊंचाई समुद्र स्किमिंग उड़ान प्रोफाइल का उपयोग करके उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों को चकमा दिया गया और लगभग पूर्ण सटीकता प्राप्त की गई।
सुखोई-30एमकेआई के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एकीकरण से भारतीय वायु सेना की मारक क्षमता में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई, जिससे 300-600 किमी दूरी से हमला करना संभव हो गया, जो कि अधिकांश शत्रु वायु रक्षा प्रणालियों की प्रभावी सीमा से कहीं अधिक है।

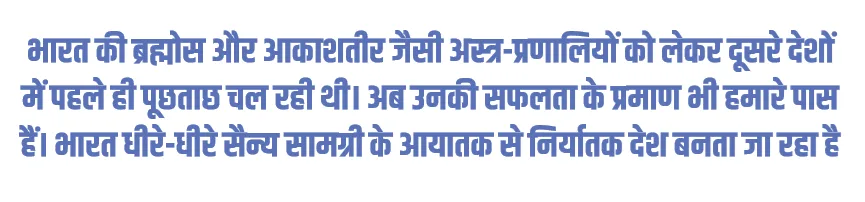
अदृश्य ढाल आकाशतीर
ब्रह्मोस ने जहां दुश्मन के ठिकानों को तबाह किया, वहीं भारत की स्वदेशी मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली ‘आकाशतीर’ ने देश की वायु रक्षा की रीढ़ बनाई। ऑपरेशन के दौरान आकाशतीर, विशेष रूप से इसके उन्नत आकाश एनजी संस्करण ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान द्वारा लॉन्च किए गए कई ड्रोन स्वार्म और मिसाइल खतरों को रोका और बेअसर कर दिया।
रडार, लॉन्चर और कमांड सिस्टम सहित इसका पूरी तरह से स्वदेशी डिजाइन भारत की तकनीकी प्रगति और विदेशों पर निर्भरता को कम करने को रेखांकित करता है। डीआरडीओ, इसरो और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) द्वारा संयुक्त रूप से विकसित आकाशतीर पूर्णतः स्वदेशी, एआई-संचालित वायु रक्षा नियंत्रण एवं रिपोर्टिंग प्रणाली है। यह आकाश अस्त्र-प्रणाली के साथ सामरिक नियंत्रण रडार रिपोर्टर, 3डी सामरिक नियंत्रण रडार और निम्न-स्तरीय हल्के रडार सहित सेंसरों की एक विस्तृत शृंखला को एकीकृत करता है, ताकि सभी कमांड और परिचालन इकाइयों के लिए निर्बाध, वास्तविक समय हवाई तस्वीर तैयार की जा सके।
आक्रामक और रक्षात्मक अभियानों के इस जटिल-तंत्र का समन्वय इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम (एकीकृत वायु कमान और नियंत्रण प्रणाली या संक्षेप में आईएसीसीएस) कर रहा था, जो स्वचालित, स्वदेशी युद्धक्षेत्र प्रबंधन उपकरण है। आईएसीसीएस ने रडार, सेंसर और अवॉक्स डेटा को एकीकृत करके वास्तविक समय की स्थिति के बारे में जानकारी और खतरे पर त्वरित प्रतिक्रिया प्रदान की, जिससे सेवाओं में निर्बाध समन्वय संभव हुआ। साथ ही, हर आने वाले खतरे का पता लगाया गया, उसे ट्रैक किया गया और नुकसान पहुंचाने से पहले उसे बेअसर कर दिया गया।
आकाशतीर को अलग बनाने वाली एक विशेषता है, स्वचालित एआई-संचालित निर्णय लेना। यह प्रणाली रियल टाइम यानी तत्काल वास्तविक समय में मिसाइलों और ड्रोन-स्वार्म सहित हवाई खतरों का पता लगाने, ट्रैक करने और बेअसर करने के लिए विशाल मात्रा में सेंसर डेटा को प्रोसेस करती है, जिससे मानवीय त्रुटि की संभावना और रिएक्ट करने का समय कम हो जाता है। यह एकीकृत बहुस्तरीय रक्षा प्रणाली भारत की इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम (आईएसीसीएस) और नौसेना के ट्राइगुन के साथ समन्वय करती है, जिससे तीनों सेनाओं के बीच तालमेल सुनिश्चित होता है और अपनी सेना पर गोलीबारी के जोखिम में कमी आती है।
आकाशतीर ने पाकिस्तान द्वारा लॉन्च की गई हर मिसाइल और ड्रोन को रोका और बेअसर कर दिया, जिसमें 600 से 1000 के बीच ड्रोन शामिल थे और वह भी बिना किसी महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाए। इस बहुस्तरीय रक्षा कवच को इस्राएल के साथ मिलकर विकसित की गई बराक-8 मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली और दुर्जेय रूसी एस-400 प्रणाली द्वारा और मजबूत किया गया। इन प्रणालियों ने पाकिस्तानी रॉकेट और ड्रोन को रोक दिया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि जवाबी हमले महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाने में विफल रहे।
आकाशतीर के साथ-साथ 1,000 से अधिक वायु रक्षा तोप प्रणालियों और 750 मिसाइल प्रणालियों को जुटाने और समन्वय करने की क्षमता ने हमलों के खिलाफ भारत की तैयारी और लचीलेपन को उजागर किया।

युद्ध-सिद्धांत
भारतीय सेना ‘एकताबद्ध-युद्ध’ के जिस सिद्धांत पर काम कर रही है, उसकी रिहर्सल भी हमें देखने को मिली। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार करीब तीन हजार ‘अग्निवीरों’ ने उस ‘डॉक्ट्रिन और टेक्नोलॉजी’ की अग्निपरीक्षा को सफलता के साथ पास कर लिया। ध्यान दें कि 22 अप्रैल के पहलगाम हमले के केवल 14 दिन बाद भारतीय सेना ने करीब बीस मिनट के अंतराल में कम से कम नौ स्थानों को अचूक निशाना बनाया। यह परिघटना पाकिस्तान को दुःस्वप्न की तरह याद रहेगी। उसके बाद उसने पलटकर अपनी झोली में मौजूद चीन और तुर्की के ड्रोनों और मिसाइलों को बुरी तरह भारत के 26 ठिकानों पर झोंक दिया। लेकिन वे कुछ नहीं कर पाए। दूसरी तरफ उसका चीनी एयर डिफेंस सरगोधा और चकलाला जैसे एयरबेसों को नहीं बचा सका।
भारतीय सेना ने अपना आक्रामक लक्ष्य 6-7 मई की रात को ही हासिल कर लिया था। उसके बाद जो भी हुआ, वह नपा-तुला और जवाबी था। भारत की योजना पाकिस्तान के ‘आतंकी नेटवर्क’ को ध्वस्त करने की थी। भारत चाहता, तो उसे और पीड़ा पहुंचा सकता था। इस लड़ाई में उसके 40 में से केवल 11 वायुसेना हवाईअड्डों पर ही आंशिक हमले किए गए। पाकिस्तान को अब पता लग चुका है कि यदि भारत, विनाशकारी हमले करने पर आता तो उन्हें रोकने के लिए उसके पास एयर डिफेंस है ही नहीं।
परमाणु धमकी
लड़ाई शुरू होने के पहले पाकिस्तानी मीडिया में ऐसे विशेषज्ञों की भरमार थी, जो बार-बार अपने एटम बमों का वास्ता दे रहे थे। उनका कहना था कि ये बम क्या हमने दिखाने के लिए बनाए हैं? इस संदर्भ में भारत के इस अभियान को उस एटमी धमकी को चुनौती के रूप में भी देखा जाना चाहिए। भारत ने परमाणु प्रहार के खतरों से विचलित हुए बिना पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे पर हमला किया, जो मनोवैज्ञानिक और सैद्धांतिक बदलाव का संकेत है। इसका व्यापक रूप से यह अर्थ लगाया गया कि भारत अब पाकिस्तान की परमाणु ताकत को लेकर संशय में नहीं है। भारत से पाकिस्तान की लड़ाई 15 अगस्त, 1947 के पहले से चल रही है, जब वह बना भी नहीं था, पर उसकी अवधारणा जन्म ले रही थी। यह बात अपनी तार्किक परिणति तक बहुत जल्द पहुंचने वाली नहीं है, पर भारत ने जैसा जवाब इस बार दिया है, वह पाकिस्तान के ‘नव-नियुक्त फील्ड मार्शल’ को ताउम्र विचलित रखेगा। बहरहाल वे मानते हैं कि दोनों देशों के बीच ‘छोटा सा संकट भी’ वैश्विक शक्तियों को उसके हक में हस्तक्षेप करने को मज़बूर करेगा।
वैश्विक मंच पर मुकाबला
पाकिस्तान का इरादा हर हाल में कश्मीर का अंतरराष्ट्रीयकरण होता है। किसी तरह भारत को बातचीत की मेज पर लाना। क्या वह अबकी बार भी ऐसा करने में सफल होगा? अभी ऐसा लगता तो नहीं, पर भारत की परीक्षा अब वैश्विक मंच पर होगी। ऐसा पहली बार हुआ है, जब दो स्थापित परमाणु शक्तियां, एक-दूसरे से भिड़ी हैं। इसके पहले ऐसी स्थितियां दो बार और बनी थीं। एक बार 1969 में उसुरी नदी के पास रूस और चीन का संघर्ष और फिर 1999 में करगिल में भारत और पाकिस्तान का टकराव। 1969 में चीन और 1999 में पाकिस्तान का नाभिकीय सामर्थ्य केवल सांकेतिक थी, बहुत बड़ी नहीं। इस बार की लड़ाई टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण थी। इसमें ‘आक्रमण और सुरक्षा’ दोनों की तकनीकों की भूमिका थी और दोनों मामलों में भारतीय सेना पाकिस्तान पर बहुत भारी पड़ी।
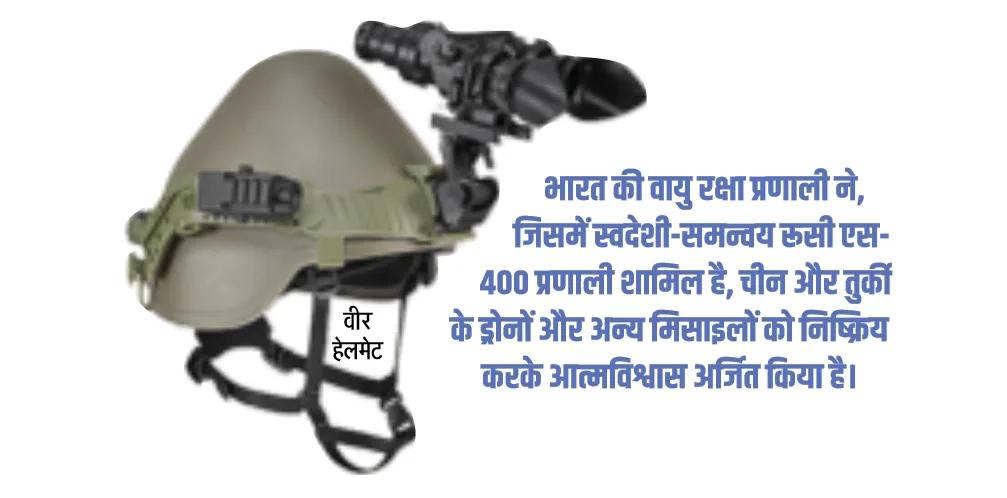
लड़ाई जारी है…
यह समय खुश होने का है, आत्मश्लाघा का नहीं। यह भी मानकर चलिए कि पाकिस्तानी आतंकवाद आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। इस लड़ाई में हमने सफलता हासिल जरूर की है, पर पाकिस्तान और उसके आका चीन ने भी कुछ सबक सीखे हैं। वह अब पाकिस्तान को और भी ज़्यादा घातक मिसाइलों और बेहतर वायु रक्षा प्रणालियों से लैस करेगा। हमें निरंतर सावधान रहने की जरूरत होगी। हमें अत्याधुनिक साइबर और सूचना-युद्ध क्षमताओं को विकसित करना नहीं भूलना चाहिए। यहां चीन असली खतरा है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं। ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की बहुत सी उपलब्धियों का पता कुछ देर से लगेगा, पर फौरी तौर पर गिनें, तो इस प्रकार हैं :
- सीमा पार किए बिना पाकिस्तान के अंदर तक मार करके भारतीय सेना ने पाकिस्तान की बड़ी कमजोरी को रेखांकित किया है। खासतौर से यह देखते हुए कि उसकी पीठ पर चीन का हाथ है।
- पाकिस्तान की एटमी धमकी खोखली साबित हुई। उसके नेता टीवी बहसों से लेकर संसदीय चर्चा तक में कह रहे थे कि हमने एटम बम क्या तहखानों में जमा रखने के लिए बनाए हैं।
- सीमा पार आतंकवाद पर भारत ने नई सीमारेखा खींच दी है कि आतंकवाद की किसी भी गतिविधि को युद्ध माना जाएगा।हालांकि युद्ध विराम कुछ जल्दी हो गया, लेकिन सिंधु जल-संधि स्थगित है, वीजा और व्यापार पर प्रतिबंध जारी हैं। भारत की वायु रक्षा प्रणाली ने, जिसमें स्वदेशी-समन्वय रूसी एस-400 प्रणाली शामिल है, चीन और तुर्की के ड्रोनों और अन्य मिसाइलों को निष्क्रिय करके आत्मविश्वास अर्जित किया है। भारत की ब्रह्मोस और आकाशतीर जैसी अस्त्र-प्रणालियों को लेकर दूसरे देशों में पहले ही पूछताछ चल रही थी। अब उनकी सफलता के प्रमाण भी हमारे पास हैं। भारत धीरे-धीरे सैन्य सामग्री के आयातक से निर्यातक देश बनता जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि देश ने अपनी विखंडित आंतरिक राजनीति के बावजूद एकजुटता दिखाई। देश के सांसदों के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल इस समय दुनिया के कोने-कोने में जाकर भारत का दृष्टिकोण दुनिया के सामने रख रहे हैं।
















टिप्पणियाँ