भारत के इतिहास के रूप में अभी तक छात्रों को दिल्ली सल्तनत का इतिहास पढ़ाया जाता है। एक विद्यार्थी को अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीतियों और मुहम्मद बिन तुगलक की नीतियों को किशोरावस्था में ही रटा दिया जाता है। यहां तक कि स्नातक एवं परास्नातक की परीक्षाओं में भी अकबर की राजपूत नीति या अकबर-राजपूत संबंधों पर एक अनिवार्य प्रश्न रहता है, जिसे विद्यार्थियों को रटना होता है। दरअसल, वामपंथी इतिहासकारों ने न केवल भारत के गौरवशाली इतिहास की अनदेखी की, बल्कि भारतीय राजाओं को दोयम दर्जे का बताया और विदेशी आक्रांताओं का महिमामंडन किया।

इतिहास विभाग, शहीद भगतसिंह कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय
इसके पीछे मंशा थी-हिंदू मानस में हीन भावना भरना व अनेक आत्मगौरव को नष्ट करना, ताकि यह स्थापित किया जा सके कि राजपूतों ने अपने गौरव एवं स्वाभिमान को मुस्लिम शासकों के सामने तिरोहित कर दिया। वही इतिहास आज तक पढ़ाया जा रहा है, इसलिए इन विदेशी शक्तियों के विरुद्ध राजपूत, मराठों, सिक्खों के दीर्घ, सशक्त विरोध और उनके शौर्य की परंपरा किसी पाठ्यक्रम का विषय नहीं है।
वास्तव में, अरबों के सिंध आक्रमण से ही यह विरोध प्रारंभ हो गया था। राजा दाहिर, उनकी पत्नी रानी बाई (जिनके बारे में चचनामा तक में विस्तार से लिखा है), जम्मू-कश्मीर के कार्कोट राजाओं से लेकर मैत्रक राजाओं तक और सैन्धव, चालुक्यों तथा गुर्जर प्रतिहारों तक, सभी ने अरब आक्रमणकारियों को परास्त किया। जम्मू-कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्तापीड ने तो कई अरब अधिकारियों को जेल में रखा और उन्हें दास बनाया।
पश्चिमी छोर में शिलादित्य चतुर्थ, बप्पा रावल, कृष्ण राज प्रथम ने अरबों को भारत भी किसी के कोने में राजनीतिक जड़ें जमाने ही नहीं दीं। चालुक्य राजा भीमसेन द्वितीय ने तो गुजरात में मुहम्मद गोरी की सेना को बुरी तरह पराजित किया था। अलाउद्दीन खिलजी के अल्प काल को छोड़कर गुजरात कभी भी दिल्ली सल्तनत का भाग नहीं रहा। नालन्दा विश्विद्यालय को नष्ट करने वाले बख्तियार खिलजी को कामरूप के राजा पृथु ने बर्बाद कर दिया था, जिसका विस्तृत विवरण तबकात-ए-नाशिरी में मिलता है। लेकिन कोई प्रश्न करने वाला नहीं है कि क्या दिल्ली सल्तनत का विस्तार समस्त भारत में था?
दिल्ली सल्तनत केवल दिल्ली के आसपास के कुछ जिलों तक सीमित एक मुस्लिम शासन व्यवस्था थी। लेकिन यह विषय समस्त भारत के विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है। क्यों? पूरे सल्तनत काल में ओडिशा कभी भी तुर्क अफगान साम्राज्य का हिस्सा नहीं रहा। ओडिशा के गंग वंश, सूर्य वंश, भोई वंश के बाद के राजवंशों ने दिल्ली और निकटतम बंगाल व बहमनी राज्य से निरंतर संघर्ष करते हुए न केवल अपनी स्वतंत्रता बचाकर रखी, बल्कि हिंदू धर्म, संस्कृति, कला, विद्या, साहित्य का अभूतपूर्व विकास भी किया। ओडिशा के गंगवंशी राजाओं ने बंगाल के मुस्लिम आक्रांताओं की बलात् कन्वर्जन नीति से त्रस्त होकर पलायन करने वाले लोगों को भुवनेश्वर स्थित सदाशिव मठ में ससम्मान आश्रय दिया था। गंग राजा अनंगभीम देव तृतीय ने भगवान जगन्नाथ को राज्य का सर्वोच्च संप्रभु घोषित करते हुए ‘जगन्नाथ संस्कृति’ का प्रवर्तन किया।
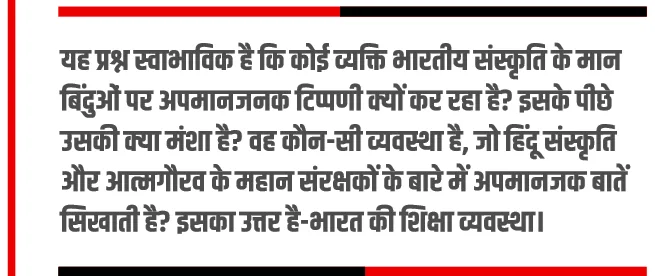
अतीत का गौरव बनाम शिक्षा प्रणाली
प्रश्न यह है कि क्या इतिहास का विद्यार्थी सामान्य रूप से इन सतत संघर्षों से परिचित है, जिन्हें हमारे राजाओं, साधुओं और सामान्य जन ने अपनी भावी पीढ़ियों के लिए किया? अभी हाल ही में संसद में ऐतिहासिक योद्धा राणा सांगा के विरुद्ध अवांछनीय, अनर्गल एवं निराधार टिप्पणी की गई। फिल्म ‘छावा’ की रिलीज के बाद औरंगजेब को ‘महान’ सिद्ध करने के अनथक बौद्धिक प्रयासों को समझने के लिए मध्यकालीन इतिहास के लेखन की प्रवृत्तियों पर गौर करना होगा। इस क्रम में सबसे पहले राणा सांगा के चरित्र को समझना होगा।
लोदियों के समय भारत वर्ष में दो प्रतापी राजा थे-उत्तर भारत में राणा सांगा और दक्षिण भारत मे विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय।
इन दोनों ने धर्म प्रतिपालक की उपाधि धारण कर रखी थी। जहां तक राणा सांगा और बाबर की कथित संधि या आमंत्रण का प्रश्न है, इस विषय में ऐसा न तो कोई साक्ष्य है और न ही सामान्य विवेक, जो यह सिद्ध कर सके कि राणा सांगा ने बाबर के साथ किसी भी प्रकार का संबंध रखा। राणा सांगा तो इब्राहीम लोदी को पहले ही तीन युद्धों में परास्त कर चुके थे। तब उनका प्रभाव क्षेत्र उत्तर भारत, मध्य भारत, गुजरात और मालवा तक था। उस समय बाबर राज्य विहीन था और मध्य एशिया में भटक रहा था। राणा को उसे आमंत्रित करने की क्या आवश्यकता थी? इसकी आवश्यकता बाबर को हो सकती थी, क्योंकि वह एक अनजान देश में आ रहा था।
यदि राणा सांगा ने अपना दूत बाबर के पास भेजा होता, तो बाबर के अलावा अन्य समकालीन मुगल या अफगान लेखकों ने अवश्य इसका उल्लेख किया होता। राजपूतों की परंपरा में बाह्य शक्ति की सहायता कभी नहीं ली गई। रही बात राणा सांगा की, तो वे स्वयं को धर्म रक्षक कहते थे। बाबर ने अपनी आत्मकथा में आलम खां लोदी और दौलत खां लोदी से की गई संधियों के बारे में विस्तार से लिखा है। अगर राणा सांगा के साथ उसने कोई संधि की होती तो वह उसके बारे में भी लिखता। जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं तो वह क्यों लिखता? इसके विपरीत कई शोध बताते हैं कि खानवा के युद्ध में पहले बाबर ने स्वयं राणा सांगा से संधि करनी चाही थी, किंतु राणा सांगा ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इससे क्रुद्ध होकर बाबर ने राणा पर विश्वासघात का आरोप लगाकर जिहाद घोषित कर दिया।
ऐसे में यह प्रश्न स्वाभाविक है कि कोई व्यक्ति भारतीय संस्कृति के मान बिंदुओं पर अपमानजनक टिप्पणी क्यों कर रहा है? इसके पीछे उसकी मंशा क्या है? वह कौन-सी व्यवस्था है, जो हिंदू संस्कृति और आत्मगौरव के महान संरक्षकों के बारे में अपमानजक बातें सिखाती है? इसका उत्तर है-भारत की शिक्षा व्यवस्था। यह ऐसी व्यवस्था है जो हमें आत्मघृणा सिखाती है, बाबर-औरंगजेब सहित इस्लामी क्रूरता के विरुद्ध बोलने से रोकती है। इस विषय पर फिल्म बनाने पर उसे साम्प्रदायिक घोषित कर देती है, जबकि हॉलीवुड में यहूदियों पर हुए अत्याचारों, द्वितीय विश्व युध्द आदि पर धड़ल्ले से फिल्में बनती हैं।
मुस्लिम-वामपंथी इतिहासकार और कांग्रेस
स्वतंत्रता के पश्चात् नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी के समय तक वैसे तो समस्त इतिहास, लेकिन विशेष रूप से, मध्यकालीन इतिहास का महिमामंडन इस तरह से किया गया मानो इस्लाम भारत में नहीं आता तो इस देश की अर्थव्यवस्था, संस्कृति, खान-पान, शिल्प और वास्तुकला का विकास ही नहीं होता! इसमें एक मुख्य कारण इस अवधि में शिक्षा मंत्री रहे मौलाना अबुल कलाम आजाद, प्रोफेसर हुमायूं कबीर और सैयद नुरूल हसन थे। इन्होंने अपना मजहबी एजेंडा चलाया, जिसे कांग्रेस सरकार का पूर्ण वैचारिक समर्थन प्राप्त था। इसके लिए बाकायदा एक तंत्र बनाया गया, जिसके केंद्र में हिंदू द्रोह, आत्मघृणा और इस्लाम का प्रचार-प्रसार करना शामिल था। इन लोगों ने ऐसा माहाैल बनाया कि समाज अपने सांस्कृतिक विध्वंस का जश्न मनाने लगा। उसने अपने पूर्वजों के अपमान को ही अपना गौरव बना लिया। दुर्भाग्य से, तब से लेकर अब तक स्कूलों और विश्वविद्यालयों तक के सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रमों के जरिये इस प्रकार का नैरेटिव पीढ़ी दर पीढ़ी वैचारिक पटल को संक्रमित करता आ रहा है।
प्रो. इरफान हबीब ने तो दिल्ली सल्तनत में तुर्कों के माध्यम से ‘नगरीय क्रांति’ को उत्पन्न करा दिया और पूर्व मध्य काल (मुख्यतः राजपूत साम्राज्य) को ‘अंधकार युग’ कहना शुरू कर दिया। इन मुस्लिम और वामपंथी इतिहासकारों ने भारत की अनवरत भक्ति परंपरा, जो वैदिक काल से चली आ रही थी, को भी सूफी आंदोलन के प्रभाव के रूप में दिखाने का प्रयास किया। लेकिन सीताराम गोयल जैसे इतिहासकार कहते हैं, ‘‘सूफी साहित्य का विशद अध्ययन करने के बाद मेरा दृढ़ विश्वास है कि सूफी सिलसिलों में अध्यात्म की खोज करना तो दूर की बात है, मानव सुलभ साधारण नैतिकता की गंध भी उसमें नहीं मिलती है।’’ अधिकांश सूफी मजार मंदिरों के खंडहरों पर बने हैं। मध्यकालीन इतिहास में मुगल-राजपूत संबंध, मध्यकालीन वाणिज्य-व्यापार पर तो बहुत कुछ लिखा गया, लेकिन बर्बर तुर्कों, मुगलों और पठानों के अत्याचारों, लूटपाट, कन्वर्जन सहित इस्लाम के वास्तविक स्वरूप के बारे में कभी नहीं लिखा गया।

हिंदुओं और आक्रांताओं के संघर्ष का युग
भारतवर्ष के इतिहास में ‘मुसलमान युग’ कभी रहा ही नहीं। जिस युग को ‘मुसलमान युग’ कहा जाता है, वास्तव में वह हिंदू जाति और मुस्लिम आक्रांताओं के बीच सतत संघर्ष का युग था। उस संघर्ष में जय हिंदू जाति की ही हुई। ध्यातव्य है कि उस महायुद्ध के लंबे कालखंड में हिंदू जाति कभी एक क्षण के लिए भी मुस्लिम आक्रांताओं के विरुद्ध संघर्ष करने के दौरान कायर मुद्रा में नहीं दिखी, बल्कि नित्यप्रति प्रचंड पराक्रम का परिचय देती रही।
वामपंथी इतिहासकारों ने औरंगजेब की ‘वीरता’, ‘पराक्रम’, ‘युद्ध कौशल’ तथा सैन्य गुणों का महिमामंडन तो किया, लेकिन राजपूतों से मिली पराजयों का जिक्र तक नहीं किया। सच यह है कि 1690 से लेकर 1707 ई. तक मराठा स्वाधीनता आंदोलन के दौर में संताजी घोरपड़े और धन्ना जी जाधव ने ताराबाई के नेतृत्व कौशल में उसे कई बार हराया था।
औरंगजेब के विरुद्ध राणा राजसिंह ने कई युद्ध लड़े और मुगलों से चित्तौड़, मांडलगढ़, मंदसौर, जीरन तथा अन्य बहुत से किलों को जीत भी लिया। उनके इस संघर्ष में मेवाड़ की आम जनता, पश्चिमी जंगलों की आदिम जातियां, प्रत्येक राजपूत योद्धा शामिल हुआ। राणा राजसिंह, उनके पुत्र जयसिंह, राजकुमार कुंवर भीमसिंह, मेवाड़ के सामंत विक्रम सोलंकी, गोपीनाथ राठौड़, वीर दुर्गादास, वीर सांवलदास तथा वीर बांकुरे दयालसिंह ने 1681 ई. में औरंगजेब की संपूर्ण सेना को भिन्न-भिन्न जगहों पर दसियों बार हराया। अजमेर, मालवा, गुजरात सभी जगह प्रतिरोध अत्यंत जटिल था। कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक ‘एनल्स एंड एंटीक्वीटीज ऑफ राजस्थान’ में इनका वर्णन किया है।
ये कथित इतिहासकार यहां तक कहते हैं कि इस्लाम के प्रगतिशील स्वरूप के कारण ही भारत में सामाजिक क्रांति आई। दरअसल, भारत में इस्लाम विजयी दिखाने के पीछे मंशा ‘जनमत में बदलाव’ करना था, जिसका प्रभाव केवल इतिहास तक सीमित नहीं था। यह कुत्सित प्रयास साहित्य व सिनेमा आदि के माध्यम से भी लोकमन में स्थापित करने का प्रयास किया गया। हिंदी के प्रख्यात लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इस्लाम के बारे में लिखतें हैं, ‘‘भारत में एक ऐसे मजहब का आगमन हुआ, जिसके केंद्र में समता का भाव था। वर्षों से हिंदू समाज का वह वर्ग, जो पददलित और हाशिये पर था, उसे इस्लाम ने अपनी बांहें फैलाकर स्वीकारा।’’
इस आत्म घृणा और इस्लाम की गौरवगाथा को इतिहास में ठूंसा गया, जबकि इसी मुस्लिम काल के बारे में विल डुरंट ने लिखा कि 8.5 करोड़ हिंदुओं का नरसंहार हुआ। हजारों मंदिरों को तोड़ा गया, संस्कृत के ग्रंथ जला दिए गए। ज्ञान आधारित एक संस्कृति को पूरी तरह नष्ट करने के सभी प्रयास किए गए। समस्त मुस्लिम शासन का स्वरूप और आदर्श प्रधान रूप से विदेशी थे। यहां तक कि कथित तौर पर सबसे ‘उदार’ अकबर के समय भी लगभग सभी अधिकारी विदेशी थे। उसके प्रशासन में भारतीय मुसलमानों को भी जगह नहीं मिलती थी।
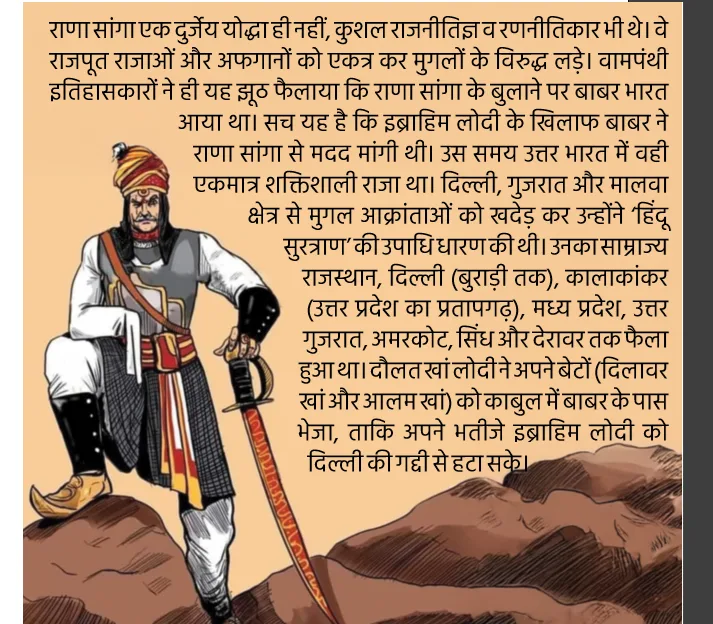
शिक्षा से दूर अय्याश थे मुगल
मुगलों के शासनकाल में करोड़ों लोगों के शारिरिक, बौद्धिक तथा नैतिक सुधार, जनता की शिक्षा के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। चित्रकारी, संगीत मुगलों का निजी शाैक था। इसका उद्देश्य देश की कला और संस्कृति का विस्तार करना कतई नहीं था। मुगलों ने अपने समूचे कार्यकाल में मुसलमान और गैर-मुसलमानों के बीच सदैव भेदभाव बनाए रखा। जहांगीर ने तो हिंदुओं पर मुस्लिम लड़कियों के साथ विवाह करने पर प्रतिबंध लगा रखा था। इसका उल्लंघन करने पर उसने मृत्युदंड की घोषणा की थी। शाहजहां भी उसी के पदचिह्नों पर चला। इसके बाद औरंगजेब और उसके बाद उसकी जो औलादें गद्दी पर बैठीं, वे कट्टर मुस्लिम और हिंदू हंता थीं।
जदुनाथ सरकार के अनुसार, शरिया कानून के कारण जनता की एकता और राजनीतिक समानता नष्ट हो जाती है और जनता सदा के लिए दो भागों में बट जाती है। मुगलों के शासनकाल में हिंदुओं को हमेशा इस बात का डर रहता था कि कठमुल्लों के नेतृत्व में मुसलमान किसी भी समय उन पर हमला कर देंगे और उन्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। (देखें बाॅक्स) मध्यकाल के इतिहास लेखन में छत्रपति शिवाजी महाराज, लाचित बरफूकन, ललितादित्य मुक्तापीड आदि को केवल क्षेत्रीय शासकों की तरह दिखाया गया है। सच यह है कि चाहे कोई भी कालखंड रहा हो, क्षेत्रीय शक्तियां या राज्य वास्तव में भारत की सातत्यता का इतिहास हैं, न कि क्षेत्रीय इतिहास। लाचित बरफूकन, ललितादित्य स्वयं को सिर्फ असम या कश्मीर के राजा नहीं मानते थे। त्रावणकोर के राजा स्वयं को पद्मनाभ स्वामी का सेवक कहते थे।
काशी के राजा स्वयं को काशी विश्वेश्वर का दास लिखते थे। महाराणा प्रताप स्वयं को सदैव एकलिंग जी का दीवान लिखते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज केवल महाराष्ट्र के राजा नहीं, अपितु हिन्दवी साम्राज्य के राजा, गो-ब्राह्मण प्रतिपालक और धर्मपालक थे। ध्यान देने योग्य है कि जिस प्रकार की उपाधि विजयनगर के संस्थापक हरिहर ने 14वीं शताब्दी में धारण की थी, ठीक उसी प्रकार की उपाधि 300 वर्ष बाद शिवाजी महाराज ने धारण की। इसलिए इन सैकड़ों वर्षों की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक लक्ष्यों की निरंतरता को देखा जाना चाहिए। जब भी अवसर आया, भारतीय राजाओं ने अपने धर्मस्थलों और श्रद्धा केंद्रों का पुनर्निर्माण करवाया।
हिंदू आज भी गांधीवाद, उदारवाद के कारण स्वयं भ्रमित होता है और अगली पीढ़ियों को भी भ्रमित करता है। इन कथित इतिहासकारों ने जितने भी भारतीय राजा थे, उनके लिए निंदनीय विशेषणों का प्रयोग किया। जैसे-महाराजा शिवाजी के लिए ‘पहाड़ी चूहा’, जाट राजाओं के लिए ‘लुटेरा’। सोचने वाली बात है कि इन इतिहास लेखकों की मंशा कितनी विषाक्त रही होगी! विश्व में इस तरह का उदाहरण किसी भी समाज में नहीं मिलता।
आजादी के पश्चात् नेहरूवादी समाजवाद, कथित पंथनिरपेक्षता और वामपंथ को अकादमिक जगत ने एक अनिवार्य और शाश्वत भारतीय मूल्य, जो किसी भी आलोचना से परे है, को विकृत रूप में स्थापित किया। इन्हीं दोयम मूल्यों-मापदंडों के आधार पर देखने की दृष्टि बनी। आज संस्कृति का जो भी भाव और सम्मान बचा है, वह समाज, परिवार, गांव के धार्मिक संस्कारों के कारण ही है। विद्या के संस्थानों में तो आत्मदोष और केवल विरोध, चाहे ब्राह्मण-दलित विरोध हो, आर्य-अनार्य विरोध या उत्तर-दक्षिण विरोध आदि में विभाजित अस्मिता के संघर्ष, को ही नैरेटिव के रूप में स्थापित किया गया। आवश्यकता है कि मध्यकालीन इतिहास को वस्तुनिष्ठ व संपूर्णता में लिखा जाए। इतिहास को किसी खास उद्देश्य के लिए उपयोग में न लाया जाएं। इसकी शुरुआत पाठ्यक्रम परिवर्तन से होनी चाहिए।
शरिया अदालतें गैर-कानूनी
दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगल काल तक लगभग सभी मुस्लिम शासकों ने भारत में शरीयत कानून को लागू करने का प्रयास किया। हिंदुओं के समक्ष जजिया जीवन का विकल्प होता था। जजिया वसूलने की पद्धति बहुत घृणित और अपमानजनक थी, जिसका वर्णन बर्नी और अबुल फजल ने किया है। विंसेंट स्मिथ और विलियम म्यूर ने इसे धार्मिक अपमान का एक उदाहरण बताया है। लेकिन इसके विपरीत मध्यकालीन इतिहासकारों द्वारा जजिया तक के औचित्य को सिद्ध करने का प्रयास किया गया। इसी प्रकार, शरीयत को भी उचित ठहराया गया।
उल्लेखनीय है कि इस शरीयत से मध्य एशिया के राजनीतिक वर्ग के मुसलमान भी परिचित नहीं थे। लेकिन अपनी एक विदेशी व श्रेष्ठ पहचान बनाए रखने के लिए उन्होंने इसे भारत पर लादना चाहा। औरंगजेब ने तो फतवा-ए-आलमगीरी पुस्तक में शरीयत का संकलन करवाया। शरीयत अच्छे से समस्त जनता में लागू हो, उसके लिए तमाम अधिकारी नियुक्त किए। उत्तर भारत के गांवों में आज भी खंडित मूर्तियां मिलती हैं। यह इसलिए हुआ कि विशाल मंदिर नीतिगत रूप से खंडित किए गए। अपने आराध्यों के विग्रहों की हिंदू समाज ने हर प्रकार से रक्षा करने की कोशिश की। इसी शरीयत को न स्वीकार करने के कारण सिख गुरुओं और उनके साहिबजादों को बलिदान देना पड़ा।
इस कुकर्म को भी राजनीतिक संघर्ष कह कर इसके आध्यात्मिक संघर्ष को धूमिल करने का प्रयास किया जाता है। इसी शरीयत के आधार पर भारत माता के विभाजन के पश्चात् भी समाज का एक वर्ग यह चाहता है कि शरीयत से राजनीति व समाज संचालित हो। जब भी संविधान के समान रूप से लागू करने की बात होती है तो वह अपनी मजहबी पहचान को ही मुख्य पहचान बताता है और सारे कथित बुद्धजीवी इसका समर्थन करते हैं।
अभी भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा शरीयत अदालतें चलाई जाती हैं। इनका प्रयास यही है कि भारत में न्याय व्यवस्था के समानांतर यह व्यवस्था चलती रहे। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय को भी कहना पड़ा कि ये शरिया अदालतें भारतीय संविधान और न्यायिक प्रणाली के विरुद्ध हैं। इनके द्वारा जारी फतवों की कोई कानूनी मान्यता नहीं है। शीर्ष अदालत ने यह निर्णय 2014 में विश्व लोचन मदान मामले में दिए गए एक निर्णय को दोहराते हुए तलाक के ताजा मामले में दिया है।
















टिप्पणियाँ