इन दिनों भारतीय न्यायपालिका की विश्वसनीयता बुरी तरह से लड़खड़ाई हुई है। दरअसल, जिस न्यायपालिका के प्रति हम सभी की, और खासकर मेरे मन में बड़ा श्रद्धा और सम्मान है, वह नैतिकता के पैमाने पर लगातार अवनति की ओर जा रही है, इसलिए लोगों में उसके प्रति संदेह उभरने लगा है।
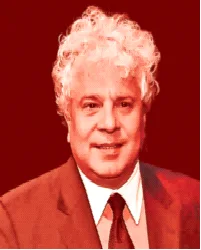
प्रख्यात मार्केटिंग गुरु
कुछ साल पहले की वे सुर्खियां सबको याद होंगी जब सर्वोच्च न्यायालय के चार तत्कालीन न्यायाधीशों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और सर्वोच्च न्याय प्रणाली के प्रति अपना विरोध प्रदर्शित किया। इस घटनाक्रम से सभी लोगों को हैरान कर दिया।
स्वाभाविक है कि ऐसा होने पर जनता के बीच आशंकाएं सुगबुगाने लगीं कि जब न्यायाधीश ही सार्वजनिक रूप से विरोध पर उतर आएं हैं तो क्या न्याय की धवलता धूमिल हो रही है ? सवाल यह है कि क्या भारतीय न्याय प्रणाली के स्तम्भ कमजोर पड़ने लगे हैं? क्या भारत की न्याय प्रणाली की प्रशासनिक व्यवस्था में अन्याय के कुछ कण उपजने लगे हैं?
न्यायिक व्यवस्था में ऐसे नियम नहीं होने चाहिए जो किसी न्यायाधीश को अन्य न्यायाधीशों को चुनने या नामित करने का अधिकार देते हों। अगर वह किसी उपयुक्त व्यक्ति को चुनता है तब भी वह पक्षपात, या भाई-भतीजावाद के आरोपों से बच नहीं पाता। सामान्यत:, यह देखा गया है कि जिन न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई, वे बहुत प्रतिभाशाली और गुणी थे और उनमें उपयुक्त पात्रता थी। उनका नैतिक दृष्टिकोण और आचरण भी श्रेष्ठ था। लेकिन हमारे सामने ऐसे भी उदाहरण हैं जिसमें कई न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद भी नया पदभार ग्रहण करने को इच्छुक रहते हैं जो भारतीय न्याय प्रणाली की निष्पक्षता को लेकर स्वाभाविक संदेह जगाता है। सेवानिवृत्त होने वाले न्यायाधीशों की सरकार से कोई लाभ हासिल करने की बलवती इच्छा सेवानिवृत्ति के तुरंत पहले दिए गए उनके फैसले को अहम रूप से प्रभावित करती है।
खर्चीली न्यायप्रक्रिया
हमारे देश की बेहद खर्चीली न्याय प्रणाली भी एक विचारणीय बिन्दु है। जिला स्तर हो, राज्य स्तर, या फिर सर्वोच्च न्यायालय, कुछ वकीलों की फीस बहुत ही अधिक होती है। फिर भी, केवल वकीलों को दोष देना उचित नहीं है। दरअसल, ऐसे वकीलों की संख्या बहुत कम हैं जो अपने मुवक्किलों के मामलों पर न्यायाधीशों के सामने जोरदार पैरवी करके उन्हें जिताने की क्षमता रखते हैं। स्पष्ट है कि अदालती मामलों में विजयी होने के आकांक्षी ऐसे वकीलों को कोई भी कीमत देने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसा महसूस होता है कि न्यायिक व्यवस्था सुरसा-सा मुंह खोल अदालती चक्रव्यूह में फंसे लोगों को लीलने के लिए आतुर है। यह स्थिति तब और घातक हो उठती है जब कोई न्यायाधीश अपने पद के तहत निर्धारित लाभों के अलावा अन्य लाभ लेने की आकांक्षा का पोषण भी करने लगता है। यह प्रवृत्ति बेहद निंदनीय है।
न्याय प्रणाली पर सवाल
हाल ही में उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के आवासीय परिसर में बेहिसाब नकदी मिलने की खबर ने हलचल मचा दी। यह मुद्दा कि नकदी रिश्वत के रूप में दी गई थी या उसे वहां रखा गया था, उतना प्रासंगिक नहीं है। बात हमारे विश्वास से जुड़ी है।
हम एक न्यायाधीश को न्याय का देवता मानते हैं जो नैतिकता का प्रतीक होता है। पर जब कोई न्यायाधीश किसी भ्रष्ट काम में लिप्त पाया जाता है तब पूरी न्याय व्यवस्था संक्रमित होने लगती है।
किसी नौकरशाह, नेता या सरकारी अधिकारी के पास आय से अधिक बेहिसाब धन मिलने पर उसे जेल हो जाती है। पर इस मामले में, उस न्यायाधीश को अदालत से हल्की-सी फटकार मिली और उन्हें उनकी मौजूदा न्यायिक जिम्मेदारियों से मुक्त कर किसी और न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया। इस घटना ने हमारी न्याय प्रणाली की अलग ही व्याख्या पेश की है, यह दोहरे मानदंडों और न्याय-विरोधी व्यवस्था को दर्शाती है जो अन्यायपूर्ण है। न्याय के दो तत्व हैं, नीति और न्याय, जिसका अर्थ है न्याय की प्रक्रिया और न्याय आधारित निर्णय। जो अंततः न्याय का अर्थ है निष्पक्षता।
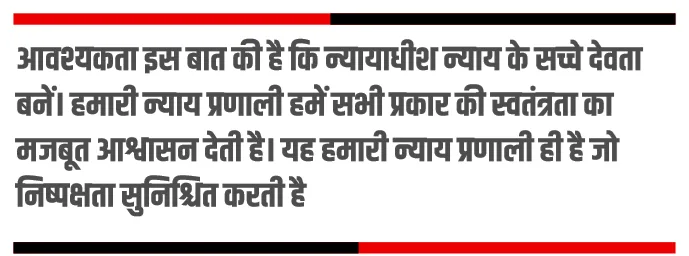 जब हम भारत की न्यायपालिका की स्थिति का विश्लेषण करते हैं तो साफ दिखता है कि हमारी न्याय प्रणाली अंतहीन, अनुचित और अन्यायपूर्ण तत्वों का पोषण कर रही है और इसके लिए उपयुक्त माहौल इसने स्वयं सबूतों, तर्कों या अन्य स्थितियों पर अपनी निर्भरता कायम करते हुए तैयार किया है। आवश्यकता इस बात की है कि न्यायाधीश न्याय के सच्चे देवता बनें। हमारी न्याय प्रणाली हमें सभी प्रकार की स्वतंत्रता का मजबूत आश्वासन देती है। यह हमारी न्याय प्रणाली ही है जो निष्पक्षता सुनिश्चित करती है; जवाबदेही सुनिश्चित करती है; यह भी सुनिश्चित करती है कि हमारा लोकतंत्र सुचारु रूप से चले। जब यह न्याय प्रणाली संदेह के घेरे में आती है, तो हमारे लोकतंत्र के हर आयाम के प्रति पर सवालों की बाढ़ आ जाती है: चाहे न्यायपालिका पर राजनीतिक प्रभाव का सवाल हो, या वह न्यायपालिका द्वारा राजनीति पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित हो; या फिर न्याय प्रणाली को प्रभावित करने के तरीके से जुड़ा हो, जैसा कि हाल की घटना में दिखा। देखना यह है कि ऐसी स्थिति में हमारी न्यायपालिका कैसे खुद को पारदर्शी बनाती है और कैसे उच्च स्तरीय ईमानदारी के मानदंडों के अनुरूप स्वयं को ढालती है।
जब हम भारत की न्यायपालिका की स्थिति का विश्लेषण करते हैं तो साफ दिखता है कि हमारी न्याय प्रणाली अंतहीन, अनुचित और अन्यायपूर्ण तत्वों का पोषण कर रही है और इसके लिए उपयुक्त माहौल इसने स्वयं सबूतों, तर्कों या अन्य स्थितियों पर अपनी निर्भरता कायम करते हुए तैयार किया है। आवश्यकता इस बात की है कि न्यायाधीश न्याय के सच्चे देवता बनें। हमारी न्याय प्रणाली हमें सभी प्रकार की स्वतंत्रता का मजबूत आश्वासन देती है। यह हमारी न्याय प्रणाली ही है जो निष्पक्षता सुनिश्चित करती है; जवाबदेही सुनिश्चित करती है; यह भी सुनिश्चित करती है कि हमारा लोकतंत्र सुचारु रूप से चले। जब यह न्याय प्रणाली संदेह के घेरे में आती है, तो हमारे लोकतंत्र के हर आयाम के प्रति पर सवालों की बाढ़ आ जाती है: चाहे न्यायपालिका पर राजनीतिक प्रभाव का सवाल हो, या वह न्यायपालिका द्वारा राजनीति पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित हो; या फिर न्याय प्रणाली को प्रभावित करने के तरीके से जुड़ा हो, जैसा कि हाल की घटना में दिखा। देखना यह है कि ऐसी स्थिति में हमारी न्यायपालिका कैसे खुद को पारदर्शी बनाती है और कैसे उच्च स्तरीय ईमानदारी के मानदंडों के अनुरूप स्वयं को ढालती है।
इस हालिया मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने जो कार्रवाई की, वह एक अच्छा उदाहरण बनी है, पर यह सब थोड़ी देरी से हुआ। जब स्थिति इतनी बिगड़ गई कि मीडिया में यह रोजाना सुर्खियों का हिस्सा बनने लगी और सोशल मीडिया पर टिप्पणियों की बाढ़ आ गई, तब जाकर न्यायपालिका ने जनता की अपेक्षा के मद्देनजर कार्रवाई की और फैसला सुनाया। भविष्य में इसी देरी से परहेज करना होगा। मेरा दृढ़ रूप से मानना है कि अगर कोई न्यायाधीश अनुचित कार्यकलापों, भ्रष्टाचार, कदाचार में लिप्त है, तो उन्हें ऐसा दंड मिले जो न्याय की पीठ पर विराजमान हर न्यायकर्ता के लिए एक पाठ हो जिससे वह अपने व्यवहार और विचारों में नैतिक मूल्यों का पालन करे और ऐसे आदर्श की स्थापना करें जो अन्य किसी पेशे में काम कर रहे लोगों से श्रेष्ठ हो।
















टिप्पणियाँ