लोकतंत्र के चार स्तंभों में से एक न्यायपालिका न्याय की सर्वोच्चता सुनिश्चित करती है, लेकिन भारत में अनेक मौके ऐसे भी आए, जब इस स्तंभ में कंपन महसूस हुआ। न्यायपालिका अपने पथ पर सीधी और सच्ची चली, इसे लेकर अनेक बार संदेह पैदा हुए। न्यायपालिका के कर्णधारों के चाल-चलन और नियमन की निगरानी भी न्यायपालिका ने अपने ही हाथों में बनाए रखने का हर संभव प्रयास किया है। इससे इतर हुए प्रयासों को निष्फल बनाने के उदाहरण सामने आते रहे हैं। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा प्रकरण में जो तथ्य उजागर हुए हैं, उन्होंने एक बार फिर लोकतंत्र के इस स्तंभ पर सवाल खड़े किए हैं। न्यायमूर्ति वर्मा या उनसे पहले सामने आए ऐसे अन्य उदाहरणों के संदर्भ में न्यायपालिका के व्यवहार ने आम जन के मन में एक सवाल जरूर खड़ा किया है कि सही-गलत को कसौटी पर कसने वाले ‘न्याय’ की अपनी कसौटी क्या है! इस विषय पर विशेषज्ञों के महत्वपूर्ण विचारों को समाहित करते हुए प्रस्तुत है यह आवरण कथा-
दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के घर में लगी आग बुझाने के दौरान बड़ी मात्रा में नकदी मिलने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने भले ही उनका तबादला इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कर दिया हो, लेकिन यह घटना चर्चा का विषय बनी हुई है। तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। न्यायपालिका में नियुक्तियां, जवाबदेही और पारदर्शिता को लेकर चर्चाएं चल रही हैं।
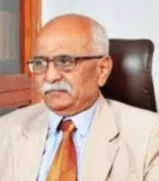
पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष
अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद्
अनुच्छेद 124 और 217 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 124(4) के तहत किसी न्यायाधीश को पद से हटाने के संबंध में संसद के दोनों सदनों द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पेश करने का प्रावधान है। भारतीय संविधान में न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में जो प्रावधान हैं, वे थोड़े जटिल हैं। संविधान के अनुसार, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से परामर्श करते हैं।
संविधान सभा में जब इस विषय पर चर्चा हो रही थी तब एक सदस्य ने सुझाव दिया था कि संविधान में जहां ‘मुख्य न्यायाधीश से परामर्श’ करने की बात लिखी है, उसे ‘मुख्य न्यायाधीश की सहमति से’ पढ़ा जाना चाहिए। इस पर डॉ. आंबेडकर ने इस सुझाव को खारिज कर दिया था। उनकी दलील थी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश भी पूर्वाग्रहों, मानवीय संवेदनाओं और भावनाओं से पूर्ण आम इंसान की तरह ही हैं। ऐसे में सहमति देने की सर्वोच्च शक्ति केवल भारत के राष्ट्रपति को ही प्राप्त होगी। इस पर संविधान सभा में शामिल लोगों की सहमति नहीं बनी, तो संविधान निर्माताओं ने नियुक्ति की शक्ति केवल कार्यपालिका को प्रदान की जिसमें परामर्श करने की बात भी जोड़ी गई।
1970 तक ‘परामर्श’ प्रभावी बना रहा, इसके चलते भारतीय न्यायपालिका ने न्यायमूर्ति वी.वी. बोस, न्यायमूर्ति पतंजलि शास्त्री, न्यायमूर्ति के. सुब्बाराव, पीबी गजेन्द्रगडकर जैसे प्रतिभाशाली न्यायमूर्ति न्यायपालिका को मिले। 1970 के बाद एक अलग प्रवृत्ति उभरने लगी। कार्यपालिका ने परामर्श किए बिना केवल जानकारी के आधार पर उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी शुरू कर दी। प्रेस और कानूनी हलकों, में इसकी जमकर आलोचनाएं हुईं। विभिन्न उच्च न्यायालयों में कुछ न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीशों ने इसके विरोध में इस्तीफा भी दिया। 1970 और 1990 के बीच ऐसी घटनाएं और बढ़ गईं।
1950-1975 के दौरान ‘परामर्श’, ‘सहमति’ और ‘सम्मति’ सभी परस्पर क्रम में जुड़े थे और नियुक्तियों के लिए मुख्य न्यायाधीश सिफारिश या अनुमोदन करते थे। प्रधानमंत्री कार्यालय की मंजूरी के साथ राष्ट्रपति कार्यालय आदेश जारी करता। आपातकाल के बाद कार्यपालिका ने न्यायपालिका पर अपना नियंत्रण बनाने की कोशिश की और वह मुख्य न्यायाधीश को सूचना भर देते हुए नियुक्तियां करती रहीं। न्यायमूर्ति जितेंद्र वीर गुप्ता (पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय) समेत कई न्यायाधीशों ने इसके विरोध में इस्तीफा दिया था।

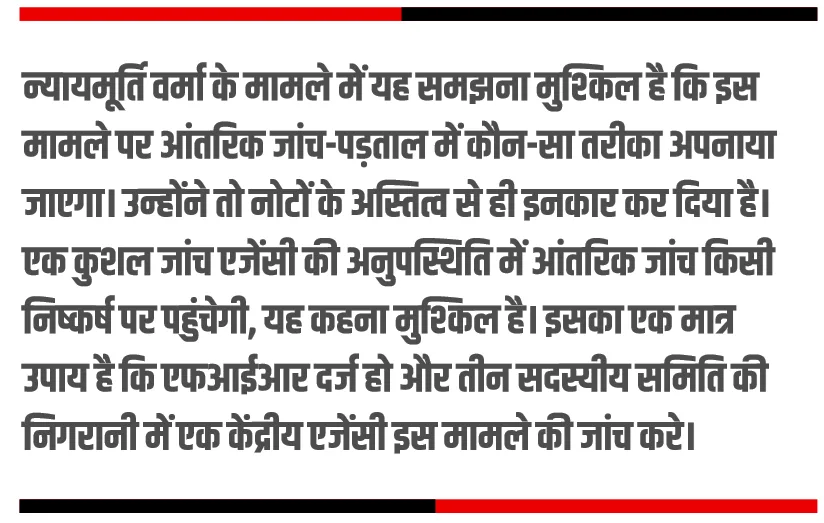
ऐसे अस्तित्व में आया कॉलेजियम
1981 में सर्वोच्च न्यायायल में ‘परामर्श’ शब्द पर बहस की शुरुआत हुई। सवाल उठा कि सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श सरकार के लिए बाध्यकारी है कि नहीं। तत्कालीन न्यायमूर्ति एसपी गुप्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को सिर्फ विचार के तौर पर परिभाषित किया। यानी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति या अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं था। इसे ‘फर्स्ट जजेज केस’ कहा जाता है।
1993 में न्यायमूर्ति जेएस वर्मा की अगुआई में सर्वोच्च न्यायालय की नौ जजों की पीठ ने इस व्यवस्था को पलटते हुए सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को मानना बाध्यकारी बताया। इस फैसले में कहा गया कि परामर्श सरकार के लिए केवल सुझाव नहीं है, बल्कि यह बाध्यकारी है। पीठ ने कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति और तबादले का अधिकार कॉलेजियम के जरिए होगा। यहीं से कॉलेजियम की शुरुआत मानी जाती है। इसे ‘सेकंड जजेज केस’ कहा जाता है। 1998 में तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायण ने संविधान के अनुच्छेद 124, 217, 222 के तहत परामर्श शब्द के अर्थ पर सर्वोच्च न्यायालय की राय मांगी। कुछ दिन बाद ही न्यायमूर्ति एसपी भरुच की अगुआई वाली नाै सदस्यीय पीठ ने 28 अक्तूबर,को आदेश दिया कि नियुक्ति के मामले में न्यायपालिका ऊपर है।
2015 में संसद के दोनों सदनों ने संविधान के संशोधित अनुच्छेद 124, 217 और 222 में संवैधानिक संशोधन किए और इसे दोनों सदनों से सर्वसम्मति से स्वीकृति भी मिल गई। इसको सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती गई। तब पांच न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला दिया कि इस मामले को बड़ी पीठ को भेजने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि पहले ही काफी समय बीत चुका है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान की मूल संरचना है। चूंकि नौ न्यायाधीशों की पीठ पहले यह कह चुकी है कि परामर्श का मतलब सहमति है और वह बाध्यकारी है। इसलिए न्यायिक प्रधानता का सम्मान होना चाहिए। इसलिए संसद का अधिनियम रद्द किया जाता है।
सुपात्र की उपेक्षा
न्यायपालिका ‘अंकल जज सिंड्रोम’ से ग्रस्त रही है। किसी न किसी कारण सुपात्र लोगों की उपेक्षा होती रही। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग ( एनजेएसी अधिनियम ) ने भी कॉलेजियम प्रणाली में कुछ कमियों को उजागर किया था। इसके बाद 16 अक्तूबर, 2015 को सर्वोच्च न्यायालय ने एनजेएसी अधिनियम को रद्द कर दिया था।
आंतरिक जांच-पड़ताल
न्यायमूर्ति वर्मा के मामले में यह समझना मुश्किल है कि इस मामले पर आंतरिक जांच-पड़ताल में कौन-सा तरीका अपनाया जाएगा। उन्होंने तो नोटों के अस्तित्व से ही इनकार कर दिया है। एक कुशल जांच एजेंसी की अनुपस्थिति में आंतरिक जांच किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी, यह कहना मुश्किल है। इसका एक मात्र उपाय है कि एफआईआर दर्ज हो और तीन सदस्यीय समिति की निगरानी में एक केंद्रीय एजेंसी इस मामले की जांच करे।
क्या था घटनाक्रम
- 14 मार्च, 2025, रात्रि 11:30 बजे: दिल्ली में न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आधिकारिक आवास के स्टोररूम में आग लगी
- 15 मार्च, 2025, अपराह्न 4:50 बजे: दिल्ली पुलिस आयुक्त ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय को घटना की सूचना दी
- 16 मार्च, 2025: मुख्य न्यायाधीश उपाध्याय ने नई दिल्ली लौटकर मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना से मुलाकात की और उनके निर्देश पर न्यायमूर्ति वर्मा से संपर्क किया
- 17 मार्च, 2025, प्रातः 8:30 बजे: दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने न्यायमूर्ति वर्मा से दिल्ली उच्च न्यायालय गेस्ट हाउस में मुलाकात की, जहां न्यायमूर्ति वर्मा ने स्टोररूम को सभी के लिए खुला बताया और इसे अपने खिलाफ साजिश की आशंका जताई
- 22 मार्च, 2025: मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया
- 24 मार्च, 2025: दिल्ली उच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति वर्मा से न्यायिक कार्य वापस ले लिया
- 28 मार्च, 2025: केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति वर्मा के इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरण को मंजूरी दी
- 5 अप्रैल, 2025: न्यायमूर्ति वर्मा ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली, लेकिन उन्हें तत्काल न्यायिक कार्य नहीं सौंपा गया
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग ( एनजेएसी ) और कॉलेजियम प्रणाली
कॉलेजियम प्रणाली एनजेएसी
यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विकसित एक प्रणाली हैें यह संसद द्वारा पारित एक वैधानिक निकाय था, जिसमें जजों के जिसमें जज ही जजों की नियुक्ति और तबादला करते हैं। अलावा कार्यपालिका और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि शामिल होते थे।
सदस्य मुख्य न्यायाधीश + 4 वरिष्ठतम जज मुख्य न्यायाधीश + 2 वरिष्ठ न्यायाधीश (सर्वोच्च न्यायालय), मुख्य न्यायाधीश + 2 + कानून मंत्री + 2 ‘प्रमुख व्यक्ति’
वरिष्ठतम जज (उच्च न्यायालय) नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी तरह से जजों के हाथ में न्यायपालिका + कार्यपालिका + सिविल सोसाइटी का मिश्रित नियंत्रण
पारदर्शिता निर्णय सार्वजनिक नहीं होते, प्रक्रिया गोपनीय अपेक्षाकृत अधिक पारदर्शिता होने का दावा किया गया था
जवाबदेही किसी बाहरी संस्था को जवाबदेह नहीं संसद और जनता के प्रति आंशिक रूप से जवाबदेह
सुझाव
- एक स्वतंत्र न्यायिक आयोग की स्थापना (एनजेएसी पर फिर से विचार किया जाए)।
- न्यायिक नैतिकता की वैधानिक संहिता तैयार कर न्यायिक आचार संहिता का कार्यान्वयन हो।
- न्यायाधीशों के लिए सार्वजनिक संपत्ति और आय की घोषणा करना अनिवार्य हो।
- जीवनसाथी और परिवार के आश्रित सदस्यों सहित चल और अचल संपत्ति की वार्षिक घोषणा हो।
- सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद कोई नया पदभार लेने पर रोक हो।
- न्यायपालिका में विविध वर्गों और समुदायों के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा मिले।
स्वतंत्रता भी जरूरी
न्यायपालिका की स्वतंत्रता न केवल उच्चतर न्यायालयों में महत्वपूर्ण है, बल्कि निचली अदालतों के स्तर पर भी यह लागू होती है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हर संवैधानिक न्यायालय अपने आप में एक स्वतंत्र निकाय है, वह किसी अन्य न्यायालय के अधीन नहीं।

















टिप्पणियाँ