भारत की सांस्कृतिक पहचान विक्रम संवत् के साथ जुड़ी है। भारत के सांस्कृतिक पर्व-त्योहार तथा राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, गुरु नानक आदि महापुरुषों की जयंती भी इसी भारतीय काल गणना के हिसाब से मनाई जाती है। विक्रम संवत् विश्व का सबसे प्रामाणिक और वैज्ञानिक संवत्सर है। इस वर्ष से विक्रम संवत् 2082 शुरू होगा। इस वर्ष का नाम सिद्धार्थी संवत्सर है। हिंदू नववर्ष 2025 के राजा और मंत्री दोनों सूर्य हैं। जिस दिन से हिंदू नववर्ष शुरू होता है, उस दिन के स्वामी को राजा माना जाता है।

अध्यक्ष, आम्बेडकर पीठ, एचपीयू, शिमला
महान सम्राट विक्रमादित्य के शासनकाल को भारतीय इतिहास में स्वर्णिम युग के रूप में जाना जाता है। विक्रमादित्य ऐसे समय सिंहासनारूढ़ हुए, जब देश में न केवल शकों का प्रभुत्व बढ़ रहा था, बल्कि पश्चिमी क्षेत्र में भी विभिन्न आक्रमणकारियों का दबदबा था। शकों ने भारत के पश्चिमी और मध्य क्षेत्रों में अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी, जिसका भारतीय संस्कृति और राजनीति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। उज्जयिनी के सम्राट विक्रमादित्य ने न केवल शकों को खदेड़ा, बल्कि देश में शांति स्थापित करने के साथ-साथ उनके प्रभाव वाले क्षेत्रों को फिर से अपने साम्राज्य में शामिल किया।
‘विक्रम संहिता’, कल्पलता, नरसिंह पुराण और अन्य ऐतिहासिक स्रोतों में विक्रमादित्य की वीरता, महानता, न्यायप्रियता और उनके युद्ध कौशल का वर्णन है। शकों पर विजय के बाद उन्होंने ईसा पूर्व सन् 57 में भारतीय उपमहाद्वीप में ‘विक्रम संवत्’ नाम से एक नए युग की शुरुआत की थी, जो भारतीय कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण अंग है। प्रख्यात प्राचीन भारतीय गणितज्ञ वराह मिहिर लिखित विक्रम संहिता खगोलशास्त्र और राजनीति पर आधारित है। इसके अलावा, कल्हण की ‘राजतरंगिणी’ में भी विक्रमादित्य की समकालीन घटनाओं और शकों के प्रभाव का उल्लेख है। शक धर्म, संस्कृति और प्रशासनिक परंपराओं के लिए खतरा बने हुए थे। शकों के खात्मे के बाद विक्रमादित्य ने न सिर्फ अपने साम्राज्य को सुदृढ़ किया, बल्कि उनके कार्यकाल में संस्कृति, विज्ञान और कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य हुए।
चैत्र में ही नव वर्ष क्यों
चैत्र मास नववर्ष मनाने के लिए सर्वोत्तम है, क्योंकि इस समय संपूर्ण धरा फूलों से सुवासित होती है और पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं। हर तरफ हरीतिमा होती है, मानो प्रकृति कोई उत्सव मना रही हो। इस माह में सर्दी की विदाई और ग्रीष्म का आगमन होता है। यह समय हर तरह के वस्त्रों के लिए उपयुक्त होता है। नया पंचांग चैत्र माह में ही आता है, जिसके आधार पर प्रत्येक भारतीय पर्व-त्योहार, विवाह और अन्य शुभ मुहुर्त निकाले जाते हैं। फसल की कटाई भी इसी समय होती है और घरों में नया अनाज आता है। व्यापारी लोग भी मार्च महीने में आर्थिक गतिविधियां पूरी कर अप्रैल से नयी खाता-बही शुरू करते हैं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से वासंती नवरात्र आरंभ होता है, इसलिए नवरात्र से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। हेमाद्रि के ब्रह्म पुराण के अनुसार, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा ने पृथ्वी का निर्माण चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी नवरात्र के पहले दिन किया था। हिंदू पंचांग के अनुसार, हर वर्ष चैत्र के पहले दिन यानी नवरात्र से ही हिंदू नव वर्ष शुरू होता है। 12 महीने का एक वर्ष और 7 दिन का एक सप्ताह रखने का चलन विक्रम संवत् से ही शुरू हुआ। इसमें महीने की गणना सूर्य और चंद्र की गति के आधार पर होती है। इसमें मौजूद 12 राशियां वास्तव में 12 सौर मास होती हैं।
पूर्णिमा को चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है, उसी आधार पर इन महीनों के नाम रखे गए हैं। दरअसल, सौर वर्ष से चंद्र वर्ष 11 दिन 3 घटी 48 पल छोटा होता है, इसलिए प्रत्येक 3 वर्ष में इसमें 1 अतिरिक्त माह (अधिमास) जोड़ दिया जाता है, ताकि दोनों के बीच का अंतर समायोजित हो सके। विक्रम संवत् में वर्ष सौर (365 दिन) और माह चंद्र (लगभग 29.5 दिन) दोनों पर आधारित होते हैं। जिस दिन नव संवत् का आरंभ होता है, उस दिन के वार के अनुसार वर्ष के राजा का निर्धारण होता है। आरंभिक शिलालेखों में ये वर्ष ‘कृत’ के नाम से आए हैं। जब सूर्य नई राशि में प्रवेश करते हैं, तो उस दिन को संक्रांति कहा जाता है। 8वीं एवं 9वीं सदी से विक्रम संवत् नाम विशिष्ट रूप से मिलता है। संस्कृत ज्योतिष ग्रंथों के अनुसार, शक संवत् से भिन्न दिखाने के लिए सामान्यतया ‘संवत्’ का प्रयोग किया गया है। नेपाल में विक्रम संवत् ही सरकारी कैलेंडर के रूप में मान्य है।
‘विक्रम संवत्’ के उद्भव एवं प्रयोग को लेकर विद्वानों में मतभेद हैं। कुछ का मानना है कि विक्रमादित्य ने ईसा पूर्व सन् 57 में इसका प्रचलन शुरू किया, जबकि कुछ विद्वान ईस्वी सन् 78 और कुछ ईस्वी सन् 544 से इसकी शुरुआत मानते हैं। फारसी ग्रंथ ‘कलितौ दिमन:’ में पंचतंत्र के एक पद्य में ‘शशिदिवाकरयोर्ग्रहपीडनम्’ अर्थात् सूर्य और चंद्रमा के ग्रहण की ज्योतिषीय घटना का उल्लेख है। विद्वानों ने ‘कृत संवत्’ को ‘विक्रम संवत्’ का पूर्ववर्ती माना है। लेकिन ‘कृत’ शब्द के प्रयोग की संतोषजनक व्याख्या नहीं मिलती। कुछ शिलालेखों में मालवगण का संवत् उल्लिखित है, जैसे- नरवर्मा का मन्दसौर शिलालेख। ‘कृत’ एवं ‘मालव’ संवत् एक ही कहे गए हैं, क्योंकि दोनों पूर्वी राजस्थान एवं पश्चिमी मालवा में प्रयोग में लाए गए हैं। इस तरह, कृत के 282 और 295 वर्ष तो मिलते हैं, लेकिन मालव संवत् के इतने प्राचीन शिलालेख नहीं मिलते। संभव है कि कृत पुराना नाम हो और जब मालवों ने इसे अपनाया तो उसे ‘मालव-गणाम्नात’ या ‘मालव-गण-स्थिति’ के नाम से पुकारा जाने लगा हो। यदि ‘कृत’ और ‘मालव’, दोनों बाद में आने वाले विक्रम संवत् की ओर ही संकेत करते हैं, तो दोनों एक साथ लगभग 100 वर्ष तक प्रयोग में आते रहे, क्योंकि 480 कृत वर्ष और 461 मालव वर्ष मिलते हैं।
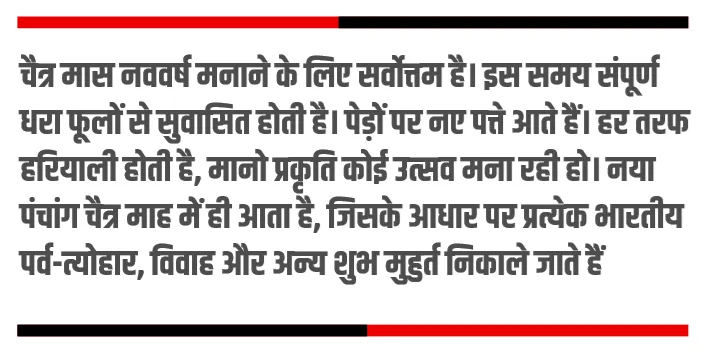
नवसंवत्सर का महत्व
ईश्वर ने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन सूर्योदय के साथ सृष्टि का प्रारंभ किया था, तभी से यह गणना चली आ रही है। यह नववर्ष किसी जाति, वर्ग, देश, संप्रदाय का नहीं, अपितु मानव मात्र का नववर्ष है। नववर्ष को नवसंवत्सर या संवत्सरेष्टि भी कहते हैं। इस समय सूर्य मेष राशि से गुजरते हैं, इसलिए इसे मेष संक्रांति भी कहा जाता है। चैत्र प्रतिपदा नवरात्र पर शक्ति की आराधना और साधना की जाती है। इसमें मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा होती है। नवमी तिथि पर भगवान राम का जन्मोत्सव और चैत्र पूर्णिमा पर श्रीराम के सबसे प्रिय भक्त हनुमान की जयंती मनाई जाती है। शास्त्रों के अनुसार, सभी चारों युगों में सबसे पहले सतयुग का प्रारंभ इसी तिथि यानी चैत्र प्रतिपदा से हुआ था। यह तिथि सृष्टि के कालचक्र का प्रारंभ और पहला दिन भी मानी जाती है। नववर्ष विशुद्ध रूप से भौगोलिक पर्व है, क्योंकि प्राकृतिक दृष्टि से भी वृक्ष, वनस्पति, फूल-पत्तियों में भी नयापन दिखाई देता है। वृक्षों में नई-नई कोपलें आती हैं। वसंत ऋतु का वर्चस्व और प्रभाव चारों ओर दिखाई देता है। मनुष्य के शरीर में नया रक्त बनता है। हर जगह परिवर्तन एवं वनत्व दिखाई पड़ता है। इस समय नक्षत्र शुभ स्थिति में होते हैं, इसलिए कोई भी नया कार्य शुरू करने के लिए यह समय अत्यन्त शुभ होता है। चैत्र माह के मध्य में प्रकृति अपने शृंगार एवं सृजन की प्रक्रिया में लीन रहती है और पेड़ों पर नए-नए पत्ते आने के साथ ही सफेद, लाल, गुलाबी, पीले, नारंगी, नीले रंग के फूल भी खिलने लगते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे पूरी सृष्टि ही नई हो गई है।
- चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही परमात्मा ने चार ऋषियों अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा को क्रमश: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के रूप में समस्त ज्ञान-विज्ञान का संदेश दिया था। इस कारण इसे वेद संवत् भी कहते हैं।
- इसी दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम ने लंका पर विजय विजय प्राप्त कर वैदिक धर्म की ध्वजा फहराई थी।
- इसी दिन से कली संवत् तथा भारतीय विक्रम संवत् युधिष्ठिर संवत् प्रारंभ होता है।
- चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी।
- इसी दिन संसार के समस्त सनातन धर्म अनुयायियों का दैविक बल जगाने के लिए धर्मराज्यम् की स्थापना की गई थी।
- वसंत ऋ तु का आरंभ भी वर्ष प्रतिपदा से ही होता है।
संपूर्ण भारत में वर्ष प्रतिपदा उत्सव बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अधिकृत तौर पर 6 उत्सव मनाता है। इनमें प्रतिपदा साल का पहला उत्सव है, जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। इसके अलावा, अन्य उत्सव हैं- हिंदू साम्राज्य दिवस, गुरु पूर्णिमा, रक्षाबंधन, विजयदशमी और मकर संक्रांति। हिंदू समाज आदिकाल से इन त्योहारों को मनाता आ रहा है। संघ ने इन्हें मनाना इसलिए शुरू किया ताकि लोग जागरूक होकर राष्ट्रीयता की भावना को अपने अंदर आत्मसात करें।
नाम अलग, भाव एक

नववर्ष विभिन्न प्रांतों में अलग-अलग तरीके से मनाया जाता है। इसे उगादी, चेटी चंड, बिहू, गुड़ी पड़वा आदि विभिन्न नामों से जाना जाता है-
चेटी चंड – सिंधी समाज चैत्र शुक्ल द्वितीय को ‘चेटी चंड’ के रूप में नववर्ष मनाता है। यह त्योहार जल देवता वरुण का अवतार माने जाने वाले स्वामी झूलेलाल की जयंती और समुद्र पूजा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सिंधी समुदाय शोभायात्राएं निकालते हैं और मीठे चावल, छोले और शरबत का प्रसाद बांटते हैं। इस अवसर पर मिट्टी के दीये में गेहूं को तेज के प्रतीक के रूप में डालकर जलाया जाता है, जिसे ‘अक्षय तेल’ कहा जाता है। यह ज्ञान और पवित्रता का प्रतीक है। यह दीपक, गेहूं के मोदक, फल, फूल और पवित्र प्रसाद के साथ ज्योत जगाने की रस्म का मुख्य हिस्सा है।
बिहू – असम में बिहू तीन बार मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है। इसमें बोहाग बिहू (असम का नववर्ष), माघ बिहू (फसलों की कटाई) और काटी बिहू (अनाज काटना और बांधना) शामिल हैं। बोहाग बिहू असम का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है, जो सात दिन तक चलता है। यह वसंत ऋतु के आगमन और नए वर्ष के प्रारंभ में मनाया जाता है। बोहाग बिहू असम की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक है। बिहू का पहला उल्लेख लखीमपुर जिले के घिलामारा क्षेत्र में 1935 में मिले चुटिया राजा लक्ष्मीनारायण के ताम्रपत्र शिलालेख में मिलता है। यह शिलालेख 1401 ई. का है।
गुड़ी पड़वा – महाराष्ट्र में चैत्र माह का पहला दिन गुड़ी पड़वा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन मराठी समुदाय के लोग अपने घरों के बाहर समृद्धि के प्रतीक गुड़ी लगाते हैं। महिलाएं गुड़ी से घर सजाती हैं। गुड़ी के लिए बांस की छड़ी तैयार कर उसके ऊपर चांदी, तांबा या पीतल का बर्तन उल्टा रखा जाता है। इसके बाद भगवा कपड़े, नीम या आम के पत्तों और फूलों से सजाकर इसे घर में सबसे ऊंचे स्थान पर लगाया जाता है। माना जाता है कि इससे पूरे साल खुशियां, सफलता और समृद्धि आती है। गुड़ी का मतलब है ध्वज यानी झंडा, जबकि प्रतिपदा तिथि को पड़वा कहा जाता है।
यह रबी फसल की कटाई का प्रतीक है। गुड़ी पड़वा छत्रपति शिवाजी महाराज की विजय के रूप में मनाया जाता है। इस पर्व पर लोग नीम के पत्ते खाते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से खून साफ होता है और रोगों से मुक्ति मिलती है। गुड़ी पड़वा पर विशेष रूप से सूर्य की पूजा की जाती है। इसके अलावा, लोग रंगीन रंगोली भी बनाते हैं और प्रसाद के रूप में पूरन पोली और श्रीखंड जैसे विशेष व्यंजन तैयार करते हैं।
पोहेला बोइशाख – पश्चिम बंगाल में नववर्ष पोहेला बोइशाख के रूप में मनाते हैं। इस शुभ दिन कई अनूठी परंपराएं, अनुष्ठान और गतिविधियां होती हैं, जो बंगाल की जीवंत और विविध संस्कृति को दर्शाती हैं। यह कृषि के समय के आगमन का प्रतिनिधित्व करता है। इस समय किसान खेतों में जुताई और बुआई शुरू करते हैं। सदियों से पोहेला बैसाख बंगाल में एक लोकप्रिय सांस्कृतिक उत्सव के रूप में विकसित हुआ है। इस दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं, मंदिर जाते हैं या सांस्कृतिक कार्यक्रमों और मेलों का हिस्सा बनते हैं। पोहेला बैशाख एक उत्सव से बढ़कर बंगाली संस्कृति, परंपरा और बंगालियों की विरासत का प्रतिनिधित्व करने वाला उत्सव है।
बैसाखी – पंजाब में नववर्ष बैसाखी के रूप में 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन सिख समुदाय के लोग पारंपरिक वस्त्र पहनते हैं और भांगड़ा करते हैं। साथ ही, घी व आटे से बना प्रसाद ग्रहण करते हैं। कई जगह पर फसल भी काटी जाती है और गुरुओं की आराधना भी की जाती है। वैसाखी का उत्सव गुरुपर्व की तरह ही मनाया जाता है। इस दिन गुरुद्वारों को सजाया जाता है और पूरे दिन झांकी, नृत्य और गायन चलता है। दसवें गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1699 में सिखों को सैनिकों के परिवार में परिवर्तित करने के लिए बैसाखी का दिन चुना था, जिसे खालसा पंथ के रूप में जाना जाता है।
जूड शीतल – इसे मैथिली नव वर्ष के नाम से भी जाना जाता है। इसे बिहार, झारखंड और नेपाल में मैथिली लोग मनाते हैं। मैथिली नव वर्ष आमतौर पर ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 14 अप्रैल को मनाया जाता है।
उगादि – उगादी या युगादी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक का नववर्ष उत्सव है। यह इन क्षेत्रों में हिंदू चंद्र-सौर कैलेंडर माह चैत्र के पहले दिन मनाते हैं। पारंपरिक मिठाइयां और कच्चे आम और नीम के पत्तों से बनी ‘पचड़ी’ (मीठा सिरप) भोजन के साथ परोसी जाती है।
विशु – यह मलयालम माह ‘मेदम’ की पहली तिथि को फसल की बुआई के प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और उनके अवतार कृष्ण की पूजा करने की परंपरा है। शुभता के प्रतीक के रूप में भगवान की मूर्ति को विशुकनी के साथ रखा जाता है। यह रोशनी और आतिशबाजी से भरा त्योहार है। दिन की शुरुआत फल-सब्जियों और मौसमी फूलों को शीशे के सामने सजाकर की जाती है। इस व्यवस्था को विशु कानी कहा जाता है।
मागे परब – यह ‘हो’ जनजाति का नववर्ष का पहला और सबसे बड़ा त्योहार है। यह फसल कटाई और खेत-खलिहान का काम पूरा होने के बाद माघ महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। मागे परब के दौरान सभी देवी-देवताओं के नाम नई फसल से बनी हंड़िया जमीन में डालकर खुशहाली और समृद्धि की कामना की जाती है। यह पर्व 6 दिन तक मनाया जाता है। मुख्य पर्व छठे दिन होता है।
नवरेह – यह कश्मीरी हिंदुओं के नववर्ष के पहले दिन का उत्सव है। कश्मीरी हिंदू नवरेह त्योहार को अपनी देवी शारिका, देवी दुर्गा या शक्ति के एक रूप को समर्पित करते हैं।
पुताण्डु – इसे पुथुरुषम या तमिल नववर्ष भी कहा जाता है। तमिल तारीख को तमिल माह चिधिराई के पहले दिन के रूप में लन्नीसरोल हिंदू कैलेंडर के सौर चक्र के साथ स्थापित किया गया है। इसलिए यह हर साल ग्रेगोरियन कैलेंडर के 14 अप्रैल या उसके आसपास ही मनाया जाता है। इस दिन तमिल भाषी ‘पुट्टू वतुत्काका!’ कहकर एक-दूसरे को बधाई देते हैं। इस दिन लोग अपने घर-द्वार की सफाई करते हैं और परिवार के साथ समय बिताते हैं। वे एक थाली भी सजाते हैं, जिसमे फल, फूल और अन्य शुभ वस्तुएं रखी जाती हैं। पुत्ताण्डु तमिलनाडु और पुद्दुचेरी के बाहर रहने वाले तमिल हिंदुओं के द्वारा भी मनाया जाता है। इनमें श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर, रीयूनियन, मॉरीशस और अन्य देशों में भी जहां तमिल भाषी रहते हैं। इस दिन चावल की खीर का भोग लगाने का विशेष महत्व माना गया है। इसी खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है।

















टिप्पणियाँ