जिस आम आदमी पार्टी का जन्म भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से हुआ था, वह खुद भ्रष्टाचार के कई मामलों का सामना कर रही है। विशेष बात यह कि इस सब पर भी शर्मिंदगी की जगह पार्टी हेकड़ी की मुद्रा में है। संभवत: यही अकड़ और दुस्साहस अब दिल्ली को खलने लगा है। विधानसभा चुनाव की ऊंची उठती लहरों के बीच जब ‘पाञ्चजन्य’ ने अलग-अलग बस्तियों और मोहल्लों में लोगों से बात की, समस्याओं का सर्वेक्षण किया और विशेषज्ञों से संवाद की शृंखला आरंभ की, तो लगा दुख में डूबी दिल्ली अब ‘विश्वासघाती राजनीति’ की नैया डुबोने वाली है। राजधानी की सबसे बड़ी टीस यह है कि 2015 में अरविंद केजरीवाल ने यहां की जनता से कई वायदे किए थे, जिन्हें पूरा करने की बजाय वह मुद्दा बदलते या कन्नी काटते रहे। इसे लेकर जनता में नाराजगी, पार्टी में आंतरिक कलह, खेमेबाजी और गिरती लोकप्रियता से तो यही लगता है कि बदलाव की जिस लहर पर वे सवार होकर आए थे, वह खुमार अब उतार पर है।
अरविंद केजरीवाल के सत्ता में आने से लोकतांत्रिक क्रिया में शुचिता और संवाद का आग्रह रखने वाले और राजनीतिक परंपराओं के जानकार यह मानते हैं कि बीते दशक में दिल्ली से उठे ‘पारदर्शिता के छलावे’ का जो गुबार उठा, उससे लोकतंत्र को भारी आघात पहुंचा है। बिना तथ्यों के किसी पर भी कीचड़ उछालने और खुद को सबसे आला और भोला दिखाने-बताने की इस राजनीति में कोरे दावे, भ्रम खड़ा करने वाले तंत्र का पोषण और संवेदनशीलता की आड़ में निर्मम होते जाने के जटिल सूत्र हैं। इसलिए आश्चर्य नहीं कि आने वाले समय में देश को इस राजनीति का अलग ही उथलापन देखने को मिले। निश्चित ही लोकतंत्र को पहुंचे इस आघात का उपचार लंबा चलेगा।
दिल्ली जिस दलदल में फंसी है (पढ़ें पेज-10 से 36 तक विभिन्न रिपोर्ट) वह छल की राजनीति के बेजा प्रयोगों, बेशर्मी व इनके बेपर्दा होने की तथ्यात्मक गाथाएं हैं। किन्तु इस राजनीति से लोकतंत्र को जो ठेस पहुंची है, उससे यह आवश्यकता एक बार फिर रेखांकित हो गई है कि इस देश को संविधान के माध्यम से मिली शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए कुछ लोग इस देश के लोकतंत्र और व्यवस्था में ही सेंध लगा सकते हैं और पूरी व्यवस्था को जर्जर कर बैठा सकते हैं। तो बात इस लोकतंत्र और इसे स्वस्थ रखने वाली प्रक्रिया, यानी लोकमत परिष्कार की।
लोकतंत्र का अर्थ और परिष्कार के पहलू
‘जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए’ शासन यानी लोकतंत्र केवल एक शासन प्रणाली नहीं, बल्कि एक जीवंत और विकसित होती प्रणाली है। समाज के बदलते स्वरूप, मूल्यों और चुनौतियों के अनुसार इसे परिष्कृत करना जरूरी होता है। लोकतंत्र का परिष्कार न केवल न्याय और समानता सुनिश्चित करता है, बल्कि यह मानवता के विकास के लिए भी अनिवार्य है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह समाज की बदलती जरूरतों के साथ कैसे तालमेल बैठाती है। सरकारें आती हैं और जाती हैं, लेकिन समाज स्थिर रहता है। इसलिए यह सुनिश्चित करना कि लोकतंत्र समाज के सरोकारों को समझे और उनके अनुसार ढले, आवश्यक है। नई तकनीक, जैसे कृत्रिम बुद्धिमता और डिजिटल मीडिया हमारे कार्य करने के तरीकों को बदल रही है। हमें अपनी पहचान खोए बिना संतुलन बनाए रखकर आगे बढ़ना होगा।
लोकतंत्र तभी सशक्त होता है, जब उसमें नागरिकों की सक्रिय भागीदारी हो। जैसे-जैसे समाज जटिल होता जा रहा है, लोकतंत्र को नई जनभागीदारी प्रक्रियाओं की आवश्यकता महसूस हो रही है। यह प्रक्रिया नागरिकों को न केवल सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों में शामिल करती है, बल्कि उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी सक्रिय भागीदार बनाती है। महात्मा गांधी का मानना था कि लोकतंत्र केवल राजनीतिक प्रक्रिया नहीं है, इसमें नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार, एक सच्चे लोकतंत्र में सभी नागरिकों को समान अवसर व अपनी आवाज उठाने का अधिकार होना चाहिए। जब तक समाज के कमजोर वर्गों को न्याय नहीं मिलता, तब तक लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं है। गेब्रियल आलमंड और सिडनी वर्बा (The Civic Culture)का भी यही कहना है कि जन भागीदारी लोकतंत्र को मजबूती देती है।
जवाबदेही और पादर्शिता
इसी तरह, जवाबदेही और पारदर्शिता भी जरूरी है, ताकि लोकतंत्र में जनता का भरोसा बना रहे। इससे न केवल लोकतंत्र मजबूत होता है, बल्कि सामाजिक न्याय और समानता को भी बढ़ावा मिलता है। निर्णय और प्रक्रियाएं खुली एवं स्पष्ट हों, ताकि लोग समझ सकें कि उनके साथ क्या हो रहा है। जब लोगों को लगता है कि कार्यों का मूल्यांकन किया जाएगा, तो वे अधिक जिम्मेदारी से कार्य करते हैं। मतलब, लोकतंत्र की शक्ति उसकी आत्म-सुधार की क्षमता में है। गेटे के अनुसार, सर्वोत्तम शासन वही है जो आत्मशासन की शिक्षा दे। थोरो ने भी कहा था कि जो सबसे कम शासन करे, वही सबसे उत्तम सरकार है। महात्मा गांधी के विचार पश्चिम के इन दर्शनशास्त्रियों से मेल खाते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी की कथनी और करनी में न केवल अंतर है, बल्कि उसमें नैतिकता का भी अभाव दिखता है। इसके अलावा, न तो पार्टी में पारदर्शिता है, न सरकार के कामकाज में। इसलिए सामाजिक कार्यकर्ता अण्णा हजारे ने अरविंद केजरीवाल को सलाह दी है, ‘‘वे उन दिनों को याद रखें, जब मैंने उन्हें सीख दी थी कि अचार विचार को शुद्ध रखकर ही हम देश और समाज की भलाई के लिए काम कर सकते हैं।’’
निगरानी और संतुलन
लोकतांत्रिक व्यवस्था में निगरानी और संतुलन भी आवश्यवक है। अगर निगरानी और संतुलन का तंत्र कमजोर हो जाए, तो सत्तावाद का खतरा बढ़ सकता है। सत्तावाद वह राजनीतिक प्रणाली है, जिसमें सत्ता का केंद्रीकरण होता है और नागरिकों के अधिकारों को सीमित किया जाता है। इसीलिए पं. दीनदयाल उपाध्याय ने स्वस्थ लोकतंत्र के लिए लोकमत के परिष्कार की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यदि लोकमत परिष्कृत नहीं होगा, तो लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। लोकतंत्र के परिष्करण से यह सुनिश्चित होता है कि सत्ता का दुरुपयोग न हो और नागरिक स्वतंत्रताएं सुरक्षित रहें। लेकिन क्या आर्थिक समानता के बिना यह संभव होगा? नहीं, क्योंकि आर्थिक असमानता न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर कर सकती है, बल्कि सामाजिक तनाव बढ़ाने के साथ-साथ विकास की गति को भी बाधित कर सकती है। आर्थिक समानता सुनिश्चित करती है कि सभी नागरिकों को समान अवसर मिले, चाहे उनकी सामाजिक स्थिति, जाति या लिंग कुछ भी हो। कल्याणकारी योजनाएं और कर सुधार लोकतंत्र को मजबूत और समावेशी बनाते हैं। इसके उलट आआपा ‘रेवड़ी कल्चर’ को बढ़ावा देती है, जो राज्य ही नहीं, अपितु देश पर भी आर्थिक बोझ डालती हैं। आआपा सरकार की योजनाएं भी समाज में भेदभाव बढ़ाने वाली हैं।
वैसे भी, सामाजिक न्याय और और समानता किसी भी समाज की नींव होती है। जाति, पंथ, लिंग व वर्ग जैसे भेदभाव लोकतंत्र की नींव को कमजोर करते हैं। सामाजिक न्याय बिना किसी भेदभाव सभी को समान अवसर और अधिकार मिलना सुनिश्चित करता है। यही कारण था कि राम मनोहर लोहिया ने जाति, वर्ग और पंथ के आधार पर विभाजन के खिलाफ आवाज उठाई। उनका मानना था कि लोकतंत्र में सभी वर्गों की भागीदारी होनी चाहिए। उनकी सप्त क्रांति की अवधारणा में आर्थिक समानता, जाति उन्मूलन, महिलाओं की मुक्ति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता शामिल थी। उनका मानना था कि समाज में समानता और न्याय स्थापित करने के लिए समतावादी दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। लेकिन दिल्ली में ऐसा नजर नहीं आ रहा है। यहां पर केजरीवाल सरकार तुष्टीकरण की राजनीति करते नजर आती है।
लोकतंत्र की चुनौतियां
आज जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, महामारी और वैश्वीकरण जैसे मुद्दे लोकतंत्र के समक्ष नई चुनौतियां पेश कर रहे हैं। ये ऐसे वैश्विक मुद्दे हैं, जिनसे अकेले कोई राष्ट्र नहीं निपट सकता। वैश्विक चुनौतियों का समाधान केवल सामूहिक प्रयासों से ही संभव है। फरीद जकरिया अपनी पुस्तक The Future of Freedom में लिखते हैं कि लोकतंत्र को वैश्विक स्तर पर सहयोग के लिए तैयार रहना चाहिए। यह परिष्करण लोकतंत्र को इन समस्याओं का समाधान खोजने में सक्षम बनाता है। कोविड-19 महामारी ने दुनिया को यह दिखा दिया कि विकसित हों या विकासशील देश, सभी को अपनी स्वास्थ्य प्रणाली मजबूत करने व टीकों का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है। कोविड के दौरान जब सारे राज्यों की सरकारें केंद्र के साथ मिल—जुलकर काम करने में जुटी थीं, तब दिल्ली के अस्पतालों में लोगों को सही से उपचार भी नहीं मिल रहा था। अरविंद केजरीवाल तब केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ रहे थे, जबकि केंद्र की तरफ से हर संभव सहायता दिल्ली को दी जा रही थी।
जन भागीदारी और नवाचार
लोकतंत्र का खुलापन विचारों की स्वतंत्रता, बहस और विविधता को बढ़ावा देता है। लोकतंत्र में नवाचार का स्थान भी महत्वपूर्ण है। ई-गवर्नेंस, सहभागी बजट और सीधी जनभागीदारी जैसे प्रयास लोकतंत्र को आधुनिक और प्रासंगिक बनाते हैं। लोकतांत्रिक समाज में विचारों का आदान-प्रदान होता है, जिससे प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है और नवाचार के लिए उर्वरक भूमि तैयार होती है।
अगर नवाचार किसी भी समाज की प्रगति और विकास का महत्वपूर्ण स्तंभ है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र की रीढ़ है। यह स्वतंत्रता सामाजिक विकास में भी सहायक है। संविधान का अनुच्छेद 19(1)(ए) सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, लेकिन आज फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा के कारण यह खतरे में है। स्वतंत्रता को सुरक्षित रखते हुए गलत सूचना पर नियंत्रण करना परिष्करण का एक प्रमुख कदम है। इसलिए बुद्धिजीवियों और मीडियाकर्मियों की जिम्मेदारी है कि वे सच्चाई को उजागर करें और झूठ के खिलाफ खड़े हों। यह केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा नहीं करता, बल्कि लोकतंत्र के लिए भी आवश्यक है।
लोकतंत्र केवल वर्तमान की समस्याओं का समाधान नहीं करता, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी नीतियां बनाता है। यह विचार हमें इस बात पर सोचने के लिए प्रेरित करता है कि हम आज जो निर्णय लेते हैं, उनका प्रभाव आने वाली पीढ़ियों पर कैसा पड़ेगा। A Theory of Justice में जॉन रॉल्स ने ‘अज्ञान का पर्दा’ (Veil of Ignorance) के सिद्धांत के माध्यम से निष्पक्ष नीति निर्माण पर जोर दिया है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक ऐसा वातावरण तैयार करें, जहां नई पीढ़ी अपनी क्षमताओं को पूरी तरह से विकसित कर सके। केवल तभी हम एक समृद्ध और स्थायी भविष्य की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं।


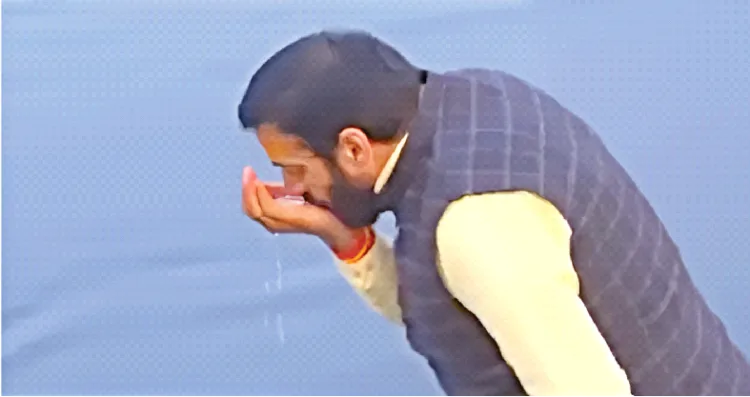














टिप्पणियाँ