प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत लोकसभा चुनाव के दौरान कहा था कि उनके तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा। पिछले छह महीनों में सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए हैं, जिनके दीर्घकालिक परिणाम होंगे, लेकिन 19 दिसंबर को संसद में प्रस्तुत ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ विधेयक से निश्चय ही इस नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। यह सही है कि लोकतंत्र एक महान शासन प्रणाली है, लेकिन यह भी सत्य है कि यह एक अत्यधिक महंगी प्रणाली है। यह सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए प्रत्येक स्तर पर अनुशासन की मांग करती है।
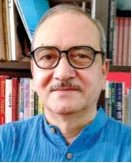
अनुशासन न रहने पर यह और भी महंगी और कभी-कभी उच्छृंखल भी हो जाती है, जिसका खामियाजा हरेक नागरिक को भुगतना पड़ता है। फिर एक समय ऐसा भी आता है, जब लोकतंत्र पर से लोगों का भरोसा ही उठने लगता है। इसलिए समय-समय पर इसके शोधन की जरूरत पड़ती है, ताकि उसमें आ गई विकृतियां दूर हो सकें। आजादी के इस अमृत काल में हमें देखना है कि हम कैसे अपने लोकतंत्र को बचाए रख सकते हैं। पिछले 77 वर्ष में अनेक मौके ऐसे आए हैं, जब हमारे लोकतंत्र की नैया डगमगाती नजर आई है। उसके मूल कारणों की पहचान करके उन्हें दुरुस्त करने की कवायद का पहला कदम है- एक राष्ट्र, एक चुनाव।


आज अमेरिका में 244 वर्ष से लोकतंत्र फल-फूल रहा है तो इसका एक ही कारण है कि वहां के लोगों ने अनुशासित होकर इसका पालन किया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति आइसनहावर ने एक बार कहा था, ‘‘हमारे गणराज्य का भविष्य हमारे मतदाता के हाथ में है।’’ अर्थात् मतदाता ही राष्ट्र का भाग्यविधाता होता है। उसका एक-एक वोट अमूल्य होता है। यदि चुनाव प्रणाली ठीक होती है तो मतदाता को उसके मत की कीमत मिल जाती है, वरना वह चुनाव के बाद खुद को छला हुआ पाता है। लोकतंत्र और उसकी प्रक्रिया पर नागरिक का विश्वास बना रहे, इसके लिए जरूरी है कि चुनाव प्रणाली दुरुस्त हो। ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ एक तरह से लोकतंत्र पर हमारे नागरिक की विश्वास बहाली की दिशा में बढ़ता हुआ कदम है।
क्रम टूटा, खर्च बढ़ा
आजादी के बाद देश में जिस तरह से चुनाव हो रहे थे, उसमें कोई समस्या नहीं थी। 1952, ’57, ’62 और ’67 में लोकसभा चुनावों के साथ विधानसभा के चुनाव भी हो रहे थे। इस पर खर्चा भी कम आ रहा था और समय की भी बचत हो रही थी। लेकिन बाद के वर्षों में कुछ राज्यों में समय से पहले विधानसभाओं के भंग होने से इस क्रम में व्यवधान आ गया। फिर इंदिरा गांधी ने भी अपनी सुविधा के लिए चुनाव आगे-पीछे करवाने शुरू कर दिए। चूंकि संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, जो इस पर रोक लगाती या ऐसे प्रयासों को हतोत्साहित करती और अगले ही चरण में इसे दुरुस्त कर देती, इसलिए यह क्रम निरंतर टूटता ही चला गया। यहां तक कि आपातकाल में तत्कालीन प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी ने संविधान संशोधन करके अपना कार्यकाल बढ़ा कर छह वर्ष कर लिया। यह संविधान का गला घोटने जैसा था। 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई तो उसने कांग्रेस शासित राज्यों की सरकारें भंग कर दीं। जब 1980 में कांग्रेस सत्ता में लौटी तो उसने भी जनता पार्टी या उसके घटक दलों की सरकारें या तो बर्खास्त कर दीं या दलबदल करवा कर सरकार बदलवा दी। इसके बाद तो यह सिलसिला चलता ही चला गया।
1989 के बाद केंद्र में लगातार अस्थिरता बने रहने से न सिर्फ लोकतंत्र कमजोर हुआ, बल्कि हम सब भी कमजोर हो गए। केंद्र कमजोर होता है तो तरह-तरह के आंदोलन खड़े हो जाते हैं और राष्ट्र विरोधी ताकतें भी सक्रिय हो जाती हैं। संवैधानिक प्रावधानों की उदारता के ही कारण अब देश में साल भर कहीं न कहीं चुनाव होते ही रहते हैं। चुनाव जीतने की होड़ में पैसा भी अनाप-शनाप बहाया जाता है। एक अनुमान के अनुसार, बीते लोकसभा चुनाव में एक लाख 35 हजार करोड़ रुपये खर्च हुए, जबकि 2019 के आम चुनाव में 60 हजार करोड़ रुपये खर्च हुए थे। विधानसभाओं में होने वाले चुनाव खर्च का तो कोई हिसाब ही नहीं है। वहीं, 1952 में हुए चुनाव में (लोकसभा और विधानसभाएं मिलाकर) कुल 10.5 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। आखिर कहां से आता है इतना धन? भारतीय करदाताओं का ही तो धन है ये। हमारी चुनाव प्रणाली की यह हालत कोई मामूली विकृति नहीं है।

ये समर्थन में
राष्ट्रीय दल – भाजपा, नेशनल पीपुल्स पार्टी
क्षेत्रीय दल – एआईएडीएमके, आजसू, अपना दल (सोने लाल), अगप, बीजद, जदयू, लोजपा (आर), मिजो नेशनल फ्रंट, नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, शिवसेना, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, शिअद, यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल, पट्टाली मक्कल काची, रिपाब्लिकन पार्टी आफ इंडिया (अठावले), तमिल मनीला कांग्रेस (एम), रालोजद, संयुक्त किसान विकास पार्टी, भारतीय समाज पार्टी, गोरखा नेशनल लिबरल फ्रंट, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, भारतीय मक्कल कालवी मुनेत्र कड़गम, इंडिजिनस पीपुल्स फ्रंट आफ त्रिपुरा, जन सुराजय पार्टी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी, निषाद पार्टी, पुठिया निधि काची, राकांपा (अजित पवार), डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी।
न्यायाधीश – पूर्व सीजेआई न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ति यू.यू. ललित, दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गोर्ला रोहिणी, न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन व न्यायमूर्ति धीरूभाई नारणभाई पटेल, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दिलीप बाबासाहब भोसले व न्यायमूर्ति संजय यादव, बॉम्बे उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रदीप नंदराजोग व न्यायमूर्ति रमेश देवकीनंदन धानुका, कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी
पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त – अचल कुमार जोति, ओपी रावत, सुनील अरोड़ा, सुशील चंद्रा
ये विरोध में

राष्ट्रीय दल – कांग्रेस, आआपा, बसपा, माकपा,
क्षेत्रीय दल – आल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, तृणमूल कांग्रेस, एआईएमआईएम, भाकपा, डीएमके, नागा पीपुल्स फ्रंट, सपा, एमडीएमके, विदुथलाई चिरुथैगल काची, भाकपा (माले), सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी आफ इंडिया
ये कुछ नहीं बोले – भारत राष्ट्र समिति, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, नेशनल कांफ्रेंस, जद(एस), झामुमो, केरल कांग्रेस (एम), राकांपा, राजद, रालोपा, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, टीडीपी, युवजन श्रमिका रायथू कांग्रेस पार्टी, रालोद, शिअद (मान)
न्यायाधीश – दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजीत प्रकाश साह, कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गिरीश चंद्र गुप्ता, मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीब बनर्जी
बाधित विकास, बढ़ती उदासीनता
साल-दर-साल चुनाव होते रहने से संबंधित राज्य में हमेशा आचार संहिता लगी रहती है। कभी लोकसभा के चुनाव, कभी राज्य विधानसभा के चुनाव तो कभी स्थानीय निकायों के चुनाव। आचार संहिता की वजह से विकास के तमाम काम बाधित हो जाते हैं, भर्तियां नहीं हो पातीं, सड़कें नहीं बन पातीं और कोई अत्यंत जरूरी काम भी आगे नहीं बढ़ पाता। 2018 में विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि 2016-17 में महाराष्ट्र में साल के 365 में से 307 दिनों में आदर्श आचार संहिता लगी रही, जिससे राज्य में विकास कार्य ठप्प पड़े रहे। फिर हमेशा चुनाव होते रहने से सरकारी कर्मचारी अपने काम की बजाय चुनाव के काम में लग जाते हैं, जिससे उनके अपने हिस्से के काम अधूरे पड़े रहते हैं। सरकार के मंत्री, सांसद-विधायक हमेशा चुनावी मुद्रा में रहने से अपने स्थायी महत्व के काम नहीं कर पाते। एक राज्य के मुख्यमंत्री, मंत्री और अन्य मशीनरी दूसरे राज्य में अपनी पार्टी के प्रचार के लिए कई-कई हफ्ते अपने मूल राज्य से नदारद रहते हैं। इससे उनके अपने राज्य का काम प्रभावित होता है। पुलिस और अर्ध सैनिक बल भी हमेशा एक राज्य से दूसरे राज्य में भटकते रहते हैं। इससे भी खर्च बढ़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमेशा चुनाव के मोड में रहने से मतदाता उदासीन होने लगता है। खासकर शहरी मध्य वर्ग और उच्च मध्य वर्ग के लोग मतदान तिथियों को छुट्टी का दिन समझने लगे हैं। यदि शनिवार और रविवार भी साथ में पड़ गए तो वे मतदान छोडकर छुट्टी बिताने बाहर निकल जाते हैं। मतदाता की यह उदासीनता और चुनाव प्रक्रिया के प्रति नकारात्मक भाव आखिर हमारे लोकतंत्र को कहां ले जाएगा? यह एक गंभीर प्रश्न है।
औसतन छह चुनाव

1952 से 2023 तक देश में हर वर्ष औसतन छह चुनाव (लोकसभा एवं विधानसभा) हुए। इसमें स्थानीय चुनावों को भी शामिल कर लिया जाए तो हर वर्ष होने वाले चुनावों की संख्या कई गुना बढ़ जाएगी। 1951-52 के पहले आम चुनाव में 17.32 करोड़ मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। उस समय चुनाव पर लगभग 10.5 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। यानी प्रति मतदाता 60 पैसे का खर्च आया था, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में बढ़कर 1,400 रुपये हो गई। इस चुनाव में 2019 से दोगुना से भी अधिक यानी 1.35 लाख करोड़ रुपये खर्च हुए। 2004 के लोकसभा चुनाव में प्रति मतदाता खर्च 12 रुपये था, जो 2009 में 17 रुपये, 2014 में लगभग 46 रुपये और 2019 में 72 रुपये हो गया था। वहीं, 1999 के लोकसभा में पूरी चुनाव प्रक्रिया पर 880 करोड़, 2004 में 1200 करोड़, 2014 में लगभग 3,870 करोड़, 2019 में लगभग 6,500 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। खर्च के लिहाज से 1957 के आम चुनाव में सबसे कम 5.9 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। यानी प्रत्येक मतदाता पर मात्र 30 पैसे खर्च हुए थे।
विपक्ष के बेतुके तर्क
संसद में एक साथ चुनाव कराने को लेकर विधेयक प्रस्तुत किया गया तो विपक्षी दलों ने इसका जम कर विरोध किया। उनका कहना है कि इससे संघीय ढांचे को नुकसान होगा। छोटी राजनीतिक पार्टियों को नुकसान होगा, उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। क्षेत्रीय दल धीरे-धीरे हाशिये पर चले जाएंगे और दूसरे राज्यों में अपने कदम नहीं बढ़ा पाएंगे। राष्ट्रीय दलों का दबदबा हो जाएगा। यह हमारे मतदाता के संवैधानिक अधिकारों पर हमला है। लोकतंत्र के लिए खतरा है। आम मतदाता मतदान करते समय भ्रमित हो सकता है। वह केंद्र और राज्य सरकारों के कार्य-प्रदर्शन को ठीक से परख नहीं पाएगा। इसलिए यह संविधान के बुनियादी ढांचे के विरुद्ध है। यह विधेयक राज्य सरकारों के कार्यकाल और उनकी शक्तियों को भी कम करता है। केंद्र सरकार उनके ऊपर हावी हो सकती है और केंद्र की तानाशाही कायम हो सकती है। आश्चर्यजनक दलील यह भी है कि साल भर चुनाव होते रहने से काला धन बाहर आता है, उससे जनता को रोजगार मिलता है और जब काला धन बाहर नहीं आएगा और जनता बेरोजगार हो जाएगी। जब हम लोकसभा चुनाव ही एक साथ नहीं करवा पाते, कई-कई चरणों में चुनाव करवाते हैं तो लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कैसे करवा पाएंगे? फिर उनका तर्क यह भी है कि जब एक साथ चुनाव होते थे, तब देश की आबादी महज 40 करोड़ थी। आज एक अरब 40 करोड़ हो गई है। ऐसे में एक साथ इतना बड़ा चुनाव कैसे हो पाएगा?
‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ का विरोध करने वालों की दलीलें वास्तव में राजनीतिक हैं। वे राजनीति के लिए राजनीति कर रहे हैं। जब 1967 तक संघीय ढांचे का हनन नहीं हो रहा था तो अब कैसे हो जाएगा? यदि यह व्यवस्था संविधान के मूल विचार के विरुद्ध होती तो संविधान में ऐसी व्यवस्था ही क्यों रखी जाती? उसकी जगह कोई और व्यवस्था क्यों न होती? किस तरह आजादी के बाद चार-चार आम चुनाव उस व्यवस्था के तहत होते? संविधान को तो और स्पष्ट और सख्त होना चाहिए था ताकि बाद के सत्ताधारी उसका अपने स्वार्थ हेतु उसके हनन करने की हिम्मत ही न कर पाते।
छोटे या क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को भी घबराने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय दलों की तुलना में उन्हें जनता की सेवा का बेहतर मौका मिलता है। वे निरंतर अपने मतदाताओं के सामने रहते हैं। इसलिए यदि वे ईमानदारी के साथ राजनीति को सेवा समझकर काम करें तो लगता नहीं कि उन्हें कोई हानि होगी। जहां तक राष्ट्रीय दलों की मजबूती का प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें मजबूत होना भी चाहिए, बल्कि हर दल को मजबूत होना चाहिए। जब-जब राष्ट्रीय दल कमजोर हुए हैं, देश अस्थिर हुआ है और नुकसान पूरे देश को उठाना पड़ा है। 1987-91 का दौर याद कीजिए, जब हम आर्थिक तौर पर इतने दीन-हीन हो गए थे कि देश का सोना विदेश में गिरवी रखना पड़ा था। ज्यादातर ताकतवर राष्ट्रों में दो या तीन दल ही चुनावी परिदृश्य में होते हैं। इसलिए उनकी नीतियों में भी एकसारता होती है और वे तरक्की भी अधिक करते हैं। अमेरिका जैसे देश में तो हर चीज पहले से निश्चित होती है। यहां तक कि चुनाव का पूरा कार्यक्रम और राष्ट्रपति के शपथ लेने की तारीख भी। उसे तोड़ने का साहस कोई नहीं करता।


परिपक्व होते मतदाता
हमारा मतदाता निरंतर परिपक्व हो रहा है। अब वह इतना विवेकवान हो गया है कि अच्छे और बुरे का अंतर समझ सकता है। वह समझ गया है कि राज्य और केंद्र के स्तर पर कौन बेहतर विकल्प है। पांच वर्ष में चुनाव आएगा तो उसमें उत्साह भी बना रहेगा और बढ़-चढ़ कर उसमें हिस्सेदारी भी करेगा। बार-बार के चुनावों की वजह से होने वाली थकान और नकारात्मकता उसमें नहीं होगी। यदि कोई सरकार गिर भी जाती है तो बाकी बचे समय के लिए चुनाव कराए जा सकते हैं, जैसा कि राज्यसभा के चुनाव में होता है। सबसे बड़ी बात ये है कि ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ लागू हो जाने से विकास कार्य बाधित नहीं होंगे। काले धन का प्रवाह कम होगा और भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी। साथ ही, सरकारों के कामकाज में स्थिरता और निरंतरता आएगी। सरकारें चाहे केंद्र की हो या राज्यों की, अपनी नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर ध्यान देंगी। देशहित में स्थायी और दूरगामी फैसले लिए जा सकेंगे। अन्यथा लोगों की नजर सिर्फ और सिर्फ चुनावों तक सीमित रहती है। देश एक किस्म के तदर्थवाद का शिकार हो जाता है। फिर एक साथ चुनाव होने से, जो भी मेहनत लगेगी, एक बार ही लगेगी। एक बार के खर्चे में दो चुनाव सम्पन्न हो जाएंगे। इस तरह से जो धन बचेगा, वह देश के विकास में लगेगा। जनहितकारी योजनाओं में लगेगा।
निश्चय ही यह एक क्रांतिकारी बदलाव की शुरुआत है। देश के विकास और दीर्घकालिक योजनाओं को साकार करने के लिए ऐसे दूरगामी फैसले देश हित में जरूरी हैं। सोचिए कि यदि ये मोदी सरकार न होती तो क्या इस तरह की पहल की कल्पना की जा सकती थी? कुछ विपक्षी दल कह रहे हैं कि यह मोदी सरकार की असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की चाल है। लेकिन क्या इससे भी कोई बड़ा मुद्दा हो सकता है? कुछ लोगों को यह मुद्दा अचानक से आया हुआ लग सकता है, लेकिन इसकी मांग 1983 से ही हो रही है। हर दल के संवेदनशील लोग इसे उठाते रहे हैं। चूंकि यह एक दूरगामी फैसला है, इसलिए सरकार भी इसे गंभीरता से ले रही है। प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि इस पर व्यापक बहस हो। हर तरह के विचार आएं और तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए भविष्य की दिशा तय हो। जिस तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 तैयार हुई है, उसी प्रकार से ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ का मसौदा भी बहुत सोच-समझ कर तैयार किया गया है। उम्मीद है कि इससे भविष्य की राजनीति का पथ प्रशस्त होगा और हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा।
उच्चस्तरीय समिति में कौन-कौन?
- 2 सितंबर, 2023 को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में 8 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन हुआ। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, गुलाम नबी आजाद, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉ. सुभाष सी. कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी, जबकि कानून एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विशेष आमंत्रित सदस्य तथा डॉ. नितेन चंद्रा इसके सचिव थे। समिति में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी भी थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया था।
- 65 बैठकें कीं उच्चस्तरीय समिति ने 23 सितंबर, 2023 से 10 मार्च, 2024 के बीच
ल्ल 191 दिनों के शोध, हितधारकों और विशेषज्ञों से बातचीत के बाद समिति ने 18,626 पृष्ठों की रिपोर्ट तैयार की है। - 21,558 लोगों के सुझाव मिले समिति को, इनमें से 80 प्रतिशत लोग एक साथ चुनाव कराए जाने के पक्ष में।
- 47 राजनीतिक दलों से भी समिति को प्रतिक्रियाएं मिलीं। 15 दलों को छोड़कर शेष 32 दल एक साथ चुनाव कराने के पक्ष में।
- 4 पूर्व सीजेआई, प्रमुख उच्च न्यायालयों के 12 पूर्व मुख्य न्यायाधीश, 4 पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त व 8 राज्य चुनाव आयुक्त तथा विधि आयोग के अध्यक्ष और चुनाव आयोग से भी ली गई सलाह
- 400 से अधिक लोकसभा और विधानसभा चुनाव हो चुके हैं देश में पिछले 7 से अधिक दशकों में।
कई देशों की चुनाव प्रक्रियाओं का अध्ययन
दक्षिण अफ्रीका – यहां विधानसभा या निचले सदन और प्रांतीय परिषदों के चुनाव, दोनों के लिए एक साथ मतदान होते हैं। लेकिन नगरपालिका और प्रांतीय चुनाव हर पांच वर्ष में अलग से होते हैं। इस वर्ष भी 29 मई को संसदीय और प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव साथ-साथ हुए।
स्वीडन – यह देश आनुपातिक चुनाव प्रणाली अपनाता है। इसका अर्थ यह है कि राजनीतिक दलों को मिले वोटों के आधार पर निर्वाचित विधानसभा में सीटें मिलती हैं। स्वीडन की चुनाव प्रणाली में संसद (रिक्सडैग), काउंटी परिषदों और नगर परिषदों के चुनाव एक साथ होते हैं। ये चुनाव हर 4 वर्ष में सितंबर के दूसर रविवार को, जबकि नगरपालिका चुनाव हर 5 वर्ष में सितंबर के दूसरे रविवार को होते हैं।
जर्मनी – जर्मनी में निचले सदन (बुंडेस्टैग), विधानसभा (लैंडटैग्स) और स्थानीय चुनाव साथ-साथ होते हैं। वे आनुपातिक प्रतिनिधित्व का पालन करते हैं और केवल अविश्वास मत से चांसलर को नहीं हटाया जा सकता। संसद में सरकार को हटाने का प्रस्ताव तभी पेश किया जा सकता है, जब वह किसी उत्तराधिकारी का नाम सुझाए।
इंडोनेशिया – यहां 2019 से एक साथ चुनाव कराए जा रहे हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय विधायी निकाय चुनाव एक ही दिन होते हैं। यहां मतदाता गुप्त मतदान करते हैं और फर्जी मतदान रोकने के लिए अपनी उंगलियां अमिट स्याही में डुबोते हैं। इस वर्ष 14 फरवरी को जो चुनाव हुए, उसे दुनिया का सबसे बड़ा एकदिवसीय चुनाव कहा गया, क्योंकि लगभग 20 करोड़ लोगों ने एक साथ मतदान किया।

















टिप्पणियाँ