सिनेमा को ‘सातवीं कला’ कहा जाता है, जो प्रतिनिधि कलाओं और निष्पादन कलाओं के संयोग से बना है। जुलाई 1896 में जब लुमियर बंधुओं ने पहली बार भारत में सिनेमा का प्रदर्शन किया, तब यह कला से अधिक कौतूहल का विषय था। कला के क्षेत्र में भारत पहले से ही समृद्ध था। सर्वप्रथम ‘नासदीय सूक्त’ में मानव हृदय की सौंदर्य अभिव्यक्ति हुई। कालिदास के ‘मेघदूतम्’ से लेकर तुलसी कृत ‘रामचरितमानस’ की चौपाई ‘सोह नवल तनु सुंदर सारी। जगत् जननि अतुलित छवि भारी’ में यही सौंदर्य बोध है।
सिनेमा पश्चिम की देन है और अस्तित्व में आने के बाद से अभी तक यह निरंतर चर्चा एवं विवादों में रहा है। चाहे 1933 में बनी फिल्म ‘कर्मा’ में देविका रानी एवं हिमांशु राय के चुंबन का दृश्य हो या 1978 में प्रदर्शित ‘किस्सा कुर्सी का’ के जरिए सरकार पर तंज से उपजा विवाद। वर्तमान दौर में ‘सावरकर’ और ‘रजाकर’ जैसी यथार्थ पर आधारित फिल्मों ने छद्म सेकुलर राजनेताओं और वामपंथी बुद्धिजीवी वर्ग को ललकारा है। इसलिए इन फिल्मों के विरोध की वजह भले ही वर्तमान कालखंड के विषय परिदृश्य में दिखे, किंतु इसकी जड़ें अतीत में हैं।
1913 में जब दादा साहेब फाल्के ने फिल्म ‘राजा हरिश्चंद्र’ बनाई तो पारसी थिएटर से जुड़े कलाकारों एवं पारसी सेठों का ध्यान इस नई कला विधा की ओर गया। नतीजा, 1930 तक 1200 से अधिक फिल्में बनीं, जिनके विषय मुख्यत: पौराणिक थे। इसी दौरान सामाजिक सुधार के लक्ष्य के साथ एक मद्धम धारा भी गतिशील हुई। चूंकि भारत में जब सिनेमा का आगमन हुआ, तब देश सामाजिक-राजनीतिक बदलाव के संक्रमण से गुजर रहा था। लिहाजा, वह मद्धम धारा भी सिनेमा में शामिल हो गई। व्ही. शांताराम की ‘दुनिया न माने’, ‘पड़ोसी’, ‘दहेज’, ‘दो आंखें बारह हाथ’ जैसी सुधारवादी फिल्मों के साथ 1922 में धीरेंद्र गांगुली की ‘इंग्लैंड रिटर्न’ और सामाजिक व्यवस्था पर व्यंग्य करती बाबूराव पेंटर की ‘सावकारी पाश’ जैसी फिल्में भी बनीं।
वामपंथ का आगमन
1917 की रूसी क्रांति से प्रेरित वामपंथ के उभार एवं इसके प्रति युवा वर्ग के आकर्षण से धीरे-धीरे सिनेमा भी प्रभावित हुआ। 1940 से 1950 के बीच ‘नया संसार’, ‘रोटी’, ‘उदायर पाथेय’, ‘धरती के लाल’, ‘नीचा नगर’ फिल्मों के माध्यम से सिनेमा समाजवाद की लड़ाई लड़ रहा था। वैसे भी 1920 के दशक में गांधीजी भारतीय समाज के मूलभूत परिवर्तन की आवाज लगा ही रहे थे। इसके बावजूद उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन में न कोई स्वीकार्यता मिली और न ही सामाजिक जीवन में कोई विशेष सम्मान। गांधीजी ने अपना आधा जीवन सामाजिक समानता स्थापित करने और छुआछूत खत्म करने में लगा दिया, लेकिन वे भी फिल्म निर्माता के बहुत आग्रह के बावजूद फिल्म ‘अछूत कन्या’ देखने को तैयार नहीं हुए।
आजादी के दो दशक बाद तक कांग्रेसी सत्ता की छत्रछाया में वामपंथी बौद्धिक जमात ने ‘नया समाज’ बनाने की जुबानी जुगाली जारी रखी। 1970 के दशक में नारीवाद, भ्रष्टाचार, सामाजिक विभेद, उन्मुक्त सेक्स, राष्ट्रवाद का विरोध आदि मुद्दों की आड़ में वामपंथी-जिहादी विचारों के प्रसार का नया दौर शुरू हुआ। ’80 के दशक में जब देश नक्सलवाद और खालिस्तान के दोहरे संकट से जूझ रहा था, तो वामपंथ को अपने बौद्धिक प्रसार के लिए यह समय उपयुक्त लगा। इसके बाद 1990 के दशक में उदारीकरण का दौर आया। उधर, वैश्विक स्तर पर कम्युनिज्म एवं सोवियत संघ की मशाल बुझने लगी, तो भारतीय वामपंथी थोड़े कमजोर जरूर पड़े, किंतु हिंदू धर्म-संस्कृति के प्रति उनकी घृणा यथावत रही।
तब इस सांस्कृतिक विघटन की कमान भूमंडलीकरण ने संभाली। उदारीकरण ने न केवल सिनेमा, बल्कि प्रदर्शन के माध्यम को भी बदल दिया। एक नए मंच के रूप में ओटीटी (ओवर दी टॉप) ने सिनेमा को डिजिटल युग में पहुंचा दिया, जिसने यौनिकता व हिंसा के साथ व्यक्तिगत कुंठा को मोबाइल की निजता के साथ पल्लवित होने का मार्ग उपलब्ध कराया। लेकिन इस दौर के आते-आते पश्चिमी पूंजीवाद के विरोध में वामपंथियों ने इस्लामिक कट्टरपंथ का दासत्व स्वीकार कर लिया था।
दरअसल, देश में सिनेमा के विकास के समानांतर हमेशा से वामपंथ प्रेरित वैचारिक षड्यंत्र एवं बौद्धिक आक्षेप की प्रक्रिया लगातार चल रही थी, जिसका अतीत पुराना है। मध्यकाल में जब यूरोप पुनर्जागरण से आह्लादित था, तब अलसाया साहित्य भी नवमार्ग-नवचेतना का अनवेशी बना जैसा कि फ्रांसीसी साहित्यकार रेबेलास का मंत्र, ‘प्यास-बौद्धिक और नैतिक प्यास, अनुभव की प्यास, यथार्थ की प्यास।’ इस साहित्य की प्यास को 19वीं सदी की वामपंथी बौद्धिक जुगाली में देखा जा सकता है, क्योंकि बुकासियो, पैटार्क, दांते से लेकर जाफरे, मूर तक की विस्तृत परंपरा ने प्राचीन धार्मिक-सामाजिक मान्यताओं के विरुद्ध मानववाद एवं भौतिकतावादी दर्शन का एक आधार तो प्रदान कर ही दिया था, जिसे साम्यवाद-मार्क्सवाद ने अपने भौतिकतावादी संदर्भ में थोड़े-बहुत बदलावों के साथ आत्मसात कर लिया।
संक्रमण का दौर
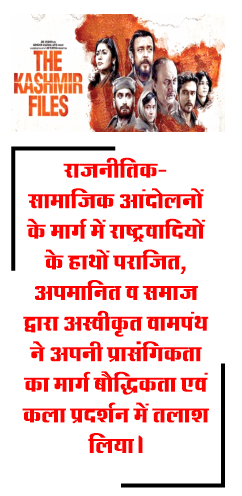 19वीं सदी के उत्तरार्ध एवं 20वीं सदी के प्रारंभिक दशकों में यूरोपीय वामपंथ से संक्रमित सज्जाद जहीर, सोफिया वादिया, मौलवी अब्दुल हक, मुंशी दयानारायण, अहमद अली, जोश मलीहाबादी, शिवदान सिंह चौहान, बलराज साहनी, ख्वाजा अहमद अब्बास, सलिल चौधरी, उत्पल दत्त, करुणा बनर्जी, ऋत्विक घटक, मृणाल सेन, अमर शेख, पृथ्वीराज कपूर जैसे वामपंथी बौद्धिकों, कलाकारों एवं संगीतकारों ने सिनेमा उद्योग में पैर पसारे। इनका प्रथम ध्येय देश के सनातन संस्कारों की तथाकथित जड़ता एवं ‘नीलांबर परिधान’ वाली भारतमाता के आभामंडल को नष्ट करना था। इसी मंशा से नेहरू के आशीर्वाद से प्रगतिशील लेखक संघ (1936) और बाद में पीसी जोशी व सज्जाद जहीर जैसे कम्युनिस्ट लेखकों के समर्थन से इप्टा (1943) जैसे संगठन अस्तित्व में आए। बाद में यही वामपंथी जमात सिने जगत के पटकथा लेखन, निर्देशन, अभिनय, संगीत, गायन जैसे विविध क्षेत्रों में काबिज हुई और कला की ओट में स्वघोषित एजेंडे को लागू करने में लग गई।
19वीं सदी के उत्तरार्ध एवं 20वीं सदी के प्रारंभिक दशकों में यूरोपीय वामपंथ से संक्रमित सज्जाद जहीर, सोफिया वादिया, मौलवी अब्दुल हक, मुंशी दयानारायण, अहमद अली, जोश मलीहाबादी, शिवदान सिंह चौहान, बलराज साहनी, ख्वाजा अहमद अब्बास, सलिल चौधरी, उत्पल दत्त, करुणा बनर्जी, ऋत्विक घटक, मृणाल सेन, अमर शेख, पृथ्वीराज कपूर जैसे वामपंथी बौद्धिकों, कलाकारों एवं संगीतकारों ने सिनेमा उद्योग में पैर पसारे। इनका प्रथम ध्येय देश के सनातन संस्कारों की तथाकथित जड़ता एवं ‘नीलांबर परिधान’ वाली भारतमाता के आभामंडल को नष्ट करना था। इसी मंशा से नेहरू के आशीर्वाद से प्रगतिशील लेखक संघ (1936) और बाद में पीसी जोशी व सज्जाद जहीर जैसे कम्युनिस्ट लेखकों के समर्थन से इप्टा (1943) जैसे संगठन अस्तित्व में आए। बाद में यही वामपंथी जमात सिने जगत के पटकथा लेखन, निर्देशन, अभिनय, संगीत, गायन जैसे विविध क्षेत्रों में काबिज हुई और कला की ओट में स्वघोषित एजेंडे को लागू करने में लग गई।
इधर, ‘परिमल’ मंडली जैसे संगठन व बांग्ला साहित्यकार रजनीकांत दास जैसे लोग इनका विरोध कर रहे थे, लेकिन नए समाज के निर्माण के उदाहरणविहीन रोमानी दावे से उनका प्रतिरोध वामपंथी सम्मोहन के समक्ष क्षीण रहा। ऊपर से नेहरूवादी निजाम में वामी-कामियों की पौ-बारह थी। कांग्रेसी सत्ता के निर्देश पर उनके साथ पूरा सरकारी तंत्र खड़ा था। 2014 के बाद नवसत्ता कालखंड में हिंदू पुनर्जागरण के राष्ट्रीय आंदोलन ने उसी सुषुप्त बौद्धिक प्रतिरोध को उभारा, जिसे वामपंथ समर्थकों ने कांग्रेस शासनकाल में दबाया था।
राजनीतिक-सामाजिक आंदोलनों के मार्ग में राष्ट्रवादियों के हाथों पराजित, अपमानित व समाज द्वारा अस्वीकृत वामपंथ ने अपनी प्रासंगिकता का मार्ग बौद्धिकता एवं कला प्रदर्शन में तलाश लिया। सिनेमा भी वामपंथ प्रेरित इसी दुरभिसंधि का एक हिस्सा रहा है। किसी राष्ट्र की आध्यात्मिक चेतना को खंडित करना हो, तो सर्वप्रथम उसकी सांस्कृतिक विरासत को नष्ट किया जाता है। 1920 के बाद और विशेषकर ’70 के दशक से अब तक वामपंथी धारा के सिनेमा ने यही किया है। कला के नाम पर वैकल्पिक धारा के मुख्य प्रवर्तकों में सत्यजित रे, ऋत्विक घटक और मृणाल सेन जैसे लोगों ने भारत और भारतीयता को अक्सर अपनी प्रगतिशीलता के नाम पर बहुत कठिन स्वरूप में प्रस्तुत किया, जिसका आम भारतीय ही नहीं, बल्कि स्वयं सिनेमा जगत भी विरोधी था।
एक बार अभिनेत्री नरगिस ने संसद में उनकी आलोचना करते हुए कहा था कि वे पश्चिमी देशों में अपनी वाहवाही के लिए भारत की गरीबी का चित्रण करते हैं। फिर भी यह चलन थमा नहीं। श्याम बेनेगल, अडूर गोपालकृष्णन और ऐसे ही कुछ निर्माता-निर्देशकों ने समानांतर सिनेमा के नाम पर जाति प्रथा, यौनाचार और सामाजिक रूढ़ियों को अत्यंत ही विद्रूपता एवं अतिरंजना के साथ प्रस्तुत किया। इसके लिए नेहरूवाद की छाया में देश की तमाम संस्थाओं में न केवल सम्मानित और पुरस्कृत होते रहे, बल्कि विदेशों में एक तरह से भारतीय कला फिल्मों के प्रवर्तक ही माने गए।
वैसे एक खास विचारधारा से पोषित सिनेमा जब समाज को नुकसान पहुंचाने लगे, तब वह कला नहीं रह जाता। राष्ट्रवादी ही नहीं, मध्य मार्ग की राजनीतिक धारा भी यह समझ रही थी कि भारतीय सिनेमा पतन के रास्ते पर जा रहा है। भारतीयता के विरुद्ध यह षड्यंत्र उन्मुक्त यौनिकता, युवा भटकाव, अनावश्यक सामाजिक विद्रोह को भव्य रूप में प्रदर्शित करना, पारिवारिक मूल्यों के क्षरण जैसे मामलों में दिखा। हालांकि सिनेमा पर ऐसे आरोप आजादी के बाद से ही लगते रहे हैं।
1953 में मद्रास के मुख्यमंत्री राजगोपालाचारी ने आरोप लगाया था कि यौनाचार एवं हिंसा पर केंद्रित फिल्में भारतीय युवाओं को पथभ्रष्ट कर रही हैं। साथ ही उन्होंने फिल्म निर्माताओं से यौन अपील कम करने एवं धार्मिक विषयों पर फिल्म बनाने का आग्रह किया था। इसके बाद, नवंबर 1954 में राज्यसभा सांसद लीलावती मुंशी ने भी सिनेमा को देश के नैतिक स्वास्थ्य के लिए खतरा तथा अपराध व सामाजिक अव्यवस्था फैलाने का बड़ा कारण करार दिया था। उन्होंने राज्य सभा में कहा था,
‘‘सिनेमा में ताकत है कि वह या तो किसी पीढ़ी और देश को सही दिशा दे सकता है या उसे बर्बाद कर सकता है।’’
इस्लामी घालमेल
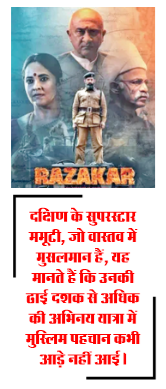 सिने जगत देश में व्यवस्थित और संस्थागत तुष्टीकरण किया है। यह देश विभाजन के लिए जिम्मेदार कट्टरपंथी मुसलमानों के स्वागत में बिछ गया। हालांकि देश का बहुसंख्यक समाज न तो विभाजन के रक्तरंजित दृश्य को भूला था और न ही इस्लामी आतंक को। इसके बावजूद, मुस्लिम गीतकार, पटकथा लेखक, गायक संगीतकार, निर्देशक से लेकर अभिनेता-अभिनेत्री को स्थापित करने के लिए ‘नाम जिहाद’ का नया पैंतरा आजमाया गया। यूसुफ खान का नाम बदलकर दिलीप कुमार, हामिद अली खान का नाम अजीत, बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी को जॉनी वॉकर बना दिया गया।
सिने जगत देश में व्यवस्थित और संस्थागत तुष्टीकरण किया है। यह देश विभाजन के लिए जिम्मेदार कट्टरपंथी मुसलमानों के स्वागत में बिछ गया। हालांकि देश का बहुसंख्यक समाज न तो विभाजन के रक्तरंजित दृश्य को भूला था और न ही इस्लामी आतंक को। इसके बावजूद, मुस्लिम गीतकार, पटकथा लेखक, गायक संगीतकार, निर्देशक से लेकर अभिनेता-अभिनेत्री को स्थापित करने के लिए ‘नाम जिहाद’ का नया पैंतरा आजमाया गया। यूसुफ खान का नाम बदलकर दिलीप कुमार, हामिद अली खान का नाम अजीत, बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी को जॉनी वॉकर बना दिया गया।
इसी तरह, नरगिस (फातिमा रशीद), मीना कुमारी (महजबी बानो) और न जाने कितने मुसलमान हिंदू नाम धारण कर सिनेमा जगत में घुल-मिल गए। यहां तक कि ‘गर्म हवा’, ‘तमस’, ‘क्या दिल्ली क्या लाहौर’, जैसी फिल्मों के जरिए कट्टरपंथी मुसलमानों के अपराधों को भावनात्मक पीड़ा में ढालकर परोसा गया। बदले में मुस्लिम पटकथा लेखकों, गीतकारों ने शुद्ध संस्कृतनिष्ठ हिंदी को खालिस ‘हिंदुस्तानी’ जुबान में बदल दिया, जो अब फारसी-उर्दू मिश्रित हिंदी हो गई है।
आश्चर्य की बात है कि इस्लाम कला, संगीत, नृत्य आदि को हराम मानता है, लेकिन धन-ऐश्वर्य के लिए मुस्लिम समाज के लोगों का सिनेमा जैसी बहुआयामी विधा से जुड़ना यह साबित करता है कि लाभ के लिए इस्लामिक मान्यताएं लचीली हो सकती हैं। बहरहाल, बहुसंख्यक समाज ने परंपरागत सहिष्णु चरित्र के अनुरूप इन मुस्लिमों कलाकारों को भरपूर सम्मान और स्नेह दिया। दक्षिण के सुपरस्टार ममूटी, जो वास्तव में मुसलमान हैं, यह मानते हैं कि उनकी ढाई दशक से अधिक की अभिनय यात्रा में मुस्लिम पहचान कभी आड़े नहीं आई। इसी के बरअक्स पाकिस्तान के सिनेमा जगत ‘लॉलीवुड’ में एक अदर हिंदू नाम तक याद कीजिए!
वामपंथी-जिहादी दुष्प्रचार
इतना सम्मान मिलने के बावजूद कट्टरपंथियों का हिंदुओं के प्रति मजहबी दृष्टिकोण न केवल बना रहा, बल्कि वामपंथी प्रश्रय के साथ धीरे-धीरे प्रकट भी होने लगा। सिनेमा के नाम पर सनातन धर्म के साथ सामाजिक-सांस्कृतिक विघटन और जातिगत विभेद के नैरेटिव गढ़े जाने लगे। ’70 के दशक में इसके अगुआ बने सलीम-जावेद, जिनकी फिल्मों में हिंदू देवी-देवताओं को कोसते-गरियाते, मजार पर चादर व बिल्ला नंबर 786 के सहारे मौत से लड़ते ‘एंग्री यंग मैन’ के रूप में सनातन धर्म-संस्कृति के विरुद्ध जिहादी षड्यंत्र का लंबा दौर चला, जिसकी कमान अलग-अलग लोगों ने संभाली।
परदे पर मुसलमानों को सदैव यथार्थ से परे महान, कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार, बहादुर सैनिक, चरित्रवान पुलिस वाला, जान देने वाले वफादार दोस्त के तौर पर दिखाया जाता था, जो 70 के दशक में और तीव्र हो गया। ‘जंजीर’ (1973) का शेर खान ईमानदार मित्र है, जबकि फिल्म ‘शान’ (1980) में अमिताभ और शशि कपूर साधुओं के वेश में जनता को ठगते हैं। वेब सीरीज ‘अपहरण’ (2022) में एक साधु वेशधारी देह व्यापार और ड्रग्स का अड्डा चलाता है। ‘गोलमाल अगेन’ में तांत्रिक तब्बू भद्दे तरीके से मंत्र पढ़ती है, जो सनातन धर्म के मंत्र पाठन को हास्यास्पद बनाता है।
इसी तरह, फिल्म ‘तहलका’ (1992) में अल्ला रक्खा कर्बला की कसम लेकर शहीद होने वाला फौजी है, जबकि सेना का हिंदू जनरल गद्दार। ‘बॉम्बे’ (1995) के एक दृश्य में भगवा झंडे और साधु-संतों के जुलूस को देखकर मनीषा कोईराला, जो एक मुस्लिम युवती की भूमिका में हैं, को भयभीत होते दिखाया गया। वैसा ही कुछ दृश्य राम मंदिर के लिए चंदा मांगते युवकों का भी है।
 इसी फिल्म में नायक का ब्राह्मण पिता खुराफाती, कट्टर है, जबकि लड़की का मुस्लिम पिता हालात का मारा रहम दिल। ‘सरफरोश’ (1999) फिल्म में सीमा पार आतंक में भी मुस्लिमों के बचाव और हिंदुओं को आक्षेपित करने के तरीके ढूंढे गए। पाकिस्तान का आतंकी गवैया हिंदू ज्योतिषी के माध्यम से सीमा पार से हथियार और ड्रग्स मंगाता है, जबकि ईमानदार इंस्पेक्टर सलीम देश को बचाता है। ऐसे ही ‘हैदर’ (2014) में कश्मीर में आंतकवाद के प्रति सहानुभूति दिखाने की कोशिश की गई।
इसी फिल्म में नायक का ब्राह्मण पिता खुराफाती, कट्टर है, जबकि लड़की का मुस्लिम पिता हालात का मारा रहम दिल। ‘सरफरोश’ (1999) फिल्म में सीमा पार आतंक में भी मुस्लिमों के बचाव और हिंदुओं को आक्षेपित करने के तरीके ढूंढे गए। पाकिस्तान का आतंकी गवैया हिंदू ज्योतिषी के माध्यम से सीमा पार से हथियार और ड्रग्स मंगाता है, जबकि ईमानदार इंस्पेक्टर सलीम देश को बचाता है। ऐसे ही ‘हैदर’ (2014) में कश्मीर में आंतकवाद के प्रति सहानुभूति दिखाने की कोशिश की गई।
फिल्म ‘इश्कजादे’ (2012) में एक भोली-भाली मुस्लिम लड़की को धोखा देकर राजनीतिक प्रतिशोध लेने वाला लड़का हिंदू है, जिसके दादा भ्रष्ट हैं। असल में ‘लव जिहाद’ के बढ़ते मामलों को एक नया मोड़ देने की कोशिश में सिनेमा ऐसे काल्पनिक तकरीरे करता रहा है। ‘पीके’ (2014) में तो आमिर खान का चरित्र खुलकर हिंदू लड़कियों से प्रेम प्रसंग के लिए मुसलमानों का बचाव करता है। हालांकि ‘पीके’ ने हिंदू धर्म का अपमान करने के लिए कला के नाम बेहूदगी की सारी सीमाएं लांघ दीं। ‘कुछ-कुछ होता है’ में एक छोटी बच्ची अचानक नमाज पढ़ने लगती है और काजोल की शादी रुक जाती है। अब इसे प्रोपेगेंडा नहीं तो और क्या कहेंगे?
इसी तरह, ‘मैं हूं ना’ (2004) में एक मुस्लिम किरदार भारत-पाकिस्तान की दोस्ती के लिए ‘शहीद’ हो जाता है और मुख्य आतंकी व खलनायक (जो हिंदू है और पूर्व में ‘बेचारे भोले-भाले’ मुस्लिमों को मारता है) को मारकर भारत-पाकिस्तान के बीच दोस्ती का मार्ग सुगम करता है। ‘बजरंगी भाईजान’ (2015) में पूरी शिद्दत से पाकिस्तानियों को अच्छा दिखाने की कोशिश हुई, जबकि ‘एक था टाइगर’ (2017) में भारत से दोस्ती के नाम पर जान पर खेलने वाले पाकिस्तानी हैं और साथ में कश्मीर पर परोक्ष पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा भी है। इन सभी फिल्मों में एक बात समान है। इनके मुख्य अभिनेता या निर्देशक, सभी मुसलमान हैं। क्या इसे संयोग माना जाए या दुर्योग?
इसी तरह, सैफ अली खान और जीशान अयूब अभिनीत ‘तांडव’ में हिंदू आस्था का अपमान, जबकि ‘सेक्रेड गेम्स’ (2018) में ‘हिंदू आतंकवाद’ की काल्पनिक पटकथा को अमलीजामा पहनाने की पूरी कोशिश की गई। यह कांग्रेस सरकार के 2008 से 2014 तक के ‘हिंदू आंतकवाद’ के नैरेटिव का समुचित समर्थन था। आश्चर्य है कि फिल्म ‘आर्टिकल 15’ के माध्यम से हिंदुओं की जाति प्रथा पर आक्षेप करने वाले सिनेमा ने कभी मुसलमानों के ‘अशराफ’, ‘अजलाफ’ और ‘अरजाल’ के कटु जातीय विभाजन पर जागरूकता का प्रयास नहीं किया। इतना ही नहीं, भारतीय संस्कृति के विभिन्न पक्षों, समाज, भाषा आदि पर आक्षेप करती, उनका उपहास उड़ाती फिल्मों की पूरी शृंखला है।
भाषा के स्तर पर ही देखिए कि फिल्मों में हिंदी को कैसे अपमानित किया गया। शुद्ध हिंदी बोलने वाले या तो मसखरी कर रहे थे जैसा ‘चुपके-चुपके’ में धर्मेंद्र या फिर ‘विश्वात्मा’ में गुलशन ग्रोवर महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे थे। वहीं, सामाजिक संरचना के विरुद्ध दीपा मेहता की ‘फायर’ (1996) में महिला समलैंगिकता को न्यायसंगत ठहराने एवं ‘वाटर’ (2005) में विधवा मनोभाव व्यक्तिकरण के नाम पर संस्कृति की अनावश्यक विद्रूपता प्रदर्शित करने का सुअवसर माना गया है।
अब परिवार तोड़ने वाला एक उदाहरण देखिए। ‘तू झूठी, मैं मक्कार’ (2023) फिल्म में मुख्य अभिनेता संभ्रांत परिवार का है, जिसके सभी सदस्य अच्छे व्यवहार वाले हैं, लेकिन अभिनेत्री परिवार के साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि उसे आजादी चाहिए। वह रिश्ता तोड़ने के लिए भाड़े पर लोगों को रखती है।
अंतत: नाटक-ड्रामे के बावजूद जब दोनों की शादी होती है, तो बहू को खुश रखने का जो फार्मूला निर्देशक ने दिखाया, वह है सास खाना बनाकर दे, उसकी सेवा करे, बहू को कुछ भी पहनने, पार्टी करने और शराब पीने आदि की आजादी हो। इसी तरह, फिल्म ‘थप्पड़’ (2020) में जिस तरह से ‘फेमिनिज्म’ को दिखाया गया है, उससे बेहूदा प्रकरण दूसरा नहीं हो सकता। संभव है कि करियर में अचानक मिले बॉस के धोखे से गुस्से में लड़का अपनी बहन, भाई, दोस्त पर हाथ उठाता हो। निजी जीवन में आपने भी ऐसे कई प्रकरण देखे होंगे, तो क्या इसके लिए परिवार ध्वस्त कर दिए जाएं, जबकि लड़का फिल्म में पूरे समय अपनी गलती के लिए माफी मांगता रहता है।
ऐसी पटकथाएं समाज को तोड़ने के लिए प्रेरित करने वाले कुतर्क और चित्रात्मक षड्यंत्र प्रतीत होती हैं। प्रश्न है कि सिनेमा के माध्यम से वामपंथी-जिहादी समूह में भारतीयता को चोटिल करने की इतनी लिप्सा क्यों है? असल में मनुष्य की इंद्रिय चेतना आंखों द्वारा सीखे गए बोध को अधिक तीव्रता से आत्मसात करती है, इसीलिए आधुनिक शिक्षा प्रणाली में छोटे बच्चों को प्रोजेक्टर से पढ़ाया जाता है।
लिहाजा, इंद्रियों के माध्यम से व्यक्ति के अवचेतन मन में अपनी प्रायोजित भावना को समायोजित करने की कला सदैव से वामपंथी बौद्धिक षड्यंत्र का हिस्सा रही है। जैसे- बिहार में लालू यादव के राज में 1992 में आरा में स्थापित वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के परिसर में लगी बाबू कुंवर सिंह की प्रतिमा को सुनियोजित तरीके से इस्लाम जैसी टोपी (कुफी या तकियाह) पहनाई गई है।
विश्वविद्यालय की विभिन्न कक्षाओं एवं कार्यालयों में लगी तस्वीरों में उन्हें इसी रूप में दिखाया गया है। अब ऐसे कौन से ऐतिहासिक स्रोत से कुंवर सिंह या किसी भी राजपूत रियासत के प्रतिनिधि या राजा को मुल्ला छाप टोपी पहनने का प्रमाण मिलता है? यह प्रमाण है दृश्य कला के जरिए युवाओं के मस्तिष्क में ‘गंगा-जमुनी तहजीब’ के काल्पनिक विचार के प्रत्यारोपण का। सिनेमा भी चलचित्र के माध्यम से यही करता रहा है।
सिनेमा और राष्ट्रवादी चेतना
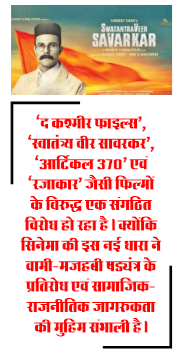 अब वर्तमान विमर्श पर लौटें। 2022 में ‘द कश्मीर फाइल्स’ के बाद 2024 में आई ‘स्वातंत्र्य वीर सावरकर’, ‘आर्टिकल 370’ एवं ‘रजाकार’ जैसी फिल्मों के विरुद्ध एक संगठित विरोध हो रहा है। विरोध क्यों? क्योंकि सिनेमा की इस नई धारा ने वामी-मजहबी षड्यंत्र के विरुद्ध प्रतिरोध एवं सामाजिक-राजनीतिक जागरूकता की मुहिम संभाली है। अपनी एक सदी से अधिक की यात्रा में पहली बार सिनेमा राष्ट्रवाद के यथार्थ को स्वीकार करने की दिशा में अग्रसर है। यही वर्तमान विवाद की मूल वजह है।
अब वर्तमान विमर्श पर लौटें। 2022 में ‘द कश्मीर फाइल्स’ के बाद 2024 में आई ‘स्वातंत्र्य वीर सावरकर’, ‘आर्टिकल 370’ एवं ‘रजाकार’ जैसी फिल्मों के विरुद्ध एक संगठित विरोध हो रहा है। विरोध क्यों? क्योंकि सिनेमा की इस नई धारा ने वामी-मजहबी षड्यंत्र के विरुद्ध प्रतिरोध एवं सामाजिक-राजनीतिक जागरूकता की मुहिम संभाली है। अपनी एक सदी से अधिक की यात्रा में पहली बार सिनेमा राष्ट्रवाद के यथार्थ को स्वीकार करने की दिशा में अग्रसर है। यही वर्तमान विवाद की मूल वजह है।
असल में वामपंथी एवं जिहादियों की सम्मिलित फौज ने सिनेमाई कला के नाम पर कई दशकों तक बरगलाया, लेकिन अब वे यथार्थ के निरूपण पर चीख-चिल्ला रहे हैं। चूंकि इन फिल्मों ने हिंदू प्रताड़ना, जिहादी षड्यंत्र जैसे राष्ट्रीय संकट को सीधे-सीधे प्रस्तुत किया, तो ‘गंगा-जमुनी तहजीब’ का यूटोपिया ढहने लगा है। इसलिए तुष्टीकरण की दुकान चलाने वालों का गुस्सा समझ आता है।
‘द केरला स्टोरी’ (2023) के निर्देशक सुदीप्तो सेन कहते हैं कि लोगों की नाराजगी इसलिए है, क्योंकि उन्होंने सच को उजागर कर दिया है। बीबीसी जैसी भारत विरोधी एवं कट्टरपंथ समर्थक मीडिया संस्थान ऐसी फिल्मों के लिए सत्ताधारी पार्टी की विचारधारा, मनगढ़ंत कहानियां, विचारधारा का हथियार और नया वैकल्पिक इतिहास बताने जैसे नए विशेषणों का प्रयोग कर रहे हैं।
‘तान्हाजी’, ‘सावरकर’, ‘रजाकार’ और ‘कश्मीर फाइल्स’ जैसी फिल्मों के विषय में यदि किसी समूह को लगता है कि ये हिंदुत्व की प्रचारात्मक क्रियाएं थीं, तो एक बात तय है कि वह हिंदुत्व को नहीं समझता। ‘हिंदुत्व’ भारत के जीवनचरित की प्राण वायु है, जैसा कि डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन लिखते हैं, ‘‘हिंदुत्व एक प्रवाह है, कोई स्थिर स्थिति नहीं, यह प्रक्रिया है परिणाम नहीं। यह एक परंपरा है, कोई स्थिर प्रकटीकरण नहीं।’’ गांधीजी के अनुसार, ‘‘हिंदुत्व सत्य के अनुसंधान की सतत साधना है और यदि आज यह मृतप्राय, निष्क्रिय, विकास के प्रतिकूल हो गया, तो इसका कारण है कि हम थक गए हैं और जैसे ही हमारी यह थकान दूर होगी, हिंदुत्व संपूर्ण विश्व पर एक ऐसी प्रखर दीप्ति के साथ छा जाएगा, जो संभवत: इसके पहले सभी के लिए अज्ञात होगा।’’ राजनीति से लेकर समाज व सिनेमा तक की राष्ट्रवादी धारा में गांधीजी की भविष्यवाणी के अनुरूप हिंदुत्व जाग रहा है, तो उसका विरोध नहीं, बल्कि सम्मान किया जाना चाहिए।
आगे मार्ग क्या हो?
इस सिनेमाई षड्यंत्र के विरोध का मार्ग तलाशना होगा, क्योंकि आधुनिक सभ्यता के युग में किसी कला-प्रतिरूप पर निषिद्ध कला न तो संभव है और न ही उचित। इसलिए सर्वप्रथम फिल्म प्रमाणन बोर्ड सख्त मानक बनाए ताकि सिनेमाई अराजकता पर रोक लगे और युवा पीढ़ी में नैतिक संस्कारों को सहेजा जा सके। प्रख्यात फिल्म निर्देशक व्ही. शांताराम का कहना था,
‘‘हमें यह देखना होगा कि हमारी फिल्में राष्ट्रीय जीवन के ताने-बाने से जुड़ी हुई हों और वे भारत की वास्तविकताओं को सही तरीके से गढ़ें और चित्रित करें।’’
दूसरे, राष्ट्रवादी विचारधारा को भी मजबूती से आगे बढ़ने होगा और वामियों-जिहादियों एवं सबसे बढ़कर पश्चिमी भोगवाद के विरुद्ध कलात्मक प्रतिरोध करते रहना होगा। तीसरे, सनातन धर्म की संस्कार परंपरा को अधिक प्रशंसित रूप में नई पीढ़ी को अपनाने के लिए प्रेरित करना होगा ताकि वह इंद्रिय नियंत्रण एवं चारित्रिक उन्नयन की महत्ता से अवगत हो सके।
यही राष्ट्रीय समाज के सुदृढ़ भविष्य का यथोचित मार्ग है, क्योंकि पश्चिम की चिंतन प्रणाली स्वयं को विज्ञानवादी तथा पदार्थ को ही चरम सत्य मानती है। भारतीय दर्शन के अनुसार,
इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्य परं मन:। मनसस्तु परां बुद्धिर्यो बुद्धे: परतस्तु स:।।
(श्रीमद्भगवद्गीता – 3/42)
अर्थात् इंद्रियां शरीर से परे हैं, इंद्रियों से परे है मन। मन से भी परे है बुद्धि और जो बुद्धि से भी परे है, वह है स्वयं ज्योति ज्ञान स्वरूप आत्मा।
यह धर्म एवं संस्कृति का मार्ग है। यही वह तात्विक सत्य है, जो सनातन धर्म से प्रेरित राष्ट्रीय चरित्र को संरक्षित करेगी और पश्चिमी भोगवाद एवं वामपंथी-मजहबी दुरभिसंधि से राष्ट्र तथा राष्ट्रीय समाज की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।
















टिप्पणियाँ