हाल ही में तमिलनाडु के नेता उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को नष्ट करने की बात की है और हालांकि उनके इस बयान पर बहुत विरोध हो रहा है, परन्तु वह अपने विचार पर कायम हैं। वह टिके हुए हैं। लोग अब उनको लेकर कह रहे हैं कि वह ईसाई हैं, इसलिए सनातन धर्म को कुचलने की बात कह सकते हैं। परन्तु यहाँ पर जिस विषय पर कम विचार हुआ है, वह इस पर कि आखिर उन्होंने यह वक्तव्य किस आयोजन में दिया था।
क्या वह कोई धार्मिक आयोजन था? यदि हाँ तो इस पर विवाद किया जा सकता है कि उनका धर्म क्या था क्या नहीं। परन्तु उन्होंने यह वक्तव्य जहाँ पर दिया था, वह आयोजन एक साहित्यिक मंच पर हो रहा था। जहां हो रहा था, वह कोई धार्मिक साहित्य का मंच नहीं था, जहां पर सनातन धर्म को नष्ट करने की बात की जाए या योजना बनाई जाए।
यह आयोजन किया गया था तमिलनाडु प्रोग्रेसिव राइटर्स एंड आर्टिस्ट एसोसिएशन अर्थात तमिलनाडु प्रगतिशील लेखक और कलाकार संघ द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या कोई साहित्यिक संगठन ऐसा कर सकता है? प्रगतिशीलता क्या होती है? और कथित प्रगतिशील साहित्य का क्या अर्थ है? क्या प्रगतिशीलता का अर्थ सनातन का विरोध है? और क्या कथित असमानता मात्र सनातन धर्म में पाई जाती है?
सबसे पहले बात प्रगतिशीलता की उस परिभाषा की, जो लगातार सनातन धर्म के विरुद्ध विषवमन करती हुई यह स्थापित करने का प्रयास कर रही है कि जो भी कमी है वह मात्र सनातन धर्म में है, क्योंकि सनातन स्वयं में सुधार का अवसर नहीं देता है और तमाम असमानताओं का वाहक है। प्रश्न यह उठता है कि आखिर यह परिभाषा आई कहाँ से है? इसके लिए हमें कुछ अतीत में जाना होगा। भारत में साहित्य सदा प्रगतिशील रहा है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण भक्तिकाल है। भक्तिकाल में तमाम संत कवियों ने कुरीतियों पर आवाज उठाई। सबसे बड़ा ग्रन्थ तो स्वयं रामचरितमानस ही कहा जा सकता है, जिसमें प्रभु श्री राम की जीवन गाथा के साथ तमाम कुरीतियों पर प्रश्न था और साथ ही एक मंत्र वहां से आया, जिसने स्वतंत्रता आन्दोलन को दिशा दी। वह मन्त्र था “पराधीन सपनेहूँ सुख नाहीं!”
एवं यह पंक्ति माता पार्वती के विवाह के समय पुत्री के लिए विह्वल माँ मैना ने कही कि
कत बिधि सृजीं नारि जग माहीं। पराधीन सपनेहुँ सुखु नाहीं॥
अर्थात एक धार्मिक ग्रन्थ में प्रगतिशीलता देखनी हो, तो यह पंक्तियाँ प्रगतिशीलता का चरम बिंदु हैं, जिसमें से एक पंक्ति कालांतर में स्वाधीनता संग्राम के समय प्रयोग किया गया। यह सनातनी साहित्य ही है, जिसमें किसी और सन्दर्भ की प्रगतिशीलता सन्दर्भ से परे आकर एक नया रूप प्राप्त कर लेती है।
फिर प्रगतिशीलता का अर्थ सनातन विनाश कैसे हो गया? इसके लिए हम चलते हैं उस काल खंड में जब वामपंथी मानसिकता अपना सिर अकादमिक जगत में उठा रही थी और भारत में अंग्रेजों का विरोध बढ़ रहा था। परन्तु साथ ही रचनाकार भारत के गर्व को लिख रहे थे और वह भारत जो सत्य है, सनातन है। वह अपने टूटे हुए मंदिरों पर लिख रहे थे, वह माँ भारती पर लिख रहे थे। ऐसे में वर्ष 1935 में मुल्क राज आनन्द, सज्जाद जहीर और ज्योतिर्मय घोष जैसे कुछ “प्रगतिशील” लेखकों ने कुछ ब्रिटिश कर्मियों के साथ मिलकर प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना की। आज जो हम सनातन विरोध का वट वृक्ष साहित्य में देखते हैं, उसका बीज 1935 में लंदन में रोपा गया था। सेन्ट्रल लंदन में नानकिंग रेस्टोरेंट में एक मैनिफेस्टो बनाया गया। जिसमें इस संघ के उद्देश्य एवं लक्ष्य लिखे गए थे। इसके लक्ष्य एवं उद्देश्य थे
“भारतीय समाज में आमूल-चूल परिवर्तन हो रहे हैं। हमारा मानना है कि भारत के नए साहित्य को आज हमारे अस्तित्व की बुनियादी समस्याओं – भूख और गरीबी, सामाजिक पिछड़ेपन और राजनीतिक अधीनता की समस्याओं से निपटना चाहिए। वह सब कुछ जो हमें निष्क्रियता, अकर्मण्यता और अकारण की ओर ले जाता है, हम उसे पुनः क्रियात्मक मानकर अस्वीकार कर देते हैं। वह सब कुछ जो हमारे अंदर आलोचनात्मक भावना जगाता है, जो संस्थानों और रीति-रिवाजों को तर्क की रोशनी में जांचता है, जो हमें कार्य करने, खुद को व्यवस्थित करने, बदलने में मदद करता है, हम प्रगतिशील के रूप में स्वीकार करते हैं’ (आनंद, पृष्ठ 20-21)।“
यद्यपि तत्कालीन हिन्दी साहित्य इन सभी दृष्टिकोण से लिख रहा था, परन्तु यथार्थवाद के नाम पर कलात्मक अभिव्यक्ति को पिछड़ा कहा जाने लगा और तर्क के आधार पर जो अब तक लिखा गया था, उसे नकार दिया गया और यहाँ तक कि जब सज्जाद लन्दन से भारत आए और कई ऐसे लोगों के साथ जब सज्जाद ने बैठकें की, जिनके साथ वह इस आन्दोलन को आगे बढ़ाना चाहते थे, उनमें से उन्होंने उन तमाम लोगों को छांट दिया, जो भारत की भारतीय छवि और भारत की हिन्दू पीड़ा को आगे लेकर जाना चाहते थे।
सोमनाथ पर उपन्यास लिखने वाले कन्हैया लाल मुंशी को लेकर उन्होंने लिखा था
”हमें यह स्पष्ट हो गया कि कन्हैयालाल मुंशी का और हमारा दृष्टिकोण मूलतः भिन्न था। हम प्राचीन दौर के अंधविश्वासों और धार्मिक साम्प्रदायिकता के ज़हरीले प्रभाव को समाप्त करना चाहते थे। इसलिए, कि वे साम्राज्यवाद और जागीरदारी की सैद्धांतिक बुनियादें हैं। हम अपने अतीत की गौरवपूर्ण संस्कृति से उसका मानव प्रेम, उसकी यथार्थ प्रियता और उसका सौन्दर्य तत्व लेने के पक्ष में थे। जबकि कन्हैयालाल मुंशी सोमनाथ के खंडहरों को दुबारा खड़ा करने की कोशिश में थे।”
यह दुर्भाग्य की बात रही कि इस प्रगतिशील आन्दोलन में उर्दू के वह तमाम चेहरे शामिल रहे जो अपनी मजहबी पहचान को फख्र से आगे लेकर बढ़ते रहे, जिनमें अल्लामा इकबाल एवं सब बुत गिरवाए जाने वाले लिखने वाले फैज़ शामिल थे।
कैसी विडंबना रही कि वह इकबाल जिन्होनें यह लिखा कि
क्या नहीं और ग़ज़नवी कारगह-ए-हयात में
बैठे हैं कब से मुंतज़िर अहल-ए-हरम के सोमनाथ!
प्रगतिशील लेखक संघ में रहे और जो कन्हैयालाल मुंशी सोमनाथ के बहाने हिन्दू पीड़ा को लिख रहे वह उन्हें प्रगतिशील लेखक संघ में सोमनाथ के खंडहरों को दुबारा जिंदा करने वाला बता दिया गया।
चूंकि रूसी साम्यवादी विचारों के आधार पर चलने वाला यह विचार तेजी से फैलता जा रहा था और धीरे-धीरे साहित्य का अर्थ ही यह रह गया कि कट्टरवाद का विरोध करके यथार्थवाद को लिखना है। परन्तु कट्टरवाद में केवल हिन्दू धर्म का ही विरोध रह गया था। हिन्दी के जो लेखक अपनी संस्कृति को आगे लेकर बढ़ रहे थे, उन्हें लेखक ही नहीं समझा जा रहा था। यहाँ तक कि 1938 में इलाहाबाद अधिवेशन में तो डॉ अब्दुल अलीम के इस लेख को लेकर भी विवाद हुआ कि हिन्दी और उर्दू की लिपि रोमन कर दी जाए। काका कालेलकर ने तीव्र प्रतिक्रिया करते हुए कहा था कि “मैं प्रगतिशील लेखक संघ से सहानुभूति अवश्य रखता हूँ किंतु यदि लेखक संघ ने रोमन लिपि के प्रस्ताव को अपना लिया तो उस स्थिति में मैं पूरे आन्दोलन का विरोध करूंगा।” परन्तु इस विचार को तब गति मिली जब इसे पंडित जवाहर लाल नेहरू का समर्थन प्राप्त हुआ। शैलेश जैदी अपने एक लेख में लिखते हैं कि
प्रगतितिशील लेखकों के सम्मेलन में जवाहर लाल नेहरू का सम्मिलित होना, एक असाधारण घटना थी। और साथ ही वह यह भी लिखते हैं कि पंडित नेहरू के भाषण का एक लाभ यह अवश्य हुआ कि वे लोग जो नेहरू जी के प्रति श्रद्धा रखते थे और प्रगतिशील सम्मेलनों में भाग लेने से कतराते थे, अब इस संस्था के लिए पर्याप्त नर्म पड़ गए।
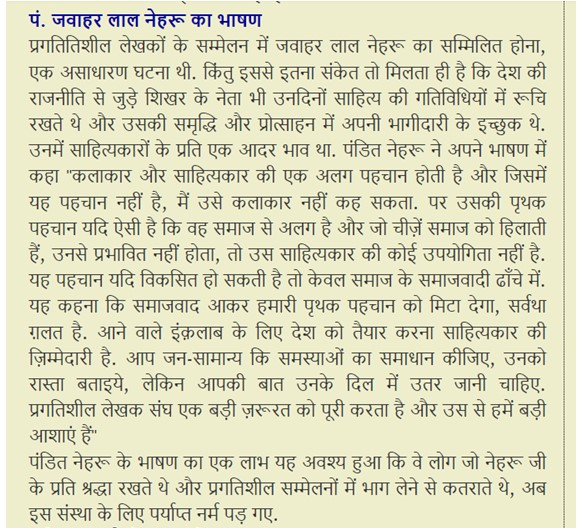
https://web.archive.org/web/20160305121647/http://yugvimarsh.blogspot.com/2008/06/blog-post_14.html
यह संगठन मुख्यत: साम्यवाद की सोच को लेकर ही समर्पित था। और लगातार उसके बाद से साहित्य का अर्थ कथित साम्यवाद रह गया। जिसने भी भारत के लोक या सनातन की बात की, उसे साहित्य से निष्कासित किया जाता रहा, बल्कि उसे साहित्यकार ही नहीं माना गया। कामायनी जैसी रचना रचने वाले जयशंकर प्रसाद से लेकर वर्तमान में महासमर जैसी रचनाओं को रचने वाले नरेंद्र कोहली तक तमाम उदाहरण देखे जा सकते हैं।
प्रगतिशीलता की इसी परिभाषा के साए तले ही यह आयोजन हुआ था, जिसमें सनातन को समाप्त करने का आह्वान था, क्योंकि वह भारत को देखते ही दूसरी दृष्टि से हैं। एक राजनेता के रूप में उदयनिधि ने क्या बोला, इससे महत्वपूर्ण यह है कि कथित प्रगतिशीलता का चोला पहने साहित्य समाज के एक बड़े वर्ग के विषय में क्या सोचता है और वह किस प्रकार प्रगतिशीलता की आड़ में इकबाल, फैज़ आदि को बढ़ावा देता है क्योंकि उसके लिए बुत की अवधारणा वही है जो इकबाल की है या फिर फैज़ की है।
उदयनिधि से लेकर खड़गे जूनियर तक हिन्दू धर्म में व्याप्त असमानता की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वह असमानता को नष्ट करना चाहते हैं, परन्तु न ही कथित प्रगतिशील साहित्य और न ही उदयनिधि और न ही जूनियर खड़गे को समानता और असमानता का अर्थ पता होगा। नेताओं की बात राजनीति करने वाले जाने, परन्तु क्या कथित प्रगतिशील साहित्य ने आज तक तमिलनाडु में ही वंचित वर्ग के ईसाइयों की उस पीड़ा के विषय में बात की होगी, जिसके विषय में वह लगातार बात करते आ रहे हैं अर्थात उनके साथ ईसाई पंथ में हो रहे भेदभाव की। जहां पर उन्हें न ही चर्च में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया जाता है और न ही यह कहते हुए उनका योगदान लिया जाता है कि उनकी परम्पराएं दूषित हो जाएँगी।
राजनीतिक व्यक्तियों से परे कथित साहित्य द्वारा राजनीतिक विचारधारा को थोपा जाना और साहित्य के नाम पर एक धर्म के प्रति वर्षों से विषवमन किये जाते रहना, मुख्य समस्या और बिंदु है, जिसका विरोध किया जाना चाहिए।


















टिप्पणियाँ