डॉ. क्षिप्रा माथुर ने ‘चक्रीय अर्थव्यवस्था’ के लिए कुदरत से तालमेल वाली जीवन शैली और उत्पादन के तौर-तरीके दोनों अपनाने से पूंजी के प्रवाह की बात करते हुए, चार साल पहले शुरू किए जल-आंदोलन की कहानी साझा की। उन्होंने जल-विरासत के जरिए परम्पराओं में समाए विवेक और विज्ञान के उदाहरण रखे। अपनी यात्राओं के दौरान देश के भिन्न इलाकों में समुदायों की समझ और कर्मठता से जीवित हुई नदियों की कहानी, किसानों की एफपीओ खड़ी होने से रुके पलायन और आर्थिक समृद्धि, तकनीक के इस्तेमाल से बारिश का पानी सहेजने के प्रयोग, परम्परागत काम में शोध शामिल करते हुए नए रोजगार सृजन और आजीविका सुनिश्चित करने की सोच का जिक्र किया
पर्यावरण कार्यकर्ता डॉ. क्षिप्रा माथुर ने कहा कि हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव कम करना जरूरी है। ऐसा न हुआ तो दुनिया को संभालना मुश्किल होगा। पाञ्चजन्य और आर्गनाइजर द्वारा दिल्ली में आयोजित पर्यावरण संवाद में स्वतंत्र पत्रकार क्षिप्रा माथुर ने विचार रखने के साथ जलांदोलन को लेकर प्रजेंटेशन भी दिया।

डॉ. माथुर ने कहा कि चार साल पहले पाञ्चजन्य के संपादक हितेश शंकर जी से चर्चा हुई कि सतत विकास के जो मसले हैं, उसमें जल सबसे अहम है। इसपर हम लोग कैसे काम कर सकते हैं? यह अनुभव हम सबको रहा है कि जनआंदोलन के बूते ही सारे बदलाव होते हैं। हमें महसूस हुआ कि जल आंदोलन की जरूरत है।
चक्रीय अर्थव्यवस्था को समझने के लिए हमारी पूरी सनातन परंपरा को समझना होगा। जहां से उद्भव हो, वहीं पर फिर समागम होता है। मिट्टी में मिल जाना होता है। इसमें कुदरत का तालमेल और सृजन भी है। हमारे पहाड़, नदी, मिट्टी, प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव को कम करना जरूरी है क्योंकि वह भावी दुनिया की जरूरत है, आबादी की जरूरत है। यह आगामी समय में इतनी बढ़ जाएगी कि उसको पूरा करने के लिए यदि हम अभी से सजग नहीं हुए तो हम शायद और बिगड़ी स्थिति में आ जाएंगे।
 क्षिप्रा माथुर ने कहा कि पाञ्चजन्य में प्रकाशित जलांदोलन कहानियों से एक बड़ा बदलाव आया है। यह बदलाव चक्रीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। इसमें महिलाओं की बड़ी भागीदारी है। महाराष्ट्र में 400 नदियां जीवित हुईं हैं। परंपरा के साथ भविष्य भी संवर रहा है। जयपुर में कचरे से सड़क बनी है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुधन की बड़ी भूमिका होती है। हमने गोचर भूमि खत्म कर दी। राजस्थान के जल-चेतन गांव ने गोचर जमीन को पशुओं के लिए संरक्षित किया है। आज राजस्थान के 50 गांव में गोचर भूमि को सहेजा जा रहा है। कुदरत बहुत पानी देती है, जिसे हमें सहेजना होगा। गांवों में जाकर हम पाते हैं कि हमें अभी बहुत कुछ करना है।
क्षिप्रा माथुर ने कहा कि पाञ्चजन्य में प्रकाशित जलांदोलन कहानियों से एक बड़ा बदलाव आया है। यह बदलाव चक्रीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। इसमें महिलाओं की बड़ी भागीदारी है। महाराष्ट्र में 400 नदियां जीवित हुईं हैं। परंपरा के साथ भविष्य भी संवर रहा है। जयपुर में कचरे से सड़क बनी है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुधन की बड़ी भूमिका होती है। हमने गोचर भूमि खत्म कर दी। राजस्थान के जल-चेतन गांव ने गोचर जमीन को पशुओं के लिए संरक्षित किया है। आज राजस्थान के 50 गांव में गोचर भूमि को सहेजा जा रहा है। कुदरत बहुत पानी देती है, जिसे हमें सहेजना होगा। गांवों में जाकर हम पाते हैं कि हमें अभी बहुत कुछ करना है।
नदियों का पुनर्जीवन
इसी तरह डॉ. माथुर ने जोधपुर के एक गांव के एक कुम्हार की कहानी साझा की। कुम्हारों की परंपरा मिट्टी से घड़े बनाना और पानी को सहेजना है। आईआईटी में इसकी जांच हुई। उसने घड़े में प्राकृतिक वाटर फिल्टर बनाया और आज इसका निर्यात हो रहा है। इस फिल्टर से मिलने वाले पानी के मानक को डब्लूएचओ प्रमाणित करता है। इस तरह हमारी परंपरा भी जीवित है, हमारा विज्ञान भी जीवित है, प्रकृति भी जीवित है और आजीविका भी जीवित है। कुदरत हमें भरपूर पानी देती है। हमें केवल इसको सहेजने की आवश्यकता है।
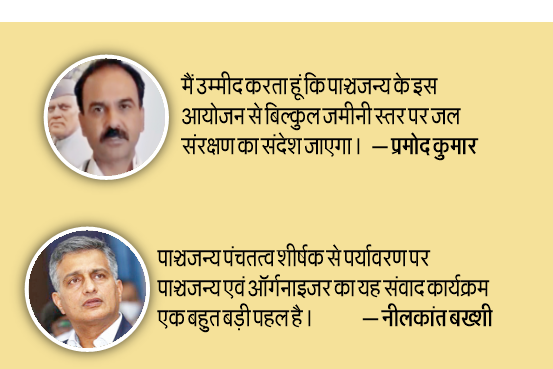
डॉ. माथुर ने अमेरिका की यूनिवर्सिटी के एक सांगल साहब की कहानी साझा की जिनके पेटेंट पर दुनियाभर की सड़कें बनती हैं। ये भारत आए और इन्होंने कहा कि अब मुझे पेटेंट का इस्तेमाल नहीं करना है और सभी मुझसे ले लीजिए। खेत का पानी खेत में, घर की छत का पानी घर में और सड़क का पानी जमीन में सहेज लें तो हमारा काफी काम ठीक हो जाएगा। यहां पर आकर इन्होंने प्रमाणित किया और एक पार्किंग स्लॉट पर सड़क बनाई जिसमें बरसात का पूरा पानी आएगा और जमीन में तिर जाएगा। ऐसी तकनीक है इनके पास।
सरहदी जैसलमेर आज अकेला ऐसा स्थान है जहां सांझी खेती का प्रयोग हो रहा है। इस गांव में लगभग 400 लोग रहते हैं। डॉ. माथुर जब इनके घर गईं तो पानी नहीं, बिजली नहीं। ये पाकिस्तान से आए विस्थापित लोग हैं। कमाई का कोई साधन नहीं है। घर के सामने से बिजली का खंभा जाता है परंतु चोरी नहीं करते। उनका कहना है कि अंदर श्रीकृष्ण जी की पूजा करते हैं तो बाहर चोरी कैसे कर सकते हूं। इसके बारे में हमें सोचना चाहिए।

















टिप्पणियाँ