|
भारत में कई कारण हैं अदालतों में मामले लटके रहने के। न्यायाधीशों की कमी से लेकर संसाधनों तक की कमी है। जिम्मेदारी के भाव की कमी सबसे चिंताजनक है
न्यायमूर्ति आर. एस. सोढ़ी
न्याय में देरी, न्याय न मिलने के बराबर होती है। समय पर मामलों का निपटारा कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जरूरी है, यह न्याय के मूलभूत अधिकार की गारंटी देता है। भारत की अदालतों में करीब 3 करोड़ मामले लंबित हैं। पुराने कानूनों को हटाने की बात की जाती है, लेकिन लंबित मामलों का संबंध क्या इन पुराने कानूनों से है? लंबित मामलों का सीधा संबंध प्रशासनिक विषयों से है, जिसमें न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका शामिल हैं। इसकी जिम्मेदारी न्यायपालिका और सरकार दोनों को लेनी होगी। बहुत से विशेषज्ञों के अनुसार 'फास्ट ट्रैक कोर्ट' इसका सरल उपाय हैं। चूंकि देश में जजों की कमी है इसलिए 'फास्ट ट्रैक कोर्ट' बना देने मात्र से इस समस्या का समाधान नहीं होगा।
'फास्ट ट्रैक कोर्ट' का क्या अर्थ है? देश में न्यायाधीशों की कमी है तो 'फास्ट ट्रैक कोर्ट' कैसे चलेगा। आपको न्यायाधीशों की कमी तो दूर करनी ही होगी। ढांचागत समस्याओं से निबटना पड़ेगा। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका समाधान निकलना ही पड़ेगा। साथ ही, कई अन्य कारक हैं जो मामलों में रुकावट पैदा करते हैं।
आपराधिक मामलों का ही उदाहरण लें तो जब पहली बार एफआईआर दर्ज होती है तो पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार करती है जो अभियुक्त होता है लेकिन जब तक उसका अपराध सिद्ध नहीं होता तब तक वह निर्दोष ही है। एफआईआर दर्ज हो जाती है तो पुलिस वैधानिक रूप से मामले की खोजबीन शुरू करने के लिए बाध्य हो जाती है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति को या तो पुलिस सुरक्षा में रखा जाता है या न्यायिक सुरक्षा में। मामले की जांच में प्र्र्रगति हो या न हो लेकिन आरोपी जेल में पड़ा रहता है। जांच पूरी हो जाती है तो पुलिस एक 'चालान' के माध्यम से जांच अदालत के सामने प्रस्तुत करती है। कई बार गलत चालान भरे जाने की संभावना बनी रहती है और मामला लटकता रहता है। उसके बाद यह मान लिया जाता है कि चालान में पर्याप्त सबूत या प्रमाण हैं और मामला अदालत में भेज दिया जाता है।
जब अदालत में मामले की सुनवाई की तैयारी होती है तो अभियुक्त अपने बचाव की सोचता है और अभियोजन पक्ष उसे कड़ी से कड़ी सजा देने की वकालत करता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि नागरिक जांच अधिकारी और अदालत की कार्रवाही के बीच झूलता रहता है। यह सिर्फ एक शुरुआत भर होती है। पूरी अभियोजन प्रक्रिया एवं साक्ष्य एकत्रित करने में तीन-चार वर्ष का समय लग जाता है। तब तक आरोपी लगातार जेल में ही रहता है। उसके नागरिक अधिकार निरर्थक हो जाते हैं। चंूकि सब कुछ अदालत में ही होता है इसलिए जाने-अनजाने अदालत के जरिए ही उसके मौलिक अधिकारों स्वतंत्रता और स्वछंदता का दमन होता रहता है। यदि आरोपी गरीब है तो उसका कष्ट और पीड़ा दोगुनी हो जाती है। न्याय दिलाने की प्रणाली में देरी के लिए किसी को भी जिम्मेदार न ठहराया जाना इसका बड़ा कारण है।
इसके साथ ही न्यायिक नियुक्तियों में बहुत बड़ी कमी भी न्याय में देरी का बड़ा कारण है। इसमें उच्च न्यायालयों की कमी है, जिनमें उत्तरदायित्व का अभाव है। चूंकि ज्यादातर नियुक्यिां उच्च न्यायालय की मांग पर होती हैं, सर्वोच्च न्यायालय के 'कोलेजियम' द्वारा यह प्रक्रिया की जाती है। लेकिन नियुक्तियों में पारदर्शिता का अभाव भी एक बड़ा कारण है। संसद ने एक कानून पारित किया है जिसे न्यायपालिका संवैधानिक रूप से अलग-थलग कर सकती है। संसद द्वारा सर्वसम्मति से 20 से अधिक राज्यों की सहमति लेकर एक कानून पारित हुआ है जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया है। यह और कुछ नहीं संविधान को 'हाइजैक' करने जैसी बात है। भारत के अलावा दुनिया में कहीं भी न्यायपालिका द्वारा स्वयं अपने यहां नियुक्ति करने का प्रावधान नहीं है।
हमें संविधान के दायरे में रहकर संतुलन स्थापित करने की जरूरत है। अंत में मामलों को रोकने और स्थगित करने का कारण मानव शक्ति की कमी नहीं कहा जा सकता। इसका एकमात्र समाधान यह है कि सारे मृत पड़े बोर्ड भंग कर दिए जाएं और जो न्यायाधीश कार्य नहीं कर रहा है, उसे तत्काल हटा दिया जाना चाहिए।
(लेखक दिल्ली उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं)










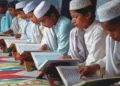

टिप्पणियाँ