|
एकात्म मानवदर्शन के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन मनीषियों में से एक थे, जिनका प्राचीन भारतीय ऋषि-मुनियों के चिन्तन, वसुधैव कुटुम्बकम् और सांस्कृतिक राष्टÑवाद पर अगाध श्रद्धा थी। उन्होंने आद्य शंकराचार्य, स्वामी विवेकानन्द, महर्षि अरविन्द जैसी विभूतियों की जीवन-दृष्टि को वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप ढालकर एकात्म मानवदर्शन का सिद्धान्त प्रतिपादित किया।
भारतीय जीवन दृष्टि
स्वतंत्रता के पश्चात् भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में उन्हें भारतीयता का उद्गाता माना जाता है। उन्होंने अद्वैत वेदांत की एकात्मता के आधार पर भारतीय जीवन दृष्टि का निरूपण किया। पंडित जी एक परम चेतना सत्ता को ही अखिल ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति का कारक तत्व मानते थे। सृष्टि उसकी इच्छा का परिणाम है। सृष्टि का उदय और विलय इसी में है। जड़-चेतन केवल नामभेद है। स्वामी विवेकानंद की भांति वे अध्यात्म को सर्वोपरि तत्व तथा विश्व को भारत की अनुपम देन मानते थे। व्यक्ति अथवा समाज से यदि अध्यात्म तत्व निकाल दिया जाए तो भारतीय जीवन दृष्टि का मूल तत्व ही विलोप हो जाएगा। वे मानव को मानव समाज से और परमात्मा से जोड़ने की कड़ी बताते हैं। यह नर से नारायण का मार्ग है। मानव में अनेक सद्गुणों-दया, सहानुभूति, परोपकार, दान, करुणा, ममता, नैतिकता आदि का भाव इससे ही उत्पन्न होते हैं। अत: भारतीयों में किसी की बात का विश्लेषण, सार अथवा चिंतन का आधार अध्यात्म माना गया है।
पंडित दीनदयाल जी स्वामी विवेकानंद तथा महर्षि अरविंद की भांति भारत को एक धर्म प्रधान देश मानते थे। धर्म भारत का प्राण है। वे धर्म का अर्थ ‘रीलिजन’ नहीं मानते थे। उन्होंने लिखा, ‘धर्म संघर्ष में नहीं, समझदारी में होता है। धर्म की सीख है कि एक-दूसरे से नाता समान स्वार्थ का नहीं, एक ही आत्मा का होता है।’ (देखें ‘पंडित दीनदयाल : विचार दर्शन’, खंड 3, पृ. 14) उनके अनुसार धर्म सबके लिए हितकारी होता है और यह मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करता है। जिन बातों से शक्तियों, भावनाओं, व्यवस्थाओं तथा नियमों की धारणा होती है वही धर्म है। धर्म धारणा के साथ-साथ सामंजस्य स्थापित करने का कार्य करता है। इसीलिए आचरण के नियम बनते हैं। ये नियम देश, काल, स्थिति एवं वस्तु के अनुसार भिन्न-भिन्न भी हो सकते हैं। कुछ नियम ऐसे होते हैं, जो सभी पर लागू होते हैं। (देखें, पंडित दीनदयाल : विचार दर्शन, खण्ड 5, पृ. 28-29)। उनका स्पष्ट मत है कि मंत्री या कोई भी व्यक्ति सार्वभौम नहीं हो सकता। सार्वभौमिकता केवल धर्म में निहित है। उनका यह भी कहना था कि धर्म की पुन: स्थापना किए बिना समाज सुखी एवं निर्भय नहीं होगा।
दीनदयाल जी संस्कृति को राष्ट्र की आत्मा मानते थे। उनका विश्वास जाति-पांति रहित राष्ट्र की रचना में था। वे मानव जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष अर्थात् चारों पुरुषार्थों को महत्वपूर्ण मानते थे। वे संस्कृति के मूल तत्व को मानव की प्रकृति, विकृति तथा संस्कृति का स्पष्टीकरण करके देते थे। एक स्थान पर उन्होंने लिखा,‘आज हमारे राजनीतिक जीवन में जो विकृतियां दिखाई दे रही हैं वे आसक्ति के कारण उत्पन्न हुई हैं। सेवा का स्थान अधिकार ने ले लिया है। जीवन के प्रति अतिशय अर्थवादी दृष्टिकोण के कारण भी अनेक विकृतियां उत्पन्न हुई हैं। मानवीय भावनाओं और जीवन मूल्यों के प्रति हमारा कोई महत्व नहीं रहा है। पैसा ही प्रतिष्ठा का आधार बन गया है। यह परिवर्तन भारतीय संस्कृति के आदर्शों के आधार पर ही हो सकता है। इस गौरवमयी संस्कृति की पुन: प्रतिष्ठापना से ही राष्ट्र जीवन में चतुर्दिक परिव्याप्त विकृतियों का शमन तथा निराकरण हो सकता है।’ (पं. दीनदयाल उपाध्याय, राष्ट्र जीवन की दशा, पृ.77)। उन्होंने अपने एक लेख में चिति का वर्णन किया। (देखें, राष्ट्रधर्म, नवम्बर-दिसम्बर, 1950)। इसका अध्ययन करते समय उन्होंने बद्रीशाह ठुनाधारिया की पुस्तक ‘दैशिक शास्त्र’ से प्रेरणा ली। उनका कहना है कि व्यक्ति की तरह राष्ट्र की भी अपनी आत्मा होती है और उसी कारण राष्ट्रीय एकता बनती है। वे उसे राष्ट्र की आत्मा या चिति कहकर पुकारते हैं। इसी चिति के कारण प्रत्येक राष्ट्र की संस्कृति को भिन्न व्यक्तित्व प्राप्त होता है। साहित्य, धर्म, कला, भाषा सभी इसी चिति की अभिव्यक्ति हैं। चिति के प्रकाश से राष्ट्र का अभ्युदय होता है। भारत का उत्थान करना है तो राष्ट्र की इस चिति या आत्मा के स्वरूप का दर्शन भारतीयों को कराना होगा। दीनदयाल जी समस्त रचना में मकड़ी के जालों को झाड़-पोंछ कर समाज को, युग के अनुकूल नए मोड़ देने को आवश्यक मानते थे। सामाजिक विषयों में उन्होंने न क्रांति का समर्थन किया और न ही यथास्थितिवाद का। (पं. दीनदयाल विचार दर्शन, खण्ड 1, पृ. 51)। उनका मार्ग था पुनर्जागरण का। वे जाति-पांति को नहीं मानते थे। वे सभी घटकों में परस्पर सामजस्य रखकर आगे बढ़ने को कहते थे। वे इसके लिए सच्चा व प्रभावशाली मार्ग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को मानते थे। (वही, पृ. 53)। वे समाज के पिछड़े, पीड़ित अंग को बराबर की सुविधाएं एवं संरक्षण देने के पक्ष में थे। केवल आरक्षण ही नहीं, बल्कि अन्य सामाजिक प्रश्नों के बारे में भी उनके विचार राजा राममोहन राय, डॉ. बी.आर. आम्बेडकर आदि सुधारकों के समान थे। पर उनका दुरुपयोग नहीं चाहते थे। वे जीवन के लक्ष्यों के लिए, उनकी प्राप्ति के लिए परिवार व्यवस्था को पुष्ट करना चाहते थे।
उन्होंने संस्कृति, धर्म, समाज के साथ भारतीय जीवन दृष्टि में आर्थिक जीवन की ओर भी विशिष्ट ध्यान दिया। अपने लेखों में राष्ट्र की अर्थनीति को परिभाषित ही नहीं किया, व्याख्यायित भी किया। उनके अर्थचिंतन पर ऐसे तेरह लेखों का संकलन हुआ है- (देखें, दीनदयाल उपाध्याय, ‘भारतीय अर्थनीति विकास की ओर’)। उन्होंने आर्थिक विकास के लिए व्यक्ति और समष्टि दोनों के उत्तरदायित्व की ओर ध्यान दिलाया है। उन्होंने एक स्थान पर लिखा ‘मनुष्य को भगवान ने पेट और हाथ दोनों दिए हैं। हाथ के लिए काम न हो तो पेट को अन्न होने पर व्यक्ति सुखी नहीं होता। नि:संतान स्त्री को जिस प्रकार अपने जीवन की अपूर्णता व्यथित करती रहती है, उसी प्रकार बेकार या पुरुषार्थहीन व्यक्ति भी अपूर्ण ही रहेगा।’(दीनदयाल उपाध्याय, एकात्म मानववाद, पृ. 65)। दीनदयाल जी समकालीन राजनीतिक-आर्थिक विचारधाराओं से पूरी तरह परिचित थे। उन्होंने बैंथम, जेम्स मिल तथा जे.एस. मिल के उपयोगितावादी सिद्धांत का भी गंभीर अध्ययन किया था। यह सिद्धांत अधिक से अधिक सुख और अधिक से अधिक लोगों की बात करता है। परंतु दीनदयाल जी भारतीय समाज रचना में सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय को ही उपयुक्त तथा सही मानते हैं। उन्होंने प्रचलित पूंजीवाद तथा समाजवाद अथवा कम्युनिज्म की चिंतनधारा का भी गंभीर अध्ययन किया था। उन्होंने सभी प्रचलित चिंतनधाराओं का विश्लेषण किया। यह सही है कि 1917 की रूसी वोल्शेविक क्रांति से लेकर आज तक रूस का इतिहास अनेक विफलताओं का इतिहास सिद्ध हुआ है। वे इस विचार प्रणाली को न केवल अपूर्णता का द्योतक, अपितु भयानक परिणामों का जन्मदाता भी मानते थे। (देखें, सतीश चंद्र मित्तल, साम्यवाद का सच, पृ. 150-165)। दीनदयाल जी ने सभी प्रचलित चिंतनधाराओं के अध्ययन के पश्चात् पुरुषार्थ चतुष्ट्य को भूलकर, भारतीयों के आयातित विचारधाराओं में फंसने की बात कही। साम्यवादी तथा समाजवादी विचारों की वकालत अनेक कांग्रेसी नेता भी करते हैं। नेहरू जी उससे मुक्त न थे। निष्कर्ष रूप में वे कहते हैं कि लोकतंत्र और मार्क्स प्रणीत समाजवाद का एक ही म्यान में रहना असंभव है। (पं. दीनदयाल विचार दर्शन, खंड 5, पृ. 45)।
भारतीय राष्ट्रवाद
सन् 1947 में भारत का विभाजन तथा उससे उत्पन्न अनेक समस्याओं, सत्ता की होड़, आंतरिक कलह, प्रादेशिक राष्ट्रवाद, अंग्रेजों द्वारा पढ़ाया विकृत इतिहास, पश्चिम से आयातित राष्ट्रवाद का स्वरूप, भारतीय राष्ट्रवाद की शास्त्रीय, भावात्मक दृष्टि आदि का दीनदयाल जी ने विस्तृत विश्लेषण तथा विवेचन किया है।
दीनदयाल जी भारत के संदर्भ में न पाश्चात्य राजनीतिक राष्ट्रवाद को मानते हैं और न मार्क्सवाद के नकारात्मक राष्ट्रवाद और न कांग्रेसी भ्रामक राष्ट्रवाद को। वे भारत को एक प्राचीन राष्ट्र कहते थे, जो प्राचीनकाल से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के रूप में इतिहास दृष्टि में जाना जाता है। वे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को भारतीयता की अभिव्यक्ति मानते थे। उनका मानना था कि परिवार का विस्तार ही राष्ट्र और सृष्टि है। वे मनुष्य के चार अवयवों (शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा) की भांति-राष्ट्र के भी चार घटकों (भूमि, जनता, संकल्प और धर्म) को जीवनमान सत्ता मानते थे। राष्ट्र का शरीर वहां की भूमि और जनता राष्ट्र का मन होता है। एक साथ जीवन-यापन के संकल्प की चेतना राष्ट्र की बुद्धि होती है। वे राष्ट्र वृद्धि को धर्म मानते हैं। धर्म के अनुसार देश के सामूहिक लक्ष्यों और आदर्शों को उन्होंने राष्ट्र की आत्मा कहा। इसका दूसरा नाम उन्होंने चिति रखा। चिति को राष्ट्र का मूलभूत ‘स्व’ कहा तथा राष्ट्र निर्माण में चिति का विशेष महत्व बताया। दीनदयाल जी का कहना था कि भारतीय राष्ट्रीयता का आधार ‘भारत माता’ है, केवल भारत नहीं। ‘माता’ शब्द हटा दीजिए तो भारत जमीन का केवल एक टुकड़ा रह जाएगा। वे विशुद्ध राष्ट्रवाद से ही देश का उत्थान संभव मानते थे। (बलवीर पुंज, ‘एकात्म मानववाद की उपयोगिता,’ दैनिक जागरण, 21 सितम्बर, 2004)। दीनदयाल जी ने राष्ट्रीय जीवन का आधार ‘सांस्कृतिक एकता’ को माना है। वे इसे आर्य, भारतीय, वैदिक या हिन्दू संस्कृति कहने में आपत्ति नहीं मानते थे, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से एक-दूसरे का पर्याय मानते थे। वे मानते थे कि इस संस्कृति का विकास इस भूमि में ‘हिन्दू’ नाम से पहचाने जाने वाले प्राचीन समाज से ही किया गया, जो अनादिकाल से हिन्दू राष्ट्र के रूप में विकसित हुआ। (दीनदयाल विचार दर्शन, खण्ड पांच, पृ. 20) वे भारतीय राष्ट्रीयता को ही हिन्दू राष्ट्रीयता मानते थे।
दीनदयाल जी भारत विभाजन के लिए मुस्लिम अलगाव की नीति, अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति तथा कांग्रेस की विकृत धारणा और तुष्टीकरण की नीति को उत्तरदायी मानते थे। दीनदयाल जी ने भारत और पाक महासंघ बनाने के लिए डॉ. राममनोहर लोहिया के साथ 12 अप्रैल, 1964 को संयुक्त विज्ञप्ति भी प्रसारित की थी।
उन्होंने अंग्रेजों द्वारा प्रसारित तथा कांग्रेस द्वारा मान्य इस धारणा का खण्डन किया कि भारत कोई नया राष्ट्र है या भारत एक बनता हुआ राष्ट्र है। वे पाश्चात्य देशों की भांति भारत राष्ट्र को किन्हीं विशेष परिस्थितियों के क्रियाकलापों का परिणाम नहीं मानते थे। संक्षेप में कहें तो दीनदयाल जी ने राष्ट्रीय चिंतन को अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान दिया था। उनका कहना था, ‘राजनीति के लिए राष्ट्रीयता नहीं, राष्ट्रीयता के पोषण के लिए राजनीति होनी चाहिए। वह राजनीति जो राष्ट्र को क्षीण करे, अवांछनीय रहेगी।’(देखें ‘राष्टÑ जीवन की दिशा’, पृ.-49)
एकात्म मानववाद
दीनदयाल जी के एकात्म मानवदर्शन को उनके मूलगामी रचनात्मक चिंतन की ही अनमोल निष्पति कहा गया है। (विचार दर्शन, खण्ड दो, पृ. 9)। इस गहन चिंतन में उन्होंने न केवल मानव और मानव के बीच के सम्बंधों का वर्णन किया है, बल्कि मानव और मानवेतर प्रकृति के पारस्परिक एकात्म सम्बंध का भी समावेश किया है। (वही, पृ. 6)। वस्तुत: यह उनके ‘मानव जीवन तथा सम्पूर्ण प्रकृति के एकात्म संबंधों का दर्शन’ है। (वही, पृष्ठ 11)
उनका यह चिंतन राष्ट्र तक सीमित न रहकर उससे भी आगे जाता है। इसमें व्यक्ति, समष्टि से लेकर परमेष्टि तक का सम्पूर्ण विचार किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई गांधी जी के अंत्योदय तथा दीनदयाल जी के एकात्म मानवदर्शन को एक-दूसरे का पर्याय मानते थे। (सुधाकर राजे, ‘डेस्टीनेशन ट्रिब्यूट टू दीनदयाल उपाध्याय : दीनदयाल जी एण्ड गांधी जी’, पृ 15)। चन्द्रशेखर ने इसे दीनदयाल जी का ‘सामाजिक ध्येय’ बताया है। (वही चन्द्रशेखर का लेख ‘इन द गैलेक्सी आॅफ सीयर्स एण्ड सेजेज’, पृ. 23) जिसमें दीनदयाल जी की कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा या स्वार्थ नहीं है। नानाजी देशमुख ने इसे भारतीय राजनीति को उनकी देन माना है। (द मैन एड द थॉट, पृ. 32)।
दीनदयाल जी ने व्यक्ति के सुखों तथा कर्तव्यों के साथ परिवार की विस्तृत चर्चा की है। उन्होने इसे समष्टि के साथ जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी बताया। परिवार के साथ कुटुम्ब की भी चर्चा की। इसके साथ समाज का चिंतन किया। उन्होंने इस प्रश्न पर गंभीर चितंन भी किया कि व्यक्ति और समाज में कौन श्रेष्ठ है। उन्होंने विचार किया कि क्या व्यक्तियों ने मिलकर, इकट्ठे होकर समाज का निर्माण किया। वे पाश्चात्य जगत की उपरोक्त धारणा को स्वीकार नहीं करते। वे इसे ऐतिहासिक दृष्टि से भी गलत मानते हैं। उनके अनुसार समाज कोई क्लब, ज्वाइंट स्टॉक कम्पनी या सहकारी संस्था नहीं है। वे पाश्चात्य जगत में प्रचलित हाव्स, लॉक, रूसो का ‘सोशल कान्टैÑक्टर थ्योरी’ को पूर्णत: अस्वीकार करते थे। उनका मत था कि समाज प्रकृति से होने वाली एक जीवमान निर्मिति है। (विचार दर्शन, खण्ड दो, पृ, 63)।
व्यक्ति और समाज के बीच सम्बंधों का विवेचन करते हुए वे कहते थे कि हम अपने व्यक्तिगत हित व अहित का विचार करते हुए भी समाज के हित और अहित का विचार करें, यही उचित व्यवस्था है। व्यक्ति का हित व समाज का हित दोनों में कोई विरोध या संघर्ष नहीं है। कुछ लोग उनसे पूछते थे कि आप व्यक्तिवादी हैं या समाजवादी? वे उत्तर देते थे कि वे व्यक्तिवादी भी हैं और समाजवादी भी। उनका कहना था, ‘हम व्यक्ति की उपेक्षा नहीं करते और समाज का विचार भी ओझल होने नहीं देते। हमारी मान्यता है कि व्यक्ति के बिना समष्टि की कल्पना करना भी असंभव है और समष्टि के बिना व्यक्ति का मूल्य शून्य है।’ व्यक्ति, परिवार, कुटुम्ब, समाज की भांति उन्होंने राष्ट्र, विश्व और सम्पूर्ण मानव का अपने एकात्म मानववाद में गहन चिंतन किया। विद्वानों ने दीनदयाल जी को युगान्तकारी चिंतन से समाज के नवचैतन्य जाग्रत करने का अनूठा अवदान माना है। वास्तव में यह मानव सम्बंधों एवं भारतीय चिंतन को व्याख्यायित करता है। आर्थिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय मुद्दों पर उनका एकात्म मानववाद का विचार कालजयी है। उनके एकात्म मानववाद दर्शन में भारत के प्राचीन चिंतन ‘सर्वे भवन्तु सुखिन:’, ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’आदि की ही प्रतिष्ठापना हुई है।
डॉ. सतीश चन्द्र मित्तल

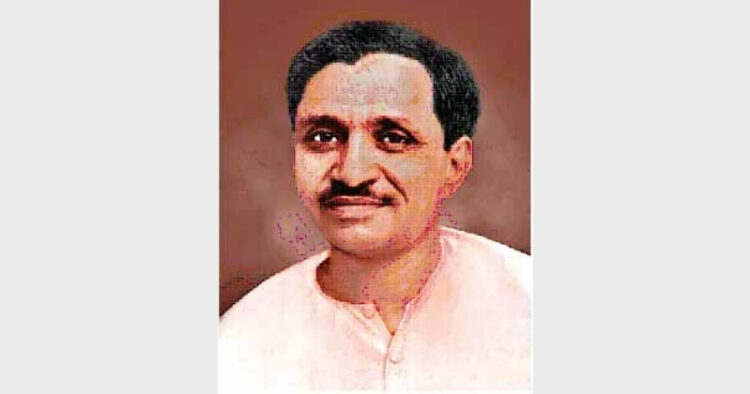










टिप्पणियाँ