|
20वीं शताब्दी के इतिहासकारों में अग्रणी नाम आर.सी. मजूमदार (1888 से 1980) ने भारत में स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास नामक तीन खंडों की पुस्तक के प्राक्कथन में स्पष्ट किया है कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का वास्तविक इतिहास विशेषकर युवा पीढ़ी तक जाना चाहिए। मजूमदार ने लिखा, सच बोलना चाहिए चाहे इसमें कितने भी विवाद क्यों न हों। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि आपसी समझ और सहमति का ठोस ढांचा झूठे इतिहास और राजनीतिक बुनियाद पर खड़ा नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार श्रेष्ठ इतिहासकार पी. वी. काणे (1880-1972), जिन्हें भारत के श्रेष्ठ नागरिक सम्मान भारतरत्न से सम्मानित किया गया था, ने 1953 में वाल्टेयर (अब विशाखापत्तनम) में भारतीय इतिहास कांग्रेस में अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा था कि वर्ष 1947 से पहले का इतिहास बच्चों को न पढ़ाना बेहतर है बजाय इसके कि हम उन्हें इतिहास का नष्ट-भ्रष्ट संस्करण पढ़ायें। घटनाओं को सच्चाई के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सत्य को उसके कारणों सहित विश्लेषित किया जाना चाहिए। सत्य को उसके विस्तार के साथ वर्णित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उसमें किसी प्रकार के पूर्वाग्रह की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इतिहास के अध्ययन में घटनाओं का चिंतन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दुर्भाग्य से भारतीयों ने स्वाधीनता संघर्ष में जो विशिष्ट भूमिका निभाई वह उस इतिहास वर्णन में कहीं दिखाई नहीं पड़ती।
गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर भी टुकड़ों में इतिहास अध्ययन की प्रणाली से दुखी थे और भारतीय सभ्यता के अपूर्ण एवं अस्पष्ट विवरणों से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने इस प्रकार के इतिहास पढ़ाये जाने पर रोष व्यक्त किया था। 1903 में बंगला भाषा में भारतवर्ष का इतिहास नामक एक निबंध में उन्होंने लिखा कि जब तक भारतवर्ष को भारतवर्ष के नजरिये से नहीं देखा जायेगा तब तक सब निरर्थक है। हमारे बचपन से ही हमें वह सब समझाया जाता है जो हमें अपना नहीं लगता।
भारत के नौनिहालों को इतिहास में पक्षपात और पूर्वाग्रहों को ही पढ़ाया जाता रहा है। उस इतिहास से आपको यह महसूस होगा कि उस समय भारतवर्ष कहीं भी अस्तित्व में नहीं रहा होगा। उस समय मानो सारी दुनिया में पठानों और मुगलों की पताकाएं उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम में लहरा रही थीं। हमें परग्रही जीवों तक के अस्तित्व को मानना पड़ता है। तो स्वाभाविक है कि भारत देश भी रहा होगा। अन्यथा इन सब थपेड़ों के बीच में कबीर, गुरुनानक, चैतन्य व तुकाराम जैसे श्रेष्ठ चिंतकों को किसने जन्म दिया। इसका मतलब यह नहीं कि उस समय केवल दिल्ली और आगरा ही अस्तित्व में थे, जब काशी और नवद्वीप जैसे पावन स्थल थे। जीवन की तरंग जो वास्तविक भारत में दिखायी पड़ती है वह कहां से प्रवाहित हुई? निसंदेह ठोस प्रयत्नों को मथ कर ही सामाजिक परिवर्तन की भावना जागृत हुई लेकिन हमारी इतिहास की पाठ्यपुस्तक से ऐसे सब अध्याय गायब हैं। वास्तविक भारतवर्ष को हमारी इतिहास की पाठ्यपुस्तकों और पूरी अध्यापन प्रक्रिया में विधिवत् रूप में रखा ही नहीं गया।
हमारे ज्यादातर इतिहासकारों ने वषार्ें तक भारत को उसी नकली चश्मे से देखा और प्रस्तुत किया, एक राजनीतिक दल विशेष के नेताओं के योगदान को ही चमकाया। व्यवस्थित दस्तावेज और घटनाक्रम को उन्होंने पूरी तरह से नकार दिया। विशेषकर स्वाधीनता के संघर्ष को व्यवस्थित एवं समग्र रूप में वर्णित करने के सभ्यता के इतिहास को कभी व्यवस्थित नहीं किया गया। भारत के विभिन्न क्षेत्रों और सामाजिक क्षेत्रों को महत्व प्रदान नहीं किया और देश की एकता में उनके योगदान को कहीं संयोजित नहीं किया गया। भारत के इतिहास का वर्णन विशेषकर स्वातंत्र्योत्तर काल व्यक्ति विशेषों द्वारा लिखाया गया जो कि भारत का एकपक्षीय विवरण देते हैं। आज भी तमिल के प्रभावी शासक राजेन्द्र चोल-प्रथम पर खुली चर्चा नहीं होती जिनका आरमदा कानून न केवल भारतीय महासागरीय क्षेत्र में बल्कि समुद्र से दूर दक्षिण में चीन महासागर के मलक्का स्ट्रेट तक भी व्यापार को नियंत्रित करता था। स्वतंत्रता के बाद विशेषकर हमारे इतिहास में सभ्यताओं की उपलब्धि और उनके आधार पर भू-रणनीतिक योजना के लिए कोई आधार तैयार नहीं किया गया जबकि चीन जैसे देश स्वयं को सभ्यतायुक्त राज्य घोषित करने साथ अपने इतिहास को उसी हिसाब से निर्मित करते रहे हैं। जबकि भारत में इतिहास के कथित अनुसंधाता और पाठ्यक्रम निर्माता मार्क्स के विचारों को ग्रहण करते हैं जो भारत के सभ्यता प्रवाह और उसके परीक्षण एवं समझदारी को। यह केवल विखंडन, संशय और संकीर्णता को बढ़ावा देता है।
भारत के इतिहास अध्ययन क्रम में जब हम स्वतंत्रता संघर्ष में विभिन्न क्षेत्रों और नेताओं के योगदान का परीक्षण करते हैं तो पाते हैं कि इसमें पूर्वाग्रहपूर्ण तरीका अपनाया गया है। 1800 से 1801 ई. के बीच भारत विशेषकर दक्षिणी क्षेत्र में ईस्ट इण्डिया कंपनी के विरुद्ध कितने विद्रोह हुए उनका विस्तृत अध्यापन कहां होता है। इसी प्रकार स्वतंत्रता संग्राम में पूर्वोत्तर भारत के योगदान की क्यों अनदेखी की गयी और ब्रिटिश काल से पूर्व इस क्षेत्र की जो सभ्यता वाली पहचान और उपलिब्ध रही उस पर क्यों कुछ सामग्री नहीं मिलती।
देशभर में इसका अध्यापन या अनुसंधान क्यों नहीं होता? क्यों आज एक नौजवान शिक्षार्थी केरल में बैठकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में रानी मां गाइदिन्ल्यू के योगदान को अथवा सेंग-खासी आंदोलन को या सभ्यता और आध्यात्मिक प्रेरणादायी ऐसे ही अन्य आंदोलनों को नहीं जानता? ठीक इसी प्रकार पश्चिमी खासी हिल्स में अध्ययन कर रहे एक युवा दिमाग को जतीन्द्रनाथ मुखर्जी (बाघा जतिन) के बलिदान के विषय में मालूम नहीं होता जो इसी प्रकार स्वदेशी आंदोलन के समय क्रांतिकारी कवि सुब्रह्मण्यम भारती के योगदान को कितनी जगह पढ़ाया जाता है? कितने लोगों को यह पता है कि वी.ओ. चिदम्बरम पिल्लई ने एक स्वदेशी 'स्टीम नेवीगेशन कंपनी' बनायी थी जिसने जहाजरानी क्षेत्र में ब्रिटिश एकाधिकार को चुनौती दी थी, बाद में उन पर देशद्रोह के कई आरोप लगाये गये और उन्हें जेल में डाल दिया गया।
स्वदेशी आंदोलन में भगिनी निवेदिता की भूमिका को कितने कम लोग जानते हैं। विश्वविज्ञान समुदाय के बीच में भारत की वैज्ञानिक चेतना को पुनर्स्थापित करने के लिए उन्होंने भारतीय वैज्ञानिकों जगदीश चंद्र बोस और प्रफुल्ल चंद्र राय को अभूतपूर्व सहयोग दिया। भारत की आजादी के शुरुआती दिनों में आर.सी. मजूमदार ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जो प्रामाणिक इतिहास लिखने और अंकित करने का प्रयास किया था उसमें उनको कई व्यवधान झेलने पड़े। वह इसलिए कि मजूमदार कुछ चिन्हांकित नेताओं को चमकाने और दूसरे वर्ग के ठोस नेताओं को अनदेखा करने से मना कर दिया। उन्हें उस समय के सत्तारूढ़ दल के नेताओं से भयानक राजनीतिक विरोध और दबाव झेलना पड़ा था। राजनीतिक प्रतिबद्धता और वैचारिक संबद्धता दरबारी इतिहास लेखकों का एक विशेष गुण रहा है। उनका प्रयास भारत में आयातित विचारधारा स्थापित करना रहा। ये लोग अच्छे संसाधन संपन्न समूह द्वारा पोषित और हमेशा पश्चिमी शिक्षाविदों के नकलची रहे। इनका लक्ष्य था भारत को, भारतीय समाज को परस्पर संघर्षरत और अस्थिर बनाना, इसके लिए उन्होंने इतिहास के अध्ययन को बूरी तरह प्रभावित किया। अपने सभी तर्कों को प्राथमिक राजनीतिक उद्देश्य समकालीन परिदृश्य में संशय का निर्माण करना था और अंतिम रूप में भारत के सभ्यतामूलक छवि को प्रस्तुत करने का विखंडन करना। इसलिए इतिहास के ऐसे सभी प्रकरण, जो भारत के स्वावलंबी सभ्यता और किसी व्यक्तिगत अथवा आंदोलन को भारतीय सभ्यता के आलोक में प्रेरणादायी सिद्ध करते हुए उसकी अनदेखी कर दी। ऐसे तथ्यों और साक्ष्यों को ढूंढने के बजाय उनकी उपलब्धियों को मिटा दिया गया। और तो और जो पश्चिमी अध्येता भारत की सकारात्मक खोज में लगे हुए थे और अपने शोध के आधार पर खोजें कर रहे थे उनपर भी ज्यादा चर्चा नहीं की गयी। ऐसे पश्चिम के प्रबुद्ध अध्येताओं में कई नाम जैसे- जॉन वुड्रोफ, स्टेला, क्रामरिश्च, सिलवेन लेवी, लूई रेनो अथवा जीन फिलोजेट आज व्यावहारिक रूप से अनसुने ही रह गये हैं। वास्तव में मौन रूप में यह एक बहुत बड़ा सुनियोजित षड्यंत्र कहा जा सकता है। भारत के मुख्यधारा के शैक्षणिक एवं शैक्षिक पाठ्यक्रम में अतीत में ऐसे चिंतकों और उनके चिंतन के विरुद्ध दुष्प्रचार किया गया। मार्क्सवादी इतिहासकारों अथवा उनके पोस्टर लेखकों ने सत्ता के बल पर इतिहास लिखने के कई अवसर पाये। ये लेखक भारतीय सभ्यता से और यहां के मूल्यों से अपरिचित थे। ये केवल उस राजनीतिक लकीर पर चले जिसने उन्हें उपकृत् ा किया। अपेक्षानुसार जैसा वे चाहते थे वैसा सत्तातंत्र ने उनसे लिखवाया। चार दशक तक भारत की जनता से लिए गए राजस्व के बूते सरकारों ने मनपसंद-मनगढ़ंत इतिहास की पुस्तकें खूब लिखवायीं।आज इतिहास लेखन और उसके अध्यापन पर बहस होनी आवश्यक है। गत एक डेढ़ वर्ष से प्रयास शुरू हुए हैं कि अपने प्रेरणादायी प्रतीकों को पुन: ढूंढा जाय और उनकी पुनर्व्याख्या की जाये। कई हाशिये पर रखे गये व्यक्तित्वों को प्रतिष्ठा दी जाए जिन्होंने अपनी सभ्यता और मूल्यों के प्रति विशिष्ट भूमिका निभाई। ऐसे ऐतिहासिक प्रकरणों, घटनाओं और उपलब्धियों को युवा पीढ़ी के समक्ष लाने की आवश्यकता है। जो पूर्वाग्रह और विखंडन की प्रणाली भारत के इतिहास लेखन में अपनायी गई उसको चुनौती दी जाए, प्रश्न उठाए जाएं और बौद्धिक योद्धाओं को भारत के स्वावलंबी एवं स्वाभिमानी सभ्यता मूलक आधार की कडि़यों को जोड़ा जाए।
ऐसे कदम उठाने से हम अपनी सभ्यता को पुन: विश्वमंच पर स्थापित करने में सफल होंगे और इसके साथ ही इसका जो दूसरा स्वरूप आयेगा वह होगा स्वतंत्रता का दूसरा आयाम-बुद्धि की स्वतंत्रता, स्वयं की स्वतंत्रता और स्वयं के आलंबन की स्वतंत्रता। -डॉ. अनिर्वाण गंागुली, जाने-माने अध्येता, लेखक और स्तंभकार डॉ. अनिर्वाण गांगुली वर्तमान में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी शोध अधिष्ठान, नई दिल्ली के निदेशक हैं।

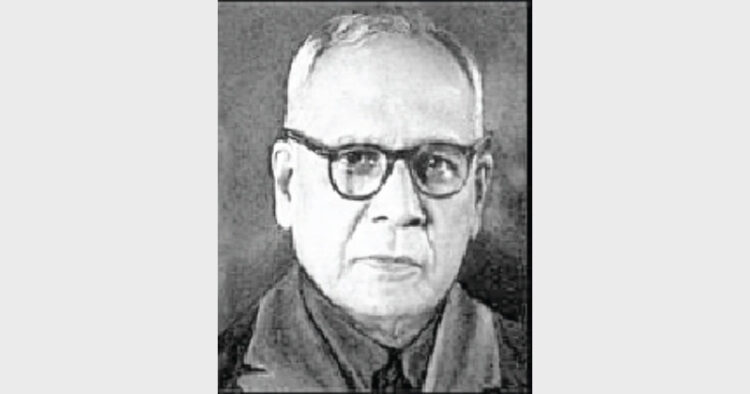










टिप्पणियाँ