ऑपरेशन सिंदूर के रूप में भारतीय सेना ने पहलगाम में उद्दंड और निर्लज्ज पाकिस्तानी सैन्य तंत्र के पाले-पोसे आतंकियों के वीभत्स और घृणास्पद कुकृत्यों का मुंहतोड़ जवाब दिया है। इस सन्दर्भ में रामचरितमानस की चौपाई ‘विनय न मानत जलधि जड़, गए तीनि दिन बीति। बोले राम सकोप तब, भय बिनु होइ न प्रीति!” को अब लगातार उद्धृत किया जा रहा है। इस सन्दर्भ को और खंगालें तो स्पष्ट है कि शांति की स्थापना के लिए शक्ति प्रयोग की अवधारणा भारतीय दर्शन के मूल में पौराणिक काल से चली आ रही है। ब्रह्मा-विष्णु-महेश की त्रिमूर्ति की परिकल्पना सृजन, पालन और संहार के प्रतीक के रूप में की गई थी। सृजन और संहार।

विंग कमांडर (से.नि.)
भय और प्रीति का ऐसा संतुलन और सामंजस्य किसी अन्य संस्कृति में कम ही दिखाई पड़ता है। भारतीय चिंतन और दर्शन ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ की भावना को युगों से महत्व देता आया है, जबकि अन्य मत—पंथों में किसी में तलवार की नोक पर कन्वर्जन का सन्देश देते हुए विधर्मियों को वाजिबुल क़त्ल क़रार दिया गया तो किसी ने पंथ प्रचार के लिए विश्व के कोने-कोने में आदिम जातियों को साम, दाम, दंड, भेद नीति का शिकार बनाया। इसके विपरीत भारत ने विश्व को हमेशा शांति और प्रेम का ही सन्देश दिया। शाक्य राजवंश के राजकुमार सिद्धार्थ ने जिस दिन सुखी जीवन का रहस्य शांति, प्रेम और सह-अस्तित्व में ढूंढ़ निकाला, उसी दिन से उन्हें प्रबुद्ध सिद्धार्थ या बुद्ध कहा जाने लगा।
बौद्ध भिक्षुओं ने श्रीलंका से लेकर तिब्बत, चीन, जापान तक अपने पंथ का प्रसार किया तो लाखों लोगों ने इस नए पंथ अपनाया किन्तु इस पांथिक क्रांति में रक्त की एक बूंद भी नहीं गिराई गई। इसके बहुत बाद दक्षिण पूर्व एशिया के जावा, सुमात्रा, बाली आदि क्षेत्रों में दक्षिण भारत के चोल राजवंश के राजेंद्रचोल प्रथम के शासन काल में हिन्दू धर्म एवं संस्कृति का अद्भुत विस्तार हुआ। लेकिन यह पूरी प्रक्रिया केवल सांस्कृतिक एवं व्यापारिक संबंधों पर आधारित रही। सदियों से भारत सकल विश्व में ‘जियो और जीने दो’ का पावन सन्देश देता रहा है। दुर्भाग्य से इस सराहनीय सन्देश का प्रसार करते-करते हम अतिक्षमाशीलता का शिकार हो गये। भारतीय चिन्तन पश्चिम से आयातित ‘एक थप्पड़ पड़ने पर दूसरा गाल आगे कर देने के भ्रामक प्रचार में आकर यह भूल गया कि पौरुषहीन प्रेम एक शिखंडी के लिए मान्य हो सकता है, किसी आत्म सम्मानी समाज या देश के लिए नहीं।
विष्णुपुराण के अनुसार भगवान शिव का संहारक होना अज्ञान के अंधेरे के नाश के लिए आवश्यक था, अतः वे विष्णु के माथे के तेज से प्रकट हुए थे। सृजन और संहार दोनों प्रकृति के चक्र के दो आयाम हैं। शक्ति के बिना संहार संभव नहीं। इसीलिए हिन्दू धर्म की त्रिवेणी वैष्णव, शैव और शाक्य धाराओं में बहती है। शाक्य चिन्तन ने मातृशक्ति को सर्वोच्च शक्ति माना, लेकिन उसका स्वरूप शिशु कृष्ण को गोद में लेकर “हलरावे, दुलरावे, मल्हावे, जोई-सोई कछु गावे” वाली यशोदा की छवि वाला नहीं रहा। दुर्गा सप्तशती में मातृशक्ति के सभी स्वरूपों की वन्दना की गई है। मातृदेवी लक्ष्मी, दया और श्रद्धा के रूप में सब प्राणियों में विराजमान हैं, लेकिन “सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता” कह कर इस सत्य को उकेरा गया है कि शक्ति का वरदान अन्य वरदानों से कम नहीं।
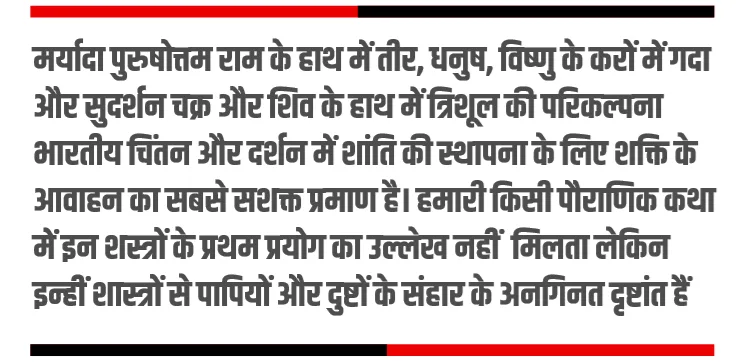
दया और श्रद्धा के साथ शक्ति का आवाहन करने वाला दुर्गा मंत्र हमारी सम्यक् दृष्टि को परिभाषित करता है। शक्ति का संतुलन न्यायसंगत और समृद्ध समाज ही नहीं, विश्वबंधुत्व के हवन की भी आवश्यक सामग्री है। व्यावहारिक स्तर पर शक्ति कई स्वरूपों में प्रकट होती है।
शक्ति राष्ट्रीय और अंतर दोनों स्तरों पर सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक और सैन्य संतुलन बनाने के लिए आवश्यक है। तभी विश्व के पालनहार चतुर्भुज विष्णु भगवान् के चारों हाथ शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुशोभित हैं। संकेत स्पष्ट है-साधुजनों के लिए पद्म की कोमलता प्रायोजित है तो दुष्टजनों के विनाश के लिए शंखनाद के बाद गदा और चक्र का प्रयोग। गीता में भगवान् कृष्ण ने घोषणा की है कि वे युग-युगांतर तक साधुओं के परित्राण और दुष्टों के विनाश के लिए आते रहेंगे। आज के परिप्रेक्ष्य में भगवान विष्णु के शास्त्रों को देखें तो लगेगा कि सुर्दशन चक्र ने आधुनिक युद्धकला में दूर से ही शत्रु का विनाश करने वाले प्रक्षेपास्त्र की और गदा ने समीप आ चुके शत्रु के साथ ‘क्लोज़ कम्बैट’ में प्रयुक्त होने वाली स्वचालित कलाश्निकोव राइफल की नींव रख दी थी।
शक्ति की भारतीय अवधारणा चाणक्यनीति के श्लोकों के अध्ययन से और भी स्पष्ट होती है। “कश्चाहं का च मे शक्तिरिति चिन्त्यं मुहुर्मुहः, ध्रुवाणि तस्य नश्यन्ति चाध्रुवं नष्टमेव हि !!” इसमें चाणक्य ने जो कहा उसी की आधुनिक व्याख्या है “ इटर्नल विजिलेंस इज़ द प्राइस ऑफ़ फ्रीडम।” चाणक्य के अनुसार, “ अपनी शक्ति और पहचान के बारे में बार-बार सोचो। जो कुछ निश्चित है वह नष्ट हो जाता है और जो अनिश्चित है वह भी नष्ट हो जाता है।” आज से सात- आठ दशक पहले जो भारतीय नेतृत्व चीन के साथ पंचशील समझौता करके भाईचारे के झूठे आश्वासन से छला गया। वह चाणक्य की इस नीति को भूल गया था, ‘नारीषु न मित्रेषु न राज्ञि न च बांधवेषु! न विश्वासों न कर्तव्यः सर्वात्रास्ति विपत्तिदाः” अर्थात् स्त्री, मित्र, राजा और संबंधियों पर भी विश्वास न करें। हर जगह विपत्ति का खतरा है।
इस तरह आवश्यकता पड़ने पर भारतीय दर्शन एवं धर्म में शक्ति के प्रयोग को सर्वथा उचित माना गया है। लेकिन दीवार पर सिर मारते जाना शक्ति का प्रयोग नहीं बल्कि बुद्धि का दुरुपयोग होता है। भारतीय पौराणिक गाथाओं में तरह तरह के दृष्टांत बताते हैं कि युद्ध और प्रेम में सब कुछ वांछित या उचित होता है। इसे आधुनिक युग की अवधारणा मानने वालों को भस्मासुर की पौराणिक कथा बताना आवश्यक है। शिव जी अपने भोलेपन में एक असुर को वरदान दे बैठे कि वह जिसके सिर पर हाथ रख देगा, वह भस्म हो जाएगा।
परिणाम प्रत्याशित निकला। वह राक्षस शिव जी के सिर पर हाथ रखकर उन्हें ही भस्म करने पर आमादा हो गया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी स्वरूप में प्रकट होकर भस्मासुर को अपने नृत्य से इतना आकर्षित किया कि वह उनकी मुद्राओं की नक़ल करते हुए नाचने लगा और स्वयं अपने सिर पर हाथ रखते ही भस्म हो गया। भस्मासुर की कथा यह सिखाती है कि हमारी परंपरा में शक्ति का प्रदर्शन करते हुए यदि सफलता संदिग्ध लगे तो छल कपट भी त्याज्य नहीं हैं। पावन लक्ष्य की प्राप्ति धर्मानुकूल डगर पर चलकर संभव न हो तो उसके लिए आपत्ति काल में धर्म की राह पकड़ने में संकोच नहीं होना चाहिए।
शक्ति की अवधारणा वस्तुतः शांति की आराधना का ही एक स्वरूप है। रक्तपिपासा को भारतीय चिन्तन में सदा से घृणास्पद माना गया है। शांतिप्रियता शक्ति की अवधारणा की नींव पर चोट नहीं करती, उसे और ग्राह्य बनाती है। यह निष्कर्ष वैज्ञानिक सोच पर आधारित है। सन् 1687 में महान यूरोपीय वैज्ञानिक आइज़क न्यूटन ने अपने शोध पत्र को ‘प्रिंसिपल्स ऑफ़ नेचुरल फिलोसोफी’ नाम दिया था। अतः उसमें प्रतिपादित नियमों को प्राकृतिक दर्शन के रूप में देखना चाहिए।
यह दर्शन हमारी आज की नीतियों को ही प्रतिबिम्बित करता है। न्यूटन ने गति के तीन नियम बताये थे। पहले नियम के अनुसार जब तक कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाए, प्रत्येक वस्तु गतिशील या स्थिर रहेगी। दूसरे नियम के अनुसार वस्तु पर लगने वाला बल ( फ़ोर्स) उसके द्रव्यमान ( मास) और त्वरण ( एक्सिलिरेशन) के बराबर होता है। और तीसरे के अनुसार हर क्रिया की एक समान और विपरीत क्रिया होती है। भारत—पाकिस्तान के रिश्तों और ऑपरेशन सिंदूर के सन्दर्भ में देखें तो दोनों देश अपनी सामान्य पड़ोसियों जैसी स्थिति में आराम से रहते यदि उसका पड़ोसी भारत के अभिमान और अस्मिता पर बल लगाने की मूर्खता न करता।
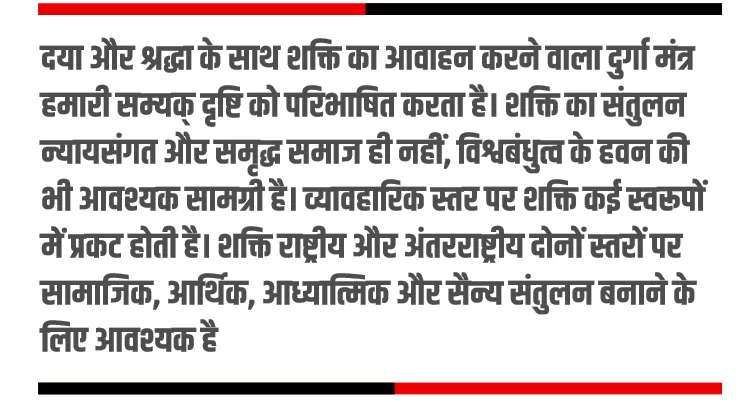
वह तो दूसरा नियम भी भूल गया कि लगाया गया बल उसकी साइज़ और हैसियत का रहने के कारण अपने से कहीं अधिक बड़े, बलशाली और समृद्ध भारत को हिला नहीं सकेगा। भारत ने अंत में उसे न्यूटन का तीसरा नियम भी सिखा दिया। पहलगाम के वीभत्स आतंकी कृत्य पर प्रतिक्रिया दिखाकर भारत ने उसके फ़ौजी हुक्मरानों के होश ठिकाने लगा दिए। एक बार फिर सिद्ध हो गया कि शांति की स्थापना के लिए भारत शक्तिप्रयोग से न कभी हिचका है, न आगे हिचकेगा। प्रधान मंत्री की दहाड़ कहती है कि आतंक के खिलाफ मुंहतोड़ जवाब “संभवामि युगे-युगे” रहेगा।
महाकवि निराला की कालजयी कविता “राम की शक्तिपूजा’ हमारी अवधारणा को बहुत सुंदर ढंग से प्रतिबिम्बित करती है। उसकी निम्न पंक्तियां दोहराए बिना यह लेख अधूरा रहेगा। प्रभु राम ने जब अधम रावण के ऊपर शक्ति को कृपालु देखा तो विचलित होकर बोल पड़े- “निज सहज रूप में संयत हो जानकी प्राण, बोले आया न समझ में यह दैवी विधान, रावण अधर्मरत भी अपना, मैं हुआ अपर, यह रहा शक्ति का खेल समर शंकर शंकर!’’
‘बोले विश्वस्त कंठ से जाम्बवान रघुवर, विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण,
हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर!
रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त।
शक्ति की करो मौलिक कल्पना करो पूजन, छोड़ दो समर यदि नहीं सिद्धि हो रघुनन्दन!
मर्यादा पुरुषोत्तम राम के हाथ में तीर, धनुष, विष्णु के करों में गदा और सुदर्शन चक्र और शिव के हाथ में त्रिशूल की परिकल्पना भारतीय चिंतन और दर्शन में शांति की स्थापना के लिए शक्ति के आवाहन का सबसे सशक्त प्रमाण है। हमारी किसी पौराणिक कथा में इन शस्त्रों के प्रथम प्रयोग का उल्लेख नहीं मिलता लेकिन इन्हीं शास्त्रों में पापियों और दुष्टों के संहार के अनगिनत दृष्टांत हैं। यही है शांति के लिए शक्ति की हमारी अवधारणा।


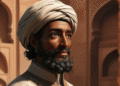

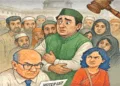













टिप्पणियाँ