लोकमंथन के चौथे संस्करण का उद्घाटन 22 नवंबर को हैदराबाद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। वर्ष 2016 में भोपाल से शुरू हुआ आयोजन आज सही अर्थों में ‘लोक’ के आचार-विचार-व्यवहार और व्यवस्थाओं को धरातल पर उतारते कर्मशीलों का जीवंत मेला बन चुका है। कहना चाहिए कि भारतीय संस्कृति के औदार्य, समझ और वैश्विक आयामों को सामने रखता यह आयोजन आज विविध विषयों और कलारूपों की प्रस्तुति के साथ भारत का सबसे प्रमुख सांस्कृतिक मंच है।

लोकमंथन का इस वर्ष का विषय था ‘लोकावलोकनम्’ यानी समग्र वैश्विक दृष्टिकोण। यह स्वदेशी संस्कृति और परंपराओं पर आधारित समाजों के जीवन के गहन विश्लेषण के लिए खुलने वाली खिड़की है। पहले लोकमंथन ने भारतीय मन की उपनिवेशवादी जकड़ से मुक्ति पर विमर्श शुरू किया, जिसका विस्तार रांची और गुवाहाटी में आयोजित सम्मेलनों में हुआ। स्वदेशी कलाओं की गरिमा को पुनर्स्थापित करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण पहल रही। यहां स्वदेशी ज्ञान, परंपराएं, कृषि, धातु विज्ञान, स्वास्थ्य और जलवायु जैसे विषयों पर सामयिक तर्क दृष्टि से ‘मंथन’ हुआ।
इस वर्ष के लोकमंथन में विश्व की कल्पना एक ‘नीड़’ यानी घोंसले के रूप में की गई। मुस्लिम ब्रदरहुड की संकीर्ण सोच से उलट, यह विश्व के लिए सहोदर भाव रखने वाले विस्तृत सह-अस्तित्व का आंगन था, जिसमें आर्मेनिया, इंडोनेशिया और अन्य देशों के सांस्कृतिक प्रतिनिधियों ने परम्पराओं के रंग भरे। रस्मी आयोजनों की लीक से हटकर, इस तरह के आयोजनों को हम समाज की सांस्कृतिक अंगड़ाई कह सकते हैं।
याद रखिए, अंगड़ाई केवल भंगिमा नहीं है। यह आलस्य को तजकर अपने कर्म के लिए उठ खड़े होने की तैयारी भी है। लोकमंथन भारतीय समाज की इसी तैयारी का नाम है। भारतीय समाज अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ा रहकर अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए कमर कस रहा है। विशेष बात यह है कि सदियों तक आक्रांताओं के आक्रमणों, औपनिवेशिक सत्ता की जंजीरों और बाद में वैचारिक हमलों से वह पस्त या निढाल नहीं है। भाग्यनगर में तीन दिन भारतीय ‘लोक’ की यही जिजीविषा, जीवंतता और भविष्य की तैयारी दिखी।
वैसे, लोकमंथन जैसे आयोजन को भारत में सांस्कृतिक मार्क्सवाद और सांस्कृतिक संघर्ष के आयाम से भी देखना चाहिए। भारत, जिसकी पहचान ही उसकी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर, गहन आध्यात्मिकता और मजबूत पारिवारिक व्यवस्था से जुड़ी है, 20वीं सदी में एक वैचारिक चुनौती से प्रभावित हुआ। यह चुनौती पश्चिम से आयातित सांस्कृतिक मार्क्सवाद की थी। इस विचारधारा ने समाज के पारंपरिक ढांचों को तोड़ने और नए सामाजिक मूल्य गढ़ने का प्रयास किया। इसका प्रभाव केवल अकादमिक जगत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि हमारे परिवार, धर्म और सांस्कृतिक परंपराओं पर भी पड़ा।

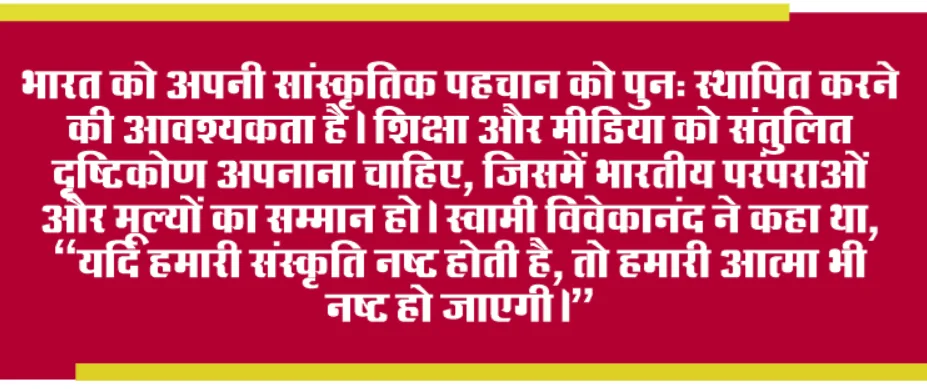 सांस्कृतिक मार्क्सवाद मूल रूप से पश्चिमी विचारकों, विशेषकर एंटोनियो ग्राम्शी और हर्बर्ट मार्कुसा के विचारों से प्रेरित था। ग्राम्शी ने लिखा कि समाज को बदलने के लिए उसकी सांस्कृतिक नींव को कमजोर करना आवश्यक है। भारत में इस विचार को विश्वविद्यालय, मीडिया और राजनीति में जड़ेंजमा कर बैठे कथित इतिहासकारों और बुद्धिजीवियों के माध्यम से प्रचारित किया गया। स्वतंत्रता के बाद भारतीय शिक्षा और अकादमिक क्षेत्र में इस विचारधारा ने जगह बनाना शुरू किया। स्कूलों और विश्वविद्यालयों में भारतीय परंपराओं को ‘पुरानी’ और ‘रूढ़िवादी’ के रूप में प्रस्तुत किया गया। भारतीय इतिहास को तोड़-मरोड़ कर लिखा गया, जिसमें हिंदू धर्म और उसके योगदान को सीमित रूप में दिखाया गया। इसके विपरीत, विदेशी विचारों और जीवनशैली को ‘आधुनिकता’ और ‘प्रगतिशीलता’ के प्रतीक के रूप में स्थापित किया गया। इसके पीछे और कुछ नहीं, बल्कि हिंदुत्व और पारिवारिक व्यवस्था को निशाना बनाने की रणनीति थी।
सांस्कृतिक मार्क्सवाद मूल रूप से पश्चिमी विचारकों, विशेषकर एंटोनियो ग्राम्शी और हर्बर्ट मार्कुसा के विचारों से प्रेरित था। ग्राम्शी ने लिखा कि समाज को बदलने के लिए उसकी सांस्कृतिक नींव को कमजोर करना आवश्यक है। भारत में इस विचार को विश्वविद्यालय, मीडिया और राजनीति में जड़ेंजमा कर बैठे कथित इतिहासकारों और बुद्धिजीवियों के माध्यम से प्रचारित किया गया। स्वतंत्रता के बाद भारतीय शिक्षा और अकादमिक क्षेत्र में इस विचारधारा ने जगह बनाना शुरू किया। स्कूलों और विश्वविद्यालयों में भारतीय परंपराओं को ‘पुरानी’ और ‘रूढ़िवादी’ के रूप में प्रस्तुत किया गया। भारतीय इतिहास को तोड़-मरोड़ कर लिखा गया, जिसमें हिंदू धर्म और उसके योगदान को सीमित रूप में दिखाया गया। इसके विपरीत, विदेशी विचारों और जीवनशैली को ‘आधुनिकता’ और ‘प्रगतिशीलता’ के प्रतीक के रूप में स्थापित किया गया। इसके पीछे और कुछ नहीं, बल्कि हिंदुत्व और पारिवारिक व्यवस्था को निशाना बनाने की रणनीति थी।
इसीलिए हिंदुस्थान की पारंपरिक पारिवारिक व्यवस्था, जो नैतिकता और सामूहिकता पर आधारित है, सांस्कृतिक मार्क्सवाद का प्रमुख निशाना बनी। इसकी रणनीति सरल थी—उन मूल्यों पर हमला करना, जो हिंदू समाज को एकजुट रखते हैं। पारिवारिक ढांचे को तोड़ने के लिए भारतीय परिवारों को पितृसत्तात्मक और दमनकारी बताया गया। फिल्मों, साहित्य और मीडिया में परिवार को एक ‘बोझिल’ संरचना के रूप में दिखाया गया, जबकि पश्चिमी जीवनशैली को ‘स्वतंत्रता’ का प्रतीक बनाया गया। इसी तरह, भारतीय धर्म, आध्यात्मिक परंपराओं को ‘अंधविश्वास’ करार दिया गया। धार्मिक अनुष्ठानों और त्योहारों को ‘अनुचित’ और ‘आधुनिक समय के अनुकूल नहीं’ बताया गया। शिक्षा में भारतीय संस्कृति की आलोचना और वामपंथी विचारधारा का प्रसार किया गया। इससे नई पीढ़ी में अपनी जड़ों के प्रति अविश्वास और विदेशी विचारों के प्रति आकर्षण बढ़ा।
कुल मिलाकर सांस्कृतिक मार्क्सवाद ने 3-आर यानी रेसिस्ट (विरोध), रिजेक्ट (अस्वीकार) और रिबेल (विद्रोह) की रणनीति अपनाई, जो समाज को उसकी संस्कृति से काटने का घातक तरीका है। युवा पीढ़ी को यह सिखाने के तरीके गढ़े गए कि पारंपरिक मूल्यों का विरोध करना ‘प्रगतिशीलता’ है। धीरे-धीरे यह विरोध धार्मिक रीति-रिवाजों से लेकर परिवार की भूमिका तक फैला। साथ ही, पारंपरिक मान्यताओं और परंपराओं को पूरी तरह अस्वीकार करने का संदेश दिया गया, जिससे युवा अपनी सांस्कृतिक जड़ों से दूर होते चले गए, जबकि सक्रिय विद्रोह के माध्यम से इन परंपराओं और संरचनाओं को चुनौती दी गई। इसका उदाहरण वे आंदोलन हैं, जिनमें धार्मिक परंपराओं या सांस्कृतिक मानदंडों को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया।
यह रणनीति न केवल भारतीय समाज के लिए, बल्कि इसके नैतिक और भावनात्मक ढांचे के लिए भी खतरनाक साबित हुई। इससे परिवार, जो भारतीय समाज का आधार है, कमजोर हुआ। इसका परिणाम सामाजिक अलगाव, नैतिक पतन और मानसिक स्वास्थ्य संकट के रूप में सामने आया। दूसरा, राष्ट्रीय एकता पर हमला किया गया। परिणामस्वरूप सांस्कृतिक विभाजन ने जातीय और धार्मिक संघर्षों को जन्म दिया। राष्ट्र के प्रति समर्पण और गर्व को ‘रूढ़िवादी’ बताया गया। भारतीय संस्कृति पर भी हमला हुआ, जो सहिष्णुता, विविधता और सामूहिकता की प्रतीक है। इसके कारण नई पीढ़ी अपनी सांस्कृतिक धरोहर से कटती गई।
भारत को अपनी सांस्कृतिक पहचान को पुन: स्थापित करने की आवश्यकता है। शिक्षा और मीडिया को संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जिसमें भारतीय परंपराओं और मूल्यों का सम्मान हो। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, ‘‘यदि हमारी संस्कृति नष्ट होती है, तो हमारी आत्मा भी नष्ट हो जाएगी।’’
यह समय है कि हम अपनी जड़ों की ओर लौटें, अपनी संस्कृति को समझें और इसे न केवल संरक्षित करें, बल्कि गर्व के साथ अगली पीढ़ी को सौंपें। केवल तभी हम इस वैचारिक संघर्ष को जीत सकते हैं।
प्रस्तुत है भाग्यनगर से प्राप्त हुए लोकमंथन के अमृत से सज्ज पाञ्चजन्य की यह विशेष प्रस्तुति
@hiteshshankar

















टिप्पणियाँ