कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है एवं यह साहित्य ही है जो जनाकांक्षाओं को सरकार के सामने रखता है। साहित्य का भारत में सदा से ही उच्च स्थान रहा है क्योंकि यह भक्ति साहित्य ही था, जिसने मुग़ल काल में अत्याचारों का सामना करने के लिए जनमानस को तैयार किया था। यह उस काल में रचे गए श्री रामचरित मानस का प्रभाव ही है कि लोगों को मानसिक बल अभी तक प्राप्त हो रहा है।
परन्तु जब से आधुनिक या कहें कि कथित प्रगतिशील साहित्य का भारत में आगमन हुआ, अचानक से ही प्रभु श्री राम साहित्य से त्याज्य हो गए, इतना ही नहीं, प्रभु श्री राम का नाम लेने वाले लोगों को भी साहित्य में अछूत या पिछड़ा घोषित किया जाने लगा। जिन्होनें प्रभु श्री राम की कथा को अपने हिसाब से तोडा मरोड़ा, उन्हें प्रगतिशील कहा गया तथा जिन कन्हैया लाल मुंशी जैसे साहित्यकारों ने सोमनाथ की पीड़ा को अपने शब्दों और रचनाओं में उकेरा तो उन्हें पिछड़ा कहा गया।
अर्थात प्रगतिशील लेखक संघ के गठन के बाद साहित्य की दिशा में परिवर्तन होना आरम्भ हुआ, और वर्ष 2022 में वहां पर आ पहुंचा, जहाँ पर वह जनता के दर्द से एकदम अलग हो गया और एक एजेंडे पर ही जैसे चलने लगा। कई अवसर ऐसे आए, जब मुख्यधारा का साहित्य जनता से परे होकर राजनीतिक अल्पसंख्यकवाद के एजेंडे पर चलने लगा। भारत के बहुसंख्यक समाज की पीड़ा से उसे कोई मतलब नहीं रहा। ऐसा भी नहीं था कि इस साहित्य को अल्पसंख्यकों से कोई लगाव है, दरअसल उसे उस एजेंडे से लगाव था, जिसके बहाने वह भारत की आत्मा पर प्रहार कर सकता था।
साहित्य में बहुसंख्यक पीड़ा के गायब होने का परिणाम यह हुआ कि जो कार्य प्रशासनिक स्तर पर दंगे आदि के बाद उठाए गए, उन्हें भी कथित अल्पसंख्यकों पर अत्याचार घोषित किया जाने लगा और साथ ही उनमें मारे गए हिन्दुओं के प्रति संवेदना शून्य की कगार पर पहुँच गयी।
ऐसा ही एक मामला अभी हाल में गुजरा है। और वह है श्री रामनवमी पर हुए प्रभु श्री राम की शोभायात्रा के दौरान हुए दंगे। जब दंगे हुए तो हिन्दुओं की शोभायात्रा को यह कहते हुए निशाना बनाया गया कि वह मुस्लिम इलाके में से निकल रहे थे और डीजे बजा रहे थे।
ऐसे में वह प्रगतिशील लेखक वर्ग, जो इन शब्दों पर दाद देता नहीं चूकता था कि “किसी के बाप का हिन्दोस्तान थोड़ी न है!” एकदम चुप ही नहीं हुआ बल्कि वह कहीं न कहीं इस बात पर बल देता हुआ घूमा कि आखिर हिन्दुओं को मुस्लिमों के इलाके के बीच जाने की जरूरत क्यों पड़ी? हिन्दू ही मुस्लिमों के इलाके में जाकर उन्हें भड़काते हैं! यह बहुत ही अजीब बात है क्योंकि एक तरफ तो यही लेखक वर्ग है जिसकी कल्पना में यह होता है कि हिन्दुओं के मंदिरों में सभी को धर्म से परे प्रवेश मिलना चाहिए तो वहीं वह लोग मुस्लिमों के लिए अलग इलाके का राग अलापते हुए दिखाई दिए।
पिछले वर्ष जब श्री हनुमान जयंती के अवसर पर दिल्ली में दंगे हुए थे, तो एकबारगी लोग हैरान रह गए थे कि क्या ऐसे भी दिन आ गए हैं कि हिन्दू अपने देवों की शोभा यात्रा भी नहीं निकाल सकते? क्या उन्हें अब यह तक अधिकार नहीं कि वह वर्ष में एक बार आने वाली अपने हनुमान जी की जयंती पर शोभायात्रा नहीं निकाल सकता? इसके साथ ही दोहरी पीड़ा तब और हुई जब यह देखा गया कि विमर्श में और प्रगतिशील लेखकों के विमर्श में बहुसंख्यकों की पीड़ा और उन पर फेंके जाने वाले पत्थरों का विरोध न होकर इस बात का विरोध था कि आखिर मुस्लिम इलाकों में जाकर उन्हें भड़काने की आवश्यकता क्या थी?
उन्हीं दिनों दंगाइयों पर कड़े कदम उठने आरम्भ हुए। इन क़दमों में एक बहुत बड़ा कदम था बुलडोज़र द्वारा अवैध निर्माण को ध्वस्त करना। परन्तु जैसे ही यह आरम्भ हुए वैसे ही एक बहुत बड़ी हलचल मच गयी। और कविताएँ लिखी जाने लगीं। दुर्भाग्य की बात यही थी कि इन कवियों में से शायद ही किसी ने बहुसंख्यक समाज की धार्मिक स्वतंत्रता पर हुए हमलों पर लिखा था, परन्तु बुलडोज़र पर लिखने के लिए वह तत्काल ही तैयार हो गए।
हालांकि ये सभी कविताएँ समालोचन पत्रिका के अप्रैल के अंक में आई थीं, तो यह हो सकता है कि यह कविताएँ बुलडोज़र के उस सन्दर्भ में उतनी न हों, जितनी वह पूरे वृहद परिदृश्य में थीं, परन्तु यह भी दुर्भाग्य है कि एक भी कविता उन बुलडोज़र के विरुद्ध नहीं कही जाती है, जो बुलडोज़र तमिलनाडु एवं केरल आदि में मंदिरों पर चलते हैं। या फिर जब बंगाल में चुनावों के बाद हिंसा हुई थी, तब भी ये तमाम प्रगतिशील लोग चुप बैठे थे।
परन्तु जैसे ही दंगाइयों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने लगे वैसे ही इनकी कविताएँ आने लगीं और “बुलडोज़र” शीर्षक से तमाम कविताएँ कई कवियों ने लिख डालीं।
राजेश जोशी, अरुण कमल। विजय कुंअर, विष्णु नागर, लीलाधर मंडलोई। अनूप शेती, बोधि सत्व। स्वप्निल श्रीवास्तव जैसे कवियों ने बुलडोज़र पर कविताएँ लिखीं।
इन सभी ने जब कविताएँ लिखीं तो जाहिर है कि प्रशासन को कठघरे में खड़ा किया, न कि उन्हें, जिन्होनें अवैध निर्माण किए थे। विजय कुमार ने लिखा कि बस्तियां ही अवैध नहीं, साँसें भी अवैध थीं।
बोधिसत्व ने बुलडोज़र पर कविता लिखते हुए लिखा कि
एक चूड़ी की दुकान में
एक सिंदूर की दुकान में
अजान के समय घुसा वह बुलडोज़र की तरह!
उसने कहा मैं चकनाचूर कर दूंगा वह सब कुछ जो मुझसे सहमत नहीं!
जो मेरे रंग का नहीं
उसे मिटा दूंगा!
और यह कविता अवश्य ही जहांगीरपुरी में हुई कार्यवाही के बाद लिखी है क्योंकि बोधिसत्व ने लिखा कि देश की राजधानी में भी हाहाकार की तरह था वह, एक अजीब सी प्रतिस्पर्धा सी लग गयी कि कैसे बहुसंख्यकों के अधिकार के विमर्श को मारा जा सकता है और उन के घावों पर विमर्श बन ही न पाए, ऐसी पूरी व्यवस्था ही जैसे कर दी गयी। यद्यपि यह तमाम कविताएँ पिछले वर्ष अप्रैल की हैं, फिर भी यह नहीं भूलना चाहिए कि इस वर्ष भी जो दंगे हुए उनके विरुद्ध भी एक भी कथित प्रगतिशील स्वर सामने नहीं आया है।
इसी बुलडोज़र कविता के दूसरे अंक अर्थात मई 2022 में तो बुलडोज़र की कार्यवाही को लेकर हिन्दुओं द्वारा प्रथम पुरुष माने जाने वाले मनु को भी कठघरे में ले लिया था। संजय कुंदन ने लिखा था
“यह रथ है मनु महाराज का
लौट आए हैं महान स्मृतिकार
अपने एक नये अवतार में
लौट आई हैं उनके साथ न्याय संहिताएं
रौंद दी जाएंगी एकलव्यों की आकांक्षाएं फिर से
शंबूकों के स्वप्न मलबे में बदल दिए जाएंगे”
बुलडोज़र को क्यों प्रयोग में लाया जा रहा है, इस पर चर्चा नहीं की गयी, दंगों में जिन लोगों के प्राण गए उनपर साहित्य ने कोई चर्चा नहीं की,
प्रफुल्ल शिलेदार ने लिखा था कि
“इस कहानी का उत्तर कथन
अब तुम्हें लिखना है कवि
उसे कलम से कागज पर नहीं
लहू से सड़क पर लिखना होगा
सकीना को बताना होगा
उसके पिता की मौत आत्महत्या नहीं थी
वह एक हत्या थी
जिसका कारण एक बुलडोज़र था
यह गहरी नींद में उसके सपनों में
आने वाला बचपन का बुलडोज़र नहीं
बल्कि दिन दहाड़े उसकी मेहनत की रोटी
छीन लेने वाला दरिंदा बुलडोज़र था
इन तमाम कविताओं में यह स्पष्ट था कि यह किन्हें निशाना बनाकर लिखी गयी थी। तमाम विमर्श जो कथित आधुनिक साहित्य उठाता है, उसमें बहुसंख्यक समाज तो छोड़ ही दिया जाए, वास्तविक पीड़ित अल्पसंख्यक समाज की पीड़ा भी नहीं होती है।
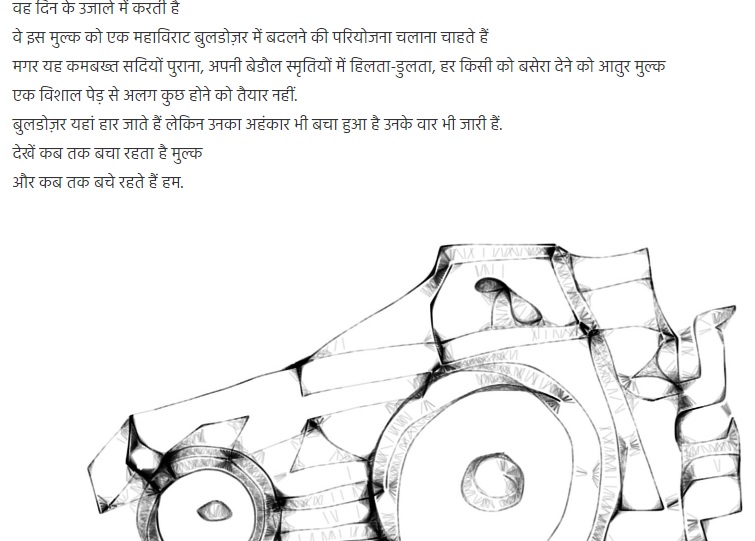
जब विमर्श में कथित प्रगतिशील लेखक एवं कवि उन कट्टरपंथी तत्वों का बचाव करते हुए दिखाई देते हैं, जो पूरे भारतीय लोक के विरुद्ध खड़े होते हैं, तो उनका हौसला बढ़ता है और फिर वह बार-बार लौटते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं उन्हें यह भान होता है कि उनके साथ मात्र वोटबैंक वाले राजनेता ही नहीं बल्कि वह कथित साहित्यकार भी है, जो अपना पूरा दम लगाने के बाद भी इस सरकार का बाल भी बांका नहीं कर पाए हैं।
काश कि जो संवेदना यह कथित प्रगतिशील कवि कट्टरपंथी तत्वों एवं अराजक तत्वों पर दिखाते हैं, उसका एक प्रतिशत भी भारतीय लोक के प्रति दिखाते तो तमाम हिंसक घटनाओं में कमी आती क्योंकि उन्हें पता होता कि उनका अनुचित समर्थन करने के लिए कथित लेखक वर्ग उपलब्ध नहीं है।
इस वर्ष श्री रामनवमी पर हुई हिंसा पर भी यदि एक भी संतुलित कविता आई हो सामने, ऐसा नहीं लगता है।
प्रश्न यह भी है कि कथित प्रगतिशील साहित्य अराजकता एवं क़ानून को तोड़े जाने को ही क्रान्ति क्यों समझता है और क्यों युवाओं को अपने एजेंडे का शिकार बनाता है, ऐसी लोक विरोधी कविताओं के माध्यम से? वह समग्रता में क्यों नहीं देखता है?


















टिप्पणियाँ