|
 ह।ल के आम चुनावों के फलस्वरूप केन्द्र में सत्ता परिवर्तन को अब 70 दिन पूरे हो रहे हैं। 'सबका साथ, सबका विकास' और 'पहले भारत, बाद में हम' जैसे राष्ट्रभक्ति व राष्ट्रीय एकता के नारों पर केन्द्रित प्रचार अभियान से जो अभूतपूर्व चुनाव परिणाम निकला, उससे आशा जगी कि अब हमारी राजनीति का चरित्र बदलेगा, जाति, पंथ, क्षेत्र और भाषा की संकीर्ण निष्ठाओं से ऊपर उठकर अखिल भारतीय राष्ट्रवाद पूरी आभा के साथ चमकेगा। पर इन सत्तर दिनों के वातावरण को देखकर लगता है कि हमारी राजनीति का चरित्र जहां का तहां खड़ा है। वह पुराने ढर्रे पर चल रही है। छोटे-छोटे मुद्दों पर जनता को भड़काना, आंदोलन के पथ पर धकेलना, पुलिस-आंदोलनकारी मुठभेड़ के दृश्य खड़े करना, इन मुद्दों और मुठभेड़ों को आधार बनाकर संसद में हंगामा खड़ा करना आदि। संसद की कार्रवाई को भंग करने की पुरानी राजनीतिक शैली ज्यों की त्यों जिंदा है। 'अच्छे दिन आने वाले हैं', इस नारे का क्या केवल यह अर्थ होना चाहिए कि अच्छे दिन लाने की जिम्मेदारी केवल सरकार की है? उसके लिए समाज और सरकार को मिलकर काम नहीं करना है? जन प्रतिनिधित्व करने वाले दलों को सरकार के साथ विचार विमर्श व सहयोग करने के बजाय केवल विरोध प्रदर्शन करना है? उदाहरणार्थ इंश्योरेंस विधेयक व यूपीएससी में भाषा विवाद को लें। ये दोनों मुद्दे पिछली कांग्रेस नीत यूपीए सरकार के कार्यकाल में खड़े हुए थे, वर्तमान नीति उन्होंने ही बनायी थी, पर अब वही सोनिया-राहुल पार्टी इनका विरोध कर रही है। आज के दृश्य को देखकर लगता है कि वर्तमान संवैधानिक रचना के भीतर विपक्ष की राजनीति अधिक सरल और लाभप्रद है, राष्ट्रनिर्माण की प्रशासकीय राजनीति बहुत कठिन और अलोकप्रिय है। क्या राजनीतिक संस्कृति में आमूल-चूल परिवर्तन आये बिना राष्ट्र निर्माण की भावात्मक कार्यशैली का उभरना संभव है? यह राजनीतिक संस्कृति जिस संवैधानिक रचना की देन है उसका भारत की स्थिति, प्रवृत्ति एवं विविधता के अनुकूल स्वस्थ विकल्प खोजे बिना संभव है? पर वह क्यों संभव नहीं हो पा रहा? क्या चुनावों में प्राप्त सफलता पर तालियां बजाने मात्र से संभव होगा?
ह।ल के आम चुनावों के फलस्वरूप केन्द्र में सत्ता परिवर्तन को अब 70 दिन पूरे हो रहे हैं। 'सबका साथ, सबका विकास' और 'पहले भारत, बाद में हम' जैसे राष्ट्रभक्ति व राष्ट्रीय एकता के नारों पर केन्द्रित प्रचार अभियान से जो अभूतपूर्व चुनाव परिणाम निकला, उससे आशा जगी कि अब हमारी राजनीति का चरित्र बदलेगा, जाति, पंथ, क्षेत्र और भाषा की संकीर्ण निष्ठाओं से ऊपर उठकर अखिल भारतीय राष्ट्रवाद पूरी आभा के साथ चमकेगा। पर इन सत्तर दिनों के वातावरण को देखकर लगता है कि हमारी राजनीति का चरित्र जहां का तहां खड़ा है। वह पुराने ढर्रे पर चल रही है। छोटे-छोटे मुद्दों पर जनता को भड़काना, आंदोलन के पथ पर धकेलना, पुलिस-आंदोलनकारी मुठभेड़ के दृश्य खड़े करना, इन मुद्दों और मुठभेड़ों को आधार बनाकर संसद में हंगामा खड़ा करना आदि। संसद की कार्रवाई को भंग करने की पुरानी राजनीतिक शैली ज्यों की त्यों जिंदा है। 'अच्छे दिन आने वाले हैं', इस नारे का क्या केवल यह अर्थ होना चाहिए कि अच्छे दिन लाने की जिम्मेदारी केवल सरकार की है? उसके लिए समाज और सरकार को मिलकर काम नहीं करना है? जन प्रतिनिधित्व करने वाले दलों को सरकार के साथ विचार विमर्श व सहयोग करने के बजाय केवल विरोध प्रदर्शन करना है? उदाहरणार्थ इंश्योरेंस विधेयक व यूपीएससी में भाषा विवाद को लें। ये दोनों मुद्दे पिछली कांग्रेस नीत यूपीए सरकार के कार्यकाल में खड़े हुए थे, वर्तमान नीति उन्होंने ही बनायी थी, पर अब वही सोनिया-राहुल पार्टी इनका विरोध कर रही है। आज के दृश्य को देखकर लगता है कि वर्तमान संवैधानिक रचना के भीतर विपक्ष की राजनीति अधिक सरल और लाभप्रद है, राष्ट्रनिर्माण की प्रशासकीय राजनीति बहुत कठिन और अलोकप्रिय है। क्या राजनीतिक संस्कृति में आमूल-चूल परिवर्तन आये बिना राष्ट्र निर्माण की भावात्मक कार्यशैली का उभरना संभव है? यह राजनीतिक संस्कृति जिस संवैधानिक रचना की देन है उसका भारत की स्थिति, प्रवृत्ति एवं विविधता के अनुकूल स्वस्थ विकल्प खोजे बिना संभव है? पर वह क्यों संभव नहीं हो पा रहा? क्या चुनावों में प्राप्त सफलता पर तालियां बजाने मात्र से संभव होगा?
दृष्टि परिवर्तन जरूरी
उदाहरण के लिए इस समय मेरे सामने दिल्ली से प्रकाशित एक अंग्रेजी साप्ताहिक 'रेडियेंस' का 3 अगस्त का ताजा अंक है। इस पत्रिका को जमाते इस्लामी जैसा प्रतिष्ठित मुस्लिम संगठन प्रकाशित करता है। एक प्रकार से यह पत्रिका भारतीय मुसलमानों के बड़े और प्रभावशाली वर्ग की सोच को प्रतिध्वनित करती है। 'रेडियेंस' के इस अंक की 'कवर स्टोरी' का शीर्षक है 'डेमोक्रेसी अंडर सीज। मेजोरिटेरियनिज्म मेथड गोज इन फुलस्विंग' (लोकतंत्र घेरेबंदी में फंसा: बहुसंख्यकवादी तरीका अपने पूरे उभार पर)। इस आधुनिक लोकतंत्रीय शब्दावली के आवरण में रेडियेंस का हमला हिन्दू बहुसंख्यकवाद पर है जो मुस्लिम अल्पसंख्या पर हमला कर रहा है। सामान्यतया लोकतंत्रीय राजनीति में भाग लेने वाले राष्ट्रीय समस्याओं पर केन्द्रित विचारधारा के आधार पर चुनाव लड़ते हैं और इसी आधार पर बहुसंख्या-अल्पसंख्या का निर्णय होता है, किंतु भारत में सन् 1885 में कांग्रेस के जन्म के साथ ही बहुसंख्या-अल्पसंख्या का आधार राष्ट्रीय प्रश्न न होकर हिन्दू बहुसंख्या व मुस्लिम अल्पसंख्या पर सीमित रह गया है। 1887-1888 में लखनऊ व 1888 में सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को कांग्रेस से दूर रहने का आह्वान देते हुए कहा कि 'कांग्रेस भारत में लोकतंत्रीय व्यवस्था की मांग कर रही है। इस व्यवस्था में बहुसंख्या का राज होगा और अल्पसंख्या को उसके अनुसार चलना पड़ेगा। भारत में हिन्दू बहुसंख्या में हैं और मुसलमान अल्पसंख्यक हैं इसलिए मुसलमानों को हिन्दुओं के अधीन रहना होगा, जो हमें स्वीकार्य नहीं है। हमारे पूर्वज हिन्दुस्थान के शासक रहे हैं। हमारी धमनियों में शासकों का रक्त बह रहा है। हम हिन्दुओं की गुलामी कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हम बहुमत-अल्पमत की भाषा नहीं समझते। हम तलवार की भाषा समझते हैं। हमें तलवार दे दो। वही फैसला करेगी कि कौन राज करेगा।' उन्होंने मुसलमानों को फटकारते हुए कहा कि 'अगर तुम्हें बहुमत की गुलामी स्वीकार है तो कांग्रेस में भर्तर्ी होकर बंगाली बाबुओं की गुलामी करो।' कांग्रेस लगातार कोशिश करती रही यह समझाने की कि मुस्लिम हितों एवं भावनाओं की पूरी चिंता की जाएगी। उनकी सहमति के बिना मुस्लिम प्रश्नों पर कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा, पर अनुनय विनय बेकार गया। और 1920 में गांधी जी की पहल पर खिलाफत के प्रश्न को स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा बनाने पर ही मुस्लिम समाज ब्रिटिश विरोधी आंदोलन में सम्मिलित हुआ। किंतु तुर्की में मुस्तफा कमालपाशा द्वारा 1922 में खिलाफत का पद समाप्त करने की घोषणा के साथ ही मुस्लिम समाज आंदोलन से अलग हो गया और कोहाट से ढाका तक हिन्दू विरोधी हिंसा की खूनी लहर छोड़ गया।
ब्रिटिश साम्राज्यवाद का झूठा विवाद
हिन्दू बहुसंख्या-मुस्लिम अल्पसंख्या का यह झूठा विवाद ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति की देन है। इस पक्ष पर कोई गहरा अध्ययन व विचार मंथन नहीं हुआ, हिन्दू शब्द का उपासना पद्धति से कोई संबंध नहीं है, हिन्दू शब्द के अन्तर्गत विभिन्न उपासना पद्धतियों से जुड़े समूह आते हैं। वस्तुत: हिन्दू शब्द इस देश में रहने वाले सभी निवासियों के लिए लागू होता रहा है। एक समय था जब अरब देशों में जाने वाले भारतीय मुसलमानों को भी हिन्दू कहा जाता था। स्वयं सैयद अहमद खान ने अपने गुरदासपुर वाले भाषण में कहा था कि 'क्या मैं हिन्दू नहीं हूं? क्या मेरा जन्म भारत में नहीं हुआ?' सर सैयद के इस कथन को अभी 25 जुलाई को गोवा के एक ईसाई विधायक डिसूजा ने दोहराया कि मैं उपासना से ईसाई हूं किंतु राष्ट्रीयता से हिन्दू हूं। और इसीलिए यह देश हिन्दू राष्ट्र है। किंतु रेडियेंस का उपरोक्त अंक डिसूजा के इस कथन का स्वागत करने के बजाए मुसलमानों के सामने हिन्दू राष्ट्र को एक हौवे की तरह पेश करता है।
ब्रिटिश शासक भी इस सत्य को जानते हैं किंतु 'फूट डालो और राज करो' की अपनी नीति के तहत उन्होंने हिन्दू शब्द को उस भू सांस्कृतिक व्याख्या से हटाकर इस्लाम और ईसाई जैसे पैगम्बर और पांथिकग्रंथ केन्द्रित मजहबों की श्रेणी में लाने के लिए मजहब वाची रंग दे दिया। यह व्याख्या परिवर्तन उन्होंने 1864-65 से प्रारंभ हुई जनगणना नीति के द्वारा किया। उस समय से 1941 में अंतिम ब्रिटिश जनगणना तक प्रत्येक केन्द्रीय एवं प्रांतीय रपट में हिन्दुइज्म को मजहबी श्रेणी में रखा गया। किंतु उसकी व्याख्या करते समय उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि हिन्दू शब्द इस्लाम और ईसाइयत की तरह पैगम्बर, पांथिकग्रंथ और एक उपासना पद्धति पर आधारित मजहब नहीं है। यह भू सांस्कृतिक अवधारणा है, किंतु जनगणना के लिए हम इसे मजहब वाची अर्थों में ही इस्तेमाल करेंगे। इसी का परिणाम हुआ कि उन्होंने हिन्दू बहुसंख्या और मुस्लिम-ईसाई अल्पसंख्या का भ्रमजाल फैलाया। वे समझ चुके थे कि भारत में राष्ट्रीयता के प्रवाह की पहचान हिन्दू शब्द से होती है अत: प्रवाह को क्षीण व अवरुद्ध करने के लिए उन्होंने अल्पसंख्यकवाद को अपना मुख्य हथियार बनाया।
सन् 1858 में कलकत्ता मदरसा के प्रिंसिपल केप्टन लीज ने गवर्नर जनरल को एक गोपनीय रपट में लिखा कि भारत के मुसलमान अपने को भारत का धरती-पुत्र न मानकर विदेशी मुस्लिम आक्रमणकारियों की संतान समझते हैं। वे अभी भी शासक मानसिकता में जी रहे हैं। उनकी इस मानसिकता का उपयोग हम अपने साम्राज्य के हित में कर सकते हैं। इसीलिए ब्रिटिश वायसराय लार्ड मेयो ने 1869 में भारत पहुंचकर आंग्ल- मुस्लिम गठजोड़ स्थापित करने का सुनियोजित प्रयास किया, भले ही उसे अंदमान में एक वहाबी कैदी के हाथों अपने प्राण गंवाने पड़े। उसी समय ब्रिटिश सरकार सैयद अहमद खान को उनके बेटे के साथ इंग्लैंड ले गयी। उन्हें सर की उपाधि प्रदान की। उन्हें अपने वैभव और सामर्थ्य का दर्शन कराया। इंग्लैंड से लौटते ही सर सैयद अहमद खान ने अपनी पूरी शक्ति इस्लाम और ईसाइयत के बीच मैत्री का पुल तैयार करने में लगायी।
दुिराष्ट्रवाद का जन्म
इधर यह पुल तैयार किया जा रहा था उधर ब्रिटिश शासकों ने 'हिन्दू' शब्द के जनाधार को संकुचित करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी। 1868 में पंजाब के जनगणना फार्म से सिखों के लिए हिन्दू से अलग खाना बनाया गया। 1881 की जनगणना में सिख की पहचान खालसा के पंचककार तक सीमित कर दी गयी। भारत की वनवासी जनसंख्या को हिन्दू शब्द से बाहर लाने के लिए उन्हें 'एनीमिस्ट' (प्रकृति पूजक) श्रेणी में रखा गया। जैन और बौद्ध धाराओं को भी अहिन्दू घोषित किया गया। फलत: 1891 की जनगणना के कमिश्नर एलेक्जेंडर बेन्स ने हिन्दू शब्द की परिभाषा देते हुए लिखा कि 'मुसलमान, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध व एनीमिस्ट जनसंख्या को अलग करने से जो बचता है वहीं हिन्दू है। इस प्रकार हिन्दू शब्द की सीमाओं को बहुत संकुचित कर दिया गया।
जनगणना नीति के साथ 1858 में रानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र से आरंभ हुई तथाकथित संवैधानिक सुधार प्रक्रिया के द्वारा भी भारतीय राष्ट्रवाद के विरुद्ध अल्पसंख्यक वाद के हथियार का इस्तेमाल किया गया। 1892 में संवैधानिक सुधार संबंधी बहस में मुस्लिम अल्पसंख्या के प्रति ब्रिटिश चिंता मुखरित हुई। 1919 के एक्ट में पहली बार अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल किया गया और मुस्लिम अल्पसंख्या के हितों की रक्षा का दायित्व अंग्रेज गवर्नरों के अधिकार क्षेत्र में दे दिया गया। तभी से भारत की संवैधानिक प्रक्रिया में अल्पसंख्यकवाद का आरंभ हुआ। किंतु मुस्लिम नेतृत्व चाहता था कि अल्पसंख्यक होते हुए भी उसके ऐतिहासिक महत्व को स्वीकार करके उनकी जनसंख्या से अधिक प्रतिनिधित्व प्रांत केन्द्रों में दिया जाए। वे आनुपातिक प्रतिनिधित्व तक सीमित रहने को तैयार नहीं थे। इसी उलझन से बाहर निकलकर उन्होंने स्वयं को एक अलग राष्ट्र घोषित कर दिया, जिससे भारत में द्विराष्ट्रवाद का जन्म हुआ। किंतु कांग्रेस का हिन्दू नेतृत्व इस पूरी समस्या को यूरोपीय परिभाषाओं की आंखों से देखता रहा।
अपनी भ्रामक सोच के कारण कांग्रेस के हिन्दू नेतृत्व ने न तो इस्लामी विचारधारा का गहरा अध्ययन किया, न भारत में मुस्लिम रणनीति की दिशा को समझने का प्रयास किया। अपवाद स्वरूप लाला लाजपतराय और विपिन चन्द्र पाल के नाम गिनाये जा सकते हैं। लाला लाजपतराय ने नवम्बर 1924 में लाहौर से प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक ट्रिब्यून में 13 किस्तों में एक लेखमाला लिखी। उसमें उन्होंने इस्लामी विचारधारा और मुस्लिम राजनीति का विवेचन करते हुए भविष्यवाणी की कि यदि मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार बना रहता है और मुस्लिम राजनीति की दिशा नहीं बदलती है तो उत्तर, पश्चिम और पूर्व में दो पृथक मुस्लिम राज्यों की स्थापना अवश्यंभावी है। विपिन चन्द्र पाल इस्लामी विचारधारा के गहरे अध्येता थे। उन्होंनेे खिलाफत प्रश्न को स्वतंत्रता आंदोलन का अंग बनाने का विरोध करते हुए 1920 के असहयोग आंदोलन से संबंध विच्छेद कर लिया, जिसके फलस्वरूप उन्हें 1932 में अपनी मृत्यु तक उपेक्षा का जीवन जीना पड़ा।
भारतीय राष्ट्रवाद का विखंडन
देश को स्वतंत्र कराने के लिए आकुल कांग्रेस का हिन्दू नेतृत्व मुस्लिम सहयोग पाने के लोभ में उनकी बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने की यथासंभव कोशिश में लगा रहा। 1937 में प्रांतीय विधानसभा चुनावों के समय कांग्रेस को मुस्लिम सीटों के लिए मुस्लिम उम्मीदवार नहीं मिल पाए, जो थोड़े-बहुत मिले वे सब चुनाव हार गये। उसी प्रकार 1946 के चुनावों में भी 98 प्रतिशत मुस्लिम मतदाताओं ने मुस्लिम लीग को वोट दिया तो 96 प्रतिशत हिन्दू मतदाताओं ने कांग्रेस के अखंड भारत के नारे को। 1937 में जवाहरलाल नेहरू ने अपने कम्युनिस्ट मित्रों के सहयोग से मुस्लिम जनसम्पर्क अभियान छेड़ा, पर वह पूरी तरह विफल रहा। इन सब अनुभवों से कांग्रेस नेतृत्व ने कोई सबक नहीं सीखा।
ब्रिटिश सरकार संवैधानिक सुधार के नाम पर लगातार भारतीय राष्ट्रवाद को विखंडित करने और मुस्लिम पृथकतावाद का पोषण करने की दिशा में आगे बढ़ती गयी और राष्ट्रीय नेतृत्व स्वतंत्रता प्राप्ति के लोभ में ब्रिटिश कूटनीति के जाल में फंसता गया। अंग्रेजों ने 1909 में मुसलमानों को पृथक मताधिकार दिया, 1919 के एक्ट में सिखों, एंग्लो इंडियनों, महिलाओं व महाराष्ट्र में मराठों को दिया, 1935 के एक्ट में से हिन्दू समाज की निम्न जातियों या वंचित वर्गों को पृथक मताधिकार देने का कुचक्र रच रहे थे कि गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू करके पूना पैक्ट के द्वारा इस कुचक्र को विफल करने का प्रयास किया, किंतु तब उन्हें आरक्षण का जहरपान करना पड़ा। यही आरक्षण का सिद्धांत स्वाधीन भारत की राजनीति के गले में हड्डी बन गया है। 1933 में कांग्रेस नेतृत्व को लगा कि शायद मुस्लिम नेतृत्व ही पृथकतावादी मानसिकता से ग्रस्त है। सामान्य समाज का मानस राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत है। इसी धारणा के वशीभूत होकर कांग्रेस नेतृत्व ने मई 1934 में पटना में पहली बार मांग उठायी कि हमें वयस्क मताधिकार द्वारा निर्वाचित संविधान सभा चाहिए जो किसी भी बाहरी हस्तक्षेप के बिना भारत के लिए संविधान तैयार करेगी। इसके बाद कांग्रेस के प्रत्येक सम्मेलन व बैठक में यह मांग दोहरायी जाने लगी। स्वाभाविक ही मि.जिन्ना, ब्रिटिश सरकार और डा. अम्बेडकर की ओर से इस मांग का विरोध हुआ। मि.जिन्ना का कहना था कि वयस्क मताधिकार से निर्वाचित संविधान सभा में हिन्दू बहुमत होगा और उस हिन्दू बहुमत द्वारा निर्मित संविधान मुस्लिम हितों का विरोधी होगा। डा.अम्बेडकर ने 1945 में अपनी 'शेड्यूल्ड कास्ट' कांफ्रेंस के सम्मेलन में कहा कि भारत के लिए 1935 का संविधान पर्याप्त है, उसके बाद किसी नई संविधान सभा का औचित्य नहीं रह जाता। इस विरोध के कारण कांग्रेस की यह मांग और जोर पकड़ती गयी। कांग्रेस ने 1935 के एक्ट को अस्वीकार किया था, पर 1937 में उसके अन्तर्गत प्रांतीय विधान सभाओं के चुनाव लड़े। 11 में से 8 राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बनीं, पर जवाहर लाल नेहरू की अध्यक्षता में उन्हें निर्देश दिया गया कि विधानसभा की पहली बैठक में ही 1935 के एक्ट को वापस लेने और वयस्क मताधिकार द्वारा निर्वाचित संविधान सभा की मांग का प्रस्ताव पारित करें।
1939 में द्वितीय विश्वयुद्ध प्रारंभ होने के बाद 4 नवम्बर 1939 को गांधी जी ने 'हरिजन' में लिखा कि ऐसी संविधान सभा ही भारत की अनेक, विशेषकर मुस्लिम समस्या का हल होगी। ऐसी संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान पूरी तरह दोषरहित होने पर भी देशज तो होगा ही। ब्रिटिश सरकार के युद्ध प्रयत्नों का बहिष्कार करने के लिए कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया तब मि.जिन्ना ने एक ओर मुस्लिम समाज को मुक्ति दिवस मनाने का आदेश दिया, दूसरी ओर वायसराय लार्ड लिनलिथगो से मिलकर मुस्लिम लीग के पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। लिनलिथगो के प्रोत्साहन पर मुस्लिम लीग ने मार्च 1940 में द्विराष्ट्रवाद का और मुसलमानों के लिए अलग राज्य बनाने का प्रस्ताव पारित किया। तब से मुस्लिम समाज स्वयं को अल्पसंख्या के बजाय अलग राष्ट्र कहने लगा।
मार्च 1942 में सर स्टेफोर्ड क्रिप्स भारत आये। उन्होंने संविधान सभा बनाना स्वीकार किया किंतु वयस्क मताधिकार के बजाय 1935 के एक्ट में निर्धारित 15 प्रतिशत सीमित मताधिकार के आधार पर।
1945 में ब्रिटिश संसद में भारत को संविधानसभा देने का आश्वासन दिया गया और वायसराय लार्ड वेवल ने भारत लौटकर उसकी तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि यदि वयस्क मताधिकार के द्वारा संविधान सभा की मांग पर अड़े रहे तो उसमें दो वर्ष का समय लगेगा। कांग्रेस नेतृत्व ने जल्दी से जल्दी सत्ता पाने के लोभ में 15 प्रतिशत सीमित मताधिकार को ही स्वीकार कर लिया। मार्च 1946 को एक योजना प्रकाशित की जिसे केबिनेट मिशन प्लान कहा जाता है। इसी प्लान में संविधान सभा और अंतरिम सरकार के गठन की रूपरेखा प्रस्तुत की गयी। पहले अंतरिम सरकार बनी। मुस्लिम लीग ने उसका बहिष्कार किया, पर वेवल उसे मनाकर ले आये। संविधान सभा के लिए चुनाव हुए। उसमें भारतीय नरेशों को 93 सीटों पर अपने प्रतिनिधि मनोनीत करने का अधिकार दिया गया और 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिलीं, कांग्रेस के पास मुश्किल से 2 मुस्लिम सीटें थीं। मुस्लिम लीग ने पहले दिन से संविधान सभा का बहिष्कार किया पर 3 जून 1947 को भारत विभाजन पर समझौते को अंतिम रूप मिल जाने के बाद 14 जुलाई 1947 को संविधान सभा की चौथी बैठक में विभाजित अर्थात हिन्दू भारत से निर्वाचित लीग के 23 प्रतिनिधि अनपेक्षित रूप से पूरी संख्या में संविधान सभा में उपस्थित हो गए। अवश्य ही इसके पीछे कोई सुविचारित निर्णय रहा होगा। उन्हें संविधान सभा में देखकर दिल्ली के देशबंधु गुप्त ने प्रश्न उठाया कि ये लीगी सदस्य द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत को बाहर छोड़कर आये हैं या उसे साथ लाये हैं?
नेहरू की गलत नीति
वस्तुत: यही उपयुक्त अवसर था जब इस विषय पर खुलकर बहस होनी चाहिए थी। किंतु जवाहरलाल नेहरू इस मुस्लिम समस्या को अल्पसंख्यक व बहुसंख्यक समस्या के रूप में देखते रहे। उनका झुकाव अल्पसंख्या अर्थात मुस्लिम समाज के पक्ष में था अत: वह बहस नहीं हुई। नेहरू को विश्वास था कि उनके नेतृत्व में यह समस्या हल हो जाएगी। इसलिए स्वाधीन भारत के नीति निर्माता बनकर उन्होंने मुस्लिम पृथकतावाद को सेकुलरवाद और राष्ट्रीयतावादी हिन्दू समाज को साम्प्रदायिकता की श्रेणी में धकेल दिया। नेहरूवादी सेकुलरिज्म के शब्द जाल में फंसा सत्तालोलुप नेतृत्व एक ओर हिन्दू समाज को जाति, भाषा व क्षेत्र के आधार पर विखंडित कर रहा है, अपनी सत्ताकांक्षा की पूर्ति के लिए छोटे-छोटे राजनीतिक दलों में बिखर गया है, तो दूसरी ओर मुस्लिम नेतृत्व ने भारी विचार मंथन के बाद निर्णय किया कि वे पृथक मुस्लिम राजनीतिक दल न बनाकर जातिवादी हिन्दू राजनीतिक दलों को अपना समर्थन प्रदान करेंगे। 1885 से 1947 तक कांग्रेस का स्वयं का इतिहास इस सत्य का साक्षी है कि मुस्लिम समाज ने स्वयं को राष्ट्रीय आंदोलन से अलग रखा। उन्होंने कभी गांधी और नेहरू की कांग्रेस का साथ नहीं दिया।
1947 में देश विभाजन के पश्चात मुस्लिम रणनीति का सूक्ष्म अध्ययन आवश्यक था, पर वह नहीं हुआ। विभाजन के बाद 1947 में मुस्लिम नेतृत्व की जो मन:स्थिति थी वही 2014 के चुनाव परिणामों से उत्पन्न हुई लगती है। उसकी रणनीति के कुछ संकेत मिलने लगे हैं। दिल्ली में 4 अगस्त को आप पार्टी के जंतर मंतर प्रदर्शन में मुसलमानों की विशाल संख्या में उपस्थिति इस रणनीति का एक संकेत है। 5 और 6 अगस्त के इंडियन एक्सप्रेस में उत्तर प्रदेश में सैकड़ों मुस्लिम दंगों के बारे में जो बड़ी रपट छपी है उसमें उल्लेखनीय है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिन मुजफ्फरनगर, शामली, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, बिजनौर आदि नगरों में बड़े पैमाने पर दंगे हुए हैं वहां सभी स्थानों पर मुस्लिम जनसंख्या बहुत अधिक है और उस क्षेत्र का निवासी होने के कारण मैं कह सकता हूंु कि वहां हिन्दू डरे हुए रहते हैं।
खतरनाक संकेत
आयेदिन समाचार पत्रों में समाचार छप रहे हैं कि भारत के पढ़े-लिखे मुस्लिम युवक इराक और सीरिया में सुन्नी मुसलमानों के जिहाद में हिस्सा लेने के लिए भारत से जा रहे हैं। सुप्रसिद्ध उलेमा अली मियां द्वारा लखनऊ से स्थापित दारुल उलूम, नदवा के प्रमुख मौलाना सलमान नदवी ने भारत के मुस्लिम युवकों को इराक और सीरिया में चल रहे जिहाद में सम्मिलित होने का आह्वान दिया है।
उन्होंने अरब देशों से प्रार्थना की है कि वे भारत से आने वाले पांच लाख जिहादियों का खर्चा वहन करे। रात-दिन सेकुलरिज्म का राग अलापने वाले भारतीय राजनेता इस पर मौन हैं। जबकि दिल्ली के महाराष्ट्र सदन की 'मेस' में खराब खाने से क्षुब्ध शिवसेना के किसी एक सांसद ने कैटरिंग सुपरवाइजर के मुंह में वहां बनी रोटी का एक टुकड़ा ठूंसने का प्रयास किया तो उसे मुस्लिम मत पर हिन्दू आक्रमण का रूप देकर दो दिन संसद को नहीं चलने दिया गया। यह संयोग था कि वह सुपरवाइजर मुस्लिम है और उस दिन वह रमजान का रोजा रखे हुए था। उसकी भावनाओं का आदर करते हुए भी यह नहीं कहा जा सकता कि शिवसेना सांसद ने धार्मिक भावना से अपने गुस्से का प्रदर्शन किया। इसके विपरीत मेरठ जिले के खरखोदा थाने में सराणा गांव के एक मदरसे में पढ़ाने वाली हिन्दू शिक्षिका के साथ बलात्कार किया गया और मत-परिवर्तन करके उससे जबरन शपथ पत्र पर हस्ताक्षर लिये गये। इस असामान्य घटना पर सेकुलरवादी अभी तक मौन हैं।
संक्षेप में, पिछले 1200 साल से मुस्लिम प्रश्न भारतीय इतिहास का केन्द्रीय बिन्दु बना रहा है। महाराष्ट्र के मुस्लिम विचारक हमीद दलवाई ने लिखा है कि मुसलमान जहां सत्ता में होते हैं वहां गैर मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बना देते हैं और जहां वे अल्पसंख्या में होते हैं वहां अपने लिए पृथक राज्य की मांग करते हैं। भारत का आधुनिक इतिहास इस सत्य का साक्षी है। 2014 के चुनाव परिणामों की स्थायी सफलता इसमें है कि भारत की मुस्लिम समस्या संतोषजनक ढंग से हल हो इसके लिए मुस्लिम समाज के भीतर राष्ट्रभक्त उदार नेतृत्व खड़ा हो। अपने को सेकुलर कहने वाले सब राजनेताओं को इस दिशा में मिलकर प्रयास करना चाहिए।
-देवेन्द्र स्वरुप, (लेखक वरिष्ठ पत्रकार ेवं शीर्ष विचारक हैं।)( 6 अगस्त, 2014 )



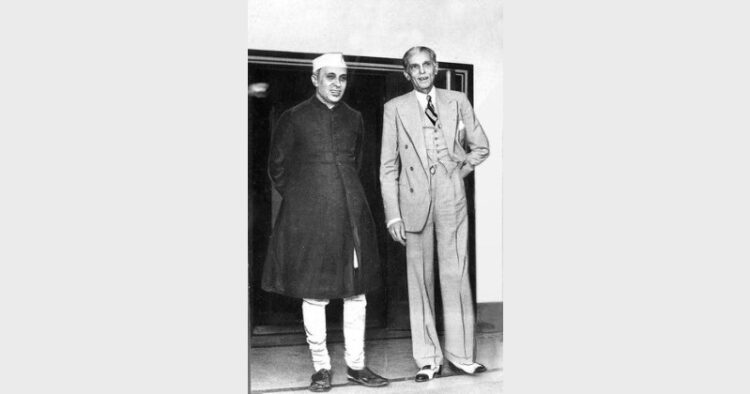










टिप्पणियाँ