प्रतिवर्ष 1 जून को ‘विश्व दुग्ध दिवस’ मनाया जाता है, जो इस वर्ष ‘आइए, दुग्ध की शक्ति का उत्सव मनाएं’ (Let’s Celebrate the Power of Dairy) विषय पर केंद्रित है। यह विषय दुग्ध उत्पादों की बहुआयामी शक्ति को रेखांकित करता है, जिसमें पोषण, आजीविका, सतत विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती शामिल है। यह केवल दूध के पोषण मूल्य तक सीमित नहीं है बल्कि डेयरी उद्योग द्वारा किसानों, उपभोक्ताओं और पर्यावरण के बीच संतुलन साधने की भूमिका को भी उजागर करता है। विश्व दुग्ध दिवस की शुरुआत वर्ष 2001 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) ने दुग्ध और डेयरी उद्योग के वैश्विक महत्व को रेखांकित करने और इसके पोषण, आर्थिक व सामाजिक योगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से की थी। 1 जून का ही दिन इसलिए चुना गया क्योंकि कई देशों में पहले से ही इस दिन दुग्ध से जुड़े कार्यक्रम आयोजित होते थे। तभी से यह दिन दुनियाभर में दूध के महत्व, डेयरी किसानों की भूमिका और दुग्ध उत्पादों की सतत आपूर्ति श्रृंखला को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है।
भारत, जो विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, इस क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरा है। भारत का दुग्ध उद्योग वैश्विक स्तर पर अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराता है। 2023-24 के वित्तीय वर्ष में भारत ने लगभग 239.3 मिलियन टन दूध का उत्पादन किया, जो विश्व के कुल दूध उत्पादन का लगभग 24 प्रतिशत है। यह उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 3.78 प्रतिशत अधिक था, जो भारतीय दुग्ध उद्योग की लगातार वृद्धि और मजबूती को दर्शाता है। प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता भी 471 ग्राम प्रतिदिन तक पहुंच गई है, जो वैश्विक औसत 323 ग्राम से कहीं अधिक है। यह संख्या भारत में दूध की बढ़ती मांग, बेहतर उत्पादन तकनीकों और कृषि-आधारित उपायों का संकेत है। दूध न केवल पोषण का महत्वपूर्ण स्रोत है बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का भी महत्वपूर्ण स्तंभ है, जहां करोड़ों किसान परिवार अपनी आजीविका के लिए इस उद्योग पर निर्भर हैं।
दुग्ध उत्पादन में भारत के विभिन्न राज्यों का योगदान महत्वपूर्ण और विविधतापूर्ण है। उत्तर प्रदेश, जो कुल उत्पादन का 16.21 प्रतिशत हिस्सा रखता है, सबसे अग्रणी राज्य है। इसके बाद राजस्थान (14.51 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (8.91 प्रतिशत), गुजरात (7.65 प्रतिशत) और महाराष्ट्र (6.71 प्रतिशत) प्रमुख स्थानों पर हैं। ये पांच राज्य मिलकर भारत के कुल दुग्ध उत्पादन का लगभग 54 प्रतिशत हिस्सा बनाते हैं। भारत में दूध उत्पादन में पशु प्रजातियों की विविधता भी देखने को मिलती है। देशी भैंसें दूध उत्पादन का सबसे बड़ा हिस्सा (लगभग 31.5 प्रतिशत) प्रदान करती हैं जबकि क्रॉसब्रिड गायें 31.1 प्रतिशत योगदान करती हैं। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि भारतीय दुग्ध उद्योग में पशुपालन की प्रजातिगत विविधता एक बड़ा स्तंभ है। इसके अलावा, देशी गायें, याक, भेड़, बकरी और अन्य पशु भी उत्पादन में योगदान करते हैं।
दुग्ध उद्योग में नवाचार और सतत विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भारत में कई महत्वपूर्ण पहल हो रही हैं। भारत की सबसे बड़ी दुग्ध सहकारी संस्था ‘अमूल’ ने मट्ठे से बायोएथेनॉल उत्पादन के सफल परीक्षण किए हैं। यह पहल न केवल ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में क्रांति ला सकती है बल्कि किसानों की आय में भी वृद्धि करेगी। मट्ठा, जो दूध के प्रसंस्करण में बचा हुआ एक अपशिष्ट उत्पाद है, उसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाना पर्यावरण की दृष्टि से लाभकारी है। इसके अतिरिक्त, अमूल असम में ₹100 करोड़ की लागत से एक नया दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित कर रहा है, जो 20,000 से अधिक स्थानीय किसानों को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाएगा। इस तरह की परियोजनाएं क्षेत्रीय विकास को गति देती हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करती हैं। बिहार की दुग्ध सहकारी संस्था कॉमफेड (सुधा) ने भी दुग्ध उद्योग में उल्लेखनीय प्रगति की है। यह संस्था प्रतिदिन लगभग 40 लाख लीटर दूध एकत्रित करती है और अपने उत्पादों का निर्यात अमेरिका, यूएई और अन्य विदेशी बाजारों में कर रही है। कॉमफेड ने किसानों के लिए ₹5 लाख की दुर्घटना चिकित्सा योजना शुरू की है, जो किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। साथ ही, डिजिटल पंजीकरण और ट्रैकिंग प्रणाली के माध्यम से पारदर्शिता और दक्षता में वृद्धि की गई है, जिससे किसानों का विश्वास और उत्पाद गुणवत्ता सुनिश्चित होती है।
निजी क्षेत्र की भागीदारी भी भारत के दुग्ध उद्योग को नई ऊंचाईयों तक पहुंचा रही है। फ्रांसीसी कंपनी डैनोन ने भारत में अपने संयंत्रों का विस्तार करने के लिए 20 मिलियन यूरो का निवेश किया है। यह निवेश यूनिलीवर, नेस्ले जैसे बड़े ब्रांडों के साथ प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में मदद करेगा। साथ ही, ऑर्गेनिक दुग्ध उत्पादन की ओर भी ध्यान बढ़ा है, जहां अक्षयकल्पा जैसी कंपनियां किसानों के साथ मिलकर जैविक डेयरी फार्म स्थापित कर रही हैं। ये फार्म पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ-साथ किसानों की आय में भी वृद्धि करते हैं। इस प्रकार, निजी क्षेत्र और सहकारी संस्थाएं मिलकर भारतीय दुग्ध उद्योग को मजबूती प्रदान कर रही हैं। भारत के दुग्ध उद्योग की भविष्य की दिशा अत्यंत उत्साहवर्धक है। 2030 तक इस उद्योग के लगभग 57 लाख करोड़ रुपये के मूल्यांकन तक पहुंचने की संभावना है। इस वृद्धि के पीछे स्वास्थ्य और कल्याण पर बढ़ते ध्यान, ऑर्गेनिक और कम वसा वाले दूध उत्पादों की मांग में वृद्धि और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से दूध और दुग्ध उत्पादों की बिक्री में बढ़ोतरी प्रमुख कारण हैं। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी नवाचारों का समावेश और किसानों के लिए बेहतर वित्तीय अवसर भी इस उद्योग को प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसके अलावा, सरकार और निजी क्षेत्र की संयुक्त पहलें, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, जैविक उत्पादन और ऊर्जा कुशल प्रसंस्करण तकनीकें भविष्य में दुग्ध उद्योग को अधिक प्रतिस्पर्धी और टिकाऊ बनाएंगी।
सरकार ने दुग्ध उद्योग के विकास और समृद्धि के लिए कई प्रमुख योजनाएं और पहल शुरू की हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन का उद्देश्य देशी गायों की बेहतर नस्लों का संरक्षण और संवर्धन करना है, जिससे दूध उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ पारंपरिक कृषि पद्धतियों को भी सशक्त बनाया जा सके। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, राज्य सहकारी दुग्ध संघ, राष्ट्रीय दुग्ध विकास कार्यक्रम और डेयरी उद्यमिता विकास योजना जैसी योजनाओं के तहत किसानों को तकनीकी, वित्तीय और प्रशिक्षण सहायता प्रदान की जा रही है। ये योजनाएं दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने, दूध की गुणवत्ता में सुधार करने और किसानों की आय बढ़ाने में सहायक हैं। साथ ही, इन पहलों से उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण दूध उपलब्ध कराने में मदद मिलती है। सामाजिक और पोषण सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी दुग्ध उद्योग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूध बच्चों के संपूर्ण विकास, गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य और वृद्ध व्यक्तियों की पोषण आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करता है।
भारत में लाखों किसान परिवारों की आजीविका दुग्ध उद्योग पर निर्भर है, जो ग्रामीण विकास का एक बड़ा आधार बनता है। दूध उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ उपभोग में समानता सुनिश्चित करना, नवाचारों को प्रोत्साहित करना और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। केवल उत्पादन बढ़ाना ही नहीं बल्कि वितरण और उपभोग के स्तर पर असमानताओं को दूर कर एक समावेशी और पोषण-सुरक्षित समाज का निर्माण करना जरूरी है। दुग्ध उद्योग को कई गंभीर चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। 2022 में लंपी स्किन डिजीज के प्रकोप ने भारत के दुग्ध उद्योग को भारी नुकसान पहुंचाया। इस रोग से 97,000 से अधिक मवेशियों की मौत हुई और लगभग 20 लाख पशु प्रभावित हुए, जिससे किसानों की आय में गिरावट आई। कच्चे माल, फीड, ईंधन और परिवहन की लागत में वृद्धि से दुग्ध उत्पादों की कीमतें बढ़ गई हैं जिस कारण कई कंपनियों ने अपने उत्पादों की कीमतों में वृद्धि की है, जिससे उपभोक्ताओं पर आर्थिक दबाव बढ़ा है। ऐसे समय में उद्योग को न केवल महामारी नियंत्रण बल्कि लागत प्रबंधन और बाजार स्थिरता पर भी ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है।
बहरहाल, भारत का दुग्ध उद्योग अपने पोषण मूल्य, आर्थिक महत्व, सामाजिक प्रभाव और सतत विकास की दिशा में उठाए गए कदमों के कारण गर्व करने लायक है। यह उद्योग न केवल देश की कृषि अर्थव्यवस्था का आधार है बल्कि लाखों किसानों, ग्रामीण परिवारों और उपभोक्ताओं के जीवन की गुणवत्ता को भी बेहतर बनाने का माध्यम है। हालांकि दुग्ध उपभोग के मामले में क्षेत्रीय और सामाजिक असमानताएं भी देखने को मिलती हैं। उच्च आय वर्ग के लोगों का प्रति व्यक्ति दूध उपभोग तीन से चार गुना अधिक है जबकि देश की सबसे गरीब 30 प्रतिशत आबादी मात्र 18 प्रतिशत दूध का उपभोग करती है। शहरी क्षेत्रों में दूध की खपत ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में 30 प्रतिशत अधिक है। पूर्वी राज्यों ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में प्रति व्यक्ति दूध उपभोग 171 ग्राम प्रतिदिन से भी कम है, जो राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे है। यह असमानता पोषण की दृष्टि से चिंता का विषय है क्योंकि दूध और दुग्ध उत्पादों में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी तथा अन्य पोषक तत्व होते हैं, जो बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। इसलिए सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए नीति निर्माताओं को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
(लेखक साढ़े तीन दशक से पत्रकारिता में निरंतर सक्रिय वरिष्ठ पत्रकार हैं)













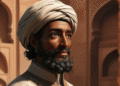
टिप्पणियाँ