भारतीय लोकतंत्र की नींव में ईंट की तरह जड़ा है संविधान का वह सिद्धांत, जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता के सूक्ष्म संतुलन की बुनियाद रखता है। यह संतुलन अक्सर न्यायपालिका की ‘सक्रियता’ और ‘संयम’ के बीच झूलता रहा है। हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 201 की प्रक्रिया में पारदर्शिता और तर्कसंगतता के मानदंड जोड़ने का निर्णय इसी झूलते हुए लोकतांत्रिक पेंडुलम को एक नई दिशा देने का प्रयास ही दिखता है। पर क्या यह प्रयास संविधान द्वारा खींची गई लक्ष्मणरेखा का सम्मान करते हुए किया गया है, या फिर यह न्यायिक सक्रियता का वही पुराना चेहरा है, जिस पर अक्सर ‘विधायिका के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण’ का आरोप लगता रहा है?

अनुच्छेद 201 का सरल अर्थ यह है कि, यदि कोई राज्य विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति के पास तीन विकल्प होते हैं: एक, विधेयक को स्वीकृति देना, दो, अस्वीकार करना या तीन, उसे अनिश्चितकाल के लिए लटकाए रखना। दशकों से यह प्रक्रिया कार्यपालिका के विवेक पर निर्भर रही है, जहां न तो निर्णय लेने की कोई समयसीमा है और न ही कारण बताने की बाध्यता। परंतु वर्ष 2025 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस परंपरागत व्यवस्था में एक क्रांतिकारी मोड़ जोड़ते हुए कहा कि राष्ट्रपति द्वारा विधेयक को रोके जाने या लौटाए जाने के निर्णय में ‘स्पष्ट तर्क’ और ‘संवैधानिक वैधता’ का समावेश अनिवार्य है। न्यायालय ने इसे ‘Judicial Mind’ का प्रयोग कहा, मानो कार्यपालिका के विवेक में न्यायिक बुद्धिमत्ता का सम्मिश्रण करना आवश्यक है।
यहां वही पुराना प्रश्न फिर से सामने आता है-क्या न्यायपालिका को यह अधिकार है कि वह कार्यपालिका को बताए कि उसे कैसे सोचना चाहिए?
इस ‘अनिवार्यता’ के समर्थक कहेंगे कि यह निर्णय पारदर्शिता की दिशा में एक साहसिक कदम है। अगर कोई विधेयक अनिश्चितकाल के लिए रोक दिया जाए, तो क्या यह संघीय ढांचे के सिद्धांतों के विरुद्ध नहीं जाता? न्यायालय का यह हस्तक्षेप ऐसे ही सवालों को कानूनी मंच देता है।
किन्तु आलोचकों की दृष्टि में यह निर्णय संविधान के मूल ढांचे से विचलन जैसा है। इस पक्ष का तर्क है कि भारतीय संविधान ने राष्ट्रपति को विवेकाधिकार दिया है, न कि न्यायिक निर्देशों का पालन करने का आदेश।
यदि न्यायपालिका कार्यपालिका को ‘कैसे सोचें’ का पाठ पढ़ाने लगे, तो शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत ध्वस्त हो जाएगा। कल्पना कीजिए कि यदि राष्ट्रपति को हर विधेयक पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेना पड़े, तो कानून निर्माण की प्रक्रिया कितनी धीमी हो जाएगी। क्या यह लोकतंत्र की गति के साथ छेड़छाड़ नहीं होगा?
इस बहस में इतिहास के पन्ने हमें दोहरे सबक देते हैं। एक ओर 1997 का विशाखा मामला है, जहां न्यायपालिका ने यौन उत्पीड़न रोकथाम हेतु दिशानिर्देश बनाए। कानून या दिशानिर्देश बनाना, यह कार्य विधायिका का था, किंतु इस कदम के समर्थकों का कहना था कि ‘न्यायपालिका ने विधायिका की निष्क्रियता की पूर्ति’ की। दूसरी ओर, 1994 का एस.आर.बोम्मई मामला है, जहां न्यायालय ने राष्ट्रपति शासन के मामलों में हस्तक्षेप करते हुए भी संयम बरता। क्या अनुच्छेद 201 की यह नवीन व्याख्या विशाखा जैसी ‘सक्रियता’ है या फिर बोम्मई प्रकरण जैसे संयम का विस्मरण?
आज जब राज्यों और केंद्र के बीच संबंधों में नई टकराहटें उभारी जा रही हैं, यह निर्णय संघीय ढांचे के लिए दोहरी चुनौती बनकर आया है। एक तरफ़, यह राज्यों को केंद्र की ‘मनमानी’ के विरुद्ध कानूनी हथियार देता है। दूसरी ओर, यह केंद्र-राज्य समीकरणों को न्यायालय की चौखट तक खींचकर राजनीतिक विवादों को न्यायीकृत करने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। जैसे, तमिलनाडु और कर्नाटक के जल विवाद को अदालत की बजाय राजनीतिक वार्ता से सुलझाना चाहिए था, वैसे ही विधायी मतभेदों को भी संसदीय संवाद से ही निपटाना चाहिए।
अंततः यह निर्णय भारतीय लोकतंत्र की उस आधारभूत उलझन को स्पर्श करता है, जहां संस्थाएं एक-दूसरे के अधिकार क्षेत्र की रक्षा करने के बजाय रस्साकशी में लगी दिखती हैं। न्यायपालिका का यह कदम निस्संदेह पारदर्शिता लाने की दिशा में प्रशंसनीय प्रयास है, परंतु अगर यह कार्यपालिका के संवैधानिक अधिकार क्षेत्र को कुंद करेगा, तो यह संतुलन के सिद्धांत के विपरीत होगा।
शायद समाधान यही है कि न्यायालय निर्णय देते समय अपने आदेशों को ‘सुझाव’ के रूप में प्रस्तुत करे, न कि ‘अनिवार्य निर्देश’ के रूप में। जैसे कोई शिक्षक छात्र को मार्गदर्शन देता है, वैसे ही न्यायपालिका को भी संवैधानिक संस्थाओं का मार्गदर्शक बनना चाहिए, न कि नियंत्रक।
भारतीय संविधान की जिस मूल भावना ने न्यायपालिका को ‘संविधान का संरक्षक’ बनाया था, उसी भावना ने विधायिका को ‘जनता की आवाज़’ और कार्यपालिका को ‘निर्णय की गति’ का प्रतीक माना था। इन तीनों की सामूहिक शक्ति ही लोकतंत्र की सफलता है। अनुच्छेद 201 की यह नई व्याख्या तभी सार्थक होगी, जब यह तीनों स्तंभों के बीच संवाद का माध्यम बने, न कि संघर्ष का हथियार।
X@hiteshshankar















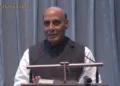


टिप्पणियाँ