न्यायाधीशों के निर्णयों में निष्पक्षता बनी रहे और उनके ऊपर कोई अनुचित दबाव न डाल सके, इसके लिए उन्हें उनके न्यायिक कार्यों के लिए विशेष कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है। यह सुरक्षा उन्हें निर्भीक होकर न्याय करने और बाहरी दबावों से बचाने के लिए दी जाती है। संविधान के अनुच्छेद 121 और 211 के अंतर्गत न्यायिक कार्यों की संसद और विधानसभा में चर्चा पर भी प्रतिबंध है। संविधान के अनुच्छेद 124(4) और 217 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सिर्फ महाभियोग के जरिए ही हटाया जा सकता है।

अधिवक्ता,सर्वोच्च न्यायालय
न्यायाधीश (संरक्षण) अधिनियम, 1985 की धारा 3 (1) के अनुसार किसी भी अन्य लागू कानून के प्रावधानों के बावजूद भी कोई न्यायालय किसी वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश के खिलाफ किसी भी नागरिक या आपराधिक कार्यवाही को दर्ज या जारी नहीं रख सकता, यदि वह कार्य, कथन या निर्णय उनके आधिकारिक या न्यायिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किया गया हो। परन्तु यह कानून भारत सरकार, राज्य सरकारों, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी को न्यायाधीशों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने से नहीं रोकता। यह कार्रवाई नागरिक, आपराधिक, विभागीय या अन्य किसी भी रूप में हो सकती है, बशर्ते वह किसी प्रासंगिक कानून के तहत हो। भारतीय न्याय संहिता की धारा 15बी भी न्यायाधीशों को उनके न्यायिक कार्यों के लिए कानूनी सुरक्षा प्रदान करती है।
पहले भी लगते रहे हैं आरोप
हालांकि संविधान और अन्य कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत मिली विशेष कानूनी सुरक्षा के दुरुपयोग के चलते कुछ न्यायमूर्तियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आवास पर लगी आग को बुझाने के दौरान अनगिनत नकदी का मिलना उनकी स्वयं की प्रामाणिकता पर गंभीर सवाल खड़े कर गया। उच्चतम न्यायालय के कोलेजियम ने उन्हें तत्काल इलाहबाद उच्च न्यायालय स्थानांतरित करके यहां के सभी न्यायिक कार्यों से मुक्त कर दिया।
जाहिर है, जब इतनी बड़ी रकम मिलेगी तो प्रश्न भी उठेंगे कि आखिर एक न्यायमूर्ति के घर इतने रुपए कहां से आ गए, कहीं यह रुपए किसी गलत फैसले देने की एवज में तो नहीं लिए गए, इत्यादि। न्यायमूर्तियों पर कदाचार व भ्रष्टाचार के आरोप तो पहले भी लगते रहे हैं परन्तु खुलेआम रुपयों को देखने का यह दूसरा मामला था।
यदि न्यायमूर्तियों को विशेष कानूनी सुरक्षा केवल न्यायिक कार्यों के लिए ही दी गई है तो फिर न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा प्रकरण में सीधे कोई प्राथमिकी दर्ज क्यों नहीं की गई, यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है। उन पर सीधे एफआईआर दर्ज न होने के कारण सर्वोच्च न्यायालय भी आलोचनाओं का शिकार हो रहा है।
दरअसल सीधे एफआईआर दर्ज न होने के पीछे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1991 में के वीरास्वामी बनाम भारत संघ मामले में दिया गया निर्णय है। इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश लोक सेवक होते हैं और उन पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 लागू होता है, लेकिन उनके खिलाफ किसी भी आपराधिक मुकदमे के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश की पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी। न्यायमूर्ति के. वीरास्वामी मद्रास उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थे और उनके खिलाफ सीबीआई ने 1976 में आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था।
1980 के दशक में यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा, जहां यह न्यायाधीशों की भ्रष्टाचार के मामलों में जांच और अभियोजन से जुड़ी संवैधानिक व्याख्या का मुद्दा बना और सर्वोच्च न्यायालय ने 1991 में निर्णय सुनाते हुए न्यायमूर्तियों पर एफआईआर दर्ज करने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की अनुमति अनिवार्य कर दी। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय की आलोचना भी हुई। प्रमुख कानूनविदों ने कहा कि यह निर्णय न्यायाधीशों को एक विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग बना देता है जिससे वे उस त्वरित जवाबदेही से बच जाते हैं, जिसका सामना आम नागरिकों को करना पड़ता है। यह अनुच्छेद 14 ‘समानता के अधिकार’ का भी उल्लंघन करता है, क्योंकि आम नागरिकों के खिलाफ बिना किसी अनुमति के मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। यह भी कहा गया कि इस निर्णय के कारण न्यायाधीशों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच और कार्रवाई धीमी हो सकती है।
न्यायमूर्ति वीरास्वामी के निर्णय के कारण न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा मामले में एफआईआर दर्ज कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जब याचिका दाखिल की गई और यह दलील दी गई कि एफआईआर दर्ज करने में देरी से सबूतों के साथ छेड़छाड़ का खतरा बढ़ गया है, इतने गंभीर आरोप के चलते न्यायपालिका पर जनता का विश्वास कमजोर हुआ है और यह भी तर्क दिया गया कि जब बेनामी नकदी का पता चल गया था, तो पुलिस को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इस मामले में आंतरिक जांच चल रही है, और जब तक यह जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक एफआईआर दर्ज करने की मांग उचित नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने ‘इन-हाउस प्रक्रिया’ को प्राथमिकता दी है।
‘इन-हाउस प्रक्रिया’ के पीछे सर्वोच्च न्यायलय द्वारा बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति ए.एम. भट्टाचार्य के मामले में दिया गया निर्णय है। 1994-95 में बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति ए.एम. भट्टाचार्य पर कुछ प्रकाशकों से उनकी पुस्तकों के लिए विदेश से धन प्राप्त करने के आरोप लगे थे। इन आरोपों के परिणामस्वरूप, बॉम्बे बार एसोसिएशन, महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल और वेस्टर्न इंडिया एडवोकेट्स एसोसिएशन जैसी बार संगठनों ने उनके इस्तीफे की मांग की। इन संगठनों ने न्यायमूर्ति भट्टाचार्य के खिलाफ जजेस (इंक्वायरी) एक्ट, 1968 के तहत कार्रवाई की भी मांग की अधिवक्ता सी. रविचंद्रन अय्यर, ने सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर करके बार काउंसिल और बार एसोसिएशनों को न्यायमूर्ति भट्टाचार्य पर इस्तीफा देने के लिए दबाव डालने से रोकने का अनुरोध किया।
1995 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और गरिमा बनाए रखने के लिए न्यायाधीशों के खिलाफ किसी भी शिकायत को सार्वजनिक रूप से उछालने की बजाए, उसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा जाना चाहिए। इस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायाधीशों की नैतिक अखंडता और आचरण पर सवाल उठाने वाले मामलों को संसद में महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से हल करना हमेशा व्यावहारिक नहीं होता। इसलिए, न्यायपालिका को अपनी प्रतिष्ठा और स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए एक आंतरिक तंत्र की आवश्यकता थी। इस फैसले के बाद, 1997 में सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जे.एस. वर्मा ने एक ‘इन-हाउस प्रक्रिया’ का मसौदा तैयार किया।
इसका उद्देश्य यह था कि अगर किसी न्यायाधीश पर आरोप लगते हैं, तो उसकी प्रारंभिक जांच न्यायपालिका के भीतर ही की जाएगी, न कि सार्वजनिक रूप से। तभी से न्यायमूर्तियों पर किसी आरोप के लगने पर सबसे पहले ‘इन-हाउस प्रक्रिया’ का चलन शुरू हुआ। अगर इन-हाउस जांच में आरोप सही पाए जाते हैं, तो न्यायाधीश को स्वेच्छा से इस्तीफा देने या सेवानिवृत्त होने का सुझाव दिया जाता है।
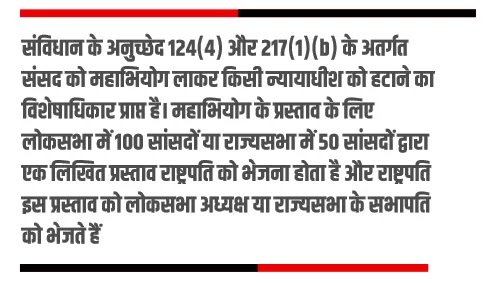
संसद को है महाभियोग का अधिकार
संविधान के अनुच्छेद 124(4) और 217(1)(b) के अतर्गत संसद को महाभियोग लाकर किसी न्यायाधीश को हटाने का विशेषाधिकार प्राप्त है। महाभियोग के प्रस्ताव के लिए लोकसभा में 100 सांसदों या राज्यसभा में 50 सांसदों द्वारा एक लिखित प्रस्ताव राष्ट्रपति को भेजना होता है और राष्ट्रपति इस प्रस्ताव को लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति को भेजते हैं। अध्यक्ष/सभापति इस शिकायत की जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के एक-एक न्यायाधीश और एक-एक वरिष्ठ न्यायविद् की तीन सदस्यीय समिति गठित करते हैं, अगर जांच समिति पाती है कि न्यायाधीश दोषी हैं। तो महाभियोग प्रस्ताव संसद में लाया जाता है। संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत से पारित होने पर ही राष्ट्रपति न्यायाधीश को पद से हटा सकते हैं।
न्यायमूर्ति निर्मल यादव बरी
 वर्ष 2008 में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति निर्मल यादव पर रियल एस्टेट मामले में रिश्वत मांगने का आरोप लगा था। मामले का पता तब चला था जब 15 लाख रु. की रिश्वत की राशि गलती से एक अन्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति निर्मलजीत कौर के निवास पर पहुंच गई थी। तब भी कॉलेजियम ने उन्हें ‘क्लीन चिट’ देते हुए उनका उत्तराखंड उच्च न्यायालय में स्थानांतरण कर दिया था, जहां से वह 2017 में सेवानिवृत्त हुईं। हाल ही में फैसला आया है जिसमें उन्हें सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया है। अपने आप में यह अनोखा मामला है जिसमें न्यायमूर्ति पर आरोप लगे उसके बाद भी वह पद पर बनी रहीं। इस मामले में फैसला आने से पहले ही कॉलेजियम ने उन्हें ‘क्लीनचिट’ दे दी थी। ऐसे में पारदर्शिता पर सवाल नहीं उठेंगे तो क्या होगा।
वर्ष 2008 में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति निर्मल यादव पर रियल एस्टेट मामले में रिश्वत मांगने का आरोप लगा था। मामले का पता तब चला था जब 15 लाख रु. की रिश्वत की राशि गलती से एक अन्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति निर्मलजीत कौर के निवास पर पहुंच गई थी। तब भी कॉलेजियम ने उन्हें ‘क्लीन चिट’ देते हुए उनका उत्तराखंड उच्च न्यायालय में स्थानांतरण कर दिया था, जहां से वह 2017 में सेवानिवृत्त हुईं। हाल ही में फैसला आया है जिसमें उन्हें सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया है। अपने आप में यह अनोखा मामला है जिसमें न्यायमूर्ति पर आरोप लगे उसके बाद भी वह पद पर बनी रहीं। इस मामले में फैसला आने से पहले ही कॉलेजियम ने उन्हें ‘क्लीनचिट’ दे दी थी। ऐसे में पारदर्शिता पर सवाल नहीं उठेंगे तो क्या होगा।
छह बार हुई महाभियोग की कार्यवाही
- भारत में अब तक छह न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही हुई है, लेकिन इनमें से किसी भी न्यायाधीश को पद से हटाया नहीं गया।
- 1993 में न्यायमूर्ति वी. रामास्वामी के विरुद्ध लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया, लेकिन बहुमत नहीं मिल सका, जिससे वे पद पर बने रहे।
- 2011 में न्यायमूर्ति पी.डी. दिनाकरण के विरुद्ध राज्यसभा के सभापति द्वारा जांच समिति गठित की गई, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही उन्होंने जुलाई 2011 में इस्तीफा दे दिया।
- 2011 में न्यायमूर्ति सौमित्र सेन के विरुद्ध राज्यसभा ने महाभियोग प्रस्ताव पारित किया, लेकिन उन्होंने लोकसभा में चर्चा से पहले ही इस्तीफा दे दिया।
- 2015 में न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला के विरुद्ध 58 राज्यसभा सांसदों ने महाभियोग का नोटिस दिया, लेकिन न्यायमूर्ति पारदीवाला ने विवादास्पद टिप्पणियां हटाकर मामला शांत किया।
- 2016 एवं 2017 में न्यायमूर्ति सी.वी. नागार्जुन रेड्डी के विरुद्ध दो बार महाभियोग प्रस्ताव लाया गया, लेकिन सांसदों द्वारा समर्थन वापस लेने के कारण प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी।
- 2018 में मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्र के विरुद्ध 71 राज्यसभा सांसदों ने महाभियोग का नोटिस दिया, लेकिन राज्यसभा के सभापति ने इसे खारिज कर दिया। इन छह के अलावा न्यायमूर्ति शामित मुखर्जी,जो दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे। हालांकि, उनके खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही पूरी नहीं हो सकी क्योंकि उन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया था।
- न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया भी अत्यंत कठिन और जटिल है, जिसके कारण अब तक किसी भी न्यायाधीश को इस माध्यम से पद से नहीं हटाया गया है। न्यायपालिका पर लगातार उठते सवाल और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इन-हाउस प्रक्रिया को ही प्राथमिकता पर रखना, न्यायपालिका की जवाबदेही और विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करते हैं।


















टिप्पणियाँ