यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः।
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः।। (श्रीमद्भागवत गीता 15.18)
अर्थात:- “मैं निरतिशय ईश्वर हूँ, क्योंकि मैं क्षरभाव से अतीत हूँ अर्थात् अश्वत्थ नामक मायामय संसार वृक्ष का अतिक्रमण किये हुए हूँ और संसार वृक्ष के बीज स्वरूप अक्षर से ( मूल प्रकृति से) भी उत्तम- अतिशय उत्कृष्ट अथवा अतिशय उच्च हूँ। अर्थात क्षर और अक्षर से उत्तम होनेके कारण? लोक और वेदमें? मैं पुरुषोत्तम नामसे विख्यात हूँ।”
प्राचीन काल से ही भारतीय वांग्मय में लोक शब्द का प्रचलन रहा है। जहाँ ऋग्वेद में “देहिलोकम्” के अनुसार लोक शब्द को “स्थान” के रूप में व्यक्त किया है, वहीं श्रीमद्भागवत गीता में योगेश्वर कृष्ण ने अतोऽस्मि लोके वेदे च कहकर लोक और वेद दोनों को स्वीकार किया है । इस प्रकार “लोक” शब्द विराट (अत्यंत) भी है और वामन (सम) भी। यह पुरुषोत्तम की तरह अनंत, अक्षर और असीम है। मानवीय जीवन का प्रतीक और जन मानस का पर्याय बन चुके “लोक” शब्द की सीमा केवल ग्राम या जन साधारण तक ही नहीं है, अपितु सम्पूर्ण सृष्टि को अपने में समाहित किए हुए है। मातृभाषा अर्थात बोली, लोकभाषा, लोक साहित्य एवं लोकांचल तक सीमित करके आंकना कहीं- न – कहीं “लोक” शब्द के साथ अन्याय होगा क्योंकि “लोक” शब्द अपने आप में सम्पूर्ण मानव जीवन पद्धति का द्योतक है । हमारी राष्ट्रीय विचारधारा “वसुधैव कुटुंबकम” ध्येय वाक्य को स्वीकार भी करती है। निश्चित रूप से संपूर्ण विश्व “लोक” में ही समाहित है और यही कारण है कि विश्व का अधिकांश साहित्य लिखित एवं वाचिक स्वरूप में “लोक” में विद्यमान है ।
भारतीय वांग्मय में लोकभाषा अर्थात मातृभाषा साहित्य के आगम एवं निगम स्वरूप को समान रूप से स्वीकारा है। यदि मातृभाषा एवं लोक बोली के प्रभाव को देखना हो तो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्रीरामचरित मानस से अच्छा कोई अन्य उदाहरण नहीं हो सकता। पांच सौ साल बाद भी श्रीरामचरित मानस को संपूर्ण देश में ही नहीं वरन विश्व भर में श्रद्धा एवं विश्वास के साथ गया एवं समझा जाता है। लोक एवं वेद के इस अंतर संबंध से गोस्वामी तुलसीदास जी भी भलीभांति परिचित थे। उन्होंने लिखा है:-
सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन उपाऊ
मातृभाषा अर्थात लोकभाषा के बिना लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता। हिन्दी भाषा के प्रचार-प्रसार के साथ ही लोक भाषाओं का प्रचार-प्रसार भी आवश्यक है। लोकभाषाएं किसी भी प्रकार से भाषा से कम नहीं हैं। लोकभाषा अर्थात मातृभाषा हमारी माँ है। जिस प्रकार माँ के आगे सारे रिश्ते गोण हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार जितनी भी भाषाएं हैं वे सभी भाषाएं मातृभाषा के आगे गोण है। कुछ भाषाओं का जन्म तो बोलियों से ही हुआ है क्योंकि बोलियां कहीं न कहीं संस्कृत एवं संस्कृति से अर्थात सनातन से जुड़ी है। मातृभाषा से ही “भाषा” समृद्ध होती है, भाषाओं का शब्द भंडार अधिकांशतः बोलियों से ही आया है। वर्तमान समय में जहां मातृभाषाओं एवं बोलियों का उपयोग कम हुआ है वहीं भाषाओं का वर्चस्व काफी हद तक बढ़ा है। इसमें कहीं कोई आश्चर्य व अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि प्रायः बेटी मां से अधिक कुशल व सफल होती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अपनी मातृभाषा को विस्मृत कर दें। ठीक वैसे ही हिंदी की अपेक्षा मातृभाषाओं की शब्द संपदा विपुल है। लोकभाषा में ऐसे अनेक शब्द हैं जिनका ठीक-ठाक पर्याय हिंदी में नहीं है। निश्चित रूप से हिन्दी को समृद्ध करने में लोकभाषाओं का अमूल्य योगदान है। इसीलिए हिंदी समाज को आधुनिक हिंदी के जनक भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की इन पंक्तियों से सीख लेने की जरूरत है :
निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल,
बिन निज भाषा-ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल,
विविध कला शिक्षा अमित, ज्ञान अनेक प्रकार,
सब देसन से लै करहू, भाषा माहि प्रचार।
अनेक देशों के राजनेता अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी मातृभाषा का ही इस्तेमाल करते हैं। जापानियों, चीनियों, कोरियनों का अपनी भाषा के प्रति गजब का सम्मान और लगाव है। बिना अंग्रेजी के इस्तेमाल के ऐसे देश विकास के दौड़ में कई देशों से काफी आगे हैं। फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश आदि भाषाओं ने कभी अंग्रेजी के सामने समर्पण नहीं किया। बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार के साथ ही “लोक” शब्द का प्रयोग मानव मात्र की वेदना, संवेदना एवं भावनाओं से विभूषित हुआ। इस धरा पर वैदिक ऋचाओं, पौराणिक आख्यानों, एवं कथाओं जैसे लिखित साहित्य के साथ-साथ वाचिक साहित्य के रूप में लोक कथाएं, बौद्ध कथाएं, दृष्टांत कथाएं आदि भी सनातन से विद्यमान हैं जो कहीं-न-कहीं हमारी मातृभाषा को समृद्धि प्रदान करते हैं।
यह बात कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, “मातृभाषा की समृद्धि, विकास, संरक्षण एवं संवर्धन में जितना योगदान मातृशक्ति का रहा है, उतना पुरुषों का नहीं रहा । लोक साहित्य, कला एवं संस्कृति के साथ-साथ लोक परंपराएं, कथा, वार्ता, गीत, संगीत एवं बच्चों के खेलकूद इत्यादि को निभाने व सहेजने का काम मुख्यतः अनादि काल से महिलाओं का ही रहा है। इसलिए एक महिला से बेहतर लोक साहित्य, संस्कृति, परंपरा एवं माँ, मातृभूमि एवं मातृभाषा को इतने अच्छे से कोई दूसरा नहीं समझ सकता ।
मातृभाषा एवं बोली में प्रचलित लोकगीतों का जन्म कब से हुआ इसका पता भले ही ना लग पाया हो लेकिन इन लोकगीतों में मानव और प्रकृति के विकास के अध्यायों को ठीक-ठीक पढ़ा जा सकता है। गोमुखी गंगा की तरह मातृभाषा में रचित इन लोकोन्मुखी गीतों से परंपरा एवं संस्कृति का जल अनादि काल से प्रवाहमान है। वर्तमान समय में लोक संस्कृति, लोकभाषा, बोली एवं लोक कला के क्षेत्र में बहुत सी विसंगतियां उत्पन्न हुई है और इन विसंगतियों के पीछे आधुनिकता की अंधी दौड़ कहीं ना कहीं जवाबदेह है। मोबाइल, इंटरनेट एवं आधुनिक पाश्चात्य संस्कृति के बेतहाशा प्रचार-प्रसार ने लोक में व्याप्त संस्कृति, परंपरा, कला एवं साहित्य को अत्यधिक नुकसान पहुंचाया है। देश से मातृभाषा एवं बोलियां ही नहीं बल्कि वर्तमान समय में मातृभाषा को समृद्धि प्रदान करने वाले माच, गरबे, लोक नृत्य, स्वांग, नाटक, नौटंकी, खेल, कठपुतली एवं इन सबसे जुड़े गायन, वादन तथा वाद्ययंत्र भी आज लुप्तप्राय से हो गये हैं।
किसी भी स्वाधीन राष्ट्र में उसकी राष्ट्रभाषा इतने समय तक उपेक्षित नहीं रही। तुर्की जब आजाद हुआ तो एक हफ्ते में वह विदेशी भाषा के चंगुल से मुक्त हो गया था। मुस्तफा कमाल पाशा की इच्छाशक्ति ने अविश्सनीय समय में तुर्की को राष्ट्रभाषा बना दिया। इससे ठीक उलट 15 अगस्त 1947 की आधी रात को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस देश के 30 करोड़ लोगों को अंग्रेजी में संबोधित किया। उसी दिन यह तय हो गया था कि देश उसी भाषा में चलेगा, जिस भाषा में नेहरू सोचते हैं। नेहरू के अंग्रेजी प्रेम की वजह से राजकाज में मातृभाषाओं को तो छोड़ ही दें, हिंदी का उपयोग भी शुरू नहीं हो सका। नेहरू के विचार में राजव्यवहार के लिए अंग्रेजी अनिवार्य थी। बाद की सरकारें इसी नजरिये से सोचती रहीं। शासन की जिम्मेवारी संभालनेवालों ने षड्यंत्र के तहत अंग्रेजी को तवज्जो देना शुरू किया और यह धीरे-धीरे व्यापक रूप लेता गया, जिसका नतीजा यह हुआ कि राष्ट्रीयता और राष्ट्रभाषा की सोच पीछे छूट गयी। अपनी भाषा के पक्ष में बोलने वालों की आलोचना होने लगी। ओर अंत में, मैं यही कहना चाहूंगा कि, अपनी मातृभाषा, लोकभाषा एवं बोली को महत्व दिए बिना लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था का कोई भी अंग संतोषजनक ढंग से तब तक काम नहीं कर सकता, जब तक की उसकी भाषा लोकभाषा के अनुरूप नहीं हो।



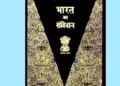














टिप्पणियाँ