बहुलतावादी समाज को यदि सागर कहा जाए तो यह समुद्र कुछ ऐसा है, जहां मजहबी आग्रह की लहरों में राजनीति की नाव अक्सर हिचकोले खाती है। आस्था आधारित राज्य व्यवस्थाएं कानून और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सिद्धांतों के साथ टकराव में आ जाती हैं।
हाल की दो घटनाओं ने इस विषय को एक बार फिर चर्चा में ला दिया। पहली घटना रोम की है, जहां पोप फ्रांसिस ने अमेरिकी प्रशासन की निर्वासन नीति की आलोचना करते हुए इसे मानवाधिकारों के लिए खतरा बताया। दूसरी घटना मलेशिया की है, जहां प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने मुसलमानों के लिए गैर-मुसलमानों के कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर एक विवादास्पद ‘गाइडलाइन’ पेश की, जिसे तीखी आलोचना के बाद वापस ले लिया गया। दोनों घटनाएं स्पष्ट रूप से दिखाती हैं कि आस्था आधारित कानून और आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्य अक्सर एक-दूसरे के विपरीत खड़े दिखते हैं।

अमेरिका में हाल ही में प्रवासियों के खिलाफ सख्त निर्वासन नीति लागू की गई है। प्रशासन का तर्क है कि यह नीति उन प्रवासियों को बाहर निकालने के लिए है, जो अपराधी हैं या जिन्होंने देश में अवैध रूप से प्रवेश किया है। अमेरिकी प्रशासन इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने का अनिवार्य कदम मानता है। लेकिन पोप फ्रांसिस ने इसे मानव गरिमा के खिलाफ बताते हुए चेतावनी दी कि ‘इसका अंत बुरा होगा।’ पोप की इस टिप्पणी ने मानवीय दृष्टिकोण को केंद्र में ला दिया, जबकि प्रशासनिक पक्ष इसे एक कानूनी आवश्यकता मानता है।
हालांकि, यहां एक विरोधाभास भी देखने को मिलता है। जब दुनिया इटली की प्रवासी नीतियों पर नजर डालती है तो पाती है कि वहां भी अवैध प्रवासियों के खिलाफ कड़े कानून लागू हैं। वैसे भी इटली में नागरिकता प्राप्त करना बेहद कठिन है। जन्म के आधार पर नागरिकता केवल उन्हीं को मिलती है, जिनके माता-पिता इटली के नागरिक हों। इसके लिए 10 वर्ष का वैध निवास और आर्थिक स्थिरता का प्रमाण अनिवार्य है। सवाल यह उठता है कि क्या पोप रोम और इटली की नीतियों की भी उतनी ही मुखरता से आलोचना करते हैं, जितनी उन्होंने अमेरिका की की है।
दूसरी घटना मलेशिया में सामने आई, जो मजहब आधारित कानूनों की सीमाओं का एक और उदाहरण है। मलेशिया की सरकार ने हाल ही में मुसलमानों के लिए निर्देश जारी किए थे, जिसमें यह तय किया गया था कि वे गैर-मुस्लिम कार्यक्रमों में कैसे शामिल हो सकते हैं। आलोचकों का मानना था कि इससे भेदभाव बढ़ सकता है और यह कदम समाज में सांस्कृतिक विविधता को कमजोर करता है। भारी आलोचना के बाद प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने इस प्रस्ताव को वापस ले लिया।
मलेशिया की इस घटना ने एक बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया—क्या एक लोकतांत्रिक और बहुलतावादी समाज में मजहब पर टिके निर्देशों का कोई स्थान हो सकता है? मलेशिया जैसा देश, जहां विभिन्न मत-पंथों और संस्कृतियों के लोग सह-अस्तित्व में हैं, वहां इस तरह की नीतियां सामाजिक ताने-बाने को तोड़ने का खतरा पैदा कर सकती हैं। आलोचकों ने इसे पांथिक स्वतंत्रता और सामाजिक समरसता के लिए खतरा बताया, क्योंकि इस ‘गाइडलाइन’ से मुसलमानों और गैर-मुसलमानों के बीच सामाजिक दूरी और अलगाव बढ़ने की आशंका थी।
मजहबी कानूनों की कठोरता का यह कोई नया उदाहरण नहीं है। ईरान का अनिवार्य हिजाब कानून, पाकिस्तान का ईशनिंदा कानून, सऊदी अरब में महिलाओं पर पाबंदिया और नाइजीरिया में बोको हराम का आतंक ये दर्शाते हैं कि आस्था का संकीर्ण स्वरूप अक्सर व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक प्रगति में बाधा बनता है।
हालांकि, सिविल सोसायटी और अंतरराष्ट्रीय दबाव के कारण कुछ इस्लामी देशों में सुधार के प्रयास भी हुए हैं। सऊदी अरब में महिलाओं को ड्राइविंग की अनुमति (2018) दी गई। ट्यूनीशिया में मुस्लिम महिलाओं को गैर-मुस्लिम पुरुषों से विवाह करने की छूट (2017) मिली। जॉर्डन ने बलात्कार कानूनों में सुधार किया और सूडान ने महिला जननांग विकृति (ऋॠट) पर प्रतिबंध लगाया।
इन घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि कठोर आस्था आधारित राज्य व्यवस्था अक्सर विविधता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आधुनिक संवैधानिक मूल्यों के लिए चुनौती बन जाती है। लेकिन सिविल सोसायटी और उन प्रगतिशील आस्था-विश्वासों के माध्यम से बदलाव संभव है, जो समय के अनुसार ढलने-बदलने योग्य लचीलापन और गुंजाइश रखते हैं। मलेशिया की घटना इसका उदाहरण है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में आलोचना और जनमत के दबाव से नीतियों में सुधार हो सकता है।
पोप फ्रांसिस की टिप्पणी मेें यह तथ्य नत्थी है कि उदारता का आधार ही यदि विसंगति से भरा हो, तो लोग उलटा आपकी आस्था और समझदारी पर सवाल खड़े करेंगे। यह याद दिलाता है कि करुणा और मानवाधिकारों को कानून से ऊपर रखने की बात अंतत: एक टकराव की ओर जाती है।
मजहब को व्यक्तिगत आस्था तक सीमित रखना और समाज में समानता, स्वतंत्रता और बहुलतावाद को प्राथमिकता देना ही एक स्वस्थ और सहिष्णु समाज की नींव रख सकता है। इतिहास ने दिखाया है कि सुधार संभव है, बशर्ते समाज इसकी दिशा में आगे बढ़ने का साहस करे। कट्टरता की काट इस साहस में ही है।
![]()
हितेश शंकर पत्रकारिता का जाना-पहचाना नाम, वर्तमान में पाञ्चजन्य के सम्पादक

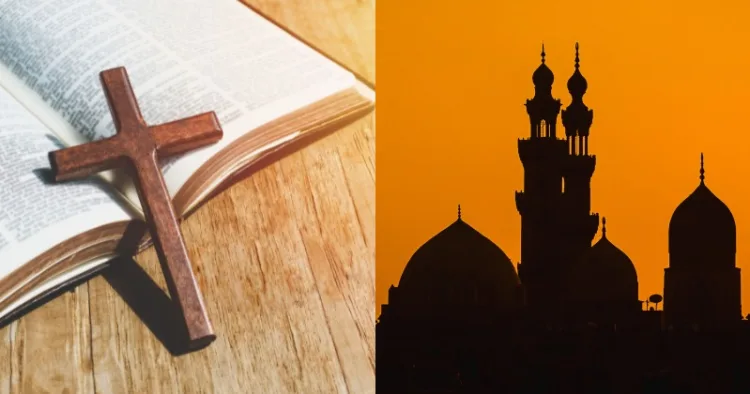
















टिप्पणियाँ