जून का महीना भारतीयों को याद दिलाता है छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का, प्लासी के संघर्ष का, रानी लक्ष्मीबाई का अमर बलिदान या फिर चापेकर बंधुओं द्वारा आताताई डब्ल्यू सी रैंड का वध। भारत के गौरवशाली दिनों से भरपूर यही जून का महीना भारतीय इतिहास के सबसे काले दिनों की भी याद दिलाता है, जब देश में लोकतंत्र की निर्मम हत्या की गई थी और जिसकी विभीषिका से हमारा देश आज भी उबर नहीं सका है. ये था 25 जून 1975, जब लोकतांत्रिक भारत में पहली बार इमरजेंसी का घृणित अध्याय जोड़ा गया। इस संहार ने न सिर्फ राजनैतिक दलों, समाजिक संगठनों और वैचारिक समूहों को अपना शिकार बनाया, बल्कि भारतीय लोकतंत्र के आधारस्तंभ मानी जाने वाली मीडिया को भी सरकार ने नहीं बख्शा।
इमरजेंसी के इन इक्कीस महीने में देश के नागरिकों ने न सिर्फ असहनीय पीड़ा सही बल्कि अनेक जघन्य अपराध होते देखे। लोकतंत्र की हत्या को छुपाने के लिए पहली बार मीडिया और प्रेस की आज़ादी का गला घोंटा गया। इंदिरा गांधी के तानाशाही के चर्चे विदेशों में भी होने लगे। इसी संदर्भ में टाइम पत्रिका ने 1975 में अपनी एक रिपोर्ट में भारत में आंतरिक आपातकाल लागू होने का जिक्र करते हुए शीर्षक दिया, “इंदिरा गांधी की तानाशाही कायम है।” आपातकाल लागू होते ही सबसे पहले तानाशाह इंदिरा गांधी सरकार अपने दमनकारी कृत्यों को छुपाने के लिए एक नया प्रावधान लेकर आR, जिसके बाद सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की रिपोर्टिंग पर तब तक रोक लगा दी गई जब तक सरकार उसे प्रकाशित करने की अनुमति न दे। इतना ही नहीं कांग्रेस सरकार ने 7 विदेशी संवाददाताओं को निष्कासित कर दिया और 29 अन्य को भारत में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया। स्वतंत्र भारत में शायद ही कभी ये कल्पना की जा सकती थी कि सरकार अपने खिलाफ उठी मीडिया की आवाज को दबाने के लिए इतने बड़े स्तर पर कार्रवाई करेगी। लेकिन इमरजेंसी के दौरान ऐसा भी हुआ जब सरकार के खिलाफ लिखने वाले 46 से अधिक पत्रकारों, 2 कार्टूनिस्ट और 6 फोटोग्राफर की मान्यता वापस ले ली गई और लगभग 258 पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया था। आश्चर्य की बात ये थी कि इंदिरा गाँधी सरकार ने ये सब “लोकतंत्र की रक्षा” और “राष्ट्र की सुरक्षा” की आड़ में किया था। लोकतंत्र क चौथे स्तंभ मीडिया को सख्त निर्देश दिए गए कि उन्हें सरकार का मुखपत्र बनकर ही काम करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, सरकार की आलोचना करने वाले लगभग सौ अखबारों और पत्रिकाओं से सरकारी विज्ञापन वापस ले लिए गए और पीटीआई जैसी न्यूज़ संस्थाओं का सरकारी समाचार तंत्र में जबरन विलय कर दिया गया. सरकार का उद्देश्य साफ था कि सरकार की आवाज ही इकलौती आवाज होगी और जनमानस की अभिव्यक्ति की आजादी को तहस-नहस कर दिया गया। यहां तक कि लोगों को सही समाचार न मिल पाए, इसके लिए सरकार द्वारा कई कुंठित प्रयास किए गए। इस दमनकारी योजना को अंजाम देने के लिए 1975 की मध्य रात्रि को आपातकाल की घोषणा के कुछ ही घंटों के भीतर, नई दिल्ली में समाचार पत्रों के केंद्र बहादुरशाह जफर रोड पर बिजली आपूर्ति काट दी गई थी, ताकि समाचार पत्र आपातकाल की घोषणा की ब्रेकिंग न्यूज़ न छाप सकें।
इन विषम परिस्थितियों में देश के बहुत से मीडिया संस्थान ऐसे भी थे जिन्होंने सरकार के सामने घुटने टेक दिए. देश के ज़्यादातर बड़े अखबार और पत्रिकाएं जैसे हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ़ इंडिया, द इलस्ट्रेटेड वीकली सरकार की प्रशंसा में बड़े-बड़े लेख निकालने लगे। टाइम्स ऑफ़ इंडिया, जो आर के लक्ष्मण के कार्टूनों द्वारा हर सामाजिक और राजनीतिक विषय पर टिप्पणी करने के लिए जाना जाता था, उन्होंने राजनैतिक कार्टून छापने लगभग बंद कर दिए. खुशवंत सिंह ने तो सरकार के समर्थन में रैलियों का आयोजन किया. सरकार ने सभी प्रकाशकों को ये फरमान जारी कर दिया कि सरकार से अनुमति लिए बिना कोई अखबार नहीं निकाला जायेगा। सरकार के इस फैसले से पत्र-पत्रिकाओं को बहुत नुकसान हुआ क्योकि केंद्र सरकार कई बार आधी रात के बाद समाचार छापने की इजाज़त देती थी और सुबह अखबार छपने में काफी देर हो जाती थी, जिससे अखबारों कि बिक्री गिरने लगी। इसके अलावा अखबारों से राजनैतिक खबरें नदारद होने लगीं जिससे अखबार खली पन्नों और बेमतलब के लेखों से भरे जाने लगे। लेकिन इस स्याह अंधेरे में भी कुछ दीप ऐसे थे जिन्होंने सरकार की निरंकुशता के आगे सर नहीं झुकाया और कड़े संघर्ष के बावजूद, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की आशाओं को जगाए रखा। इस दौरान कोई पत्र पत्रिका सरकार का डटकर सामना कर पायी तो वो थी इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया टुडे और स्टेट्समैन आदि। विरोध के तौर पर इन पत्रिकाओं ने अपने सम्पादकीय खाली छोड़ने शुरू किये। मीडिया पर हुए इस पक्षाघात ने कई भावी पत्रकारों और मीडिया संस्थानों को बर्बाद कर दिया, और कई पत्र पत्रिकाओं को अपना प्रकाशन बंद करने को मजबूर होना पड़ा। स्वतंत्र मीडिया को अपनी स्वतंत्रता की कीमत चुकानी पड़ी। जिन संपादकों ने सरकार के खिलाफ खबर छापने की हिमाकत की उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा और भारतीय अखबारों के दफ्तरों में इंदिरा गांधी सरकार के दरबारी पत्रकार नज़र आने लगे।
रेडियो और सिनेमा भी खुद को नहीं बचा पाए
रेडियो और सिनेमा जैसे मीडिया उपक्रम भी सरकार की निरंकुश नीतियों से खुद को बचा नहीं पाए। सरकार ने भारतीय सिनेमा का इस्तेमाल अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए करने का भरसक प्रयास किया। सूचना और प्रसारण मंत्री विद्या चरण शुक्ल ने हिंदी सिनेमा और रेडियो पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी। प्रसिद्द फिल्मकारों को मजबूर किया गया कि वो संजय गाँधी के 20 सूत्रीय कार्यक्रम के लिए फिल्म और गाने बनायें, वहीं सरकार की ज्यादतियों पर बनी फिल्मों को बैन कर दिया गया। जैसे संजय गांधी ने अपने खिलाफ बनी फिल्म ‘किस्सा कुर्सी का’ को न सिर्फ बैन करवाया बल्कि सरेआम उसकी रील्स को आग लगा दी गई, वहीं आंधी फिल्म को सिर्फ इसलिए बैन कर दिया गया क्योंकि वो इंदिरा गांधी के जीवन से प्रभावित बताई जा रही थी।
अमिताभ बच्चन जैसे कलाकारों ने इंदिरा को दिया समर्थन
इस दौरान बहुत से फिल्मी कलाकारों ने इंदिरा गांधी की सरकार के प्रति अपना समर्थन जताया जिनमें अमिताभ बच्चन जैसे बड़े कलाकार और बी आर चोपड़ा जैसे फिल्मकार शामिल थे। वहीं कई और कलाकारों ने स्वाभिमान और देशप्रेम को वरीयता देते हुए इंदिरा गांधी का मुखर विरोध किया। इन कलाकारों में देवानंद और अमोल पालेकर शामिल थे। सरकार की खिलाफत करने के लिए कई कलाकारों को सजा दी गई, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण थे मशहूर गायक किशोर कुमार, जिन्होंने संजय गांधी के बीस सूत्रीय कार्यक्रम पर गाना गाने से इंकार कर दिया, जिसके कारण उन्हें लंबे समय तक ऑल इंडिया रेडियो से बैन कर दिया गया।
सरकार ने रेडियो और सिनेमा को एक ऐसे माध्यम के रूप में देखा जिससे करोड़ों लोगों तक अपनी बात एक साथ पहुंचाई जा सकती थी। इसलिए इमरजेंसी के दौरान सरकार ने सरकारी रेडियो और दूरदर्शन पर अपना एकछत्र आधिपत्य स्थापित किया। इस दौरान दूरदर्शन पर कौन से शब्दों का प्रयोग हो रहा है, इस बात की भी निगरानी रखी जाती थी, और रेडियो और दूरदर्शन से सरकार को चुभने वाले शब्दों को ही गायब कर दिया गया।
पर्चों ने निभाई भूमिका
इस काल में बहुत से संगठनों और राजनैतिक पार्टियों के मुखपत्रों पर भी अंकुश लगा दिया गया. प्रसिद्ध विचारक प्रोफेसर राजेंद्र सिंह बताते है कि इमरजेंसी के दौरान जब सरकार ने सभी तरह कि प्रेस पर अंकुश लगा दिया था, तब कुछ संगठनों ने सरकार की आलोचना करते हुए कई पैम्फलेट प्रकाशित करके गुप्त रूप से बंटवाए थे। इन पैम्फलेट ने सरकार के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने में बड़ी भूमिका अदा की थी। हालांकि सरकार ने इन पैम्फलेट को भी दबाने की बहुत कोशिश की लेकिन क्योंकि ये पर्चे अलग अलग नामों से और अलग-अलग जगहों से छपते थे इसलिए इन्हें पकड़ पाना सरकार के लिए मुश्किल हो जाता था। इस तरह सीमित स्तर पर ही सही, इन पर्चों ने वो भूमिका अदा की जो बड़े-बड़े समाचार पत्र और पत्रिकाएं नहीं कर पाईं।
तानाशाह को आलोचना बर्दाश्त नहीं
इमरजेंसी का दौर भारतीय इतिहास का निर्मम और निरंकुश काल रहा और इस दौरान स्वतंत्र भारत में क्रूरतम यातनाएं दिखीं। वह दौर हमें याद दिलाता है कि एक तानाशाह बेहद डरपोक होता है जो हल्की सी आलोचना से भी सिहर जाता है। उसे हर तरफ षड्यंत्र दिखता है, हर कोई दुश्मन नजर आता है। ऐसे में वो पूरी दुनिया में सिर्फ अपनी आवाज सुनाना चाहता है, सिर्फ अपनी तस्वीर दिखाना चाहता है, सिर्फ अपनी बड़ाई कराना चाहता है। इसका सबसे सुगम मार्ग जो उसे नजर आता है वो है मीडिया। इसलिए हर तानाशाह मीडिया और अखबार पर कब्जा करने को आतुर रहता है ताकि उसके शासन की हकीकत दुनिया तक न पहुंच पाए। लेकिन अटल सत्य ये भी है कि डर के साम्राज्य में प्रशंसा ज्यादा देर पनप नहीं पाती। आज के समय जब मीडिया पर सरकार के प्रभाव की बात होती है तो हमें वो दौर याद आता है जब सच बोलने के लिए पत्रकारों को अपनी जान हथेली पर रखनी पड़ती थी। भारतीय मीडिया ने वो दौर भी देखा है जब खबरे अखबार नहीं सरकार तय करती थी, और पत्रकारों को कठपुतलियों की तरह नचाया जाता था। भारत उस दौर से काफी आगे आ गया है और उम्मीद करता है कि उसे भविष्य में फिर कभी ऐसा दौर नहीं देखना पड़े।
(लेखिका वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन की प्रोजेक्ट हेड हैं , सह लेखक वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन में रिसर्च एसोसिएट हैं)















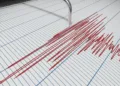

टिप्पणियाँ