मरुस्थलीकरण आज दुनिया की विकट समस्या बनता जा रहा है, जिसका पर्यावरण पर गहरा असर पड़ रहा है। मरुस्थलीकरण का अर्थ है रेगिस्तान का फैलते जाना, जिससे विशेषकर शुष्क क्षेत्रों में उपजाऊ भूमि अनुपजाऊ भूमि में तब्दील हो रही है। इसके लिए भौगोलिक परिवर्तन के साथ-साथ मानव गतिविधियां भी बड़े स्तर पर जिम्मेदार हैं। शुष्क क्षेत्र ऐसे क्षेत्रों को कहा जाता है, जहां वर्षा इतनी मात्रा में नहीं होती कि वहां घनी हरियाली पनप सके। पूरी दुनिया में कुल स्थल भाग का करीब 40 फीसदी (लगभग 5.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर) शुष्क क्षेत्र है और मरुस्थलीकरण प्रायः ऐसे ही शुष्क इलाकों में ज्यादा देखा जा रहा है।
वैश्विक स्तर पर रेत का साम्राज्य बढ़ते जाने के कारण कई देशों में अन्न का उत्पादन घटने से मानव जाति तो प्रभावित हो ही रही है, जीव-जंतुओं की तमाम प्रजातियों पर भी भयानक दुष्प्रभाव हो रहा है।
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से वैश्विक स्तर पर मरूस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए जन-जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1995 से प्रतिवर्ष 17 जून को ‘विश्व मरूस्थलीकरण रोकथाम और सूखा दिवस’ मनाया जा रहा है। मरूस्थलीकरण और सूखे की बढ़ती चुनौतियों के मद्देनजर इससे मुकाबला करने हेतु लोगों को जागरूक करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1994 में मरूस्थलीकरण रोकथाम का प्रस्ताव रखा था।
इस दिवस के जरिये लोगों को जल तथा खाद्यान्न सुरक्षा के साथ पारिस्थितिकी तंत्र के प्रति जागरूक करने, सूखे के प्रभाव को प्रत्येक स्तर पर कम करने के लिए कार्य करने और नीति निर्धारकों पर मरूस्थलीकरण संबंधी नीतियों के निर्माण के साथ उससे निपटने के लिए कार्ययोजना बनाने का दबाव बनाने का प्रयास किया जाता है। इस वर्ष यह दिवस ‘भूमि के लिए एकजुटता, हमारी विरासत, हमारा भविष्य’ विषय के साथ मनाया जा रहा है, जो भावी पीढ़ियों के लिए हमारे ग्रह के महत्वपूर्ण भूमि संसाधनों को संरक्षित करने के लिए सामूहिक कार्रवाई के महत्व को रेखांकित करता है।
विश्व का 95 प्रतिशत भोजन कृषि भूमि पर उत्पादित होता है, यही भूमि हमारी खाद्य प्रणालियों का आधार है लेकिन चिंता का विषय है कि इसमें से एक तिहाई भूमि वर्तमान में क्षरित हो चुकी है, जो दुनियाभर में 3.2 बिलियन लोगों को प्रभावित करती है, विशेष रूप से ग्रामीण समुदायों और छोटे किसानों को, जो अपनी आजीविका के लिए भूमि पर निर्भर हैं, जिससे भूख, गरीबी, बेरोजगारी और जबरन पलायन में वृद्धि होती है। जलवायु परिवर्तन इन मुद्दों को और गंभीर बना देता है, जिससे टिकाऊ भूमि प्रबंधन और कृषि के लिए गंभीर चुनौतियां उत्पन्न होती हैं तथा पारिस्थितिकी तंत्र का लचीलापन कमजोर हो जाता है।
जलवायु संकट सूखा, बाढ़, जंगलों में आग लगने की घटनाओं के जरिये मरुस्थलीकरण को बढ़ा रहा है। एक ओर जहां जलवायु का गहराता संकट मरुस्थलीकरण की समस्या को बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी ओर मरुस्थलीकरण जलवायु संकट को और गंभीर बना रहा है अर्थात् मरुस्थलीकरण और जलवायु संकट एक-दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं। जलवायु संकट में भू-क्षरण का भी बहुत बड़ा योगदान है। पर्यावरणविदों के मुताबिक मिट्टी में वातावरण में मौजूद कार्बन से तीन गुना ज्यादा कार्बन है और पृथ्वी पर मौजूद कार्बन का सबसे बड़ा भंडार मिट्टी में ही है।
कार्बन का उत्सर्जन मिट्टी से निकलकर वातावरण में पहुंचकर वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी कर रहा है और मरुस्थलीकरण के कारण यह समस्या और ज्यादा बढ़ रही है। पृथ्वी का निरन्तर बढ़ता तापमान, सौर ऊर्जा और हवा की प्रकृति में भी बदलाव ला रहा है। आंकड़ों के अनुसार विश्वभर में कुल कार्बन उत्सर्जन के 10-12 फीसदी (3.6-4.4 बिलियन टन) उत्सर्जन के लिए भू-क्षरण जिम्मेदार है और भारत को तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक माना जाता है, जहां कुल उत्सर्जित कार्बन डाईऑक्साइड की तुलना में भू-क्षरण से 50 फीसदी ज्यादा कार्बन डाईऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है।
सूखा मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया को तेज कर देता है और भारत की आबादी का एक बहुत बड़ा भाग तो शुष्क इलाकों में ही रहता है। देश का लगभग 70 प्रतिशत भूभाग (करीब 22.83 करोड़ हेक्टेयर) शुष्क माना गया है और इस शुष्क भूभाग की उत्पादकता काफी कम है। देश का करीब 7.36 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्रफल मरुस्थलीकरण से प्रभावित है और भारत के कई इलाके तो प्रायः सूखे की चपेट में रहते हैं।
विश्व में मौजूद कुल मवेशियों का 8 फीसदी पालन भारत में होता है जबकि भारत में दुनियाभर में मौजूद कुल चरागाहों का केवल आधा फीसदी ही भारत में है। इसी प्रकार भारत के पास विश्व के कुल स्थल भाग का केवल 2.4 फीसदी ही है लेकिन कुल मानव आबादी का 18 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा हमारे देश में ही है। विश्व के अन्य शुष्क इलाकों की तुलना में भारत के शुष्क इलाकों में मानव आबादी और मवेशियों का दबाव कहीं ज्यादा है। मनुष्यों और मवेशियों का यह असहनीय दबाव मरुस्थलीकरण की समस्या को बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा है।
शुष्क इलाकों का प्राकृतिक तंत्र मनुष्यों द्वारा डाले जाने वाले अनावश्यक दबाव के कारण चरमराने लगता है और इस विघटनकारी प्रक्रिया को नहीं रोके जाने की स्थिति में समूचा तंत्र रेगिस्तान की भेंट चढ़ जाता है। लकड़ी के लिए पेड़ों की अंधाधुंध छंटाई अथवा अत्यधिक चराई के कारण उस तंत्र में प्राकृतिक उपयोगी पौधों की संख्या काफी घट जाती है, जिनका स्थान अनुपयोगी और अखाद्य पेड़-पौधे ले लेते हैं, जिसका दुष्परिणाम यही होता है कि वह प्राकृतिक तंत्र पहले से भी बहुत कम संख्या में मनुष्यों और मवेशियों को पोषित कर पाता है और यही दुष्चक्र मरुस्थलीकरण को गति प्रदान करता है।
रेगिस्तानी इलाकों में चूंकि बारिश बहुत ही अनियमित ढ़ंग से होती है, ऐसे में ऐसे इलाकों में उपलब्ध पानी की बेहद सीमित मात्रा से कृषि उत्पादकता पर काफी असर पड़ता है। वैसे तो शुष्क इलाकों में वर्षा कम होती है लेकिन जो वर्षा होती है, वह काफी तेज और तूफानी किस्म की होती है, जिससे प्रायः ऐसे इलाकों में बारिश बाढ़ का रूप लेकर उपजाऊ मिट्टी को ही बहा ले जाती है और वहां बड़े-बड़े गड्ढ़े तथा नाले बन जाते हैं, जो प्रायः खेती के लिए बेकार हो जाते हैं। कई क्षेत्रों में इसी के चलते रेत के बड़े-बड़े टीले बन जाते हैं। एक अनुमान के अनुसार प्रतिवर्ष बंजर इलाकों में प्रति हेक्टेयर क्षेत्र से पानी के कटाव के कारण 16.35 टन मिट्टी बह जाती है।
बार-बार आने वाला सूखा मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया को तेज कर देता है। मिट्टी का कटाव होने का एक दुष्परिणाम यह भी है कि पानी के साथ बहकर आने वाली मिट्टी जलाशयों में भर जाती है, जिससे उनकी जलधारण क्षमता घट रही है और इस कारण बाढ़ की स्थिति काफी गंभीर हो जाती है। बीते कुछ वर्षों से देश के कई इलाकों में लाखों लोगों को बारिश के कारण बाढ़ का कहर झेलने को विवश होना पड़ रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण यही है। यही नहीं, बड़ी-बड़ी पनबिजली परियोजनाओं के सरोवरों में मिट्टी भर जाने से उनसे निर्मित होने वाली बिजली की मात्रा भी घट जाती है।
जहां तक वातावरण में कार्बन कम करने का सवाल है तो तापमान में डेढ़ डिग्री सेल्सियस कमी के लक्ष्य को हासिल करने के लिए वातावरण से कार्बन को तेजी से सोखने की जरूरत है और पर्यावरणविदों के मुताबिक यह प्राकृतिक कार्बन सिंक की क्षमता में वृद्धि करके ही हो सकता है और जंगलों तथा कृषि की समस्या को कम करने वाले सिंक मैकेनिज्म से एक तिहाई से भी ज्यादा जलवायु आपदा कम की जा सकती है। इसका सबसे बेहतर तरीका यही माना जा रहा है कि कार्बन को वनों, चारागाह और मिट्टी में समेट दिया जाए, जो मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए भी बेहद जरूरी है।
वनीकरण, वनस्पति कवर में सुधार, जल का दक्षतापूर्ण उपयोग, मिट्टी के कटाव को बेहतर कृषि पद्धति के जरिये कम करना इत्यादि उपायों के जरिये मिट्टी में बायोमास उत्पादन और जैविक कार्बन कंटेंट में सुधार संभव है। पर्यावरणविदों का मानना है कि जंगलों का नुकसान रोककर और दोबारा लगाकर 2050 तक 150 बिलियन टन से भी ज्यादा कार्बन कम किया जा सकता है और इस अवधि में शुष्क क्षेत्रों में कृषि भूमि के अलावा 30-60 बिलियन टन कार्बन का संचय किया जा सकता है।
बहरहाल, मरुस्थलीकरण की समस्या बढ़ते जाने से कृषि की उत्पादनशीलता में जो कमी आ रही है, उससे होने वाले नुकसान को करीब 25 हजार करोड़ रुपये आंका गया है। चिंताजनक स्थिति यह है कि भारत जैसे विकासशील देश में निरन्तर बढ़ती आबादी की मूलभूत जरूरतों की पूर्ति के लिए कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने की जरूरत महसूस की जाती रही है लेकिन मरुस्थलीकरण के चलते इसमें आती कमी नीतियों में बड़े बदलावों की जरूरत पर जोर देती है।
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार, पर्यावरण मामलों के जानकार और ‘प्रदूषण मुक्त सांसें’ पुस्तक के लेखक हैं)






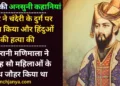











टिप्पणियाँ