जाने क्यों, पिछले कुछ वर्षों से भारत के कुछ राज्यों में राज्यपालों के प्रति राज्य सरकारों का विद्वेष से भरा रवैया देखने में आया है। वैचारिक विरोध को राज्यवासियों के हितों पर आघात के अस्त्र के नाते प्रयोग करने के इसी प्रयत्न को पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और दिल्ली में बहुत साफ देखा गया। क्या कोई राज्य सरकार राज्यपाल के पद को अपमानित कर सकती है? राज्यपाल पद की गरिमा को लेकर संविधान निर्माताओं ने क्या कहा है? राज्यपाल की किसी राज्य में क्या भूमिका होती है? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिन पर एक निष्पक्ष दृष्टि डालने की जरूरत है।
‘राज्यपाल’ का शाब्दिक अर्थ होता है राज्य का पालक और ‘मुख्यमंत्री’ का शाब्दिक अर्थ होता है राज्य के सभी मंत्रियों का मुखिया! भारत के हर राज्य में राज्यपाल को राष्टÑपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। राज्यपाल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156 के तहत मनोनीत किए जाते हैं। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन वह अपने सभी निर्णय मुख्यमंत्री व उनकी मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर संवैधानिक दायरे में रहते हुए करता है।
संविधान राज्यपाल को संवैधानिक प्रहरी तथा केंद्र और राज्य के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी की भूमिका प्रदान करता है। राज्यपाल एक स्वतंत्र संवैधानिक पद होता है अत: वह केंद्र सरकार के अधीन नहीं होता। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव आंबेडकर ने राज्यपालों से संबंधित प्रावधानों को बहुत बारीकी से स्थापित किया है। उनकी इसी दूरदर्शिता की वजह से आज भारत विश्व का सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली लोकतंत्र है जहांसंघ व राज्य की शक्तियां बहुत से अंतर्विरोधों के बाद भी कुशलता के साथ आपसी समन्वय रखते हुए देश को आगे ले जा रही हैं।
संविधान के इस संबंध में अनुच्छेदों के अनुसार ही, जब राज्य विधानमंडल राज्यपाल के समक्ष कोई विधेयक प्रस्तुत करता है तब उसके पास अनेक विकल्प होते हैं, जैसे, एक, वह विधेयक पर सहमति देकर उसे अधिनियम बना सकता है। दो, वह विधेयक पर अपनी सहमति न दे, जिसका अर्थ है कि विधेयक निरस्त कर दिया जाए। तीन, वह विधेयक के उपबंधों पर पुनर्विचार के अनुरोध के साथ उसे राज्य विधानमंडल को वापस भेज दे। चार, यदि उक्त विधेयक विधानमंडल द्वारा संशोधन के बाद या बिना संशोधन किए राज्यपाल को वापस भेज दिया जाता है तब वह उस विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। राष्ट्रपति या तो उस पर सहमति दे सकते हैं या अनुमति रोक सकते हैं अथवा राज्यपाल को विधेयक पर पुनर्विचार करने के लिए राज्य विधानमंडल को वापस भेजने का निर्देश दे सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि यदि कोई विधेयक राज्य के उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता हो तब राज्यपाल द्वारा विधेयक पर रोक लगाना अनिवार्य हो जाता है। विधेयक यदि संविधान के प्रावधानों, राज्य के नीति-सिद्धांतों, देश के व्यापक हितों या गम्भीर राष्ट्रीय महत्व के विरुद्ध हो अथवा संविधान के अनुच्छेद 31ए के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो तब उस संबंध में उचित फैसला लेना राज्यपाल के विवेकाधीन होता है।
राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति मंत्रिपरिषद की तुलना में बहुत सुरक्षित होती है। डॉक्टर आंबेडकर का बनाया संविधान राज्यपाल को प्रभाव एवं शक्ति दोनों से सुशोभित करता है। वास्तव में संघीय व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए ही राज्यपाल के पद को भारतीय संविधान में सुरक्षित रखा गया है।
इसी संविधान के अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद 356 पर भी चर्चा करना समीचीन रहेगा। अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल के अनुरोध पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। यहां ध्यान रहे कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में 1956 से 2009 तक 90 बार केंद्र सरकारें राज्यों की सरकारों को बर्खास्त करके वहां राष्ट्रपति शासन लगा चुकी हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने स्वयं 50 बार इस अनुच्छेद का दुरुपयोग किया था। आपातकाल में इस संविधान का दुरुपयोग साफ देखने में आया था। 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी ने देश पर आपातकाल थोप दिया था। तब इंदिरा सरकार ने संविधान निर्माताओं व समाज सुधारकों के सबसे प्रिय रहे मौलिक अधिकारों का भी हनन कर दिया था।
देश की स्वतंत्रता के पश्चात कांग्रेस पार्र्टी तीन आम चुनावों में भारी बहुमत से जीती थी, परंतु चौथे आम चुनाव का परिणाम एक बड़े परिवर्तन की शुरुआत का माध्यम बना था। 1951 से 1967 तक के लोकसभा चुनाव राज्यों के चुनावों के साथ हुए थे, परंतु चौथे आम चुनाव के बाद केन्द्र में इन्दिरा गांधी की सरकार तो बनी लेकिन उसे उतना बहुमत नहीं मिला था। साथ ही अनेक राज्यों में गैर कांग्रेसीगठबंधन जीते थे। ऐसे में केन्द्र व राज्य सरकारों के बीच कड़ी के नाते काम करने वाले राज्यपाल के पद को कसौटी पर कसा जाना ही था। यही समय था जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 50 राज्य सरकारों को अनुच्छेद 356 के माध्यम से बर्खास्त किया था।
उल्लेखनीय है कि केन्द्र की वर्तमान मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्ष में अत्यधिक संयम बरतते हुए किसी भी राज्य की चुनी हुई सरकार को बर्खास्त नहीं किया है, जबकि अनेक राज्यों में इस प्रकार के हालात अनेक अवसरों पर देखने में आए हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां ममता बनर्जी की सरकार ने पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ की गरिमा को अनेक बार ठेस पहुंचाई और उस पद को खुलेआम चुनौती दी। अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से उद्दंडता के सारे मापदंडों को तोड़ा है। तो भी मोदी सरकार ने संयम ही बरता और अनुच्छेद 356 का प्रयोग नहीं किया। वहां राष्टÑपति शासन नहीं लगाया। जबकि तमाम मीडिया और समाचारपत्र पश्चिम बंगाल में संविधान के खुलेआम किए जा रहे अपमान पर लंबे-लंबे लेख छाप रहे थे, बहस छिड़ी थी कि ‘अब तो हद हो गई, ममता सरकार बेलगाम होती दिख रही है, वहांं राष्टÑपति शासन लगाए जाने के हालात बन गए हैं’, आदि।
पश्चिम बंगाल में सन्देशखाली में तृणमूल कांग्रेस की शह पर अपराधी किस्म के दबंग तत्व महिलाओं पर वर्षों से जिस प्रकार के अत्याचार करते आ रहे थे, उसकी पिछले दिनों पोल-पट्टी खुली थी। तिस पर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पीड़ित महिलाओं के प्रति घोर असंवेदनशील होकर शाहजहां शेख सरीखे अपराधियों को बचाने का ही प्रयास करती दिखीं, और आज भी चुनाव रैलियों में वे कट्टर इस्लामी अपराधी तत्वों को अभयदान सा देती दिखती हैं।
संदेशखाली के उन दर्दनाक खुलासों के बाद भी देश में यह आवाज उठी थी कि पश्चिम बंगाल में अब राष्ट्रपति शासन लगाया ही जाना चाहिए। लेकिन वहां के राज्यपाल और केंद्र सरकार ने असामान्य धैर्य का परिचय देते हुए पश्चिम बंगाल सरकार को संविधान की मर्यादा का ध्यान रखने की सलाह दी, वहां राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया।
उधर दक्षिण के राज्य केरल में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को भी मुख्यमंत्री पिनरई विजयन की सरकार बेवजह अपमानित करने का अभियान जैसा चलाती आ रही है।
तमिलनाडु में स्टालिन के नेतृत्व वाली द्रमुक सरकार राज्य के राज्यपाल आर. एन. रवि पर लगातार हमलावर रहती है। इसी संदर्भ में दिल्ली की आआपा की केजरीवाल सरकार का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। केजरीवाल सरकार 2013 से 2016 तक, लगातार 4 साल तत्कालीन उपराज्यपाल नजीब जंग पर बेवजह के आरोप लगाती रही थी, अपनी नाकामियों के पीछे उन्हें दोषी ठहराती रही थी। आज भी केजरीवाल की आआपा सरकार उपराज्यपाल के संदर्भ में लगभग उसी ढर्रे पर चल रही है।
दिल्ली के वर्तमान उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के द्वारा निर्गत आदेशों की जान-बूझकर अवहेलना की जाती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हाल ही में अपने एक साक्षात्कार में स्पष्ट कहा है कि उनकी सरकार संविधान को सर्वोपरि और पवित्रतम मानती है। इसके दुरुपयोग अथवा गलत विवेचना को न तो केन्द्र सरकार स्वीकारती है, न ही यह चाहती है कि कोई राज्य सरकार ऐसा करे।
संघ और राज्य के आपसी संबंधों और समन्वय को लेकर भी केन्द्र का पूरा प्रयास सकारात्मक रहता है। मोदी स्वयं 15 वर्ष गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं इसलिए राज्यों के अधिकारों, दायित्वों और चुनौतियों को समझते हैं। उनका पूरा प्रयास रहता है कि संघ-राज्य संबंध संविधान में उल्लिखित सिद्धांतों पर ही चलें और आपस में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाए। लेकिन दुर्भाग्य से, जिन राज्यों की ऊपर चर्चा की गई है, उनकी सरकारें भिन्न विचारधारा के प्रति इस हद तक असहिष्णु रही हैं कि हर चीज को राजनीति के चश्मे से देखती हैं।
राज्यपालों का अपमान करके वे भले अपने कैडर की नजरों में चढ़ती हों, देश, लोकतंत्र और संविधान के साधकों की नजर में नि:संदेह तिरस्कृत ही होती हैं।
(लेखक सर्वोच्च न्यायालय में अपर महाधिवक्ता हैं)

















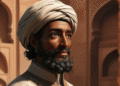
टिप्पणियाँ