केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रीजीजू ने पाञ्चजन्य के साबरमती संवाद में न्यायपालिका के लिए सकारात्मक सुझाव के साथ बदलाव के बिंदुओं को बड़ी बारीकी से रेखांकित किया। उन्होंने न्यायिक एक्टिविज्म, आंतरिक स्वनियम तंत्र की आवश्यकता, कोलेजियम सिस्टम, अंकल जज सिंड्रोम, न्यायपालिका की आलोचना, औपनिवेशिक बोझ, भाषा के दबाव जैसे बिंदुओं पर खुलकर बात की। प्रस्तुत है केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रीजीजू से पाञ्चजन्य के संपादक हितेश शंकर की बातचीत

आज की राजनीति में भागदौड़ बहुत हो गई है। क्या बदल गया है देश की राजनीति में। पहले मंत्री को इतनी मेहनत करनी पड़ती थी क्या?
सबने बदलती हुए राजनीति को करीब से देखा है। एक जमाने में चुने हुए या पद पर बैठे नेता दिशा दे देते थे, तो काम अपने-आप चलता था। आज राजनीति में नेता जो कुछ भी कहे, उस पर अमल के लिए उसे पीछे लगना पड़ता है। सोशल मीडिया के आने से कुछ चीजें आसान हुई हैं तो कुछ चुनौतियां भी बढ़ी हैं। आपके सवाल से सीधी जुड़ी एक बात कहना चाहता हूं – कांग्रेस के जमाने में मैं सांसद था। कांग्रेस के मंत्री काम भी करते थे और परिवार के साथ छुट्टियां भी मनाते थे। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरा, देश का कार्य करने के लिए इतना काम है कि हम जितना भी समय दें, वो काफी नहीं होता। जिंदगी में सीमित समय है। इसलिए आज के समय में जनसेवा कोई आसान काम नहीं रह गया है। मोदी जी के नेतृत्व में तो आपको हर पल लोगों के बीच में ही रहना है। यही समय की मांग भी है।

पहले कहा जाता था कि राजनीति पके-पकाये लोगों का क्षेत्र है। आपको एक युवा के तौर पर केन्द्रीय मंत्रिमंडल में लिया गया। अलग-अलग भूमिकाओं में परखा भी गया और आगे भी बढ़ाया गया। इसे आप कैसे देखते हैं? क्या पहले की राजनीति में यह संभव था?
काफी चीजें बदल गई हैं और समय के साथ हमको बदलना होता है। आज कई देशों में 35 साल में प्रधानमंत्री, 34 साल में राष्ट्रपति बन जाते हैं। अभी अमेरिका के राष्ट्रपति 80 साल के हैं। अब उम्र कोई मायने नहीं रह गई है। आप किस ऊर्जा के साथ कार्य करते हैं, उसे आपको देखना होगा। मैं राजनीति से पहले एबीवीपी से जुड़ा रहा। बाद में 1996-97 में राजनीति करना शुरू किया। कुशाभाऊ ठाकरे जी जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मैं तब से राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हूं। फिर आडवाणी जी और राजनाथ जी के समय में राष्ट्रीय सचिव रहा। इतने सालों से भाजपा के साथ काम करने के बाद मैं अपनी उम्र, पृष्ठभूमि के बारे में कभी नहीं सोचता। देश के लिए काम करना है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपनी टीम में मुझे जो दायित्व दिया है, उस जिम्मेदारी को सही ढंग से निभाने के बारे में सोचता हूं। वर्तमान सरकार के सभी मंत्रियों को प्रधानमंत्री जी की सोच के साथ तादात्म्य बनाकर ही काम करना होगा। एक विभाग की सोच अलग, दूसरे की अलग, ऐसे बिखरी हुई नहीं, बल्कि एक दिशा में चलने वाली सरकार है।
लोग सोचते हैं कि आमतौर पर कानून मंत्री बड़ी उम्र के, प्रख्यात न्यायविद् होते हैं। लेकिन मेरा काम अदालत में वकालत करना नहीं है। मेरा काम न्याय व्यवस्था ठीक से चले, न्याय आम लोगों के दरवाजे तक पहुंचे, सरकार के हर विभाग को विधिक सेवा दी जाए, यह देखना है। राज्य सरकारों से, संगठनों से, सबसे मिलकर सामूहिक रूप से बातचीत करना एवं सामंजस्य बनाना ही एक मंत्री की जिम्मेदारी होती है। इसलिए मैं वरिष्ठ या कनिष्ठ के हिसाब से नहीं देखता। मैं स्वयं को देश का एक सिपाही मानता हूं और मंत्री होने के नाते मेरा एक ही दायित्व है, देश को संभालना, देश की मदद करना एवं देश की सेवा करना।

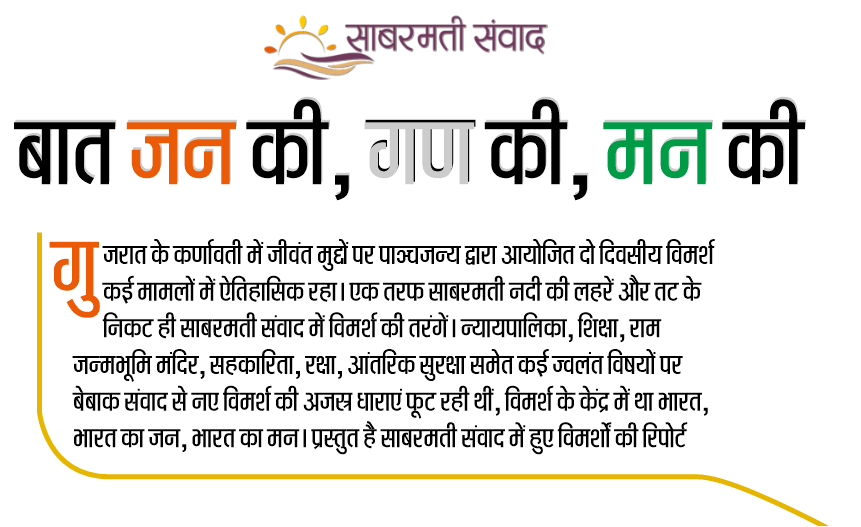
 देश में न्यापालिका के अधिकार क्षेत्र की बात होती है। इसके साथ ही कई बार यह भी आरोप लगता है कि एक्टिविज्म न्यापालिका को भी प्रभावित कर रहा है। न्यायिक एक्टिविज्म की भी बात आती है। आप इस पूरे परिदृश्य को कैसे देखते हैं?
देश में न्यापालिका के अधिकार क्षेत्र की बात होती है। इसके साथ ही कई बार यह भी आरोप लगता है कि एक्टिविज्म न्यापालिका को भी प्रभावित कर रहा है। न्यायिक एक्टिविज्म की भी बात आती है। आप इस पूरे परिदृश्य को कैसे देखते हैं?
यह सारी चीजें हमारे समाज की सोच से उत्पन्न होती हैं। हमलोग अगर अपने-अपने दायरे में रहें, अपने काम पर ध्यान रखें तो इस तरह की समस्या नहीं आती। संविधान हम लोगों का सबसे पवित्र दस्तावेज है और संविधान से ही हमको अपने अधिकार प्राप्त होते हैं। कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें संविधान में लिखित रूप से उजागर नहीं किया गया है। कई चीजें ऐसी हैं जिन्हें बहुत ही बारीक तरीके से विभाजित किया गया है। लोकतंत्र के हमारे तीन स्तंभ हैं- न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। हमारी कार्यपालिका और विधायिका अपने दायरे में बिल्कुल बंधी हुई हैं। अगर इसमें भटकाव आता है तो न्यायपालिका उसे सुधारती है। परंतु यदि न्यायपालिका भटकती है तो उसे सुधारने की व्यवस्था नहीं है।
लोकतंत्र में कभी-कभी तुष्टीकरण की राजनीति होती है। कोई भी दल ऐसा नहीं दिखाना चाहता कि वह न्यापालिका के खिलाफ है। हमने आठ साल मोदी जी के नेतृत्व में कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे न्यायपालिका को नुकसान हो, या न्यायपालिका को चुनौती दें या नजरअंदाज करें। लेकिन जब हम कोई सुधार लाना चाहते हैं तो सुधार के साथ देश की भावना जुड़ना जरूरी है। न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका में किसका प्रभुत्व है, हमारे लिए यह विषय है ही नहीं। संविधान में रेखांकित किया गया है। लेकिन जब हम राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लाये तो उसे चुनौती दी गई और सर्वोच्च न्यायालय में हड़ताल हुई। यहां से शुरू होता है आपके प्रश्न का उत्तर। देश में जैसी व्यवस्था है, उसमें यदि न्यायपालिका पर अंकुश की व्यवस्था नहीं है तो न्यायिक सक्रियता जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है।
कई न्यायाधीशों की टिप्पणियां उनके निर्णय का हिस्सा नहीं होतीं। वे टिप्पणी करके एक तरीके से अपनी सोच उजागर करते हैं। समाज में इसका विरोध भी होता है। मेरी जब भी न्यायाधीशों से बात होती है, मैं बहुत उन्मुक्त और खुले तौर पर उनसे कहता हूं कि न्यायाधीश को जो भी कहना है, वह अपने आदेश के जरिये कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, न कि टिप्पणियों के जरिए। दूसरे, न्यायपालिका जब अपने दायरे से बाहर जाती हैं, उदाहरण के लिए अगर एक न्यायाधीश कहता है कि यह कूड़ा यहां से हटाकर वहां डालो, ये नियुक्तियां दस दिन में पूरी करो, तो ये सारा काम कार्यपालिका का होता है। न्यायाधीश के रूप में आपको यह नहीं पता कि वहां व्यावहारिक दिक्कत क्या है, आर्थिक स्थिति कैसी है। सारे विषय को आप मिलाकर देखेंगे तो जिसे जिस चीज का दायित्व दिया गया है, उसी चीज में अपना ध्यान रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा नहीं तो हमें भी लोग कहेंगे कि हम एक्जीक्यूटिव सक्रियता कर रहे हैं। इंदिरा गांधी के जमाने में तीन जजों की वरिष्ठता को दरकिनार करके किसी को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, परंतु हमने तो यह नहीं किया। आज हम कुछ नियंत्रित करने के कदम उठाते हैं, तो वही लोग, जो न्यायपालिका पर कब्जा करना चाहते थे, आज कहते हैं कि हम न्यायपालिका पर हावी होना चाहते हैं, जजों की नियुक्ति में रोड़ा डाल रहे हैं, हम न्यायपालिका को नियंत्रित कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। यह बातें सोच से उत्पन्न होती हैं।
अभी जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं, वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बड़े पैरोकार हैं। इसी संदर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि न्यायपालिका की गरिमा के लिए अवमानना का नियम आवश्यक है, परंतु जब हम अभिव्यक्ति की बात करते हैं तो क्या न्यायपालिका, रचनात्मक समीक्षा से परे है? इसे आप कैसे देखते हैं?
सांसद हो या न्यायाधीश, एक विशेषाधिकार होता है। संसद के अंदर हम कुछ भी चर्चा करते हैं तो बाहर अदालत में उसकी पड़ताल नहीं की जा सकती। परंतु संसद के भीतर ही एथिक्स कमेटी होती है। संसद के अध्यक्ष के तहत इस पर अमल किया जाता है। कुछ असंसदीय शब्द, या कभी कोई कुछ ऐसी-वैसी बात कह देता है तो उसे वापस लेना पड़ता है, खारिज करना पड़ता है। न्यायपालिका में यदि न्यायाधीश कुछ ऐसी व्यवस्था देते हैं या कुछ बातें कहते हैं जो समाज के लिए अनुकूल नहीं हैं, तो उसे सुधारने के लिए न्यायपालिका के भीतर तंत्र नहीं है। सरकारी तंत्र यानी कार्यपालिका बिल्कुल नियम से चलती है, प्रधानमंत्री से लेकर दरबान तक नियम से बंधा होता है। लोकतंत्र में यही नियम हमारी विधायिका में भी होना चाहिए और न्यायपालिका में भी होना चाहिए। विधायिका में विधायन के नियम व प्रक्रियाएं होती हैं जिनसे काफी चीजों को नियंत्रित किया गया है।
न्यायपालिका में यदि कुछ अंदरूनी तंत्र बनाया जाए जो न्यायपालिका के भीतर नियमन करे तो यह सबसे अच्छा और उपयोगी होगा न कि हम न्यायपालिका के लिए कोई कानून बनाएं। एक स्वनियमन तंत्र पर न्यायपालिका स्वयं गंभीरता से सोचे तो अच्छा होगा, खास तौर पर आजकल सोशल मीडिया के जमाने में। सर्वोच्च न्यायालय ने लाइव स्ट्रीमिंग कर दिया है। कई उच्च न्यायालयों ने भी लाइव स्ट्रीमिंग टेलीकास्ट शुरू कर दिया है। अब हर न्यायाधीश के व्यवहार को लोग भी देख रहे हैं। मैंने पटना की कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि हम तो चुने हुए लोग हैं। हम तो हर पांच साल पर जनता के बीच जाएंगे। जनता चाहेगी तो हमें बैठाएगी, नहीं तो किसी और को सरकार चलाने का दायित्व देगी। न्यायाधीशों को तो लोग नहीं चुनते हैं लेकिन अब जनता न्यायाधीशों पर नजर रखेगी। तो मैं न्यायपालिका को सतर्क करना चाहता हूं कि आप भी लोकतंत्र का हिस्सा हैं, जनता की नजर में हैं, इसलिए आपका भी व्यवहार हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुकूल हो। इसलिए आप स्वयं के लिए एक नियमन तंत्र बनाएं तो यह देश के लिए अच्छा होगा।
न्यायपालिका के लोगों की चयन प्रक्रिया अलग है। समाज में इसे लेकर भी एक विमर्श खड़ा होता है। न्यायपालिका में जो संविधान में नहीं हैं, वह भी दिखता है जैसे कोलेजियम सिस्टम। क्या इस पर न्यायपालिका में सुधार का रास्ता निकलेगा? कोलेजियम व्यवस्था को आप कैसे देखते हैं?
देखिए, संविधान तो साफ है, लेकिन संविधान को किस तरीके से परिभाषित किया गया है, उसे देखिए। 1993 तक सभी न्यायाधीशों, जजों की नियुक्ति सरकार करती थी। सिर्फ भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श होता था। संविधान में लिखा है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करेंगे। यानी विधि मंत्री पूरी फाइल पर काम करते हैं, प्रधानमंत्री जी की अनुमति से राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। मुख्य न्यायाधीश के पास सिर्फ परामर्श के लिए भेजते थे। 1993 के बाद सबसे पहले जब न्यायाधीश की नियुक्ति का मामला आया, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान में लिखे परामर्श (कन्सल्टेशन) शब्द को सहमति (कन्करेन्स) के रूप में परिभाषित किया, जबकि ऐसा नहीं है। किसी भी जगह कन्सल्टेशन का मतलब कन्करेंस नहीं होता। सिर्फ न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में कंसल्टेशन को कॉन्करेंस के रूप में परिभाषित किया गया। इसके बाद कोलेजियम सिस्टम का 1998 में विस्तार किया। आज उच्च न्यायालय के कॉलेजियम से फाइल विधि मंत्री के पास आती है। इसके बाद इसमें प्रक्रिया पूरी की जाती है। दूसरी बात, दुनिया में कहीं भी न्यायाधीश अपनी बिरादरी की नियुक्ति नहीं करते हैं। तीसरी बात, न्यायाधीशों का काम मूल रूप से लोगों को न्याय देना है।
आज मैं कानून मंत्री होने के नाते महसूस करता हूं कि न्यायाधीशों का दिमाग और आधा समय अगला न्यायाधीश किसे बनाना है, इस पर खर्च हो रहा है न कि पूरा समय न्याय देने में। कोलेजियम सिस्टम में परामर्श बहुत व्यापक होता है। यह प्रक्रिया बहुत गहन होती है, दिखती नहीं है। राजनीति में बहुत उथल-पुथल दिखती है, न्यायपालिका के भीतर की राजनीति दिखती नहीं है। वहां चयन प्रक्रिया में इतनी गहन बहस होती है कि गुटबाजी तक हो जाती है। किसे अगला न्यायाधीश बनाना है, उसकी प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। तो यह प्रक्रिया धीरे-धीरे उच्च न्यायालय होते हुए हमारे पास आती है। हम भी इसकी जांच-पड़ताल करते हैं। कार्यपालिका होने के नाते यह हमारा काम है। लेकिन जो मूल सवाल आपने पूछा है कि कोलेजियम सिस्टम चलने से न्यायपालिका की आलोचना की बात, ये भी मैं समझता हूं। अगर कोई भी न्यायाधीश अगले न्यायाधीश की नियुक्ति में शामिल नहीं है तो न्यायाधीशों की आलोचना का भी कोई रास्ता नहीं खुलता। अगर न्यायाधीश ही अगले न्यायाधीश की नियुक्ति करता है तो फिर वे कार्यपालिका की प्रक्रिया में आ गए। तो वे आलोचना से दूर नहीं रह सकते। आप कार्यपालिका की भूमिका अदा करेंगे तो उसकी समीक्षा जरूर होगी।
आज से पहले यह बात इतनी मुखरता से, इतनी स्पष्टता से नहीं कही गई है। एक पत्रिका ने एक बार स्टोरी की थी और राजनीति में जो भाई-भतीजावाद का आरोप लगता है, उसके माध्यम से न्यायपालिका में भी अंकल जज सिंड्रोम के बारे में बात हुई थी। इसे आप कैसे देखते हैं?
आपने अंकल जज सिंड्रोम की बात की है, मान लीजिए आप न्यायाधीश हैं। अगले न्यायाधीश को मनोनीत करना है तो आप तो वही न्यायाधीश चुनेंगे जिसे आप जानते हैं। ये स्वाभाविक है। आप ऐसा व्यक्ति तो नहीं चुनेंगे जिसे आप नहीं जानते। जब किसी न्यायाधीश की नियुक्ति को लेकर मेरे पास न्यायाधीशों की लिखित टिप्पणी आती है तो उसमें वे लिखते हैं कि मैं इनको जानता हूं। ये मेरे न्यायालय में पेश हुए हैं। इनकी बहस अच्छी है, आचरण अच्छा है। वे जानते हैं, तभी तो सिफारिश करते हैं। आप कार्यपालिका की प्रक्रिया में आ गए हैं तो आप जिसे जानते हैं, जो करीबी हैं या परिवार से जुड़े हैं, उसी को आप मनोनीत करेंगे। इसलिए ये आरोप तब लगते हैं जब न्यायाधीश ही न्यायाधीश की नियुक्ति में शामिल होते हैं। 1993 से पहले न्यायपालिका या न्यायाधीशों पर उंगली नहीं उठती थी क्योंकि न्यायाधीशों की नियुक्ति में उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं थी, वे इस प्रक्रिया से दूर रहते थे। परंतु आज ज्यादा हो रही है। सोशल मीडिया पर कई लोग तो गालियां दे रहे हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने मुझे पत्र लिखा कि न्यायाधीशों, न्यायपालिका पर आक्रमण हो रहे हैं, इसे नियंत्रित किया जाए और इस पर कठोर कार्रवाई की जाए। अभी तक मैंने सोच-समझकर ही उत्तर नहीं दिया है।
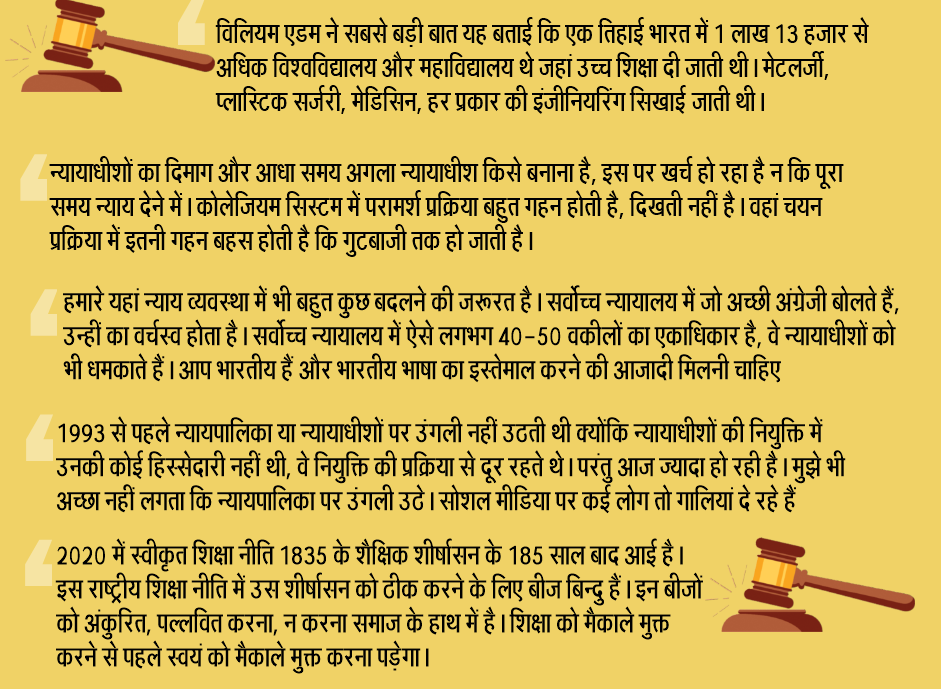
ये स्वतंत्रता का 75वां वर्ष है। स्वतंत्रता में जो स्व है, उसी स्व की मैं बात करूंगा। प्रधानमंत्री जी ने भी पंच प्रण की बात की थी। उसमें से एक प्रण ये भी था कि औपनिवेशिक बोझ, औपनिवेशिक मानसिकता को लेकर हम कितना आगे और कितना अपनी गति से चल सकते हैं। क्या न्यायपालिका पर यह बोझ है?
न्यायपालिका के बारे में औपनिवेशिक बोझ कहना ठीक नहीं होगा। वो तो पूरा का पूरा औपनिवेशिक प्रणाली ही है। वहां तो भाषा, पोशाक सब वही है। मैं मुख्य न्यायाधीश महोदय से बात करूंगा कि हम हमेशा ये अंग्रेजी पोशाक लेकर चलेंगे कि अपने मौसम के अनुकूल पहनेंगे। मैं मूल बात बताना चाहता हूं। गहराई से देखें तो आज भी हमारी सोच पर बहुत हद तक अंग्रेजों के उस 200 साल के शासनकाल का दबदबा है। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से पांच प्रणों की घोषणा की जिसमें यह भी कहा कि गुलामी का कोई निशान हमारे देश में नहीं रहना चाहिए, इसके लिए देश के हरेक नागरिक को मिलकर काम करना चाहिए।
मेरे ख्याल से हरेक भारतीय को चाहिए कि प्रधानमंत्री जी की इस घोषणा को मन में और बाहर भी लोगों के बीच लेकर जाए तो देश के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हमारे देश में आज भी ऐसा क्यों है कि अच्छी अंग्रेजी बोलते वाले को ज्यादा इज्जत मिलती है, गोरी चमड़ी को इज्जत मिलती है और काले को नीचा देखते हैं। विदेश से कोई पुरस्कार मिले तो जश्न मनता है, देशी पुरस्कारों की चर्चा तक नहीं होती। यही मानसिकता हमारे लिए बहुत बड़ा बोझ है और इसे उतार फेंकना बहुत जरूरी है। मैं खुद मानता हूं कि हमारे यहां न्याय व्यवस्था में भी बहुत कुछ बदलने की जरूरत है। सर्वोच्च न्यायालय में जो अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, उन्हीं का वर्चस्व होता है। सर्वोच्च न्यायालय में ऐसे लगभग 40-50 वकीलों का एकाधिकार है, वे न्यायाधीशों को भी धमकाते हैं। आप भारतीय हैं और भारतीय भाषा का इस्तेमाल करने की आजादी मिलनी चाहिए। कई उच्च न्यायालयों में हिन्दी का इस्तेमाल करने की इजाजत है। बाकी में भी भारतीय भाषाओं में काम करने की अनुमति मिलनी चाहिए। आगे चलकर सर्वोच्च न्यायालय में भी भारतीय भाषाओं का विकल्प होना चाहिए जिसके लिए अनुवाद का व्यवस्था हो। हमारी सोच उस दिशा में जानी चाहिए।


















टिप्पणियाँ