सांस्कृतिक जीवनमूल्य परिवार के माध्यम से ही एक से दूसरी पीढ़ी को हस्तान्तरित होते हैं। यह जीवन्त प्रक्रिया है, इसलिए हर पीढ़ी उसे अपने पुरुषार्थ से समृद्ध बनाती रहती है, साथ ही देश-काल-परिस्थिति के अनुरूप परिवर्तन कर उसे परिष्कृत भी करती रहती है। यह ही युगानुकूल परिवर्तन है। -पं. दीनदयाल उपाध्याय

ओ३म्
प्रिय बनवारी,
आज शायद जितने विक्षुब्ध हृदय से पत्र लिख रहा हूं, इस प्रकार शायद अपने जीवन में मैंने कभी नहीं किया होगा। मैं चाहता तो था कि अपने हृदय के इस क्षोभ को अपने ही तक सीमित रखूं, परन्तु अब तक अनुभव बताता है कि यह क्रिया अत्यंत वेदनोत्पादक एवं व्यथाकारी है। तुम विचारवान हो एवं संवेदनात्मक रूप से सोचने की तुममें शक्ति है, इसलिए तुमको लिख रहा हूं।
8 तारीख से ही मैं तुम्हारी सतत् बाट देख रहा था, वैसे तो मैं जानता था कि तुम नहीं आओगे, परंतु एक यों ही आशा लगी हुई थी कि शायद तुम मेरे कार्य की महत्ता का अनुभव कर सको और आ जाओ, परंतु तुम शायद न समझ पाए कि मेरा जाना भी मेरी दृष्टि से कितना आवश्यक है। एक स्वयंसेवक के जीवन में संघ कार्य का कितना महत्व है, काश! तुम इसको समझते होते! तुम जानते हो कि साधारण रूप से जीवन-यापन के अनुकूल योग्यता और साधन होते हुए भी, उस मार्ग को छोड़कर भिन्न मार्ग ही मैंने स्वीकार किया है। मैं भी सुख-चैन से रहने की इच्छा करता हूं।
मैं यह भी जानता हूं कि इस प्रकार कार्य करने में कुटुम्ब का कोई व्यक्ति और विशेषकर मामा जी प्रसन्न नहीं हैं। मामा जी ने मुझको पढ़ा-लिखाकर इस योग्य बनाया और अब उनकी इच्छा के विपरीत कार्य करके उनके हृदय को दु:ख देकर, उनकी आशाओं को ठेस पहुंचाकर जो कृतघ्नता का एक पातकीय कृत्य मैंने किया है, उसका पूर्णरूपेण विचार किया है एवं इस बुराई के टीके को अपने माथे पर लेकर भी, तथा अन्य समस्त बुराई-भलाई का विचार करने के बाद जिस मार्ग को ग्रहण किया है, और फिर वह मार्ग भी कांटों से परिपूर्ण है, सदैव इधर-उधर घूमते फिरना, न रहने का ठिकाना, न खाने का ठिकाना, जिसने कहा उसके यहां खाया, जहां मिला वहां रहा आदि अनेक कठिनाइयों को पहले भी और बाद में अनुभव से जानने पर भी जिस कार्य के लिए अपना समस्त जीवन लगाने का विचार किया है उसका मेरे लिए कितना महत्व है, इसको शायद तुम तब ही अनुभव कर पाते जब मैं मामा जी को इसी प्रकार छोड़कर यहां से चला जाता।
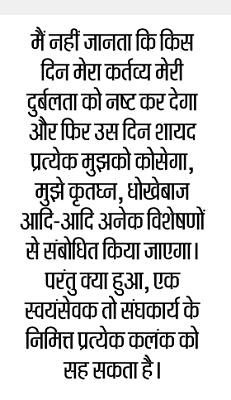
मैं जानता हूं कि यदि मैं दस रुपये का भी कहीं नौकर होता तो इस प्रकार का कार्य करने की हरेक सलाह देता, फिर यह कोई भी नहीं कहता कि नौकरी छोड़कर इस प्रकार पड़े रहो। तब तो शायद मामाजी भी और तुम भी और प्रत्येक इस बात की पूरी चिंता रखता कि यदि मैं एक दिन की छुट्टी लेकर आया होता तो ठीक समय पर नौकरी पर पहुंच जाऊं। इस बात को मैं तुम्हारे और भाई साहब के विषय में देखता हूं, इसलिए नहीं, कि वे तुम दोनों को कोई अधिक प्यार करते हैं वरन् केवल इसलिए कि तुम नौकर हो।
तो क्या समाज का कार्य एक नौकरी के बराबर भी महत्व नहीं रखता? मैं सोचता हूं कि यदि मैं कहीं नौकर होता तो आज नौकरी छोड़कर मैं सहर्ष यहां पड़ा रहता, इसमें मुझे शांति मिलती। मामा जी का मेरे जीवन में एक विशेष स्थान है और उनके लिए इस प्रकार नौकरी छोड़ना मुझे किसी भी प्रकार नहीं अखरता।
जीजी की बीमारी में मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ी, छात्रवृत्ति छोड़ी। वह केवल इसलिए की जीजी के आराम होने से मामा जी को शांति मिलेगी। परन्तु आज मेरी शांति नष्ट हो चुकी है। मेरा कर्तव्य मुझे बार-बार पुकारकर कहता है कि मुझे लौटकर जाना चाहिए। रात-दिन मेरे मस्तिष्क में यही चक्कर लगता रहता है और इस मानसिक संघर्ष एवं उथल-पुथल का परिणाम है कि आज मैं छोटी-छोटी बातों को भी भूल जाता हूं।
दवा तक देने का समय पर ध्यान नहीं रहता है, परिचर्या के लिए इतनी सतर्कता चाहिए, उतनी इच्छा होते हुए भी मैं नहीं रख पा रहा हूं, मेरी आत्मा मेरी दुर्बलता पर मुझको सदैव धिक्कारती रहती है। रात्रि को जब भी आंख खुल जाती है तो निस्तब्ध वातावरण में आत्मा की प्रतारणा स्पष्ट अनुभव होती है। मेरी कर्तव्य बुद्धि मुझको अपने कार्य क्षेत्र की ओर प्रेरित करती है, पर हृदय की दुर्बलता मुझे अशक्त बना देती है। यह बुद्धि और हृदय का संघर्ष निरंतर चल रहा है। मैं नहीं जानता कि किस दिन मेरा कर्तव्य मेरी दुर्बलता को नष्ट कर देगा और फिर उस दिन शायद प्रत्येक मुझको कोसेगा, मुझे कृतघ्न, धोखेबाज आदि-आदि अनेक विशेषणों से संबोधित किया जाएगा। परंतु क्या हुआ, एक स्वयंसेवक तो संघकार्य के निमित्त प्रत्येक कलंक को सह सकता है।
संघकार्य के निमित्त यदि उसे ऐसे पापकर्म में लीन होना पड़े जिसके लिए कि उसे जन्म-जन्मांतर तक घोर नरक-यातनाएं भी भुगतनी पड़ें तो उसे भी वह सहर्ष कर जाएगा। समाज का कार्य ही उसके सम्मुख एकमेव कार्य रहता है। तुम कहोगे कि ये बड़ी-बड़ी बातें और इतना ओछा व्यवहार! और यही मैं कहता हूं कि यह मेरे हृदय की दुर्बलता है वह भी केवल मामा जी के लिए। परंतु मैं यह भी जानता हूं कि मेरी यह दुर्बलता भी अधिक नहीं टिक पाएगी।
अपनी ओर से यद्यपि मेरा यही प्रयत्न है कि कम से कम मामा जी की बीमारी तक तो मेरा कर्तव्य मेरे ऊपर हावी न हो। इसलिए गीता, जो कि मेरे लिए अत्यंत प्रिय पुस्तक है, जिसके एक अध्याय का मैं नित्य पाठ करता था, उसी गीता को तुम्हारे कहने पर भी और मामा जी की इच्छा होने पर भी नहीं सुनाता हूं, वरन् टालमटोल करता रहता हूं, क्योंकि जब-जब मैंने गीता मामा जी को सुनाई है, मुझे अनुभव होता है कि उसका एक-एक श्लोक मुझे अपने कर्तव्य की याद दिलाता है। फलत: गीतापाठ के पश्चात् सदैव ग्लानि चिंता से आवृत्त हो जाता हूं। परंतु मेरे प्रयत्नों के बावजूद आत्मा की प्रतारणा तो दिन-रात सदैव होती है, रहती है।
जमीन में जिस प्रकार थोड़ा-थोड़ा पानी रिसता जाता है और वही पानी एक बड़े भारी ज्वालामुखी के रूप में फूट पड़ता है। उस रिसते हुए पानी को कोई नहीं रोक सकता है और ज्वालामुखी के उभाड़ को भी; उसी भांति मैं चाहता हुआ भी अपने कर्तव्य के आकर्षण को रोक नहीं सकता हूं।
मैं इसीलिए चाहता था कि कर्तव्य की मैंने जो इतनी बड़ी उपेक्षा की है, उसके लिए थोड़ा सा तो शांति का कार्य कर लूं। तुम जानते हो कि मुझे 11 बजे तुम्हारी चिट्ठी पीलीभीत में मिली और 3 बजे की गाड़ी से मैं चल दिया, न किसी से कुछ कह पाया और न सुन पाया और न शाखा का प्रबंध ही कर पाया। अब मैं अनुभव करता हूं कि मैंने यह मूर्खता की, परन्तु मैं यह कभी सोचकर नहीं चला कि मैं इस प्रकार अनिश्चित काल के लिए रहूंगाा।
मैं तो अधिक से अधिक 15-20 दिन रहने के विचार से आया था। अब तुम ही सोचो कि इस प्रकार एकाएक चले आने पर क्या तुम करोगे? मैं जानता हूं कि पहले तो तुम एकाएक इस प्रकार आओगे ही नहीं और आ भी गए तो शीघ्र से शीघ्र लौट जाने का प्रयत्न करोगे, हां, ठीक प्रबंध होने पर एवं उच्च अधिकारियों की आज्ञा मिलने पर फिर शायद निश्चित काल तक रह सकते। मैं नहीं समझता कि मैं इस प्रकार भाग खड़ा हुआ। एक राष्ट्र कार्यकर्ता के नाते तो मुझे कुटुम्ब का इस प्रकार का मोह नहीं होना चाहिए, परंतु हृदय खींच लाया। तुम जानते हो ‘‘भावना से कर्तव्य ऊंचा है।’’
मैं केवल इसलिए पीलीभीत और लखीमपुर जाना चाहता था कि अब तक वहां का कुछ स्थायी प्रबंध कर दूंगा तथा इस प्रकार कर्तव्य की क्षति को कुछ पूरी करके अगले जितने दिन भी मैं यहां रहूं, शायद कुछ शांति से रह सकूं। इसीलिए मैंने तुमसे प्रार्थना की थी, भिक्षा मांगी परंतु तुमने उसको ठुकरा दिया और अब हृदय रो रहा है; जी में आता है कि तुम्हारी ओर से इस प्रकार निराश हो अपने हृदय की भावनाओं को एक ओर कर अपने कर्तव्य क्षेत्र में एकदम वापस लौट जाऊं। परन्तु अभी तो शायद मैं विवश हूं। मुझको यह अवश्य अनुभव हो रहा है कि समाज की दृष्टि से मैंने एक जघन्य कृत्य किया है और उसके लिए पश्चाताप की अग्नि से मुझको दग्ध होना ही पड़ेगा।
राष्ट्रकार्य व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर
तुम शायद सोचते होगे कि आज मेरे ऊपर मुसीबत आयी है और उसी मुसीबत में दीनदयाल बजाय सहायक होने के रोड़े अटका रहा है। परंतु मेरी केवल एक ही प्रार्थना है कि तुम जरा मेरे दष्टिकोण से सोचो, मेरे कार्य को अधिक नहीं तो कम से कम इतना महत्व तो दो जितना की तुम मेरी नौकरी को देते।
मुझे याद है कि जिस समय जयपुर में जीजी बीमार थीं; जीजाजी छुट्टी लेकर निरंतर उनके पास थे, परंतु गर्मी की छुट्टी होने के पहले दो दिन के लिए स्कूल अटैण्ड (उपस्थित) करने वे भी चले गए थे, केवल इसलिए कि यदि ऐसा न किया गया तो सारी की सारी महीने की छुट्टियां उनकी लीव (ग्रीष्मावकाश) में शामिल कर ली जाएंगी और उनको उसकी तनख्वाह नहीं मिलेगी। मरणासन्न रोगी को छोड़कर एक व्यक्ति केवल इतनी थोड़ी सी बात के लिए चला जाए और उसको तुम सब ठीक समझो और यहां एक शाखा नष्ट हो रही है, पिछले सारे किए धरे पर पानी फिर रहा है और उसके प्रबंध हेतु दो दिन को भी जाने की फुरसत नहीं। तुमको अपने एरियर्स (बकाया वेतन) का ख्याल है, सी.ई. की प्रसन्नता-अप्रसन्नता का ख्याल है, अपने इन्क्रीमेंट्स का ख्याल है, आदि-आदि पचासों बातों का ख्याल है परन्तु राष्ट्र के इस कार्य का ख्याल नहीं है, मेरी व्यथा को तुम नहीं जानते हो और न उसकी तुम्हें चिंता ही है।
मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी आपत्तियों को बढ़ाऊं, बल्कि मेरा हृदय कहता है कि मैं उसमें सहायक ही होऊं (यद्यपि कर्तव्य तो मेरा अन्यत्र निश्चित ही है) परंतु मैं नहीं चाहता कि इस प्रकार सहायक होने से अपने जीवन के ध्येय-मार्ग पर जितने कदम आगे बढ़ चुके हैं, उनको भी लौटा लूं। अपने ध्येय के भव्य भवन को आगे मैं न अभी बना पाऊं, उसको कुछ रुक कर बना लूं, यह हो सकता है, इसमें जो आत्मा को कष्ट होगा, उसको सहा जा सकता है, परंतु यह मैं कदापि सहन नहीं कर सकता कि इस भवन को जितना बनाया है, उसको भी गिरा दूं। किसी भी दृष्टि से देखो, यह तो मैं अवश्य समझता हूं कि तुम मुझे मेरे इस अधिकार से वंचित नहीं कर सकते कि मैं कम से कम दो-चार दिन के लिए जाकर अपने कार्य का निश्चित प्रबंध कर आऊं। तुम नौकरी कर रहे हो, तुमको जितने दिन की छुट्टी मिलती है, उससे अधिक रहने में तुम अपने को विवश समझते हो।
भाई साहब का भी यही हाल है और मेरा भी यही होता, यदि मैं नौकर होता, तब यहां कौन रहता? मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, आज चाहे कहने को तुम या कोई कुछ भी कह दे कि हममें से कोई भी नौकरी छोड़कर नहीं रहता और न मामा जी भी इस बात को पसंद ही करते। क्या तुम समझते हो कि रुपये का बंधन ही सब कुछ है? अनुशासन का भी तो बंधन है, आत्मा का भी तो बंधन है। आज प्रत्येक को अपने कार्य की चिंता है और मुझसे आशा की जाती है, मैं अपने कार्य को बिल्कुल ही भूल जाऊं, उसका कुछ प्रबंध भी न कर सकूं। यह कहां का न्याय है, मेरी समझ में नहीं आता।
खैर, पत्र बहुत बड़ा हो गया है और इस समय तो विक्षुब्ध हृदय में भाव इतने भरे हैं कि मैं कितना ही लिखता जाऊं, समाप्त न होंगे। इतना अवश्य लिखे देता हूं कि इस पत्र का एक-एक शब्द मेरी आत्मा से निकला है और मैंने सोच-विचार कर लिखा है। यों ही जोश में आकर नहीं लिखा है। प्रत्येक शब्द सार्थक है और उसके पीछे विचार एवं मेरी कार्यशक्ति की सामर्थ्य है। आज मामा जी ने भी तुम्हारी बहुत बाट देखी, तुम्हारे अथवा तुम्हारे किसी पत्र के न आने से वे बहुत चिन्तित रहे। फलत: आज उनका तापमान फिर 106 डिग्री हो गया, यद्यपि कल 100 डिग्री तक ही रहा था। पत्र तो जल्दी-जल्दी डालते रहा करो, इससे उनको सांत्वना ही मिलती है।
भाग्याधीन न रह पाऊंगा
पुनश्च:-
तुम इतवार को कुछ मिनटों के लिए आए। तुमने अपने न आ सकने का कारण बताया। इस पर अविश्वास करने का मुझे कोई भी न्यायसंगत कारण दृष्टिगत नहीं होता है। परंतु तुम्हारे जाने के पश्चात् भाग्य के इस क्रूर कुठाराघात पर हृदय खूब ही रोया। तुम शायद विश्वास न करो कि अपने प्रिय बंधु-बांधवों की मृत्यु पर भी जिन आंखों में आंसू न आए, वे आंखें भी अश्रु-जलपूरित थीं। तुमने कहा कि अप्रैल में छुट्टी लूंगा। उस समय आवेश के कारण मैं तुमसे कुछ कह न पाया परंतु अपै्रल की छुट्टी मेरे किस काम की ‘का वर्षा जब कृषि सुखाने’। तुम समझते होगे कि मैंने होली की छुट्टियों में जाने का विचार आकस्मिक ही किया था, या केवल इसीलिए कि तुम्हारी छुट्टियां होंगी, चलो इन दिनों ही आऊं। नहीं।
5 तारीख को प्रांतीय प्रचारक गोला में आए थे। उनके आगमन एवं आदेश का पूवार्भास होने के कारण ही मैंने ये दिन निश्चित किए थे और अब तुम कहते हो कि अप्रैल तक जाकर क्या मैं अपना सिर फोडूंगा और अब भी मैं निश्चित कहता हूं कि तुमको छुट्टी नहीं मिलेगी। खैर, आत्मा का संघर्ष मेरे भाग्य में है, भुगतूंगा जब तक कि उसका कोई एकपक्षीय निर्णय न हो जाए।
एक बात अवश्य है, वह मैं भाई साहब से भी कह चुका था कि 15 मई से हमारा ओ.टी.सी. कैम्प (संघ शिक्षा वर्ग) होता है, अत: 15 के बाद मेरा किसी भी दशा में रुकना असंभव हो जाएगा। वैसे तो मेरा ख्याल है कि भगवत्कृपा से उस समय तक मामाजी ऐसे हो जाएंगे कि केवल नौकर के साथ अकेले रह सकें, परन्तु यदि भाग्य ने तब भी धोखा दिया तो उस समय निश्चित ही मैं भाग्याधीन न रह पाऊंगा, मुझको जाना ही होगा, विचार कर लेना।
हां, एक और साथ में पत्र रख रहा हूं, फिर एक तरफ से आवाज आ रही है, इस विषय में तुम क्या कहोगे? उपेक्षा ही न, पर क्या यह उचित है? जरा शांत हृदय से सोचो।
अच्छा मामाजी की तबीयत अभी वैसी ही है। उस दिन जल्दी-जल्दी में तुमसे घी के बारे में कहना भूल गया। घी आज समाप्त हो गया है। यहां पहाड़ी घी साढ़े चार छटांक का मिलता है, वह भी विश्वास के योग्य नहीं, देशी साढ़े तीन छटांक। अत: किसी प्रकार हो सके तो वहीं से 6 रुपया, 8 रुपया, या ज्यादा का घी भेज देना, तुम्हारा बर्तन खाली है, लौट जाएगा। फलों में सेब, अनार भेजने की जरूरत नहीं है। डॉ. शर्मा छुट्टी पर हैं, दो एक दिन में आएंगे। डॉ. श्री खण्डे आगरा हैं, अभी राउण्ड नहीं लगाया है। प्रह्लाद भाई साहब का पत्र आया हो तो लिखना, यहां तो कोई पत्र आया नहीं है। विशेष पत्र लिखना।
— ह. दीनदयाल उपाध्याय
1
‘स्वदेशी’ के विचार से पुरातनपंथी कहा जाता है और हम गर्व से विचार, पूंजी से लेकर हर चीज विदेशी प्रयोग करते हैं। इससे हम फिर गुलाम बन जाएंगे। —पं. दीनदयाल उपाध्याय
2
पश्चिम में जो यह नारा लगाया जाता है कि कमाने वाला ही खाएगा, यह ठीक नहीं। छोटा बालक व रोगी नहीं कमाता, फिर भी खाता है। जो जीवित है, वह खाएगा। कमाई (कर्म) और उजरत (पारिश्रमिक) का मेल पश्चिम के अर्थशास्त्र में है, हमारे यहां नहीं। हमारे यहां कर्म इसलिए किया जाता है, क्योंकि हमारा धर्म है। — दीनदयाल उपाध्याय
3
आज की परिस्थिति में यदि किन्हीं दो शब्दों का प्रयोग कर अपनी अर्थ व्यवस्था की दिशा के परिवर्तन को बताना हो, तो वे हैं ‘विकेन्द्रीकरण’ और ‘स्वावलंबन’। —पं. दीनदयाल उपाध्याय

















टिप्पणियाँ