प्रकृति संरक्षण एवं संवर्धन, अकादमिक विमर्श के साथ ही जनमानस के चिंतन-मनन का अनिवार्य विषय बनना चाहिए। हमें वसुधा के भविष्य एवं इसमें पल्लवित-पुष्पित मानव सभ्यता एवं जैविकी की निरंतरता के लिए चिंतित होना चाहिए। इस खतरे के मूल में मानव समाज की बढ़ती हुई उपभोगवादी जीवन शैली के समक्ष उपस्थित ऐसी चुनौतियां हैं,
जलवायु परिवर्तन प्रकृति एवं उसके समस्त घटकों के अस्तित्व के लिए खतरा बनता जा रहा है। अतएव प्रकृति संरक्षण एवं संवर्धन, अकादमिक विमर्श के साथ ही जनमानस के चिंतन-मनन का अनिवार्य विषय बनना चाहिए। हमें वसुधा के भविष्य एवं इसमें पल्लवित-पुष्पित मानव सभ्यता एवं जैविकी की निरंतरता के लिए चिंतित होना चाहिए। इस खतरे के मूल में मानव समाज की बढ़ती हुई उपभोगवादी जीवन शैली के समक्ष उपस्थित ऐसी चुनौतियां हैं, जो प्राकृतिक संसाधनों के दोहन एवं तद्जनित अवांछित घटकों द्वारा उत्पन्न प्रदूषण की वजह से साकार हो रही हैं।
मानव समाज के साथ-साथ संपूर्ण चेतन एवं अचेतन जगत जलवायु परिवर्तन और वैश्विक ताप से उत्पन्न समस्याओं के मध्य अस्तित्व के निमित्त संघर्षरत है। भविष्य में इन समस्याओं की गहनता में उत्तरोत्तर वृद्धि की अत्यधिक संभावना है। चरम जलवायुवीय घटनाएं जैसे तापमान एवं समुद्र स्तर में निरंतर वृद्धि, मरुस्थलीकरण, हिमनदों का पिघलना, बेमौसम वर्षा, आंधी-तूफान, चक्रवात, बाढ़, सूखा के साथ ही जल, वायु और मिट्टी का असहनीय स्तर तक प्रदूषण आदि वसुधा के स्वास्थ्य को कैंसर की भांति निगल रहे हैं। वर्तमान समाज की सुख-सुविधाओं एवं आवश्यकताओं की सीमा ‘इवन स्काई इज नॉट द लिमिट’ हो गई है। इस विकृत मानसिकता के संपोषण हेतु प्राकृतिक संसाधनों का ‘शोषण के स्तर तक दोहन’ हमारे जीवन का उद्देश्य बन गया है।
संसाधनों का दोहन
वर्तमान जीवन शैली पर दृष्टिपात करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मानव समाज ने प्रकृति के साथ सम्यक व्यवहार नहीं किया है और वह पर्यावरण का अच्छा संरक्षक भी सिद्ध नहीं हुआ है। इसका मूलभूत कारण यह है कि हम अपनी सनातन संस्कृति एवं जीवन मूल्यों के अच्छे संपोषक सिद्ध नहीं हो सके। आज मानव व्यक्तिगत एवं सामूहिक, दोनों स्तरों पर अपनी स्वार्थपूर्ति हेतु प्राकृतिक संसाधनों का अबाध दोहन कर रहा है। अधिकांश लोग भौतिक समृद्धि की प्राप्ति हेतु गलाकाट प्रतिस्पर्धा में शामिल हैं। वर्तमान में मनुष्य के दैनिक क्रियाकलापों से ऐसे अपशिष्ट उत्पन्न हो रहे हैं जो स्वत: अपघटित नहीं होते, जिससे हमारे स्थलमंडल, जलमंडल, जीवमंडल एवं वायुमंडल तीव्र गति से प्रदूषित हो रहे हैं। पृथ्वी की सतह भी दिनोंदिन गर्म हो रही है। परिणामस्वरूप मौसम चक्र अनियमित, अस्थिर एवं अप्रत्याशित होता जा रहा है। वर्तमान पीढ़ी के लिए जीवनदायक शुद्ध जल, स्वच्छ वायु और उर्वर भूमि की कमी होती जा रही है। मानव जाति के अस्तित्व एवं जैव-विविधता के प्रसार हेतु पृथ्वी का पारिस्थितिकी तंत्र दिनोंदिन अनुपयुक्त होता जा रहा है। मानव अपने इस मिथ्या दंभ तले स्वयं दबता जा रहा है, कि वह पृथ्वी पर सर्वाधिक प्रज्ञावान प्रजाति है। विचारणीय है कि, क्या कोई मानवेतर प्रजाति भी है, जो स्वयं के साथ-साथ अन्य जीवों के पर्यावासी क्षेत्रों को मात्र लोभवश नष्ट करने में संलग्न हो?
वर्तमान में मनुष्य के दैनिक क्रियाकलापों से ऐसे अपशिष्ट
उत्पन्न हो रहे हैं जो स्वत: अपघटित नहीं होते, जिनसे हमारे
स्थलमंडल, जलमंडल, जीवमंडल एवं वायुमंडल तीव्र गति से
प्रदूषित हो रहे हैं। पृथ्वी की सतह भी दिनोंदिन गर्म हो रही है।
परिणामस्वरूप मौसम चक्र अनियमित, अस्थिर एवं अप्रत्याशित
होता जा रहा है। वर्तमान पीढ़ी के लिए जीवनदायक शुद्ध जल,
स्वच्छ वायु और उर्वर भूमि की कमी होती जा रही है। मानव जाति
के अस्तित्व एवं जैव-विविधता के प्रसार हेतु पृथ्वी का पारिस्थितिकी
तंत्र दिनोंदिन अनुपयुक्त होताजा रहा है।
आज हमारे दैनिक क्रिया-कलाप सनातनी जीवन मूल्यों के ठीक विपरीत हो गए हैं। हम विश्व के सर्वाधिक बुद्धिमान प्राणी – आज नदियों से जल नहीं रेत, पर्वतों से औषधि नहीं पत्थर और खेतों से अनाज नहीं, नकदी फसल का दोहन कर रहे हैं। हमारी तथाकथित बुद्धिमत्ता की वास्तविकता यह है कि हम प्राय: पर्यावरण को विनष्ट करने हेतु दैनिक उपयोग की गैर-जैवअपघटित वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं एवं वायु को प्रदूषित करने के लिए कृषि अवशेषों को जलाते हैं। कृषि उत्पादों, मिट्टी तथा जल को प्रदूषित करने हेतु रसायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का असीमित उपयोग करते हैं। क्या हमने कभी सोचा है कि पर्यावरणानुकूल मिट्टी के घरों के बजाय बहुमंजिला कंक्रीट की इमारतें, भूजल की अत्यधिक निकासी एवं पेपर नैपकिन हेतु वृक्षों की अंधाधुंध कटाई किस प्रकार तापमान वृद्धि का कारण बन रही है? क्या हमें इस बात की रंच मात्र भी चिंता है कि कृषि अपशिष्टों के दहन से प्राणवायु प्रदूषित होती है? सर्वविदित हैं कि प्लास्टिक के अवशेष, मिट्टी और जल के स्वास्थ्य को अपूरणीय क्षति पहुंचाते हैं। ध्यातव्य है कि रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक मृदा एवं जल को प्रदूषित कर रहे हैं, फलस्वरूप पारिस्थितिकी तंत्र और जैव-विविधता खतरे में हैं।
सनातन संस्कृति और पर्यावरण
मानव सभ्यता के सबसे प्राचीन अभिलेख वेदों, पुराणों एवं उपनिषदों में, जो कि मानव चिंतन एवं सनातन ज्ञान-परंपरा की पराकाष्ठा माने जाते हैं, पर्यावरण के चराचर घटकों के पारस्परिक संबंध उल्लिखित हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा मनुष्य को अज्ञानता के घोर अंधकार से मुक्त करने का सामर्थ्य रखती है। भारतीय चिंतन में भूमि, जल, वायु, पहाड़ियां-पर्वत, जंगल, नदियां, महासागर, पेड़-पौधे, जड़ी-बूटियां, झाड़ियां, यहां तक कि ग्रह-नक्षत्र एवं तारे भी जीवंत माने गए हैं एवं इनकी पूजा-वन्दना और संरक्षण सनातनी संस्कृति की केंद्रीय भूमिका में रहे हैं। यदि किसी विशेष परिस्थिति में प्राकृतिक संसाधनों के अतिदोहन की आवश्यकता भी पड़ती थी तो ऋषिगण क्षमा-याचना करते हुए कहते थे -‘हे पृथ्वी! हम जो कुछ भी आपसे ग्रहण कर रहे हैं, वह शीघ्रातिशीघ्र प्राकृतिक अवस्था में आ जाए। हे शोधक! हम आपके प्राण और हृदय को क्षत-विक्षत न करें। ऋग्वेद के एक श्लोक में जल को दैवीय मानते हुए कहा गया है – ‘जो दिव्य जल आकाश से प्राप्त होते हैं, जो नदियों में सदा गमनशील हैं, जो स्वयं स्रोतों द्वारा प्रवाहित होकर पवित्रता बिखेरते हुए समुद्र में समाहित होते हैं, वे दिव्य जल हमारी रक्षा करें’। श्री गुरु ग्रन्थ साहिब जी के अंग 8 में वर्णित है कि मनुष्य के जीवन में पवन का स्थान गुरु समान, जल पिता तुल्य एवं पृथ्वी माता का प्रतिरूप है।
हमारे पूर्वजों ने प्रकृति को उसकी समग्रता में समझते हुए उसको पूजनीय समझा। ‘शांति मंत्र’ संपूर्ण सृष्टि के अंतर्सर्बंध को रेखांकित करते हुए, सभी के मध्य समन्वय की कामना करता है, जिसका आशय है कि जल, वृक्ष, प्राकृतिक ऊर्जा और समस्त जीव सद्भावपूर्ण एवं शांतिमय रहें। इस मंत्र के द्वारा हम आकाश, पृथ्वी, जल, वृक्ष, समस्त देवताओं, ब्रह्मांड, ब्राह्मण समेत सबकी ‘शांति’ की कामना करते है। ऋग्वेद के एक श्लोक में वर्णित है- ‘आकाश मेरा पिता है, पर्यावरण मेरा भाई है, एवं पृथ्वी मेरी माता है’, जिनसे सभी प्राणियों का पालन-पोषण होता है। पशु-पक्षियों के मिलन ऋतु में उनका शिकार नहीं किया जाता था ताकि प्रकृति चक्र बाधित न हो। हरी शाखा न काटकर वृक्षों से मात्र सूखी लकड़ियां ही ली जाती थीं। ईशावास्योपनिषद के एक मंत्र का तात्पर्य है कि ‘दूसरों को उनका अधिकार सुनिश्चित करके ही हमें अपना अधिकार स्वीकारना चाहिए, साथ ही भोग में भी त्यागवृत्ति बनी रहनी चाहिए’। यानी भारतीय जीवन दृष्टि मात्र भौतिक विकास पर ही नहीं, अपितु प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए मनुष्य के आध्यात्मिक विकास पर भी बल देती है। प्राचीन साहित्य स्पष्ट उद्घोषणा करता है कि यह प्रकृति समस्त जैविक-अजैविक प्राणियों के लिए है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम ‘सर्वेभवन्तु सुखिन:’ मंत्र को अपने आचार-व्यवहार में शिरोधार्य करते हुए सभी के सुख के लिए प्रकृति की रक्षा करें।
प्रकृति क्षरण के दुष्प्रभाव
वर्तमान में प्रकृति संवर्धन एवं दैनिक जीवन में इसके साथ साहचर्य ‘स्थापित’ करने के इतर ‘तोड़न’ की प्रवृत्ति पनप रही है, जहां पर्यावरणीय पारिस्थितिकी को ताक पर रख कर मनुष्य तथाकथित सुखमय जीवनयापन करने हेतु प्रकृति क्षरण हेतु अनेक संसाधनों को विकसित कर रहा है। आईपीसीसी की वर्ष 2022 की रिपोर्ट में उल्लिखित है कि पुरा-औद्योगिक काल की तुलना में यदि वैश्विक ताप 1.5 डिग्री सेंटीग्रेट बढ़ जाएगा तो इसके दुष्प्रभाव अपरिवर्तनीय होंगे। सतही एवं भूमिगत जल, नदियों के उद्गम स्थलों एवं मार्गों, हिमनदों, समुद्रतटों और पर्वतों की पारिस्थितिकी पर इसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा। इन पारिस्थितिकी क्षेत्रों की वनस्पति एवं जैव विविधता से लेकर मानव जीवन भी इसके दंश के शिकार होंगे। चिंतनीय है कि इक्कीसवीं सदी के अंत तक औसत वैश्विक ताप 2.0 डिग्री सेंटीग्रेट तक बढ़ सकता है। इस रिपोर्ट में यह भी उल्लिखित है कि 3.5 अरब आबादी, जो दुनिया की कुल जनसंख्या का 45 प्रतिशत है, किसी न किसी पर्यावरणीय संकट से घिरी हुई है। इसके साथ ही वर्ष 2050 तक भारत की 3.5 करोड़ आबादी को तटीय क्षेत्रों में बाढ़ का सामना करना पड़ेगा एवं समुद्र जल स्तर में वृद्धि के कारण मुंबई को 162 अरब डॉलर का नुकसान होगा और देश की 40 प्रतिशत आबादी को गुणवत्तापूर्ण जल की अनुपलब्धता की समस्या से जूझना पड़ेगा। इसके इतर तापमान वृद्धि के फलस्वरूप अनाजों, फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में गिरावट आने से खाद्य-पदार्थों की आपूर्ति बाधित होगी। साथ ही जलवायु परिवर्तन जनित विसंगतियों की रोकथाम हेतु निरंतर बढ़ते हुए व्यय की वजह से वास्तविक आर्थिक वृद्धि में भी कमी आयेगी।
समाधान के शाश्वत सूत्र
भारत सहित विश्व के अन्यान्य राष्ट्रों को इन समस्याओं के निदान हेतु त्वरित उपाय करने होंगे। इसकी शुरूआत सनातनी संस्कृति, परंपरा और जीवन मूल्यों के शरण में पुन: जाने से संभव है। भारतीय संस्कृति पृथ्वी को समस्त जैविक और अजैविक घटकों का ‘हाउस’ नहीं अपितु ‘होम’ के रूप में स्थापित करती है। ‘होम’ मानने की यह परिकल्पना केवल बौद्धिक और वैज्ञानिक दायरे तक सीमित नहीं है, अपितु ‘होम’ के सभी सदस्यों की तरह पृथ्वी मां के समस्त घटकों में सहजीवन एवं सहअस्तित्व के संबंधों को स्थापित करने का पाथेय है। ‘माता भूमि पुत्रोअहं पृथिव्या: का यही पाथेय हमारे शाश्वत जीवन एवं उसके निर्वहन हेतु सतत विकास यात्रा का मूल मंत्र है। इन पाथेयों की उपेक्षा हमें प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के लिए विवश करती है एवं प्रकृति को अपूर्ण कर मानव सभ्यता के अस्तित्व को प्रश्नांकित करती हैं। प्रकृति के साथ मानव समाज की घनिष्ठता कितनी संवेग, संज्ञान और आध्यात्मिकता से परिपूर्ण है, इसका अनुमान इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि तथाकथित आधुनिक जीवन व्यतीत करते हुए भी हम शांति की खोज में पृथ्वी मां की ऐसी गोद को तलाशते हैं, जो प्रकृति के मूल तत्वों से संपन्न हो, जहां मानव-जनित प्रदूषण न्यूनतम हो एवं प्रकृति अपने अक्षत रूप में उपस्थित हो। हालांकि यह भी एक समस्या है कि इसे मनुष्य ने उद्योग का रूप दे दिया है।
हमारी लोक परंपराओं, संस्कारों, रीति-रिवाजों एवं विभिन्न क्षेत्रों-समुदायों के दैनिक चर्या में प्रकृति संरक्षण हेतु प्रचुर मात्रा में अतुलनीय उपाय निहित हैं। हमारे लोक-पर्वों में भी इनकी जीवंतता विद्यमान है। हम अपने ईश्वर के विभिन्न स्वरूपों को देखें तो ज्ञात होगा कि वे प्रकृति के ही विभिन्न रूप हैं। श्रीराम का वनवास काल वनवासियों, जीव-जन्तुओं, वानरों, पक्षियों, नदी-नालों, पर्वतों, वनस्पतियों एवं प्रकृति के अन्यान्य घटकों के साहचर्य का आदर्श काल ही है। यदि प्रकृति हमारे आराध्यों को प्रिय है तो हमें क्यों नहीं? हमें उनका संरक्षण क्यों नहीं करना चाहिए? सनातन सभ्यता में पृथ्वी के सभी घटक मात्र संसाधन ही नहीं अपितु प्राकृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन के मध्य सामंजस्य की सशक्त कड़ी हैं। मात्र मनुष्य योनि में पैदा होने के नाते हम स्वयं को सर्वोपरि ना समझें अपितु सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एवं सबका प्रयास के मूलमंत्र का पालन करते हुए समस्त चेतन-अचेतन जगत को साथ लेकर चलें तथा उनके साथ चलें। इसके इतर आज हम अपनी भावी पीढ़ी की चिंता किये बगैर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित उपभोग कर रहे हैं। इन परिस्थितियों से निजात पाने हेतु हमें अपने प्राचीन जीवन मूल्यों की तरफ लौटना होगा। इस सन्दर्भ में दो सूत्रों – ‘कम से कम संसाधनों में जीवन यापन करना’ एवं ‘धरती माता भावी पीढ़ियों की है, और हम इसके संरक्षक मात्र हैं’ का पूर्णरुपेण अनुपालन करना समीचीन होगा।
2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन की क्षमता को 500 गीगावॉट करना, कुल ऊर्जा की आवश्यकताओं का 50 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से पूर्ण करना, कार्बन उत्सर्जन को एक बिलियन टन कम करने के साथ ही अर्थव्यवस्था में कार्बन की सघनता को 45 प्रतिशत तक कम करना शामिल है। इस हेतु सरकार का यह भी दायित्व बनता है कि वह गुणवत्तापरक शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवहन की सस्ती सुविधांए जन-सामान्य को उपलब्ध कराये। जिससे किसानों पर अत्यधिक उत्पादन का दबाव न बने एवं रासायनिक खाद और कीटनाशको के उपयोग में कमी आए।
लेना होगा संकल्प
इस सन्दर्भ में यह सोचना होगा कि क्या हम पुन: अपनी वास्तविक सनातनी जीवन पद्धति को अंगीकार कर सकते हैं? क्या हम प्लास्टिक के सभी रूपों के उपयोग को पूर्णरूपेण प्रतिबंधित करने हेतु जन-आंदोलन प्रारंभ कर सकते हैं? क्या हम जैविक कृषि, फसल क्रमावर्तन एवं मिश्रित और बहुप्रकारीय कृषि का सहारा पुन: ले सकते हैं? क्या हम कम से कम इतने वृक्ष लगा सकते हैं, जो हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाईआॅक्साइड को अवशोषित कर सकें तथा हमारे फेफड़ों हेतु समुचित आक्सीजन प्रदान कर सकें? क्या हम कम से कम उतना जल पृथ्वी को वापस कर सकते हैं, जितना उसके उदर से ग्रहण करते हैं? क्या हम यह संकल्प ले सकते हैं कि हम जल की एक बूंद, अन्न का एक दाना और बिजली की एक यूनिट भी बर्बाद नहीं करेंगे? क्या हम महंगी कार के उपयोग के साथ-साथ घर की विद्युत आपूर्ति हेतु सौर ऊर्जा का प्रबंध भी कर सकते हैं? क्या हम उन सात पापों से बच सकते हैं, जिनका उल्लेख महात्मा गांधी जी ने किया था? क्या हम कविवर तुलसीदास की चौपाई ‘क्षिति जल पावक गगन समीरा, पञ्च रचित अति अधम सरीरा’ को सर्वमान्य करते हुए इन पांच तत्वों को पुन: प्रदूषण रहित बना सकते हैं? क्या हम पुन: अपनी प्रकृति को वही आदर-सम्मान दे सकते हैं जो सनातन संस्कृति में निहित हैं, जिसके कारण वह युगों से संरक्षित है?
प्रकृति संरक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा अनेक सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं। कार्बन उत्सर्जन को कम करना हो या वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को खोजना, विकास के वैकल्पिक प्रयोगों को आगे बढ़ाना हो या पर्यावरण संरक्षण के अन्य मुद्दों को प्राथमिकता देना, इन सभी संदर्भों और प्रकरणों में वर्तमान सरकार अपनी सार्थक एवं प्रभावी उपस्थिति दर्ज करा रही है। स्वच्छ भारत मिशन और नमामि गंगे योजना इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने अंतरराष्ट्रीय मंच से पंचमित्र योजना की घोषणा की। इसमें वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन की क्षमता को 500 गीगावॉट करना, कुल ऊर्जा की आवश्यकताओं का 50 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से पूर्ण करना, कार्बन उत्सर्जन को एक बिलियन टन कम करने के साथ ही अर्थव्यवस्था में कार्बन की सघनता को 45 प्रतिशत तक कम करना शामिल है। इस हेतु सरकार का यह भी दायित्व बनता है कि वह गुणवत्तापरक शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवहन की सस्ती सुविधांए जन-सामान्य को उपलब्ध कराये। जिससे किसानों पर अत्यधिक उत्पादन का दबाव न बने एवं रासायनिक खाद और कीटनाशको के उपयोग में कमी आए।
इस संदर्भ में सरकार द्वारा पेट्रोल में वर्ष 2025 तक 20 प्रतिशत एथनॉल के मिश्रण का निर्णय स्वागत योग्य है। सरकार द्वारा एकल उपयोग प्लास्टिक को पूर्णरूपेण प्रतिबंधित करना एक अन्य सराहनीय कदम है। परन्तु इस दिशा में मात्र सरकारी प्रयास ही काफी नहीं हैं। यदि हमें 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन वाले देशों में सम्मिलित होना है, तो हमें प्रकृति संरक्षण विषय को सनातन संस्कृति के अनुरूप जन-जन का आन्दोलन बनाना पड़ेगा।
(लेखक पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, बठिंडा के कुलपति हैं)

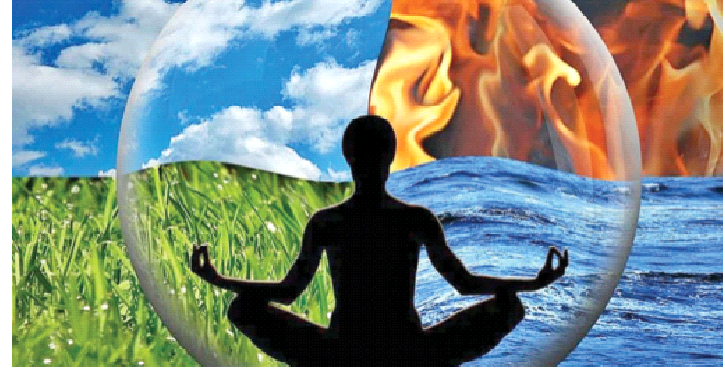









टिप्पणियाँ