|
वर्तमान लोकतांत्रिक-व्यवस्था हमने पश्चिमी देशों से प्राप्त की है। समय के साथ हमारी व्यवस्था स्थानीय अनुभवों के साथ विकसित हो रही है। हमें अपनी परिस्थितियों का अध्ययन करने के साथ-साथ दूसरे देशों और समाजों में हो रहे बदलावों पर भी ध्यान देना चाहिए

प्रमोद जोशी
दोवर्ष में यह बात कई बार जोरदार ढंग से कही गई है कि देश को एक बार फिर से ‘आम चुनाव’ की अवधारणा पर लौटना चाहिए। हाल में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बजट सत्र के अपने अभिभाषण में यह बात कही। प्रधानमंत्री ने संसद के दोनों सदनों में इसे दोहराया। वे इससे पहले भी कई बार यह बात कह चुके हैं। मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालय के न्यायमूर्तियों की कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने इस बात को उठाया। संसद की एक संयुक्त स्थायी समिति ने इसका रास्ता बताया है। एक मंत्रिसमूह ने भी इस पर चर्चा की है। बजट सत्रों के पहले होने वाली सर्वदलीय बैठक में अनौपचारिक रूप से यह विषय चर्चा में आया है। इन सब सुझावों के काफी पहले विधि आयोग ने अपनी 170 वीं रिपोर्ट में इसका सुझाव दिया था। चुनाव सुधार के सिलसिले में चुनाव आयोग की भी यही राय है।
इस सलाह के विरोध में कुछ पार्टियों और विशेषज्ञों ने कहा है कि यह भारतीय लोकतंत्र की विविधता के विपरीत बात होगी। यह तर्क अपेक्षाकृत नया है।
1951 में जब हम अपने देश में चुनावों का श्रीगणेश कर रहे थे, तब किसी के मन में यह विचार नहीं था कि एक साथ चुनाव कराने से देश की राजनीतिक विविधता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। बहरहाल, इस विचार पर भी गम्भीर विमर्श की जरूरत है। अलबत्ता यह भी देखा जाना चाहिए कि इस सिलसिले में वैश्विक दृष्टिकोण क्या है। दुनिया बिखरे हुए चुनाव पसंद करती है या सुगठित और सुनिर्धारित समय पर चुनावों को पसंद करती है। चुनाव एक साथ कराने के पीछे प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों प्रकार के दृष्टिकोणों पर विचार किया जाना चाहिए। इससे समय की बचत होगी, खर्च भी कम होगा। चुनाव के दौरान लगाई जाने वाली आचार संहिता के कारण सरकारें बड़े फैसले नहीं कर पाती हैं। इस वजह से कई काम रुकते हैं। चुनाव एक साथ हों तो केंद्रीय बलों एवं निर्वाचन कर्मियों की तैनाती और बंदोबस्त में होने वाला खर्च कम होगा। पर बात इतनी ही नहीं है। मतदाता को भी अतिशय चुनावबाजी से मुक्ति मिलनी चाहिए।
चुनाव महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक कर्म है। इसकी वजह से राष्ट्रीय महत्व के तमाम प्रश्नों पर बहस होती है। तमाम जानकारियां सामने आती हैं, पर बेतहाशा चुनावबाजी के नकारात्मक पहलू भी हैं। हमारे मन पर लगातार चुनाव के नारे हावी रहते हैं। इससे सामाजिक जीवन में जहर घुलता है। चुनाव के दौर के भाषण एक खास उद्देश्य से जुड़े होते हैं। सामान्य काम-काज के दौर को चुनावी मनोदशा से जोड़ना ठीक नहीं। चुनाव के दौरान काला धन के इस्तेमाल की समस्या भी उठती है। कुछ साल पहले तक मतदान केन्द्र कब्जाने, गुंडागर्दी और हत्याओं का भी चुनावों के साथ घनिष्ठ मेल हो गया था। इसके लिए चुनाव व्यवस्था ही दोषी नहीं है। इसमें सामाजिक विसंगतियों की भी भूमिका है, पर चुनाव की पृष्ठभूमि में उन्हें भड़कने का मौका मिलता है। इनमें से काफी चीजें हमारे समाज की देन हैं।
राजनीतिक स्थिरता का सूचकांक
चुनाव देश की स्थिरता का सूचकांक भी है। दुनिया के अपेक्षाकृत स्थिर देशों में शायद ही ऐसे हालात मिलें। ज्यादातर देश चार या पांच साल में चुनाव कराते हैं और शेष समय में अपनी प्रशासनिक-व्यवस्था को सुदृढ़ करते हैं। हमारी व्यवस्था में भी अब धीरे-धीरे स्थिरता आ रही है। 1999 के बाद से बनी सभी लोकसभाओं ने अपना कार्यकाल पूरा किया है। 2004 में समय से कुछ पहले चुनाव कराए गए थे, पर ऐसा सरकार के निश्चय के कारण हुआ था कोई राजनीतिक दबाव नहीं था। ज्यादातर राज्यों की सरकारें अपना कार्यकाल पूरा कर रही हैं। अगले दसेक साल में ज्यादातर राज्य स्थिर हो जाएंगे। इस स्थिरता को अब पुष्ट करने की जरूरत है।
दिसम्बर 2015 में संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट इस मामले में महत्वपूर्ण प्रस्थान-बिन्दु बन सकती है। इस समिति में दोनों सदनों का प्रतिनिधित्व था और सभी महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों के अलावा विशेषज्ञों की भी इसमें भूमिका थी। इस रिपोर्ट के अलावा नीति आयोग ने एक विमर्श-पत्र भी तैयार किया है, जिसमें इस काम के लिए व्यावहारिक कदम किस प्रकार उठाए जा सकते हैं, इसका संकेत है। देश के पहले आम चुनाव 1951-52 में हुए थे। उस वक्त सभी विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव साथ-साथ ही हुए। इसके बाद 1957, 1962 और 1967 तक साथ-साथ चुनाव हुए।1967 में कई राज्यों में गैर-कांग्रेसी सरकारें बनीं। कुछ राज्यों में समय से पहले ये सरकारें गिरीं और वहां चुनाव हुए, जिससे एक साथ चुनावों का चक्र टूट गया। इसके बाद 1970 में पहली बार केन्द्र सरकार ने समय से पहले चुनाव कराने का फैसला किया और 1971 में केवल लोकसभा के चुनाव हुए।
वैश्विक बदलाव
लोकतांत्रिक-प्रक्रिया एक वैश्विक परिघटना है। इसमें नागरिकों की भागीदारी एक महत्वपूर्ण कारक है। इस भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए ही चुनाव की पद्धतियों का विकास हुआ। देश-काल और ऐतिहासिक परिस्थितियों से ढली और विकसित हुई इन पद्धतियों का उद्देश्य है नागरिकों को व्यवस्था में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी देना और व्यवस्था को व्यावहारिक रूप से उपयोगी बनाना। चुनाव-प्रणाली के विकास के समानांतर तकनीकी विकास भी चल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक-वोट इसका एक उदाहरण है। केवल जन-प्रतिनिधियों को चुनने में ही नहीं, जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी व्यक्ति को अपनी राय देने का मौका मिल रहा है। टीवी के रियलिटी शो से लेकर जीवन के हर क्षेत्र में व्यक्ति की राय जानने के लिए नई तकनीकें सामने आ रही हैं। स्मार्ट फोन ने इसमें क्रांतिकारी भूमिका निभाई है। भविष्य की तकनीक के बारे में अनुमान ही लगाए जा सकते हैं, पर इतना तय है कि बदलाव बहुत तेजी से हो रहा है। हमें इस बदलाव के परिप्रेक्ष्य में भी सोचना चाहिए। इस सिलसिले में हो रहे वैश्विक-परिवर्तनों पर नजर रखने की जरूरत भी है।
जब हम वैश्विक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे सामने कई तरह की उलझनें आती हैं। कोई ऐसा मानक सूत्र उपलब्ध नहीं है, जिसके चश्मे से वैश्विक व्यवस्थाओं को देखा जा सके। अलग-अलग देशों के अलग-अलग अनुभव उन्हें अपने-अपने तरीके ईजाद करने को प्रेरित करते हैं। संयोग से नीति आयोग के विमर्श-पत्र और संसदीय समिति की रिपोर्ट में वैश्विक पृष्ठभूमि पर प्रकाश नहीं डाला गया है। इधर-उधर से जो जानकारी हासिल हुई है, उसे देखें तो कुछ निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। इस सिलसिले में सुव्यवस्थित अध्ययन की जरूरत है।
वर्तमान लोकतांत्रिक-व्यवस्था हमने पश्चिमी देशों से प्राप्त की है। समय के साथ हमारी व्यवस्था स्थानीय अनुभवों के साथ विकसित हो रही है। हमें अपनी परिस्थितियों का अध्ययन करने के साथ-साथ दूसरे देशों और समाजों में हो रहे बदलावों पर भी ध्यान देना चाहिए। हमारा समाज अपेक्षाकृत देर से लोकतांत्रिक-प्रक्रिया में शामिल हुआ है, पर उसमें आ रहे बदलाव दुनिया में सबसे तेज हैं और अगले एक-दो दशकों में हमें और बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। शुरू में हमारा लोकतंत्र द्वि-स्तरीय था।1992 में हुए 73वें और 74वें संविधान संशोधनों के बाद लोकतंत्र की एक तीसरी सतह भी तैयार हो गई है।
अपना मॉडल विकसित करें
अब जब हम एक साथ चुनाव की व्यवस्था बनाने पर विचार कर रहे हैं, तब तीनों सतहों पर एक साथ चुनाव की परिकल्पना भी उभर कर सामने आ रही है। यों नीति आयोग के विमर्श पत्र में कहा गया है कि तीसरी सतह का नियमन राज्यों के अधिकार क्षेत्र में है। इसलिए और इन निकायों की विशाल संख्या को देखते हुए इस तीसरी सतह के चुनावों को भी वृहत चुनाव-व्यवस्था से जोड़ पाना असंभव है। हालांकि दुनिया के कई देशों में तीनों स्तरों पर एक साथ चुनाव कराने की व्यवस्था है। हमने ब्रिटेन से संसदीय लोकतांत्रिक-प्रणाली को हासिल किया है। वहां तीनों स्तरों पर चुनाव एक साथ कराने की अवधारणा को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया गया है। भारत में ग्राम पंचायतों, ब्लॉक पंचायतों और जिला पंचायतों की अनुमानित संख्या 2.51 लाख है। नगर निकायों की संख्या इनके अलावा है। जाहिर है कि इतने बड़े लोकतांत्रिक समाज के लिए कोई वैश्विक मॉडल मिलना आसान नहीं है। उसका आविष्कार हमें ही करना होगा। भारत में 4120 विधानसभा और 543 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव होता है। पहले हमें इन चुनावों को एक साथ कराने के व्यावहारिक तरीकों पर विचार करना चाहिए।
चुनाव पद्धतियों का अध्ययन करते वक्त हमें दो-तीन बातों पर और ध्यान देना होगा। एकीकृत व्यवस्था में ऐसे फैसले करना सरल होता है, जिनका स्वरूप एकीकृत हो। संघीय व्यवस्था में फैसले करने के पहले संघीय-भावना से जुड़े पहलुओं पर भी विचार करना होगा। हमारी शासन-व्यवस्था संसदीय है, अध्यक्षात्मक नहीं। अमेरिकी व्यवस्था अध्यक्षात्मक है, जिसमें सरकारें एक निर्धारित समय के लिए चुनी जाती हैं। हमारी व्यवस्था में सरकारों की स्थिरता की गारंटी नहीं है।
इस मामले में मतदान की पद्धति भी महत्वपूर्ण है। हमारी व्यवस्था ‘फर्स्ट पास्ट द पोस्ट’ है। इसमें सबसे ज्यादा वोट पाने वाला व्यक्ति चुनाव जीतता है। दुनिया के दूसरे देशों में आनुपातिक और एकल हस्तांतरणीय मत-प्रणालियां भी हैं, जिनसे प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत बेहतर हो सकता है, पर उन पद्धतियों की जटिलता और अपने देश की विशालता को देखते हुए उनकी कल्पना नहीं की जा सकती। भारत की संघीय शासन-व्यवस्था और संसदीय-प्रणाली की तुलना दुनिया की व्यवस्थाओं से करना मुश्किल काम है। फिर भी उन राजनीतिक-व्यवस्थाओं पर नजर डालनी चाहिए, जो या तो संघीय हैं या संसदीय प्रणाली से जुड़ी हैं। इस लिहाज से इन देशों की व्यवस्थाओं को देखना चाहिए। अमेरिका, आॅस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन, बेल्जियम, स्वीडन, इटली और ब्राजील। भारत के आकार की तुलना चीन से की जा सकती है, पर वहां की व्यवस्था हमारी जैसी नहीं है।
अतिशय खुला या बंद?
इन दिनों चीन में 13वीं राष्ट्रीय जन-कांग्रेस का सालाना सत्र चल रहा है। चीनी जन-कांग्रेस में इस समय 1980 सदस्य हैं। इनका चुनाव हर पांच साल में होता है। 10 से 15 दिनों का इसका सत्र साल में एक बार होता है। वस्तुत: इसके डेढ़ सौ सदस्यों की स्थायी समिति ही व्यावहारिक रूप से सारे काम करती है। इसके समानांतर वहां कम्युनिस्ट पार्टी की पूरी व्यवस्था है, जो इस लोकतांत्रिक तंत्र के पीछे काम करती है। हमारे खुले मीडिया और खुली-बिखरी राजनीति के मुकाबले चीन में तकरीबन बंद राजनीति है।
चीनी व्यवस्था के विपरीत अमेरिका की राजनीति है। वहां हालांकि संविधान ने चुनावों के दिन तक तय कर रखे हैं, पर उनसे जुड़े ज्यादातर पहलू राज्यों के नियमों से जुड़े हैं। अमेरिका की संघीय व्यवस्था में राज्य बहुत शक्तिशाली हैं। वहां मतदान की पद्धति से जुड़ी राज्यों की व्यवस्थाएं अलग-अलग हैं। वहां संघ, राज्य और स्थानीय निकाय के चुनावों को राज्य संचालित करते हैं। इसलिए वहां एक साथ चुनाव नहीं होते, पर व्यवस्थित और स्थिर चुनाव-तंत्र वहां स्थापित है।
यूके यानी यूनाइटेड किंग्डम आफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड में हाल के वर्षों में चुनाव-कार्यक्रम को साधने की कोशिश की जा रही है। वहां चुनाव का दिन गुरुवार तय है। 1997 से 2015 तक यह व्यवस्था बनी भी रही। 2011 में यहां फिक्स्ड टर्म पार्लियामेंट एक्ट पास हुआ और हर पांच साल में मई महीने में पहले गुरुवार को आम चुनाव कराने की व्यवस्था की गई है। कुछ विशेष परिस्थितियों में चुनाव समय से पहले कराने की छूट भी इसमें दी गई है। संयोग से पिछले साल ऐसा हो भी गया। नई व्यवस्था के तहत 7 मई, 2015 को पहले चुनाव हुए और अगले चुनाव की तिथि 7 मई, 2020 तय कर दी गई थी। इस बीच ‘ब्रेक्जिट’ के कारण ऐसी स्थिति पैदा हुई कि फिर से चुनाव कराने की नौबत आ गई। पिछले साल अप्रैल में संसद ने एक विशेष प्रस्ताव पास करके जल्दी चुनाव कराने का फैसला किया। इस वजह से स्थानीय निकायों और संसद के चुनाव अलग-अलग दिनों में हुए। बहरहाल 2022 के चुनावों की तिथियां तय हैं। इटली, बेल्जियम और स्वीडन में भी संसद और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ होते हैं। स्वीडन में राष्ट्रीय संसद, प्रांतीय विधायिकाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव हर चार साल बाद एक निश्चित दिन सितम्बर के दूसरे रविवार को होते हैं। नवीनतम व्यवस्था 2014 से लागू है। इसके पहले चुनाव सितम्बर के तीसरे रविवार को होते थे। स्वीडन में यूरोपियन संसद के चुनाव भी हर पांचवें साल जून के एक रविवार को होते हैं।
कनाडा में पालिका चुनावों का समय निश्चित है, पर प्रांतों और संघीय चुनावों का समय तय नहीं है। यों संसद के चुनाव चार साल में होते हैं। देश में ‘फिक्स्ड इलेक्शन डेट’ आंदोलन चला था, जिसके बाद मई 2007 में संसद ने ‘फिक्स्ड इलेक्शन डेट एक्ट’ पारित किया। इसके तहत हर चौथे साल अक्तूबर के तीसरे सोमवार को वहां चुनाव होते हैं। पर समय से पहले संसद के भंग होने पर चुनाव जल्दी भी हो सकते हैं।
दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रीय और प्रादेशिक प्रतिनिधि सदनों के चुनाव एक साथ पांच साल के लिए होते हैं। इनके अलावा हर दो साल बाद नगरपालिकाओं के चुनाव होते हैं। विकासशील देशों में दक्षिण अफ्रीका को चुनावी स्थिरता के लिए पहचाना जा सकता है। आॅस्ट्रेलिया की व्यवस्था संघीय है। वहां भी चुनाव से जुड़े संघीय नियम अलग हैं और प्रांतीय नियम अलग। वहां एकल हस्तांतरणीय वोट प्रणाली है। 1977 में सीनेट और जन-प्रतिनिधि सदन के चुनाव साथ-साथ कराने के लिए जनमत संग्रह हुआ था, जो पास नहीं हुआ।
मोटे तौर पर एक बात नजर आती है कि काफी देशों ने एक साथ चुनाव कराने की प्रणाली विकसित करने का प्रयास किया है और उसके लिए सांविधानिक-व्यवस्थाएं भी की हैं। ज्यादातर देशों में चार या पांच साल के अंतर से चुनाव होते हैं। अलग-अलग देशों की लोकतांत्रिक संस्थाएं अलग-अलग प्रकार की हैं।
उनकी मतदान पद्धति भी अलग है। मसलन भारत में ‘फर्स्ट पास्ट द पोस्ट’ पद्धति है, तो आॅस्ट्रेलिया में एकल हस्तांतरणीय वोट है, जिसमें मतदाता सामने खड़े प्रत्याशियों को वरीयता प्रदान करते हैं। दक्षिण अफ्रीका में आनुपातिक पद्धति है, जहां पार्टियों की सूची में से प्रत्याशियों को पार्टी को मिले वोट के अनुपात में चुना जाता है।
एक साथ चुनाव की मांग के हमारे देश में और बुलंद होने के आसार के चलते हमें हर तरह की व्यवस्था की बारीक पड़ताल कर लेनी होगी।
चुनाव का दिन तय
विश्व में काफी बड़ी संख्या में ऐसे देश हैं, जहां चुनाव के दिन तक निर्धारित हैं। इससे चुनाव को लेकर असमंजस नहीं होता। काफी देशों में रविवार का दिन इस काम के लिए तय है। बहुत से देशों में सप्ताह के दूसरे दिन भी इसके लिए तय हैं। कुछ देशों के दिन इस प्रकार हैं:-
यहां रविवार को होते हैं चुनाव
ल्ल अल्बानिया, आॅस्ट्रिया, बेल्जियम, बोलीविया, बोस्निया और हर्जगोवीना, ब्राजील, बुल्गारिया, कोस्टारिका, चिली, कोलम्बिया, क्रोएशिया, अल सल्वाडोर, एस्तोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हांगकांग, हंगरी, इटली, जापान, लेबनॉन, लिथुआनिया, लक्जम्बर्ग, मकदूनिया, मलेशिया, मैक्सिको, मोंटेनेग्रो, निकरागुआ, पनामा, पैराग्वे, पेरू, पुर्तगाल, रोमानिया, रूस, सर्बिया, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, तुर्की, यूक्रेन, उरुग्व और वेनेजुएला
यहां ये दिन तय हैं चुनाव के
आस्ट्रेलिया, सायप्रस, आइसलैंड, लात्विया, माल्टा, न्यूजीलैंड, ताइवान अर्जेंटीना: संसद के कार्यकाल की समाप्ति के पहले अक्तूबर का चौथा रविवार
कनाडा: हर 4 साल में अक्तूबर का तीसरा सोमवार
चेक गणराज्य: सामान्यत: चुनाव शुक्रवार के तीसरे पहर शुरू होते हैं और शनिवार की दोपहर को खत्म होते हैं डेनमार्क:आमतौर पर मंगलवार, पर सप्ताह के दूसरे दिनों में भी चुनाव हुए हैं
आयरलैंड: प्राय: शुक्रवार, पर निश्चित तिथि की घोषणा सरकार करती है
इस्रायल: नियमत: हिब्रू माह चेश्वान का तीसरा मंगलवार।
नीदरलैंड्स,दक्षिण कोरिया: बुधवार



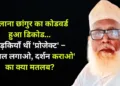



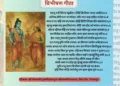
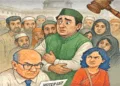



टिप्पणियाँ