|
‘हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्वसंपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली, बंधुता बढ़ाने के लिए, दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ईस्वी (मिति माघशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत् 2006 विक्रमी) को एतत्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।’
(भारतीय संविधान की उद्देशिका)
प्रथम शिक्षा नीति आजादी के लगभग 20 वर्ष बाद 1968 में बनी, लेकिन उसमें भी भारत की उपेक्षा की गई। आज भारतीयता को पुष्ट करने वाली शिक्षा की जरूरत है। इसलिए उसी के अनुरूप हमारी शिक्षा नीति बने

चांद किरण सलूजा
भारतीय संविधान की उद्देशिका, जिसे संविधान निर्माण के समय भावी भारत के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक-सामाजिक दर्शन की आधारशिला के रूप में देखा गया था, इस बात को स्पष्ट रूप से उकेरने का प्रयास करती है कि भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों का लक्ष्य भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्वसंपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में संरचित करना है। यहां यह ध्यातव्य है कि न्यायालयों में, विशेषतया उच्चतम न्यायालय में आए विभिन्न वादों के संदर्भ में, इन चारों शब्दों की विशिष्ट व्याख्याएं की गई हैं। ध्यातव्य यह भी है कि संविधान की इस उद्देशिका में समाजवादी एवं पंथनिरपेक्ष शब्द संविधान संशोधन के 42वें अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़े गए थे। इनके जोड़े जाने के कारण, प्रभाव अथवा निहितार्थ यद्यपि विचारणीय हो सकते हैं, तथापि यह स्पष्ट ही है कि वैयक्तिक एवं सामूहिक दृष्टि से इनका विशिष्ट स्थान एवं महत्व है। यह सुविदित है कि भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों की स्पष्टता अथवा व्याख्या का दायित्व मूलत: न्यायालय के अधीन है। यहां यह स्पष्ट होना चाहिए कि न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में इस बात को स्पष्ट रूप से उजागर करने का प्रयास किया गया है कि ‘समाजवाद’ में मूलत: ‘समत्व युक्त सामूहिकता’ का भाव अन्तर्निहित है, तथा भारतीय संविधान की उद्देशिका में निहित ‘न्याय, समता, स्वतंत्रता एवं बंधुता’ इन चार आधारभूत मूल्यों की प्राप्ति ही संविधान के विभिन्न प्रावधानों का उद्देश्य है। भाषा को इन चारों मूल्यों के आधारभूत तत्व के रूप में लिया जा सकता है। यह भाषा ही है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सबमें, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली, बंधुता सम्बन्धी उद्देश्यों को आकार दे सकता है।
इन उद्देश्यों के अन्तर्गत भाषा से संबद्ध अभिव्यक्ति एवं तद्नुसार ग्राह्यात्मकता का विशिष्ट महत्व है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबद्ध संविधान का अनुच्छेद 19 इस तथ्य का सबल प्रमाण है। चार अध्यायों में विभक्त संविधान का भाग 17 (राजभाषा) के अनुच्छेद 343-351 सम्पूर्णतया राज्य की भाषानीति से संबद्ध है :
(1) संघ की भाषा
(2) क्षेत्रीय भाषाएं
(3) उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों की
भाषा एवं
(४) विशिष्ट निर्देश
इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान के अनुच्छेद : 14, 21, 29, 30, 46, 120, 210 एवं आठवीं अनुसूची प्रत्यक्षत: अथवा अप्रत्यक्षत: भाषा-नीति से ही संबद्ध हैं। न्यायालयों द्वारा प्रदत्त विभिन्न निर्णय इस बात का स्पष्ट निर्देश-सा देते हैं कि भारत में भाषा का प्रश्न सैद्धान्तिक तौर पर मौलिक अधिकार के रूप में सामाजिक न्याय से जुड़ा है। इसका संबंध सीधे तौर पर जहां व्यक्ति की वैयक्तिकता से जुड़ा है तो वहीं बृहद् समाज से भी। यही कारण है कि न्यायालयों में, विशेषत: उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न वादों में यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधान मौलिक अधिकार के रूप में व्यष्टि को महत्व देते हुए भी कल्याणकारी तत्वों का स्वरूप लिए हुए राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्तों के रूप में व्यापक समष्टि तक व्याप्त हैं। पूर्वोक्त संविधान संशोधन के 42वें अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत संविधान में भाग 4 (अ)के रूप में ‘मौलिक कर्तव्यों’ का जोड़ा जाना इसका सर्वाधिक सबल प्रमाण है। यह सुस्पष्ट ही है कि इनके अनुपालन हेतु एक सुगठित एवं व्यवस्थित सामाजिक जीवन का होना अनिवार्य-सा हो जाता है। यही कारण है कि व्यष्टि एवं समष्टि को महत्व देने वाले भारतीय संविधान की उद्देशिका में ‘न्याय, स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता’ जैसे आधारभूत मूल्यों का अपना एक विशिष्ट स्थान एवं महत्व है। हमारे संविधान में इन्हें केवल विशिष्ट व महत्वपूर्ण स्थान ही नहीं दिया गया, अपितु यह भी स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि अन्तत: भारतीय समाज का भावी स्वरूप कैसा होना चाहिए!
संविधान की उद्देशिका के प्रारम्भिक शब्द, ‘हम, भारत के लोग’ इस चिन्तन के लिए प्रेरित करते हैं कि अन्तत: ‘हम’ एवं ‘भारत के लोग’ से क्या अभिप्राय हो सकता है! इन दो शब्दों का प्रयोग एक राष्ट्र के रूप में भारतीय भू-भाग एवं इसमें निवास करने वाले जन-समुदाय की किन विशिष्टताओं की ओर संकेत देता है!
1994 में उच्चतम न्यायालय द्वारा संस्कृत से संबद्ध दिए गए एक वाद के निर्णय में इस बात को बहुत ही स्पष्टता के साथ स्पष्ट करने-कराने का प्रयास किया गया था कि ‘हम, भारत के लोग’ शब्दों का प्रयोग सीधे तौर पर भारत की पहचान अथवा अस्मिता के रूप में संस्कृत से ही जुड़ा हुआ है। परिणामत: भारत की शिक्षा-नीति में संस्कृत का विशिष्ट स्थान होना अनिवार्य हो जाता है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार, ‘हमारी संस्कृति का स्रोत सूख जाएगा यदि हमने संस्कृत के अध्ययन को निरुत्साहित किया (अनुच्छेद 3)……हम बोर्ड जैसी उत्तरदायी संस्था जिसे देश की युवा पीढ़ी को शिक्षित करने का कठिन कर्तव्य सौंपा गया है ‘जिसके हाथों में भविष्य झूल रहा है’ द्वारा दिए गए मत को समझने में असमर्थ हैं क्योंकि वह पूर्णतया अतर्कसंगत है। संस्कृत के अध्ययन के बिना भारतीय दर्शन, जिस पर हमारी संस्कृति और विरासत आधारित है, को स्पष्ट रूप से समझना सम्भव नहीं है।
(1994(6) एस.सी.सी. 579 की रिपोर्ट)
भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों से संबद्ध अनुच्छेद 51(अ) के विभिन्न उपबंध, विशेषत: (क),(ख),(ग),(घ),(ङ) एवं (च), भारत के वैविध्य में समाए ऐक्यभाव एवं भारत की समृद्ध संस्कृति एवं मूल्यों के संरक्षण के प्रति हमारे कर्तव्य का बोध कराते हैं। अनुच्छेद 51(च) के अनुसार प्रत्येक भारतीय का यह कर्तव्य है कि वह, ‘हमारी सामासिक संस्कृति की समृद्ध धरोहर को सम्मान देते हुए हुए उसका संरक्षण करे।’
उच्चतम न्यायालय के अनुसार स्पष्ट ही है कि ‘शिक्षा एवं संस्कृति’ मूलत: जहां जीवन-चक्र के दो अभिन्न पक्ष हैं, वहीं राष्ट्रीय जीवन की अस्मिता का अभिन्न अंग। संस्कृति के द्वारा यदि जीवन के आदर्शों को निर्धारित किया जा सकता है तो शिक्षा उन आदर्शों को प्राप्त करने की साधिका की भूमिका का निर्वहन करती है। जीवन का यह रूप ही मूलत: राष्ट्रीय संचेतना का वाहक बनता है। परंतु विभिन्न कारणों से शैक्षिक परिस्थितियों से उपजी शून्यता इस तथ्य की संकेतिका है कि भारत में परिचालित शिक्षा व्यवस्था भारत में चलते हुए भी ‘भारतीय’ नहीं हो पाई। अथवा, भारत में चलने वाली शिक्षा अपना ‘राष्ट्रीय’ रूप नहीं ले पाई, जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गठित अंतरराष्ट्रीय आयोग ने अत्यन्त स्पष्ट रूप से अपने शैक्षिक प्रतिवेदन में स्पष्ट करने का प्रयास किया था कि शिक्षा को जिन चार मूलभूत स्तंभों पर खड़ा होना चाहिए उनमें से ‘लर्निंग टू लिव टूगेदर..’ ‘मिल कर चलने हेतु शिक्षा’ का भाव मूलत: ऋग्वैदिक उद्घोषणा ‘संगच्छध्वम् संवदध्वम्.’ पर ही आश्रित है। उसी तरह ‘लर्निंग टू बी’ ….. ‘मनुष्य बनने हेतु शिक्षा’ कथन भी मूलत: अपने-आप में वैदिक संदेश ‘मनुर्भव…..मनुष्य बनो’ की भावना को अभिव्यक्त करता है। अत: यह अनिवार्य हो जाता है कि शिक्षा को भारतीयता का स्वरूप दिया जाए।
इसका कारण बहुत स्पष्टता से खोजा जा सकता है। इस कारण का मूल एक राष्ट्र के रूप में एक स्पष्ट भाषा-नीति के अभाव में निहित है। स्पष्ट ही है कि किसी भी राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था का उत्स मूलत: उस राष्ट्र की संस्कृति में निहित रहता है, तो उस संस्कृति का मूल उस राष्ट्र की भिन्न-भिन्न भाषाओं में। यही कारण है कि प्रत्येक राष्ट्र की शिक्षा-नीति मूलत: भाषा-शिक्षा के रूप में ही प्रतिबिम्बित-सी होती दृष्टिगत होने लगती है, अथवा उसे इसका प्रतिबिम्बन होना ही चाहिए, अन्यथा इसके अभाव में उस राष्ट्र की शिक्षा-व्यवस्था अपने राष्ट्र के जन-जन के साथ सात्मीकरण नहीं कर पाती जिसके परिणामस्वरूप वह राष्ट्र की अस्मिता से अलग-थलग हो विदेशी-सी प्रतीत होने लगती है। यह ध्यातव्य है कि किसी भी राष्ट्र में भाषा संबंधी प्रश्न मूलत: मानवीय अधिकार संबंधी एक आधारभूत प्रश्न है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मातृभाषा के रूप में मनाया जाने वाला दिवस इसी तथ्य की गाथा गाता है। यही कारण है कि किसी भी राष्ट्र की शिक्षा-नीति का एक आधारभूत लक्ष्य उस राष्ट्र की संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन एवं परिशोधन से संबद्ध होने के नाते भाषा-नीति से अनिवार्य रूप से जुड़ा होता है। भारतीय शिक्षा-व्यवस्था इस तथ्य का अपवाद न होते हुए भी, इस सन्दर्भ में, अपनी बहु-भाषी विशिष्टता के कारण विशिष्ट अवश्य ही होनी चाहिए थी। इस ओर विशिष्ट ध्यान एवं प्राथमिकता देना इसका आवश्यक लक्ष्य एवं कार्य समझा जाना चाहिए था। अत: स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राष्ट्र के विकास का स्वप्न राष्ट्र की महती संस्कृति की गोद में लेते हुए स्पष्ट भाषा-नीति युक्त शिक्षा-नीति की महक से होना चाहिए था परन्तु इसे ‘दुर्घटना’ ही कहा जा सकता है कि ‘राजनैतिक’ दृष्टि से स्वतंत्र भारत की प्रथम भारतीय शिक्षा नीति का निर्माण स्वतंत्रता प्राप्ति के लगभग 20 वर्ष पश्चात हुआ और इसमें भी ‘त्रि-भाषा’ सूत्र नाम से विख्यात ‘भाषा-नीति’ का पक्ष अत्यन्त सशंकित, अव्यावहारिक एवं दुर्बल-सा दृष्टिगत होता है। यह केवल गणना तक ही सिमट कर रह गया। स्पष्ट होना चाहिए कि भाषा-नीति को केवल ‘कितनी एवं कौन-कौन-सी भाषाएं पढ़ाई जानी चाहिएं’ तक परिसीमित नहीं किया जा सकता। विशेषत: भारत जैसे वैविध्यपूर्ण राष्ट्र के लिए जिसके सन्दर्भ में भाषा-विज्ञान की यह उक्ति चरितार्थ होती हुई अपना मुखर रूप दिखा रही हो ‘चार कोस पर पानी बदले आठ कोस पर बानी’ तथा समान संस्कृति होते हुए भी राज्यों का पुनर्गठन ‘भाषा’ के आधार पर हुआ हो। तथापि यह वैधानिक रूप से घोषित किया गया कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिन्दी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिन्दुस्तानी में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके अन्य भाषाओं से शब्द भंडार के लिए मुख्यत: संस्कृत से गौणत: अन्य भाषाओं से ग्रहण कर सके।
(अनुच्छेद 351; भारत का संविधान)
इस वाद एवं संस्कृत से संबद्ध अन्य वादों में दिए गए उच्चतम न्यायालय एवं अन्य न्यायालयों अथवा विभिन्न आयोगों / समितियों की अनुशंसाओं अथवा संविधान सभा की परिचर्चाओं आदि के भावानुसार भारतीय भाषाओं के उच्चतम विकास की दृष्टि से, भारतीय भाषाओं की आधारभूत भाषा होने के कारण शिक्षा-व्यवस्था में संस्कृत का महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए।
ध्यातव्य है कि आधुनिक ज्ञान-विज्ञान का मूल भी संस्कृति में ही अधिष्ठित रहता है तथा इसके अन्तर्गत संपूर्ण जीवन-शैली निहित रहती है। यह आधुनिक ज्ञान-विज्ञान का आधार भी बनी रहती है। यह स्पष्ट ही है कि आधुनिक ज्ञान-विज्ञान को समझने के लिए ज्ञान-विज्ञान की सुदीर्घ परम्परा को समझना अनिवार्य-सा हो जाता है। भारतीय दृष्टि से संस्कृत इस ज्ञान-विज्ञान की परम्परा का आधार है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के ज्ञानात्मक विषयों की शब्दावली का निर्माण करके भारतीय भाषाओं को समृद्ध किया जा सकता है, तथा इन भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रयुक्त कर शिक्षा की प्रक्रिया को सहज एवं सुलभ बनाया जा सकता है। यहां यह ध्यातव्य एवं विचारणीय है कि अपने दैनिक व्यावहारिक रूप में मातृभाषा से भली-भांति सुपरिचित होने के नाते बच्चे विद्यालय-प्रवेश से पूर्व ही साक्षर होते हैं जिसके आधार पर उनकी शिक्षा की औपचारिक प्रक्रिया को मातृभाषा के द्वारा सहज रूप में प्रारम्भ किया जा सकता है। यह अनुभूत सत्य है कि विद्यालय-प्रवेश से पूर्व बच्चा ‘कोरी सलेट’ नहीं होता, जिस प्रकार की पूर्वकल्पना कुछ अधिगमनात्मक प्रतिमानों ने की है। इस दृष्टि से भाषा-नीति किसी भी शिक्षा-नीति का आधारभूत ‘सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग’ है जिसकी ओर सर्वप्रथम ध्यान देने की आवश्यकता रहनी चाहिए। स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात प्रजातांत्रिक प्रक्रिया के अनुपालन की दृष्टि से यह सर्वाधिक प्राथमिकता का विषय बनना चाहिए था। परन्तु आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि हमारी प्रथम शिक्षा-नीति ही स्वतंत्रता-प्राप्ति के लगभग 20 वर्ष पश्चात1968 में घोषित हुई। हमारा प्रथम शिक्षा-आयोग संविधान-निर्माण से पूर्व ही ‘विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग’ के रूप में गठित हुआ था न कि शिक्षा-नीति अथवा प्राथमिक शिक्षा-आयोग के रूप में। इसमें भाषा सम्बन्धी चर्चा तो अवश्य दृष्टिगत होती है पर भाषा-नीति के रूप में नहीं शनै: – शनै: विद्यालयी शिक्षा विश्वविद्यालयी शिक्षा की पूर्ति का का रूप लेती गई। इसका स्वतंत्र स्वरूप विकसित नहीं हो पाया। विद्यालयी शिक्षा के विषयों का स्वरूप इस बात से अधिक निर्धारित होने लगा कि विश्वविद्यालयी शिक्षा में प्रवेश का आधार क्या है? इस तथ्य की प्राय: उपेक्षा होती रही कि व्यक्ति एवं समाज के विकास हेतु भाषा की ही आधारभूत भूमिका होती है। यह स्पष्ट ही है कि अन्तत: ‘व्यक्ति एवं समाज’ का विकास शिक्षा पर ही निर्भर करता है तो ‘शिक्षा’ का विकास भाषा की भूमिका पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344(3) में इस बात को बड़े ही सुन्दर रूप से उकेरने का प्रयास किया है :
खंड (2) के अधीन अपना अनुमोदन करने में, आयोग भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का और लोक सेवाओं के संबंध में अहिंदी भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्यायसंगत दावों एवं हितों का भली-भांति ध्यान रखेगा।
(अनुच्छेद 344(3); भारत का संविधान)
अत: भाषा-शिक्षा के प्रति उपयुक्त अवधान न देने का आभास अत्यन्त ही सतही एवं अपरिपक्व दृष्टि का उदाहरण ही माना जा सकता है।
संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त होने पर भी (संविधान निर्माण के समय यह संख्या 15 थी), उच्च शैक्षिक स्तर पर किसी भी भारतीय भाषा को आवश्यक-सा स्थान प्रदान नहीं किया गया। संविधान की आठवीं सूची में अंग्रेजी का उल्लेख नहीं है, परन्तु संविधान के अनुच्छेद 343 में अंग्रेजी को केन्द्रीय स्तर पर सह-राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई तथा हिन्दी को राजभाषा के रूप में। परन्तु, शिक्षा व्यवस्था में उच्च स्तरीय शिक्षा तक अंग्रेजी को ही आवश्यक-सा स्थान प्राप्त होता चला गया जबकि भारतीय भाषाओं को संविधान के अनुच्छेद 350(क) के अनुसार केवल संकेतित रूप में प्रारम्भिक शिक्षा तक स्थान प्राप्त है,
‘‘प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर स्थानीय प्राधिकारी भाषायी अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकेगा जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चत कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता है।’’ (अनुच्छेद 350(क);भारत का संविधान)
यह परिस्थिति केवल प्राथमिक स्तर तक मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था हेतु प्रयास करने से संबद्ध है न कि उसके आवश्यक स्वाभाविक अधिकार के रूप में आवश्यक।
इसके पश्चात की शिक्षा हेतु किसी भारतीय भाषा का उल्लेख नहीं है। सन् 1968 की शिक्षा नीति, जिसका पुन: अनुमोदन सन् 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किया गया, के अनुसार अंग्रेजी को पुस्तकालयी भाषा के रूप में प्रदर्शित किया गया, साथ ही द्वितीय भाषा के रूप में आवश्यक-सा स्थान प्रदान किया गया है।
इस सम्पूर्ण परिप्रेक्ष्य में, भारतीय शिक्षा-व्यवस्था में भाषा-नीति अथवा भाषा-शिक्षा के रूप में ‘भारतीय भाषाओं का स्थान क्या हो?’ एक अत्यन्त ही चुनौती भरा महत्वपूर्ण प्रश्न रहा है। इस प्रश्न के मूल को स्वतन्त्रता पूर्व की ब्रिटिशकालीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था के मूल में खोजा जा सकता है, विशेषत: सन् 1835 के ‘टी.मैकाले मिनिट्स’ के पश्चात स्वतंत्रता पश्चात भारतीय राज्यों तथा संविधान के निर्माण के पश्चात यह प्रश्न निरन्तर अधिक कठिन प्रश्न होता गया।
भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में भारत की विभिन्न भाषाओं का उल्लेख किया गया है :
1. असमी 2. बंगला 3. बोडो 4. डोगरी
5. गुजराती 6. हिन्दी 7. कन्नड़ 8. कश्मीरी
9. कोंकणी 10. मैथिली 11. मलयालम
12. मणिपुरी 13. मराठी 14. नेपाली
15. ओड़िया 16. पंजाबी 17. संस्कृत
18. संथाली 19. सिन्धी 20. तमिल
21. तेलुगू 22. उर्दू
यह ध्यातव्य है कि सह-राजभाषा के रूप में स्वीकृत अंग्रेजी भाषा इस सूची में नहीं है।
अनुमोदित त्रि-भाषासूत्र के सम्मुख प्रमुखत: निम्नलिखित तीन
प्रश्न रहे :
’ मातृभाषाओं का स्थान ’ शिक्षा का माध्यम ’ भारत में एक सम्पर्क भाषा
यह सूत्र मूलत: भारतीय संविधान के दो अनुच्छेदों पर आधारित है :
’ अनुच्छेद 343 तथा ’ अनुच्छेद 350
तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार इसमें प्रारम्भिक स्तर की शिक्षा के पश्चात की शिक्षा हेतु (विशेषत: विज्ञान की शिक्षा हेतु) माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा को स्थान दिया गया था तथा यह विचार भी समक्ष आया था कि शनै:-शनै: भारतीय भाषाओं का विकास करते हुए उच्चस्तरीय शिक्षण-सामग्री भी भारतीय भाषाओं में विकसित कर ली जाएगी तथा भारतीय भाषाएं ही शिक्षा के माध्यम का रूप धारण कर लेंगी।
1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने त्रिभाषा सूत्र की नीति में कोई परिवर्तन न करते हुए 1968 की इसी नीति का ही अनुमोदन किया था।
1968 की शिक्षा नीति ने भाषाओं के विकास से संबद्ध प्रश्न पर अत्यन्त विस्तार से परीक्षण किया था। इसके आवश्यक प्रावधान आज भी उसी प्रकार से सार्थक हैं जैसे पहले थे, अत: इनमें संशोधन की अपेक्षा नहीं है। परन्तु इस भाग का कार्यान्वयन अत्यन्त असमान रहा है। अत: इस नीति का दृढ़ता से अनुपालन किया जाएगा।(अनुच्छेद 8.7)
साथ ही,
भारत में विद्या, मानविकी और सामाजिक विज्ञान में शोध कार्य को समुचित समर्थन दिया जाएगा। ज्ञान के संश्लेषण की आवश्यकता की पूर्ति हेतु अन्तर्विषयक शोध को प्रोत्साहित किया जाएगा। भारतीय ज्ञान के प्राचीन भण्डार की खोज करके उसे समकालीन वास्तविकता से जोड़ने के प्रयास किए जाएंगे। इसका अर्थ यह होगा कि संस्कृत के गहन अध्ययन की सुविधाओं का विकास किया जाए।
(अनुच्छेद 5.33; राष्ट्रीय शिक्षा नीति,1968, उच्चतम न्यायालय द्वारा उद्धृत,1994)
संस्कृत आयोग ने संस्कृत के संदर्भ में विशेष रूप से ‘स्वतंत्र भारत में संस्कृत की आवश्यकता’ के सन्दर्भ में चर्चा करते हुए विशिष्ट अनुमोदन किए हैं।
उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में, विशेषत: शिक्षा के संदर्भ में, हमारे सम्मुख भाषा संबंधी प्रमुखत: निम्नलिखित आयाम उभरते हैं :
’ शिक्षा-व्यवस्था में भाषा/भाषाओं के स्थान, आवश्यकता एवं स्वरूप सम्बन्धी नीति:
समकालीन आवश्यकताओं, भारतीय संस्कृति/ मूल्य, ज्ञान-निर्माण एवं बच्चों की सृजनात्मक-क्षमता को अभिव्यक्तयात्मक रूप देने आदि के परिप्रेक्ष्य में भाषाओं के महत्व को समझते हुए भाषा-शिक्षण के स्वरूप को पुनर्व्याख्यायित करना होगा। समकालीन प्रचलित प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय भाषा के रूप में भाषा-शिक्षण/अधिगमन की अवधारणा के सन्दर्भ को भारतीय भाषाओं के शिक्षण हेतु यथावत् रूप में स्वीकृत नहीं किया जा सकता। मूलत: यह ‘विदेशी-भाषा-शिक्षण’ की संकल्पना पर आश्रित है। यथा, भारत में संस्कृत का तृतीय भाषा के रूप में शिक्षण विदेशी भाषा का शिक्षण नहीं हो सकता। भारतीय परिवेश में संस्कृत विदेशी भाषा नहीं मानी जा सकती।
’ विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के माध्यम के रूप में भारतीय भाषा का अनिवार्य रूप से प्रयोग: प्रारम्भिक-शिक्षा से उच्च-स्तरीय शिक्षा तक भाषा संबंधी नीति एवं अधिनियम का निर्माण करना होगा।
(इस परिप्रेक्ष्य में संवैधानिक संशोधन (अनुच्छेद 351)
अनिवार्य है।)
’ भारतीय भाषाओं में उच्च-स्तर तक की शिक्षा-सामग्री-निर्माण संबंधी-नीति का निर्माण राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद्, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/परिषद्/संगठन जैसी संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों आदि के माध्यम से भारतीय भाषाओं में पाठ्य-सामग्री का निर्माण करना/करवाना। इस सन्दर्भ में सेवानिवृत्त अथवा संलग्न अनुभवी अध्यापकों को विशिष्ट प्रायोजनाएं दी जा सकती हैं। इसी संदर्भ में निजी प्रकाशकों, स्वयंसेवी संगठनों आदि को भी विशिष्ट सहायता एवं प्रोत्साहन दिया जा सकता है। विभिन्न वृहद् एवं सक्षम शिक्षा-संगठनों एवं समूहों के माध्यम से भी सामग्री का निर्माण कराया जा सकता है। इस प्रकार से निर्मित सामग्री के निर्माण एवं मूल्यांकन हेतु मानक विशेषज्ञों की समिति द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं।
’ शिक्षा-संस्थानों में भारतीय भाषाओं के शिक्षण-शास्त्र (ढीँिङ्मॅ८) के स्वरूप का निर्धारण की दृष्टि से विभिन्न प्रकार के विषय-संबद्ध-विशिष्ट-उद्देश्यों के परिप्रेक्ष्य में बहु-आयामी-पाठ्यचर्याओं, शिक्षण-विधियों, उपागमों, शिक्षण-सामग्री, शिक्षक-प्रशिक्षण, उद्देश्यनिष्ठ-मूल्यांकन आदि संबंधी शिक्षण-प्रशिक्षण एवं कार्यशालाओं का आयोजन किया जाना चाहिए।
’ संपूर्ण राष्ट्र में सम्पर्क -भाषा-नीति का व्यापक संदर्भों में निर्माण एवं अनुपालन हेतु कार्यान्वयन।
’ राष्ट्रीय एकत्व, सामरस्य, सामंजस्य, नूतन-ज्ञान-संबद्ध-शब्दावली-निर्माण एवं वैश्विक संबंधों के परिप्रेक्ष्य में संस्कृत के स्थान, स्वरूप एवं शिक्षण-नीति का निर्धारण।
’ भारत में अंग्रेजी एवं अन्य विदेशी भाषाओं का स्थान, स्वरूप एवं तुल्यता संबंधी नीति : इनका शिक्षण स्वेच्छा पर आश्रित होना चाहिए।
’ अंग्रेजी एवं अन्य विदेशी भाषाओं के शिक्षण आदि की पाठ्यचर्या एवं विधियों के स्थान एवं स्वरूप पर पुनर्विचार करना होगा।
’ भाषा-शिक्षण संबंधी भारतीय भाषिक सिद्धांतों से संबंद्ध शोधात्मक अध्ययनों एवं उनके कार्यान्वयन को नीतिगत ढंग से प्रोत्साहित करना चाहिए। एतदर्थ विश्वविद्यालयों में विषय-निर्धारण एवं प्रविधि संबंधी विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन किया जा सकता है।
’ पाठ्यचर्याओें के अन्तर्गत सन्दर्भसूचियों में भारतीय भाषाओं के माध्यम वाली पुस्तकों का उल्लेख अनिवार्य रूप से हो।
’ शिक्षक-शिक्षा के अन्तर्गत भारतीय भाषाओं के माध्यम से अध्यापन के अभ्यास की ओर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। इसलिए शिक्षण की सामग्री को भारतीय भाषाओं एवं संदर्भों में सज्जित करने के लिए कार्यशालाओं का गठन करके सज्जित किया जा सकता है।
’ इसी प्रकार उच्च स्तर पर भारतीय भाषाओं के माध्यम से अध्यापन हेतु विभिन्न प्रकार के अभ्यास क्रमों को तैयार कर के कार्यशालाओं का आयोजन किया जा सकता है। वर्तमान सन्दर्भों में इस प्रकार के कार्यक्रमों के लिए नूतन शिक्षण संसाधन एवं शिक्षण-सामग्री का निर्माण किया जा सकता है। प्रशिक्षण भी इसी प्रकार दिया जा सकता है। कुशल अध्यापकों का समूह निर्मित कर अध्यापक-पुस्तिकाओं का निर्माण करना भी अच्छा होगा।
’ आधुनिक तकनीकी के उपयोग द्वारा कार्य को गति दी जा सकती है।
उपर्युक्त कुछ प्रमुख सन्दर्भ हैं। परन्तु इनके लिए एक मानसिक धरातल तैयार करने एवं प्रतिबद्धता की अवश्यकता है। योजनाबद्ध एवं सोपानश: कार्य को सिद्ध किया जा सकता है।
(लेखक संस्कृत संवर्धन प्रतिष्ठान के शैक्षणिक निदेशक हैं)

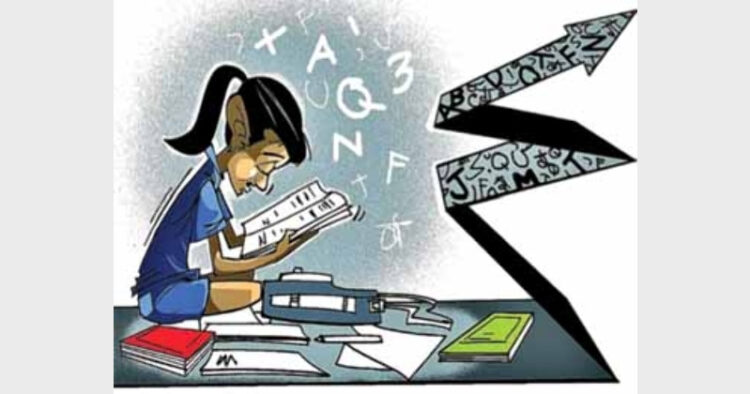









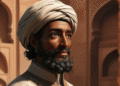
टिप्पणियाँ