|
-राजेन्द्र चड्ढा –
किसी संस्कृति विशेष के उत्थान-पतन विषयक उतार-चढ़ावों का जितना सफल अंकन लोक-साहित्य में होता है, उतना अन्यत्र नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी भी संस्कृति की धूल उसकी आत्मा से जुड़ी होती है। अब अगर देश की बात की जाए तो भारतीय संस्कृति जितनी अधिक प्राचीन है, उतनी ही अधिक विभिन्न संस्कृतियों के सम्मिलित स्वरूप की वाहक भी। विभिन्न संस्कृतियों ने समय-समय पर इस पर आघात पहुंचाने के प्रयत्न भी किए परंतु इसे नष्ट करने के बजाए वे स्वयं ही इसकी अंगभूत बन गईं। अत: प्रश्न उठता है कि वे कौन से तत्व हैं जो इसे विशिष्ट बनाए हुए हैं। आखिर जीवन भी एक प्रकार का सरित प्रवाह है।
भारत का नाम सिंधु नदी (हालांकि आज कम भारतीय ही इस तथ्य से वाकिफ हैं कि वह नदी नहीं, नद है और दूसरा नद ब्रह्मपुत्र है) के नाम पर पड़ा जो कि आज पाकिस्तान से होकर बहती है और जैसा कि सर्वविदित है कि पाकिस्तान 1947 में अंग्रेजों के औपनिवेशिक शासन के अंत के साथ हुए भारत-विभाजन के बाद अस्तित्व में आया। इस तरह भारतीय राष्ट्रवाद एक दुर्लभ घटना है।
भारतीय राष्ट्रवाद, एक विचार आधारित राष्ट्रवाद है जो कि एक सनातन भूमि का विचार है। इसकी उत्पत्ति एक प्राचीन सभ्यता से हुई, जिसे एक समान इतिहास ने एकता में पिरोया और एक बहुलवादी लोकतंत्र ने निरंतरता प्रदान की। भारत के भूगोल ने इसे संभव बनाया और उसके इतिहास ने इसकी पुष्टि की। दुनियाभर में भारत के सम्मान का एक बड़ा कारण यही है कि वह सभी प्रकार के दबावों और तनाव के बावजूद कायम रहा है (इकबाल के शब्दों में कहें तो कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा), जबकि कइयों (विस्टन चर्चिल जैसे) ने उसके अवश्यंभावी विघटन की भविष्यवाणी करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इस तरह भारत ने बिना एकमत हुए भी सहमति बनाते हुए अपने अस्तित्व को कायम रखा है।
हिंदी के प्रसिद्ध विचारक-निबंधकार विद्या निवास मिश्र कहा करते थे, ''मैं हिंदू धर्म को लोकशास्त्र कहता हूं तो मेरा अभिप्राय इतना ही है कि वह विचारक, भावक और भावित सबको मिलाकर है। लोक साहित्य की भावधारा श्रुति परंपरा के सहारे अगणित मोड़ लेती हुई आज भी अपने प्राचीन रूप में प्रवाहित है। इसका लिखित साहित्य पहले उपलब्ध नहीं था। ग्रामीण जनता की यह निधि अत्यंत ही भावपूर्ण है और यह प्रकीर्ण साहित्य अत्यधिक विस्तृत है। उसमें कृत्रिमता का अभाव है, अनुभूतियों का सहज स्पंदन है। लोकगीतों की मानसी गंगा की समता बंधनयुक्त शास्त्रीय राग-रागनियां नहीं कर सकती हैं।''
जनता का काव्य एवं जनता की परंपराएं लोकवार्ता शब्द द्वारा अभिहित होती हैं। हिंदी में इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डॉ. वासुदेवशरण अग्रवाल ने किया। उल्लेखनीय है कि वे भारतीयता के अन्वेषी थे। इसे उन्होंने लोक में खोजा और वेद में भी। लोके वेदे च आधार सूत्र ने उनकी मदद की। इस तरह से कहा जा सकता है कि उन्होंने भारत और भारतीयता को समझने की दृष्टि दी। लोक साहित्य मानव जाति की वह धरोहर है जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरित होती हुई निरंतर गतिमान होती हुई अक्षुण्ण बनी रहती है। लोक-साहित्य का रूपाकार अवश्य किसी देश या जाति की भौगोलिक सीमा में आबद्ध रहता है। पर उसकी आत्मा सार्वभौम और शाश्वत है, उसकी स्थिति और परिस्थिति, आशा-निराशा, कुंठा और विवशताएं एक सी हैं।
डॉ. अग्रवाल मानते हैं कि लोक साहित्य लोक जीवन का विधायक होने के कारण निजी महत्व रखता है, संस्कृति के उत्थान-पतन का जैसा वास्तविक चित्र लोक साहित्य में उपलब्ध होता है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। लोक साहित्य वस्तुत: संस्कृति के स्वरूप की स्थापना करने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। उदाहरण के लिए, कागज के नोट के प्रति लोक मानस की क्षोभ मिश्रित वेदना की यह अभिव्यक्ति समस्त परिवेश को सजीव रूप में प्रस्तुत करती हुई दिखाई देती है, यथा-'भाभी चल्यौ छेद को पईसा, जाय तू नार में लटकाय लीजो। तथा तू काहे को बनवाबेगी हमेल, रूपैया है गयो कागज को?' यह अनायास नहीं है कि वे जनपदीय-साहित्य और लोक-साहित्य को पर्यायवाची मानते हैं।
हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार निर्मल वर्मा 'कला का जोखिम' निंबध में कहते हैं कि किसी भी सार्थक संवाद के लिए हमें अनिवार्यत:, तीन सीढि़यां पार करनी पड़ती हैं-दुनिया को पहचानना, उस पहचान से अपने को जानना, उस जानने को दूसरे में परखना। इन तीनों सोपानों में मनुष्य का कर्म बराबर मौजूद रहता है।
उल्लेखनीय है कि इस लोक में मनुष्यों का समूह ही नहीं, सृष्टि के चर-अचर सभी सम्मिलित हैं, पशु-पक्षी, वृक्ष-नदी, पर्वत सब लोक हैं। जबकि पश्चिम में हिन्दू धर्म को प्रस्थापित करने वाले स्वामी विवेकानंद इसी बात को रेखांकित करते हुए कहते हैं कि जीवों में मनुष्य ही सवार्ेच्च जीव है और यह लोक ही सवार्ेच्च लोक है। हमारा ईश्वर भी मानव है और मानव भी ईश्वर है। हमारे लिए इस जगत को छोड़ और किसी जगत को जानने की संभावना नहीं है और मनुष्य ही इस जगत की सवार्ेच्च सीमा है।
शायद यही कारण है कि स्वामी विवेकानंद ने न केवल क्रांतिकारियों को प्रभावित किया, बल्कि उत्तरोत्तर काल के राष्ट्रवादियों और स्वतंत्रता सेनानियों को भी। रोमां रोलां बताते हैं कि बेलूर मठ की वाटिका में दिए एक व्याख्यान में महात्मा गांधी ने स्वीकार किया था कि विवेकानंद के अध्ययन और उनकी पुस्तकों ने उनकी देशभक्ति को बढ़ाया। इस प्रकार, भारत की आजादी के लिए गांधी जी के आंदोलन में विलीन होने वाले सभी क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन स्वामी जी की सिंह-गर्जना उठो, जागो के बाद ही शुरू हुए।
लोकवार्ता एक जीवित शास्त्र है। लोक का जितना जीवन है, उतना ही लोकवार्ता का विस्तार है। लोक में बसने वाला जन, जन की भूमि और भौतिक जीवन तथा जन की संस्कृति इन तीनों क्षेत्रों में लोक के पूरे ज्ञान का अन्तर्भाव होता है। लोकवार्ता का संबंध भी इन्हीं के साथ है। लोक वार्ता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग लोक साहित्य है। लोकगीत, लोक कथाएं, लोक गाथाएं, कथागीत, धर्म गाथाएं, लोक नाट्य, नौटंकी, रामलीला आदि लोक साहित्य के विषय हैं। लोक साहित्य, लोक मानस की सहज और स्वाभाविक अभिव्यक्ति है।
लोक साहित्य बहुधा अलिखित ही रहता है और अपनी मौखिक परंपरा द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आगे बढ़ता रहता है। इस साहित्य के रचयिता का नाम अज्ञात रहता है। लोक का प्राणी जो कुछ कहता-सुनता है, उसे समूह की वाणी बनाकर और समूह के साथ घुल-मिलकर ही कहता है। लोकभाषा के माध्यम से लोक चिंता की अकृत्रिम अभिव्यक्ति लोक साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है। महाभारत और रामायण इसके प्रबल प्रमाण हैं। राम और श्रीकृष्ण विषयक लोकगाथाएं लोक जीवन में प्रचलित थीं। 'दूसरे शब्दों में' निबंध में निर्मल वर्मा लिखते हैं, ''भारतीय संस्कृति की ये महान काव्य रचनाएं न तो ओल्ड टेस्टामेंट और कुरान की तरह निरी धर्म-पुस्तकें और आचार-संहिताएं हैं, न ग्रीक महाकाव्यों-ईिलयड और ओडिशी- की तरह 'सेक्युलर' साहित्यिक कृतियां हैं। वे दोनों हैं और दोनों में से एक भी नहीं हैं। वे मनुष्य को उसकी समग्रता में, उसके उदात्त और पाशविक, गौरवपूर्ण और घृणास्पद, उजले और गंदले- उसके समस्त पक्षों को अपने प्रवाह में समेटकर बहती हैं। कला में सौंदर्य का आस्वादन और सत्य की बीहड़ खोज कोई अलग-अलग अनुभूतियां न होकर एक अखंडित और विराट अनुभव का साक्ष्य बन जाती है।'' डॉ. वासुदेवशरण अग्रवाल के शब्दों में, संस्कृति मनुष्य के भूत, वर्तमान और भावी जीवन का सर्वांगपूर्ण प्रकार है। इसका मूर्तिमान रूप होता है। जीवन के नाना विधि रूपों का समुदाय ही संस्कृति है।
लोकगीतों और लोकनृत्यों में लोक संस्कार मुख्य होते हैं। लोकगीत और लोकनृत्य संस्कारवत् लोक जीवन से लिपटे होते हैं। लोकगीतों के संदर्भ में वेरियर एल्विन का कथन है कि इनका महत्व इसलिए नहीं है कि इनके संगीत, स्वरूप और विषय में जनता का वास्तविक जीवन प्रतिबिम्बित होता है, प्रत्युत इनमें मानव शास्त्र के अध्ययन हेतु प्रामाणिक एवं ठोस सामग्री हमें उपलब्ध होती है। काका कालेलकर के अनुसार, लोक साहित्य के अध्ययन से हम कृत्रिमता का कवच तोड़ सकेंगे और स्वाभाविकता की शुद्ध हवा में फिरने-डोलने की शक्ति प्राप्त कर सकेंगे।
लोक संस्कृति ऐसे संस्कारों को हमेशा सहेज कर रखती है। समन्वयात्मकता लोक संस्कृति की मुख्य विशेषता है। यही गुण लोक जीवन को जिन्दा रखता है। हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, लोक शब्द का अर्थ जनपद या ग्राम्य नहीं है, बल्कि नगरों और गांवों में फैली हुई वह समूची जनता है, जिनके व्यावहारिक ज्ञान का आधार पोथियां नहीं हैं। ये लोग नगर में परिष्कृत रुचि सम्पन्न तथा सुसंस्कृत समझे जाने वाले लोगों की अपेक्षा अधिक सरल और अकृत्रिम जीवन के अभ्यस्त होते हैं और परिष्कृत रुचि वाले लोगों की समूची विलासिता और सुकुमारता को जीवित रखने के लिए जो भी वस्तुएं आवश्यक होती हैं, उनको उत्पन्न करते हैं। जबकि देवेंद्र सत्यार्थी के शब्दों में, लोक साहित्य की छाप जिसके मन पर एक बार लग गई फिर कभी मिटाए नहीं मिटती। सच तो यह है कि लोक-मानस की सौंदर्यप्रियता कहीं स्मृति की करुणा बन गई है, तो कहीं आशा की उमंग या फिर कहीं स्नेह की पवित्र ज्वाला। भाषा कितनी भी अलग हो मानव की आवाज तो वही है।
इस दृष्टि से अगर हिंदी साहित्य, उसमें भी विशेष रूप से छायावादी काल का अवलोकन करें तो सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' का व्यक्तित्व अलग से नजर आता है जो कि स्वयं अपने जीवन से, अपने आचरण से लोक मंगल को चरितार्थ करते हैं। निराला इस बात को समझते थे कि लोक जीवन को केवल उसके भाव, दृश्य, व्यापार में ही नहीं लिया जा सकता। उसके लिए उसकी भाषा भी आवश्यक होती है।
रामदरश मिश्र 'छायावाद का रचनालोक' पुस्तक में निराला के इसी गुण को रेखांकित करते हुए लिखते हैं कि दो ऐसी बातें हैं जो इनमें विशेष रूप से उभरती हैं वे हैं-भाषा और भाव की सापेक्षिक लोकोन्मुखता तथा भक्ति की ओर विशेष झुकाव। आखिर निराला के गीत हों या कविता शास्त्र और लोक का यह संगम अद्भुत है। यह अनायास नहीं है कि हिन्दी का भक्तिकालीन संत साहित्य व्यावहारिक लोकसम्मत ज्ञान के आधार पर पुस्तकीय ज्ञान के धनी को ललकारते हुए कहता है,
तू कहता कागद की लेखी
मैं कहता आंखिन की देखी।
यह संगम-मंथन शब्द बड़ा रहस्यात्मक है। सीधे शब्दों में इसका अर्थ होता है मिलन। कुंभ के संगम-मंथन पर लिखे अपने निबंध में निर्मल वर्मा कहते हैं, ''मैं वहीं बैठ जाना चाहता था, भीगी रेत पर। असंख्य पदचिह्नों के बीच अपनी भाग्यरेखा को बांधता हुआ। पर यह असंभव था। मेरे आगे-पीछे अंतहीन यात्रियों की कतार थी। शताब्दियों से चलती हुई, थकी, उद्भ्रांत, मलिन, फिर भी सतत प्रवाहमान। पता नहीं, वे कहां जा रहे हैं, किस दिशा में, किस दिशा को खोज रहे हैं, एक शती से दूसरी शती की सीढियां चढ़ते हुए? कहां है वह कुंभ घट जिसे देवताओं ने यहीं कहीं बालू के भीतर दबा कर रखा था? न जाने कैसा स्वाद होगा उस सत्य का, अमृत की कुछ तलछटी बूंदों का, जिसकी तलाश में यह लंबी यातना भरी धूलधूसरित यात्रा शुरू हुई है। हजारों वषार्ें की लॉन्ग मार्च, तीर्थ अभियान, सूखे कंठ की अपार तृष्णा, जिसे इतिहासकार भारतीय संस्कृति कहते हैं!''
शायद यही कारण है कि स्वाधीन जिज्ञासा को भारतीयता की खोज का मूल उपकरण मानने वाले हिंदी कवि-संपादक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन 'अज्ञेय' ने माना है-''भावनाएं तभी फलती हैं जब उनसे लोक कल्याण का अंकुर फूटे।'' 'अज्ञेय रचना संसार, भागवत भूमि यात्रा' पुस्तक में अपनी इसी सोच के अनुरूप वे एक यक्ष प्रश्न पूछते हैं। क्या लोक संस्कृति की जो परंपरा ब्रज और द्वारका को जोड़ती है, उसके साक्ष्य का महत्व हमारे लिए उस तथाकथित ऐतिहासिक साक्ष्य से अधिक नहीं होगा जो कुछ ठीकरों, मृद्भाण्डों और कुछ खंडित मूर्तियों या मंदिरों के अवशेषों पर अपने को खड़ा करता है? लोक परम्परा का साक्ष्य जीवन्त और सातत्य-युक्त साक्ष्य है, ऐतिहासिक साक्ष्य मरा हुआ और विखण्डित साक्ष्य। इससे क्या कि लोक परम्परा रूपकाश्रयी चिंतन का सहारा लेती है और इतिहास अपनी छानबीन को वैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित बताता है? रूपकाश्रयी चिंतन भी तथ्य तक पहुंचने का एक दूसरा रास्ता है, उससे मिलने वाला ज्ञान भी ज्ञान है, यद्यपि विज्ञान के उद्दिष्ट से भिन्न कोटि का ज्ञान। फिर अज्ञेय ठीक दुखती नाभि पर अंगुली रखकर कहते हैं-पौराणिक चिंतन या रूपकाश्रयी चिंतन शायद वैज्ञानिक चिंतन यानी लॉजिकल चिंतन का समानांतर और पूरक हो सकता है। जहां वैज्ञानिक प्रक्रिया का नकार निगति का कारण बनता है, क्योंकि वहीं परिवर्तनशीलता और विकास की गति को नकारता है, वहीं मिथकीय पद्धति का नकार भी निगति का कारण बनता है, क्योंकि उसकी परिणति कल्पना और संवेदना की मृत्यु में होती है-मनुष्य यंत्र में बदल जाता है। यह यंत्र में बदलता मनुष्य ही चिंता का कारण है।
उनके शब्दों में भारत तथा यूरोप में धर्म चिंतन एक सा नहीं है, क्योंकि हमारा धर्म तो संस्कृति-दर्शन मिथक परंपरा आदि की सभी धुरियों में भिदा हुआ है। उसे संस्कृति से जुदा नहीं किया जा सकता। जुदा करते ही धर्म-धर्म नहीं रहता, और कुछ हो जाता है, जिसे संप्रदाय कहा जाता है। धर्म-संस्कृति के बृहत्तर अर्थ-संदभार्ें पर अज्ञेय की टिप्पणी है, भारत में धर्म न केवल सांस्कृतिक आधार है, बल्कि जिसे आधुनिक अर्थ में संस्कृति कहा जाता है, वह धर्म के अनुष्ठान पक्ष का एक विस्तार ही रही है। अज्ञेय समाज के साथ हैं, समाज में व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में जो खाई है उसे वे सेतु से पाट देना चाहते हैं।
लोक विभाजन नहीं जानता, समाहार जानता है, संकीर्णता नहीं जानता, व्याप्ति जानता है। यह अनायास नहीं है कि स्वांत: सुखाय रचना करने वाले 'रामचरितमानस' के रचयिता आचार्य तुलसीदास समाज में रामराज के माध्यम से लोक मंगल और मर्यादा की स्थापना ही करना चाहते थे। 'संसार में निर्मल' पुस्तक निर्मल वर्मा कहते हैं कि अगर हम भारतीय और हिंदू प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या ईसाई और मुस्लिम प्रतीकों का इस्तेमाल करेंगे? ये प्रतीक तो सहज रूप से हमारे रक्त में प्रवाहित होते हैं! जब हम यूरोप का साहित्य पढ़ते हैं तो उनमें बाइबल और यूनानी पौराणिक ग्रंथों से लिए गए रूपक और प्रतीक मिलते हैं। हम उन्हें स्वीकार करते हैं। नस्लीय दृष्टि से हम क्या उसे देख पाएंगे? आज हम निराला का तुलसीदास या राम की शक्ति पूजा पढ़ते हैं, तो क्या यह कहेंगे कि यह हिन्दूवादी कविता है? क्या हम उसे साम्प्रदायिक कविता कहकर खारिज कर सकते हैं? मैं समझता हूं ऐसी बातें करना हमारी आलोचनात्मक विपन्नता का प्रतीक है।
याद करें तो यही लड़ाई महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ ठाकुर और कला के मोर्चे पर आनंद कुमार स्वामी ने लड़ी थी। धर्म के मोर्चे पर इसे विवेकानंद ने लड़ा था। ये वे स्वदेशी लड़ाइयां थीं, साम्राज्यवादी आधुनिकता जिन्हें आज भी उखाड़ फेंकना चाहती है। मैकाले के वंशजों की विपुल तादाद के बीच इन ठिकानों पर खड़े होना और लड़ना जिन कुछेक के लिए दीवानगी से कुछ कम नहीं था। भवानी प्रसाद मिश्र ने इसी बात को अपनी कविता में इस तरह कहा है,
यह कि तेरी भर न हो तो कह
और सादे ढंग से बहते बने तो बह
जिस तरह हम बोलते हैं, उस तरह तू लिख
और इसके बाद भी, हमसे बड़ा तू दिख।
हाल के भूमंडलीकरण ने अनेक भारतीयों के मन में यह आशंका पैदा की जो कि निर्मूल साबित हुई कि आर्थिक उदारीकरण अपने साथ एक तरह का सांस्कृतिक साम्राज्यवाद-कि बे वाच और बर्गर भरतनाट्यम और भेलपूरी को बेदखल कर देंगे-लाएगा। जबकि हाल में ही पश्चिमी उपभोक्तावादी उत्पादों के साथ भारत का अनुभव बताता है कि हम बिना कोक के गुलाम हुए कोका कोला पी सकते हैं। अगर महात्मा गांधी के शब्दों में कहें तो हम अपने देश के दरवाजे और खिड़कियों को खोलने और विदेशी हवा के हमारे घरों में बहने के बावजूद किसी भी तरह से कमतर भारतीय नहीं होंगे क्योंकि भारतीय इतने सक्षम हैं कि इन हवाओं से उनके पैर नहीं उखड़ेंगे। हमारी लोकप्रिय संस्कृति एमटीवी और मैकडानल्ड का सफलतापूर्वक सामना करने में सक्षम सिद्ध हुई है। साथ ही भारतीयता की वास्तविक शक्ति विदेशी प्रभावों को समाहित करने और उसे भारतीय हवा, पानी और मिट्टी के अनुकूल परिवर्तित करने में निहित है। (लेखक प्रज्ञा प्रवाह केे राष्ट्रीय सह संयोजक है)

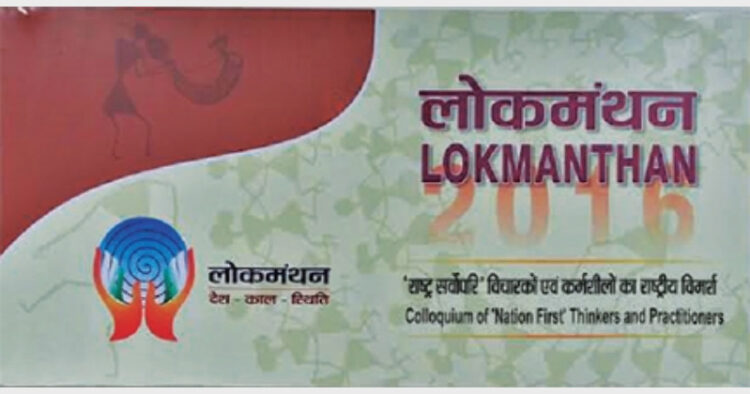



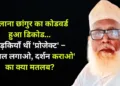



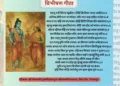
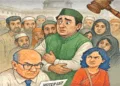

टिप्पणियाँ