|
जान को जोखिम में नहीं डाल सकते तो समस्या से कभी नहीं लड़ सकते। बीचमें एक समय ऐसा आ गया था कि मुठभेड़ हो या न हो, कोई मरना नहीं चाहिए। यह कैसे संभव है, यदि पहले ही से यह तय हो जाएगा तो फिर लड़ा कैसे जाएगा?
प्रकाश सिंह
सवाल है कि हम माओवादी समस्या का कैसे सामना करें? इसमें केन्द्र और राज्यों का समन्वय काफी अहम है। इसके अभाव में या यूं कहिए जितना समन्वय होना चाहिए वह देखने को नहीं मिलता है। इस कारण यह समस्या और ज्यादा बढ़ती जा रही है। माओवादी समस्या से निपटने के लिए अभी तक कोई राष्ट्रीय नीति नहीं बनाई गई है। ऐसा क्यों हुआ, यह नहीं मालूम। यह समस्या सबसे पहले 1971 में शुरू हुई थी। यदि तब से देखें तो 45 वर्ष तो हो ही चुके हैं। इतना समय पर्याप्त था देश में माओवादी समस्या को दूर करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई नीति बन जानी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो सका। करीब दो वर्ष पहले मैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार समिति का सदस्य था। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मैंने पूछा था कि माओवाद से लड़ने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई नीति क्यों नहीं बनाई गई? प्रधानमंत्री ने तभी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को इस संबंध में कार्रवाई के लिए कहा, लेकिन उस पर ठंडा पानी डाल दिया गया। फिर कुछ समय बाद मेरा कार्यकाल समाप्त हो गया।
नीति इसलिए आवश्यक है क्योंकि हर सरकार के कार्य का तरीका अलग-अलग होता है। हर सरकार की समस्या से निपटने की अलग शैली होती है। गृहमंत्री के रूप में शिवराज पाटील आए तो और वनवासियों को भाई-बहन बताया और माओवादी अपनी शक्ति को बढ़ाते रहे। इसी तरह शिंदे साहब आए। उनकी क्या नीति रही, यह पता नहीं लगा और उनका कार्यकाल भी बीत गया। चिदम्बरम जी आए तो उन्होंने कोई नीति तो नहीं बनाई, लेकिन तीन शब्द बहुत बार कहे- 'क्लिअर, होल्ड एंड डेवलप'। इन तीन शब्दों का अर्थ काफी महत्वपूर्ण था। किसी क्षेत्र को पहले माओवादियों से साफ कर दिया जाए, फिर वहां प्रशासन मजबूती से काबिज हो और फिर विकास किया जाए, आर्थिक प्रगति की जाए। इसकी शुरुआत करते हुए उन्होंने बड़े पैमाने पर सुरक्षाबलों को माओवादी क्षेत्रों में भेजा। दुर्भाग्य से कुछ समय तक तो स्थिति ठीक चलती रही, लेकिन कुछ समय बाद लगा कि कोई चिदम्बरम साहब को पीछे से खींच रहा है। एक बार गृहसचिव श्री पिल्लै से मिलना हुआ तो उनसे मैंने पूछा कि आखिर मामला क्या है, शुरू तो डंके की चोट पर हुआ और अब इतना ढीला क्यों हो रहा है। वे कहने लगे कि 'कभी मेरे दफ्तर, आओ,' मैं उनके दफ्तर तो नहीं गया, लेकिन उनकी बात से लगा कि कुछ अंदर ही अंदर खिंचाव हो रहा था। किसी ने यह कहा या मुझे लगा कि यदि चिदम्बरम साहब इस योजना में सफल हो गए तो कहीं प्रधानमंत्री पद के दावेदार न हो जाएं, जबकि दावेदार तो हमारे राजकुमार हैं। कुछ लोगों ने सोनिया गांधी को भी कहा कि कार्रवाई से कहीं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से वोट बैंक कांग्रेस के हाथ से न निकल जाए। उसके बाद से कोई योजना अभी तक नहीं आई है, हो सकता है कि उसका खाका तैयार हो चुका हो। दुर्भाग्य से यहां पर जो चीजें फाइलों में दबी रह जाती हैं, वह दब ही जाती हैं। कभी हमें ही महत्वपूर्ण चीजें देखने को नहीं मिल पाती हैं। 'सभी की अपनी-अपनी डफली, अपने-अपने राग हैं।' हर मुख्यमंत्री का अपना दृष्टिकोण है, नीतीश बाबू ने पूछने पर कहा कि माओवादियों के साथ सख्ती कैसे हो सकती है, इस समस्या से जीतने का एकमात्र उपाय है कि आप इनका आर्थिक विकास कीजिए, उससे यह समस्या स्वत: समाप्त हो जाएगी। केन्द्र राज्यों में अभियान के लिए अपना सुरक्षाबल भेजता है और राज्य अभियान चलाते नहीं हैं। ममता बनर्जी ने सत्ता में आने पर माओवादियों को अपना साथी कहा, धीरे-धीरे जब तृणमूल और माओवादियों में टकराव होने लगा तो उन्होंने सुरक्षाबलों को ढील दी कि जाकर माओवादियों को मार गिराओ। उन्होंने पुलिस, सुरक्षाबल और गुप्तचर विभाग को नक्सल का सफाया करने की पूरी छूट दी। उसी का असर है कि पश्चिम बंगाल से माओवादियों के पांव उखड़ गए। झारखंड में वर्तमान सरकार आने के बाद से स्थिति ठीक है। केन्द्र और राज्य सरकार में कोई मतभेद देखने को नहीं मिला, दोनांे में समन्वय है। इससे पहले शिबू सोरेन के रहने तक माओवादियों के प्रति ढुलमुल नीति थी। छत्तीसगढ़ सरकार से कभी भी समन्वय को लेकर दिक्कत नहीं रही, चाहे कोई भी सरकार रही हो। छत्तीसगढ़ में जो समस्याएं हैं, वे आंतरिक हैं। दरअसल मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने तो छूट दी हुई है, लेकिन प्रशासन मनमाना काम कर रहा है। नौकरशाही माओवाद को समाप्त करने में विश्वास नहीं रखती है। छत्तीसगढ़ मंे सुरक्षाबलों और राज्य में समन्वय का अभाव है। बीच में कुछ समय पूर्व पता लगा था कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के बीच समन्वय नहीं है।
मेरा मानना है कि अतिरिक्त बल न होने की बात कहकर पल्ला झाड़ा जाता है। आप में जब खतरे से लड़ने की शक्ति नहीं है, जान को जोखिम में नहीं डाल सकते तो समस्या से कभी नहीं लड़ सकते। बीच में एक समय ऐसा आ गया था कि केन्द्र की नीतियां भी उसके लिए जिम्मेदार थीं। ऊपर से हुक्म थे, मुठभेड़ हो या न हो, कोई मरना नहीं चाहिए। यह कैसे संभव है, यदि पहले ही से यह तय हो जाएगा तो फिर लड़ा कैसे जाएगा? मुठभेड़ के दौरान कोई न मारा जाए, ये आदेश थे और काफी समय तक चले। जहां तक सुरक्षाबल की संख्या का सवाल है तो वह पर्याप्त है, उसके सही इस्तेमाल की आवश्यकता है। नये हथियार आते रहते हैं और केन्द्र सरकार ने कभी इस क्षेत्र में कमी नहीं छोड़ी है।
आखिरी बिंदु है इंटेलीजेंस। केन्द्र का राज्य और राज्य का दूसरे राज्यों से सूचनाओं का आदान-प्रदान। एक बार पश्चिम बंगाल और झारखंड वाले एक-दूसरे पर सूचनाओं का आदान-प्रदान न करने का आरोप लगा रहे थे। इस दृष्टि से कई खामियां हैं। इंटेलीजेंस की यदि बात की जाए तो उसमें आंध्र प्रदेश की एसआईबी का काम काफी सराहनीय रहा है, एसआईबी न केवल अपनी, बल्कि दूसरे राज्यों और कई बार राष्ट्रीय स्तर की सूचनाएं रखती थी। दिल्ली तक उन्होंने अपनी सूचनाएं पहंुचाई हैं। हर प्रदेश अलग ढंग से लड़ रहा है। किसी का बल प्रयोग तो किसी का आर्थिक प्रगति का दृष्टिकोण है। यही कारण है कि यह समस्या एक गांव से शुरू होकर आज 180 जिलों में फैल चुकी है। कोई सरकार चुनाव को ध्यान में रखकर माओवादियों से दोस्ती निभाती है। कई मुख्यमंत्रियों पर आरोप लग चुके हैं कि वे माओवादी नेताओं को अपने पक्ष में मतदान के लिए बोलते हैं। आंध्रप्रदेश में जिला स्तर पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक स्वयं अपने स्तर पर योजनाएं बनाकर गांव-गांव में लोगों से संपर्क साधते थे। खुद पुलिस अधीक्षक गांव में बच्चों के लिए खेल-कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाते थे।
कई बार जिन परिवारों के बच्चे माओवादियों के संपर्क में आकर चले जाते थे, उनके परिवार के सदस्यों की पुलिस देखभाल करती थी। बीमार परिजनों के उपचार से लेकर उन्हें आर्थिक मदद मुहैया करवाई जाती थी। इसका असर यह हुआ कि माओवादियों का इस तरह की कार्यप्रणाली से हृदय परिवर्तन भी हुआ और यही वजह रही कि प्रशासन की चुस्ती के चलते आंध्र प्रदेश से माओवाद खत्म हो गया।
(लेखक बीएसएफ के महानिदेशक रहे हैं)



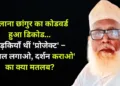



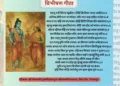
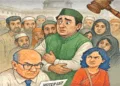



टिप्पणियाँ