|
सम्माननीय डॉ. मोहन भागवत जी
विजयादशमी के इस पावन दिन पर मैं आपको हृदय से शुभकामना प्रदान करता हूं। और आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे देश के सबसे बड़े राष्ट्रवादी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच यह उत्सव मनाने का अवसर दिया। विजयादशमी भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम की विजय का प्रतीक है। यह श्रीराम जैसे गुणी व्यक्ति की रावण जैसे बुराई के पर्याय असुर पर विजय है। इसलिए यह बुराई के ऊपर गुणों की और अच्छाई की विजय है। आज हमारा देश कई कठिनाइयों के दौर से गुजरकर विकासशील देश से विकसित देश की ओर संक्रमण की यात्रा में है। अब समय आ गया है कि हम सब इन कठिनाइयों से ऊपर उठने के लिए ठोस कदम उठाएं। और भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करें। लेकिन इससे पहले क्यों न हम वास्तविक रूप में इस लड़ाई से लोहा लेने की योजना का विश्लेषण करें। हमारे लिए यह जरूरी है कि हम अपने देश की ताकत और कमजोरियों को भली प्रकार से समझें।
वास्तव में इस देश की ख्याति स्वयं अपनी बनायी हुई है। वर्ष 2002 में भारत की एक विशेष छवि उभरकर विश्व पटल पर आई। 'अतुल्य भारत' अपनी उसी विशेषता के साथ विविधता में एकता 'जिसमें सभ्यताओं की समृद्ध विरासत है जो किसी भी पक्ष को अछूता नहीं रख सकी। यह तत्व भारतीयता या 'इण्डियानेस' का है। हां, यह भारतीयता ही है, जीवनमूल्य जो सनातन हैं और समय के साथ बदलते नहीं हैं। इसलिए इन्होंने ही इस महान देश को विशाल विविधताओं के बावजूद एक साथ रखा हुआ है। यह भारतीयता वैदिक, बौद्ध और इस्लामी सभी के लेखन में जीवन के दैनंदिन उपयोग के लिए एक अद्भुत विशेषता के रूप में निकली है। इसलिए इस तत्व को एक अनिश्चित, कालनिरपेक्ष और सार्वभौमिक उत्तराधिकार पूंजी के रूप में माना जाता है।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भारतीयता की अवधारणा की व्यापक व्याख्या की है, जिसका अर्थ संस्कृति से है जो पश्चिमी विचारों से जीवन को देखने के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करती। अपितु यह जीवन को अपने आप में पूरा और समग्र मानती है। उनके अनुसार भारतीयता अपनी व्याख्या केवल संस्कृति से नहीं अपितु राजनीति से भी स्वयं कर सकती है। भारत पूरे विश्व को सांस्कृतिक समभाव के साथ समर्पित जीवन के कर्तव्य का भी बोध कराता है।
हमारे राष्ट्र के निर्माण के लिए आवश्यक है गरीब से गरीब व्यक्ति को शक्तिशाली बनाने का संकल्प। उसे रोजगार, विकास और प्रभावी बुनियादी सेवाओं में सहभागी बनाना है।
गरीबी से सशक्तिकरण की ओर
भारत का मानव विकास सूचकांक बताता है कि जीवन की गुणवत्ता और सामान्य सेवाओं की उपलब्धता पर और अधिक ध्यान देने की जरूरत है।
* 680 करोड़ भारतीय अपनी अनिवार्य जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते।
* बुनियादी सेवाओं पर खर्च हुआ 50 प्रतिशत सार्वजनिक व्यय लोगों तक नहीं पहुंच पाता।
* बुनियादी सेवाओं का 46 प्रतिशत औसत परिवारों तक नहीं पहुंच पाता।
* आर्थिक प्राप्ति का तीन चौथाई नौकरियों और उत्पादकता वृद्धि से प्राप्त होता है।
* 2022 तक 580 करोड़ लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सकता है।
* अगले दशक तक 115 करोड़ अतिरिक्त गैर कृषि रोजगार की आवश्यकता पड़ेगी।
* अगले दशक तक कृषि फसलों में 70 प्रतिशत से अधिक की आवश्यकता पड़ेगी।
* स्वास्थ्य सुविधाओं, पानी और सफाई के लिए आज के 20 प्रतिशत की तुलना में सार्वजनिक और सामाजिक व्यय का 50 प्रतिशत करने की आवश्यकता पड़ेगी। आय की माप के लिए नये और अधिक तर्कसंगत मानकों की आवश्यकता पड़ेगी। एक परिवार के लिए अपनी आठ बुनियादी आवश्यकताओं- भोजन, ऊर्जा, आवास, पेयजल, सफाई, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए न्यूनतम आर्थिक लागत की जरूरत होती है। एक न्यूनतम स्वीकृत जीवन स्तर के लिए आठ बुनियादी सेवाओं में योगदान इस प्रकार हो सकता है-
स्वच्छ रसोई, ईंधन और बिजली की न्यूनतम ऊर्जा, जो न्यूनतम उपभोग स्तर पर आधारित है, उस पर जोर।
* 215 वर्ग फुट ग्रामीण और 275 वर्ग फुट शहरी क्षेत्र के लिए आवास की स्वीकृति
* 70 लीटर ग्रामीण अथवा 135 लीटर शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन पाइप लाइन से जल की आपूर्ति।
* ग्रामीणों के लिए स्वच्छ शौचालय और भूमिगत सीवर व्यवस्था के साथ शहरी क्षेत्रों में शोधित जल संचयन की व्यवस्था
* प्रत्येक स्तर पर अनिवार्य स्वास्थ्य सेवा पर जोर
* सभी बच्चों के लिए स्वीकृत मानकों पर आधारित प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर जोर (विकल्प के तौर पर प्राविधिक प्रशिक्षण)
* 2 फीसद प्रीमियम पर आधारित आय क्षति को जीवन बीमा से निपटाना
* अधिकृत गरीबी रेखा से उपभोग के स्तर को ऊंचा करने के प्रयत्न
क्योंकि हमारी ज्यादातर जनसंख्या गांव में निवास करती है और उसका जीवनयापन कृषि पर आधारित है, इसलिए हमें कृषि क्षेत्र को और अधिक सशक्त बनाने पर ध्यान देना होगा।
भारत की खेती : भविष्य की फसल
लगभग 300 करोड़ ग्रामीण भारतीय गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। यहां साक्षरता मात्र 46 प्रतिशत है और पांच में से केवल एक व्यक्ति ही सफाई पर जोर देता है। भारतीयों में दो तिहाई लोग देश के दुर्गम स्थानों पर रहते हुए कृषि करते हैं और सकल घरेलू उत्पाद का कुल 14-15 प्रतिशत ही अर्थव्यवस्था के कृषि खाते में जाता है। भारतीयों के पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चे 42 फीसद बच्चे शारीरिक रूप से कमजोर हैं, जो कि विश्व में दूसरे स्थान पर हैं। क्या भारतीय कृषि एक विशेष प्रकार के भविष्य के निर्माण में सहायक होगी? जिसमें ग्रामीण नागरिक अधिकाधिक समृद्ध होंगे। इनके बच्चे अधिक से अधिक पुष्ट और प्रकृति की अर्थव्यवस्था और अधिक मजबूत होगी।
हां, यह संभव है
हम एक सफल भविष्य में विश्वास करते हैं क्योंकि विगत में भी सफलताएं देखी हैं। कम ढांचागत सुविधाओं, नीतियांे के बाधकों जैसे-अनाजों के भण्डारण और विपणन तथा जमीनों के कानून आदि की कई समस्याएं रहीं। भारतीय किसानों ने पूरे साहस के साथ परिस्थितियों का मुकाबला करते हुए अत्यधिक परिश्रम किया। आज भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है। हम प्रतिवर्ष 260 मिलियन टन कृषि उत्पादन कर केला, आम, पपीता, दूध, मसालों, वनस्पति तेलों और कई बीजों के उत्पादन में वैश्विक नेतृत्व कर रहे हैं।
भारत की बढ़ती जनसंख्या के साथ खाद्यान्न उपभोग भी प्रतिवर्ष 4 प्रतिशत बढ़ रहा है। ऐसे समय में भारत में उपभोक्ता उच्च गुणवत्ता युक्त सुरक्षित और स्वस्थ खाद्यान्न की मांग करेंगे।
ऐसी गतिमान अर्थव्यवस्था में जबकि वर्तमान शासन तंत्र में नीतियां भी पक्ष में हैं। यह भारतीय कृषि के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। यह सही समय है कि जब हम दूसरी हरित क्रांति करके भारतीय कृषि को वैश्विक कृषि की एक बड़ी ताकत बना सकते हैं। 2030 तक हम 620 बिलियन कृषि की उपलब्धता पा लेंगे और ग्रामीण नागरिक को भी एक सम्मानजनक आय उपलब्ध करा सकेंगे।
क्या किया जाना चाहिए
बीज और खेती के तरीकों समेत कृषि तकनीकों को सुधारने की जरूरत है। अलग-अलग क्षेत्रीय जलवायु के हिसाब से उपयुक्त बीज उपलब्ध कराये जाने चाहिए। किसानों को इन सभी को अपनाने के लिए शिक्षित किया जाना चाहिए। आधुनिक सिंचाई के तंत्र को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। वर्षा जल संचयन के माध्यम से सिंचाई होनी चाहिए। फसल उत्पादन के बाद के प्रबंधन को सुधारते हुए फसल की बर्बादी को बचाया जाये।
– मिट्टी और पानी के रखरखाव को प्राथमिकता
– भारत को अपने आधारभूत ज्ञान को बेहतर बनाने की आवश्यकता है।
-मिट्टी के प्रकारों और जल उपलब्धता का राष्ट्रीय मानचित्र बनाया जाना चाहिए।
-विभिन्न भू-उपयोग गतिविधियों एवं जल परियोजनाओं को नियंत्रित करने के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) का प्रयोग हो।
-फसलों पर शोध हो ताकि मिट्टी की गुणवत्ता बढ़े और भूमि का क्षरण कम किया जा सके।
-मिट्टी, खाद, उर्वरक, बीज और पानी की जांच के लिए प्रयोगशाला बनाई जायें।
-किसान-उत्पादक संगठन (एफपीओ) के साथ क्षेत्रीय स्तर पर कंपनियों और समूहों के गठन को बढ़ावा मिले।
-कृषि उत्पादों की विपणन व्यवस्था को मुक्त कर दिया जाये।
-किसानों को अपना उत्पाद सीधे बाजार में बेचने की अनुमति हो।
-किसानों को शोषण से बचाने के लिए उत्पाद मूल्यों को सूचना तकनीक के माध्यम से एकीकृत किया जाये।
-निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाये।
-केन्द्र और राज्य सरकारांे को कृषि व्यवसाय के लिए वित्त निवेश हेतु, अंश उपलब्ध कराना चाहिए। दोनों को 50-50 फीसद का सहयोग करना चाहिए।
-70 वर्ष पूर्व महात्मा गांधी ने घोषित किया था कि भारत गांव के रूप में प्रारंभ हुआ था और गांव के रूप में ही समाप्त होगा। आइये, हम उनके सपने को साकार करें।
सच्ची शिक्षा
हमारी वर्तमान शिक्षा पाश्चात्य आदर्शों-आधुनिक विज्ञान के मिथक और तकनीक की ओर बढ़ रही है। हमारे प्राचीन वैज्ञानिक और दार्शनिक इसमें पूरी तरह उपेक्षित कर दिये गये हैं। गुरुत्वाकर्षण, गति के नियम, शून्य, अनंत, प्लास्टिक सर्जरी आदि की खोजों में कहीं भी हमारी वैज्ञानिक पुस्तकों का उल्लेख नहीं है, जबकि ये सब चीजें हमारे भारतीय वैज्ञानिकों और दार्शनिकों द्वारा पश्चिमी दुनिया से कई वर्ष पूर्व प्रवर्तित कर दी गई थीं। हमें अपनी स्वतंत्रता और सच्चाई के साथ शिक्षा को बढ़ाने की आवश्यकता है। सच्ची शिक्षा का वास्तविक अर्थ यही है कि जीवन अनुभवों से परिपूर्ण हो, केवल औपचारिक शिक्षा ही नहीं, बल्कि एक ऐसा प्रशिक्षण भी जो बहुआयामी व्यक्तित्व सामने लेकर आए। शिक्षा का अर्थ कहीं भी सीमित या आंकने मात्र से नहीं है, बल्कि वास्तविक जीवन की स्थितियों से बाहर निकालने के उपाय बताने से है। शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास ही होना चाहिए। सच्ची शिक्षा चेतना लाती है। चेतना से ही क्रांति आती है और क्रांति से ही परिवर्तन होता है और परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। नियम आचरण की संहिता है। इसलिए सचेतना के बिना शिक्षा का कोई अर्थ नहीं है। शिक्षा आजीवन जारी रहने वाली प्रक्रिया है। हम जब तक जीते हैं, तब तक सीखते रहते हैं। हम सीखने के लिए जीते हैं, लेकिन हमें जीने के लिए सीखना होगा। भारत की परम्परागत बुद्धिमत्ता जीवन से अलग होने की शिक्षा नहीं देती।
स्वामी विवेकानंद ने कई वर्षों पूर्व यह चेतावनी दे दी थी कि केवल राजनीतिक ताकत प्राप्त करने का कोई महत्व नहीं है, जब तक भारत की समूची जनता बहुत अच्छी तरह शिक्षित नहीं हो जाती, बहुत अच्छा भोजन प्राप्त नहीं करती, स्वास्थ्य-सुविधाएं उपलब्ध नहीं करती है। उसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए श्रेष्ठ शिक्षा की आवश्यकता है।
सच्ची शिक्षा और आत्म नियंत्रण के अभाव में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। भ्रष्टाचार धन, सत्ता, पद और भौतिक लाभ की प्राप्ति के लिए किया जाता है जिससे नैतिक मूल्यों का पतन होता है।
सच्ची शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति और भ्रष्टाचार के निर्मूलन के लिए एक मजबूत इच्छाशक्ति दिखानी होगी। भ्रष्टाचार युक्त समाज एवं मनुष्य में इन्हें चरित्र निर्माण के लिए वर्षों पुरानी जीवन मूल्यों वाली वैदिक परंपरा से सीख लेने की जरूरत है। इन मूल्यों में आचार, विचार, आहार और व्यवहार शामिल हैं। जब व्यक्ति को चेतनायुक्त मानवीय और संवेदनापूर्ण शिक्षा प्राप्त होगी तभी एक व्यक्ति समाज जीवन के मुद्दों को जड़ से समझने में समर्थ हो सकेगा। तभी वह भाई-भतीजावाद, सत्ता लिप्सा और कालाबाजारी जैसी समस्याओं से निपट सकेगा।
सबके स्वास्थ्य की चिंता
विश्वभर के लोग आज चेन्नई, मुंबई और दिल्ली में शीर्ष अस्पतालों में अलग-अलग रोगों के इलाज के लिए पहुंचते हैं। सैकड़ों-हजारों मेडिकल पर्यटक यहां आते हैं। प्रतिवर्ष प्रतिभा के साथ कम लागत वाली अस्पताल का आभार व्यक्त करते हैं। वे हमारे नवदक्षता युक्त चिकित्सकों की जिस प्रकार का प्रभावी और समर्थ उपचार विदेशी प्राप्त करते हैं क्या सभी भारतीयों को यह प्राप्त नहीं हो सकता।
शिशु मृत्युदर
भारत में शिशु मृत्यु दर एक हजार में से प्रति 44 शिशु है। यह दर चीन से तिगुनी पर, श्रीलंका और थाईलैंड से चौगुनी है। और तो और यह बंगलादेश और नेपाल से भी अधिक है। 5 वर्ष से कम आयु के 42 प्रतिशत भारतीय बच्चे कुपोषण का शिकार होते हैं। भारत में चेचक और टीबी से मरने वाले बच्चों के मामले में तीसरे स्थान पर आता है। हमारे यहां स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यशक्ति की संख्या में कमी है और शहरों में कार्य करने की मानसिकता के कारण चिकित्सकों वितरण भी सही नहीं है। विशेषज्ञ चिकित्सकों के साथ-साथ प्राथमिक चिकित्सकों, नर्सों, संबद्ध स्वास्थ्य कर्मियों तकनीशियन और पैरामेडिक्स तथा समुदाय सेवा कार्यकर्ताओं की भी कमी है।
भारतीय स्वास्थ्य तंत्र
भारत में परंपरागत रूप से स्वास्थ्य सेवाएं सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा ही संचालित होती थीं। लेकिन 1980 के बाद से निजी क्षेत्र के प्रवेश से यह और सशक्त हो गया है। कमजोर निगरानी तंत्र के कारण गुणवत्ता या लागत नियंत्रण सही ढंग से नहीं हो पाया। आज गांवों में कई अपेक्षा से कम योग्य लोग चिकित्सा अभ्यास में लगे हैं तो शहरों में अनेकों कार्पोरेट अस्पताल खुल रहे हैं। 12वीं योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य क्षेत्र में कुछ विशेष कार्यक्रम शुरू किए गए जो इस प्रकार हैं-
* राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) जो 2005 में शुरू किया गया था, इसके माध्यम से कई राज्यों में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार पर जोर दिया गया।
* जननी सुरक्षा योजना के तहत गर्भवती महिलाओं के लिए नकद प्रोत्साहन प्रारंभ किया गया ताकि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली महिलाएं घर के बजाय मेडिकल सुविधाओं में बच्चे को जन्म दें।
* राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरबीएसवाई) एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम है जो असंगठित क्षेत्र और अन्य वंचित समूहों को बीमार होने पर अस्पतालों में सरकारी छूट प्रदान करते हैं।
वर्तमान केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में बदलकर सबके स्वास्थ्य की सुरक्षा का अभियान चलाया है।
ऑपरेशन आशा (एएसएचए) के तहत 30 हजार से अधिक टीबी के मरीजों का करोड़ों अतिरिक्त केस बनने से पूर्व ही निदान किया गया है।
स्मार्ट गांव
हाल के समय में भारत में बहुत अधिक शहरीकरण बढ़ा है। अगले 20 वर्षों में यह संभावना है कि प्रत्येक मिनट में 30 लोग गांव छोड़कर शहर की ओर आएंगे। इस दर पर देश को अगले दो दशकों में कम से कम 500 नये शहरों की जरूरत पड़ेगी। ऐसा आकलन किया जा रहा है कि 2050 तक भारत की कुल जनसंख्या का आधा हिस्सा शहरों में बस चुका होगा। लगभग 250-300 मिलियन से अधिक लोग शहरों में अपना डेरा जमा चुके होंगे। कई शहरों का आकार लगभग दो गुना हो जाएगा।
बिजली
विश्व में लगभग 1.4 बिलियन लोग ऐसे हैं जिनके पास बिजली नहीं है। भारत में लगभग 300 मिलियन लोग ऐसे होंगे।
पानी
भारत में शहरी परिवारों में केवल 74 प्रतिशत को पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध है। किसी भी भारतीय शहर में हफ्ते भर में एक दिन भी पूरे चौबीसों घंटे पाइप का पानी उपलब्ध नहीं है। प्रतिदिन औसत 4-5 घंटे ही आपूर्ति वाला जल उपलब्ध रहता है।
ढांचागत विकास
बेशक ढांचागत निवेश में बढ़ोत्तरी हो रही है। इसके बावजूद अगले पांच वर्षों में देश के संसाधनों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए और ढांचागत विकास को सुलभ कराने के लिए एक ट्रिलियन की आवश्यकता पड़ेगी।
परिवहन
वर्ष 2021 तक उम्मीद है कि भारत में निजी वाहनों की संख्या वर्तमान समय से तिगुनी बढ़ जाएगी।
वैश्चिक ताप
यह संभावना है कि 2020 तक भारत अमरीका और चीन के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा कार्बन डाइआक्साइड प्रयोक्ता देश बन जाएगा।
शहरीकरण और सकल घरेलू उत्पाद
सकल घरेलू उत्पाद में शहरी क्षेत्र सबसे बड़े हिस्से का योगदान देता है। आज शहरों में रहने वाली भारत की 21 प्रतिशत जनसंख्या देश के सकल घरेलू उत्पाद में 60 प्रतिशत से अधिक की योगदान करती है। यह अनुमान लगाया गया है कि अगले 15 वर्षों में राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में शहरी भारत 75 प्रतिशत का योगदान देगा।
गांव से शहर की ओर लोगों का पलायन मुख्य रूप से रोजगार, आर्थिक गतिविधियों और बेहतर जीवन जीने की आकांक्षा के कारण बढ़ रहा है। मेरे विचार में शहरीकरण का मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि गांव के लोग शहरी क्षेत्रों में आएं और निराशा, बेराजगारी का जीवन जीयें और पहले से ही अपर्याप्त ढांचागत विकास से संकटग्रस्त शहरों पर और अधिक बोझ डालें। मेरा विचार है कि अच्छा तरीका यह होता कि शहर की सुविधाओं की तरह ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सुविधाएं दी जाएं। स्वर्गीय डॉक्टर कलाम ने पीयूआरए के तहत ऐसी ही योजनाओं का सुझाव दिया था और बहुत पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भी एक एकीकृत ग्राम की अवधारणा दी थी जिसमें स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता हो। ऐसे सभी मूलभूत सुविधाएं जो जनसंख्या को सशक्त बनाएं- भोजन, ऊर्जा, आवास, पेयजल, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा। ये सभी सुविधाएं गांव में हों और इनके साथ संचार और ई-मोबाइल सुविधा उपलब्ध होंगी तो गांव शहर से भी समृद्ध और आत्मनिर्भर हो जाएंगे। ऐसे स्मार्ट गांव में जब रोजगार होगा, नवीनतम सेवाएं और पर्यावरणीय सुरक्षा के साथ सुधार होगा तो नागरिक उनका बखूबी उपयोग करेंगे।
सतत् विकास
20वीं सदी चली गई और 21वीं सदी चल रही है। 20वीं सदी के आदमी की कमजोरी यह थी कि वह भावी पीढ़ी के हितों की अनदेखी कर केवल अपनी वर्तमान पीढ़ी पर विशेष ध्यान देते थे।
वर्तमान विश्व को बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास दोनों के ही संतुलन की आवश्यकता है। केवल आध्यात्मिक विकास से ही विकास की अवधारणा संतुलित हो सकेगी।
विकास के पांच आयाम हैं।
* विकास किसी व्यक्त्ि विशेष को किस तरह प्रभावित कर सकता है।
* यह समाज को किस प्रकार प्रभावित करता है।
* यह जीवन के विविध रूपों पर कैसे प्रभाव डालता है?
* यह पर्यावरण को कैसे प्रभावित करता है?
* यह दुनिया को कैसे प्रभावित करता है।
संतुलित विकास को मजबूत बनाने के लिए पांच आयामों पर जोर देना पड़ेगा-
भौतिकवादी, आर्थिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक। वर्तमान समय में सतत् विकास के लिए आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक इन तीनों को स्तंभ मानकर चला जाता है।
ऐसे पारिस्थितिकी संतुलन के लिए उपभोग में कमी, हरित निर्माण को बढ़ावा, सातत्य के लिए शिक्षा, सांस्थानिक सातत्य और इसी प्रकार सातत्य नेतृत्व के माध्यम से सभी विकास कार्यक्रमों को एकीकृत किया जाए।
पांच ऐसे क्षेत्र हैं जहां तकनीशियन सकारात्मक योगदान दे सकते हैं, क्षेत्र हैं- ऊर्जा संरक्षण, गैर नवीकृत ऊर्जा कोयला एवं तेल के स्थान पर नवीकृत ऊर्जा सौर व पवन का प्रचलन बढ़ाना, कूड़े-कचरे को उपयोगी बनाना, तीन ई-इंजीनियरिंग, इकोलॉजी और अर्थव्यवस्था में सही संतुलन ढूंढना।
कुल मिलाकर प्रकृति के सौंदर्य के प्रति प्रेम दिखाते हुए हमें मानवीय लाभ के लिए उसके दोहन में आध्यात्मिक पहचान का भी ध्यान रखना होगा।
आध्यात्मिकता और सातत्य विकास की भूमिका कई शताब्दियों से आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय चिंताएं विकास के साथ चली आ रही हैं। परमात्मा ने केवल जैविक और प्राकृतिक दुनिया बनाई थी लेकिन मनुष्य ने अधुनातन तकनीक का दुरुपयोग करते हुए एक कृत्रिम दुनिया बना ली। मनुष्य इन दोनों ही दुनिया में प्रमुख कारक है। विश्व चेतना के अंतर्गत रचनात्मकता और समभाव एकता का तत्व आता है जब आंतरिक संप्रेषण असफल होते हैं तो विनाश की संभावना बढ़ती है।
विकास सार्थक तभी होगा जब मनुष्य की आवश्यकताओं को देखकर विकास योजना बनेंगी साथ ही प्रकृति का भी सम्मान बरकरार रख सकें। हम प्रत्येक स्तर पर सचेतन संप्रेषण करें और धन एवं सत्ता को अपने ऊपर हावी न होने दें। इस संप्रेषण का सरल तरीका है कि प्रकृति का सम्मान किया जाए और मनुष्य की केवल दोहन मात्र की आकांक्षा को भी मर्यादित किया जाए।








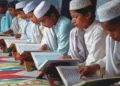



टिप्पणियाँ