|
इंडिया यानी इंग्लिश। भारत यानी क्षेत्रीय भाषा। इंडिया यानी शहर।भारत यानी गांव। इंडिया का मतलब पश्चिमी संस्कृति। भारत का मतलब भारतीय मूल्य। इंडिया अमीरों का तो भारत गरीबों और भोलेभाले लोगों का। नेता इंडिया के लेकिन उनका वोट बैंक भारत में। इंडिया ग्लोबल और मॉडर्न लेकिन भारत सामंतवादी। इंडिया उत्पीड़क तो भारत उत्पीड़न सहने वाला सही या गलत, इस 'टू नेशन थ्योरी' और 'रूरल-अरबन डिवाइड' पर बहस नई नहीं है लेकिन आज हम सिनेमा, खासकर हिंदी सिनेमा की दृष्टि से इसे देखेंगे।
सबसे पहले, बड़ा सवाल यह कि क्या आज वाकई हिंदी सिनेमा में दो भारत दिखते हैं? या क्या सिर्फ हमारी फिल्में इंडिया की प्रतिनिधि होकर रह गयी हैं? क्या फिल्मकारों के लिए भारत का अस्तित्व नगण्य है?
जवाब तलाशने के लिए हमें चंद साल पीछे जाना पड़ेगा। नब्बे के दशक के बीच में जब इस देश में मल्टीप्लेक्स कल्चर की शुरुआत हुई और अनिवासी भारतीय या एनआरआई हिंदी सिनेमा के बड़े अन्नदाता के तौर पर सामने आये। यह कालखंड इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने हिंदी सिनेमा के स्वरूप को बदल दिया और इसे 'भारत' से दूर कर 'इंडिया' के करीब ले आया। मल्टीप्लेक्स के प्रादुर्भाव के पहले और हिंदी सिने के अमीर दर्शक के तौर पर एनआरआई समुदाय के अभ्युदय के पहले, बॉलीवुड का बड़ा राजस्व छोटे शहरों और कस्बों के सिनेमा हॉल से आता था। मल्टीप्लेक्स के आने से पहले तक भारत भर में फैले करीब 12,000 सिनेमाहॉल, जिन्हें अब 'सिंगल स्क्रीन' थिएटर कहकर उपेक्षा भाव से देखा जाता है, हिन्दुस्तानी सिने दर्शकों के लिए मनोरंजन के एकमात्र विकल्प थे। इनमें से बड़ी संख्या उन सिनेमा हॉल की थी जो कस्बों और छोटे शहरों में फैले थे। गांवों और कस्बों में रहने वाले लोग हिंदी सिनेमा के बड़े दर्शक समुदाय थे। फिल्मकारों के लिए यह बड़ी चुनौती थी कि वे कैसे वैसी फिल्में बनायें जो इनके समेत देश के समस्त दर्शक समुदाय को पसंद आयें। अमिताभ बच्चन, धर्मेन्द्र, जीतेंद्र, रेखा, श्रीदेवी, विनोद खन्ना जैसे सितारों की फिल्में दिल्ली, मुम्बई समेत छोटे शहरों, कस्बों में समान रूप से लोकप्रिय थीं और कमाई करती थीं। किसी फिल्म की सुपर सफलता को तय करने के लिए इस्तेमाल होने वाले 'सिल्वर जुबली' और 'गोल्डन जुबली' जैसे अब खत्म हो चुके जुमले यदा-कदा सुनायी पड़ते थे।
नब्बे के दशक के उदारीकरण की पृष्ठभूमि में आये मल्टीप्लेक्स संस्कृति ने सब कुछ बदल दिया। हिंदी सिनेमा का वर्गीकरण या कहें बंटवारा हो गया। आज फिल्म इंडस्ट्री के धुरंधरों ने व्यापार के लिहाज से 'मल्टीप्लेक्स फिल्म' और 'सिंगल स्क्रीन फिल्म' को आपस में बंट दिया है। शहरी विषय और शहरी छवि वाले सितारों की फिल्में सिर्फ मल्टीप्लेक्स में लगती हैं। ग्रामीण या कस्बाई विषय या माहौल की फिल्में जिनमें वैसे अभिनेता होते हैं जिनकी गांव और कस्बों में प्रशंसक होते हैं, वे सिंगल स्क्रीन के सिनेमा हॉल में रिलीज की जाती हैं। हालांकि ऐसे एक्टर भी अब न के बराबर हैं और ऐसी फिल्मों के कथानक में भी अब शहरीकरण आ चुका है।
आज देश में करीब 12,000 सिनेमा हॉल हैं। इनमें करीब 10,000 सिंगल स्क्रीन या एक परदे वाले सिनेमा हॉल हैं जो मुख्य रूप से अब छोटे शहरों और कस्बों में ही सीमित रह गए हैं। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो देश में कुल सिंगल स्क्रीन 10,167 हैं। इनमें से करीब 70 प्रतिशत तो दक्षिण भारतीय राज्यों में ही हैं। यहां हम बात हिंदी सिनेमा की कर रहे हैं तो दक्षिण के सिनेमा पर नहीं जाते हैं क्योंकि वहां कई मामलों में स्थितियां हिंदी सिनेमा से भिन्न हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे बड़े शहरों समेत मझोले शहरों के भी कई सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल या तो बंद हो गए हैं या होने की कगार पर हैं। उनकी जगह मल्टीप्लेक्स ने ले ली है जिनमें 3 या ज्यादा स्क्रीन हैं। 1997 में देश में पहला मल्टीप्लेक्स खुला जिसमें 3 स्क्रीन या परदे थे। आज 17-18 साल बाद करीब 2050 मल्टीप्लेक्स स्क्रीन पूरे देश में हैं। 2014 की शुरुआत तक पीवीआर के पास 408 स्क्रीन, बिग सिनेमा के पास 254, आईनोक्स के पास 296, सिनेपोलिस के पास 100, केरल के कार्निवाल सिनेमा के पास 260 मल्टीप्लेक्स स्क्रीन थे। इनके अलावा देश में 15-16 क्षेत्रीय कंपनियां और कई स्वतंत्र व्यापारी मल्टीप्लेक्स चलते हैं। अब अगर यहां ंतुलना चीन या अमरीका से करें तो हम देखते हैं कि इस मामलें में हम उनसे बहुत पीछे हैं। मसलन, अमरीका में 40,000 मल्टीप्लेक्स स्क्रीन हैं तो चीन में 20,000 हैं. जबकि हमारे पास सिर्फ 2100 के करीब! हम हर साल 1000 फिल्में बनाते हैं और 400 करोड़ सिनेमा टिकट बेचते हैं लेकिन हमारी 10 लाख की आबादी के लिए सिर्फ 9 स्क्रीन हैं जबकि चीन में इतनी ही आबादी पर 25 सिनेमा स्क्रीन हैं।
हालांकि, पीवीआर और आइनोक्स अब उत्तर भारत के कई छोटे शहरों में मल्टीप्लेक्स लाने की योजना बना रहे हैं। और तो और, सलमान खान ने भी देश भर में, खासकर के छोटे शहरों में किसी बड़ी कंपनी के साथ मिलकर मल्टीप्लेक्स चैन खोलने की योजना बनाई है। मकसद है, इन शहरों में सिनेमा हॉल की कमी को पूरा करना और छोटे शहरों के लोगों को भी मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखने का मजा दिलवाना। तो सवाल यह है कि तो क्यों बंद हो रहे हैं सिंगल स्क्रीन या एक परदे वाले पुराने सिनेमा हॉल जिनमें 'भारत' फिल्में देखा करता रहा है? क्यों बढ़ रहे हैं मल्टीप्लेक्स जिनमें 'इंडिया' फिल्में देखता है? क्या इसकी वजह सिर्फ जमीन की बढ़ी कीमतें हैं? नहीं!
इस तथ्य के बावजूद कि अभी भी देश में सिंगल स्क्रीन वाले सिनेमा हॉल की संख्या मल्टीप्लेक्स के परदे से ज्यादा हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लिए मल्टीप्लेक्स ही क्यों माई बाप बन गए हैं? व्यापार के लिहाज से भी देखें तो आज अगर किसी फिल्म की टिकट बिक्री से होने वाली कमाई 100 रुपये है तो मल्टीप्लेक्स से होने वाली कमाई का प्रतिशत 80 रुपये से भी ज्यादा है। कहना न होगा कि मल्टीप्लेक्स के टिकट, सिंगल स्क्रीन के सिनेमा हॉल के टिकेट के मुकाबले महंगे भी होते हैं। तो जब करीब 2100 मल्टीप्लेक्स स्क्रीन ही फिल्म इंडस्ट्री के लिए 80 प्रतिशत कमाई कर रहे हैं तो सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल या उन हॉल में फिल्में देखने वाले सीमित संसाधनों वाले कम दर्शकों की परवाह क्यों क तो भारत बनाम इंडिया का ये एक व्यापारिक पक्ष है। इसे नजरअंदाज करना मुश्किल है क्योंकि व्यापारिक सोच तो यही कहती है कि हमें ऐसी फिल्में बनानी चाहिए जो मल्टीप्लेक्स में जाकर फिल्में देखने वाले देखें? हमें भारत को भूलकर इंडिया के लिए फिल्में बनानी चाहिए। तो जहां सिर्फ एंटरटेनमेंट ही एक मुद्दा है, उस कमर्शियल सिनेमा के लिए लाभ एकमात्र एजेंडा है।
लेकिन ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ कि सिंगल स्क्रीन वाले सिनेमा हॉल या उनमें फिल्में देखने वाले दर्शक अब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए उतनी बड़ी प्राथमिकता नहीं रहे? गांव और कस्बों में रहने वाले लोग जिन सिनेमा हॉल में फिल्में देखते हैं, उनकी पसंद या नापसंद अब के फिल्मकारों के लिए पहले जैसी महत्वपूर्ण क्यों नहीं रही? क्या इसका कारण सिर्फ व्यावसायिक है जिसकी चर्चा अभी हमने की?
एक प्रमुख थ्योरी यह है कि हिंदी सिनेमा के दर्शकों का स्टैण्डर्डाईजेशन या मानकीकरण हो गया है। देश भर के दर्शकों की सोच, उनकी आकांक्षाएं और उम्मीदें अब एक सी हो गयी हैं। इसलिए ये जो गांव और शहर की दूरी है, वह दूसरे मामलों (आर्थिक, सामाजिक) में सच हो सकती है, यह सिनेमा के लिए सच नहीं है। तर्क यह है कि मेरठ हो या बुलंदशहर, मनाली हो या मधेपुरा, पटना हो या पुणे, हर जगह लोगांे के एस्पिरेशन, उनकी महत्वाकांक्षाएं एक सी हो गयी हैं। सीमित आमदनी वाले एक श्रमिक को या दूसरे के घरों में काम करने वाली बाई को भी अब वह सब चाहिए जो उसके नियोक्ता (एम्प्लायर) के पास है।थोडा भी संसाधन हो तो वे अपने बच्चों को सरकारी हिंदी माध्यम के स्कूल के बजाय अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ने के सपने देखते हैं। खेतों में काम करने वाला किसान हो या दिहाड़ी मजदूर, मोबाइल और उसपर इन्टरनेट ने उसे बाकी दुनिया से जोड़ दिया है। भारत अब इंडिया से मिल गया है। भारत और इंडिया के सपने और उम्मीदें अब एक हो गयी हैं।
मोटे तौर पर कहें तो 1970 के दशक के सिनेमा में जो ग्रामीण और छोटे शहरों का पीडि़त, दमित समाज दिखता था, वह अब करण जौहर और फरहान अख्तर जैसे फिल्मकारों की देशी अनिवासी अमीर भारतीयों की गोवा, न्यूयार्क, लन्दन, पेरिस जैसे शहरों की चमक-दमक के पीछे गायब हो गया है। इन फिल्मकारों को हिंदी समाज और उसकी समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। रही सही कसर उन्होंने बॉलीवुड की नकल करके पूरी कर दी है जिसने बलीवुड में रूरल-अर्बन डिवाइड को और बड़ा कर दिया है।
लेकिन एक तर्क यह भी है कि यह जो रूरल-अरबन डिवाइड है, यह फिल्मों के दर्शकों में नहीं बचा है, यह फिल्मों के कथानक या विषय के चुनाव में जरूर दिख जाता है। यह डिवाइड शायद 10-15 साल पहले तक बचा था , जब कहा जाता था कि मिथुन चक्रवर्ती, सनी देओल या अजय देवगन सिंगल स्क्रीन के हीरो हैं क्योंकि उनकी फिल्में उन स्क्रीन पर ही ज्यादा चलती हैं और शहरों के सिनेमा हॉल में कम। अब वैसा भी नहीं है। आज अजय देवगन या सनी देओल की फिल्मों को भी अगर पैसे बनाने हैं तो उन्हें मल्टीप्लेक्स पर ही चलना होगा।
इस तर्क से आप सहमत हों या न हों, इससे इनकार करना मुश्किल है कि आज हिंदी सिनेमा में बाजार ही प्रभावी है। जो बिकता है वही दिखना चाहिए, आदर्श वाक्य है।तो प्रॉफिट कौन दे सकता है? जिसके पास पैसा है। पैसा शहरों में रहने वाले दर्शक खर्च कर सकते हैं। वे मल्टीप्लेक्स जाते हैं। वे शॉपिंग मॉल जाते हैं। बॉलीवुड उनके लिए फिल्में बनाता है। उनकी पसंद, नापसंद, अपेक्षाओं, उम्मीदों को ध्यान में रखकर एक काल्पनिक संसार रचता है। उसके लिए, दिल्ली में रहने वाला ठेले वाला, रिक्शा वाला महत्वपूर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि वह वर्ग मल्टीप्लेक्स की महंगी टिकट को खरीद नहीं सकता।
तो आज सिंगल स्क्रीन वाले सिनेमा हॉल में कैसी फिल्में लगती हैं? उन फिल्मों को कौन देखता है? लेकिन यहां हमें इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि कस्बों में सीमित रह चुके सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल में सिर्फ ग्रामीण या कस्बाई पृष्ठभूमि की कहानियों वाली फिल्में लगती हैं या पसंद की जाती हैं। आज बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल, पंजाब, राजस्थान, मध्यप्रदेश जैसे राज्यों में उनकी क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों के अलावा (अगर वे हैं तो) आमतौर पर बी या सी ग्रेड की वैसी हिंदी फिल्में लगती हैं जो न भारत की हैं और न ही इंडिया की। इन फिल्मों में दिखने वाले गांव या इलाके इस देश में कहां हैं, ये इन फिल्मों के बनाने वालों को भी नहीं पता। उनके पात्र जिस बोली में बोल रहे हैं, वह हिंदी है, अवधी या भोजपुरी या मगही, यह फिल्म का संवाद लेखक ही बता सकता है। सेक्स, मारधाड़ और घिसे-पिटे कथानक वाली इन फिल्मों को आप बॉलीवुड की बड़ी मसाला फिल्मों की खराब नकल कह सकते हैं जिनमें आमतौर पर ऐसे कलाकार काम करते हैं जिन्हें आमतौर पर मुख्यधारा की फिल्मों में नहीं देखा जाता। कम बजट की इन फिल्मों का बाजार सीमित होता है और दर्शक भी।
ऊपर हमने बात की उस तर्क की जिसके हिसाब से रूरल-अरबन डिवाइड अब फिल्मों के दर्शकों में नहीं बचा है लेकिन फिल्मों के कथानक या विषय के चुनाव में जरूर यदा-कदा दिख जाता है।
थीम या कहानी के लिहाज से फिल्मकारों या लेखकों का एक छोटा समूह है जो रूरल-अरबन डिवाइड या भारत-इंडिया डिवाइड को ध्यान में रख कर फिल्में बना रहा है या लिख रहा है। ये लोग बनारस, हजारीबाग, पटना, भोपाल या जमशेदपुर जैसे शहरों या छोटे कस्बों से आये हुए लोग हैं। इन्होने जमीनी सच्चाई देखी हैं और ये भारत की समस्याओं से भली-भांति वाकिफ हैं। हॉल की 'मसान' का उदाहरण लीजिये। या कुछ समय पहले की 'पीपली लाइव', या 'गैंग्स ऑफ वास्सेपुर' जैसी फिल्मों की । अनंत महादेवन की 'रेड अलर्ट' ग्रामीण समाज और एक गरीब किसान के नक्सलवाद के चंगुल में फंसने की कहानी थी तो सुशील राजपाल की फिल्म 'अंतर्द्वंद' बिहार और उत्तरप्रदेश में कभी मौजूद में जबरिया शादी की प्रथा पर थी।
किसान हत्याओं पर फिल्मकार अनुषा रिजवी की 'पीपली लाइव' बहुत ही संवेदनशील तरीके से इस समस्या को तीखे व्यंग्य का लेप लगाकर दिखाती है. कुछ लोग मानते हैं कि शेखर कपूर की 'बैंडिट क्वीन' के बाद असली लोगों का चित्रण फिल्मी परदे पर नहीं हुआ। 'पीपली लाइव' उस कड़ी में शायद दूसरी ऐसी फिल्म होगी। यह पूरी तरह सच नाभी हो लेकिन यह सच है कि 'पीपली लाइव' भारत के गांव और शहरों की बीच की खाई को सही तरीके से दिखा पाई जहां बड़ी चुनौती शहरों की ओर पलायन और उससे उपजी समस्याएं हैं।
लेकिन यहां एक बड़ा विरोधाभास है। गांवों या छोटे कस्बों की 'पीपली लाइव' या 'मसान' जैसी कहानियां देश के छोटे कस्बों में या सिंगल स्क्रीन में नहीं चलतीं। क्योंकि इनके दर्शक भी वही हैं जो मल्टीप्लेक्स में 'बजरंगी भाईजान' देखते हैं और इन्हीं में से कुछ लोग जाकर 'मसान' देखते हैं जो किसी मल्टीप्लेक्स में ही लगती है। मोटी बात ये कि रूरल इंडिया की स्टोरी को अब सिर्फ अर्बन इंडिया देख रहा है। तो सच्चाई यह है कि 'भारत' केन्द्रित इन फिल्मों के दर्शक भारत के या भारत में बसे गांव या कस्बों के लोग नहीं हैं। इनके भी दर्शक शहरों के मल्टीप्लेक्स में जाकर फिल्में देखने वाले लोग हैं। उदाहरण के लिए, 'पीपली लाइव' की कहानी और वह जगह जहां यह कहानी घटित होती है, उसे देखने भर से गांव और शहर के बीच की खाई सामने नजर आ जाती है। लेकिन साथ में यह हमारे सामने कुछ सवाल भी छोड़ जाती है। 150 रुपये से लेकर 800 रुपये का एक टिकट लेकर मल्टीप्लेक्स में मध्यमवर्ग के ही कितने लोग जाकर नियमित फिल्में देख सकते हैं? क्या किसी शहरी गरीब की हैसियत है कि वह यहां आकर 'पीपली लाइव' देखे क्योंकि यह उनकी समस्याओं पर आधारित है? या क्या कोई गरीब ग्रामीण खुद को ऐसी फिल्मों के जरिया मनोरंजन करवाना पसंद करेगा?
ऐसी फिल्में बनती रहें, इसके लिए यही अच्छी बात है कि 'बजरंगी भाईजान' के 100 दर्शकों में से 20 भी 'मसान' देख ले रहे हैं। इन फिल्मों का कम बजट देखते हुए,यही 'मसान' जैसी फिल्मों के लिए बड़ी सफलता है।
श्याम बेनेगल ने जब 'वेलकम तो सज्जनपुर' (2008) तो गांव की इस कहानी को शहरी लोगों ने पसंद किया। उन्होंने उस वक्त एक इंटरव्यू में कहा था कि गांव के दर्शक मुंबई में बनने वाली फिल्मों से पूरी तरह कटे हुए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुंबई के फिल्मकार इस दर्शक समुदाय के लिए फिल्में नहीं बना रहे। उनकी ज्यादातर फिल्में 'एस्पारेशनल' होती हैं। हालांकि ग्रामीण युवा वर्ग ने अपनी उम्मीदों और महत्वाकांक्षाओं को अब शहरी भारत से जोड़ लिया है लेकिन फिर भी वे इन शहर आधारित फिल्मों को नहीं समझ पाते, लिहाजा इससे दूर रहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण तर्क है।
भारत भर की फिल्मों को तो छोड़ ही दें, बलीवुड में भी जो सिनेमा बन रहा है क्या वह 'रियल इंडिया' है? क्या वह मुंबई के बारे में है? शायद नहीं? वह एक काल्पनिक दुनिका की कहानी है जिसका अस्तित्व कहीं नहीं है। बलीवुड अगर मुंबई के किसी गैंगस्टर की कहानी कहेगा तो उसका हीरो जन अब्राहम जैसा बडी बिल्डर होगा। ऐसे गैंगस्टर कहां होते है? गैंगस्टर तो अरुण गवली जैसे होते हैं लेकिन वैसे असली चरित्र फिल्मों में कहां दिखता हैं? बॉलीवुड किस 'इंडिया' की कहानी कहता है? इस बात को मान लेना ही बेहतर है कि आज का सिनेमा अंतत: एक फंतासी दुनिया है। यह शहरी समाज के लिए है। 90 प्रतिशत दर्शक उसी तरह की फिल्मों को देखने के लिए आता है जो उसे कुछ समय के लिए एक फंतासी दुनिया में ले जाए। उन्हीं में से कुछ उन फिल्मों को देख लेते हैं जो गांव और कस्बों की कहानियां कहते हैं।
हिंदी सिनेमा में पचास-साठ के दशक की 'मदर इंडिया', 'गंगा जमुना', 'नया दौर', 'दो बीघा जमीन' जैसे फिल्में ग्रामीण विषयों पर बनी बड़ी फिल्मों के चंद उदहारण हैं जिन्हें पूरे भारत में हर वर्ग के लोगों ने पसंद किया। तब सिनेमा में भारत बनाम इंडिया की बात नहीं थी लेकिन तब भी सितारों की छवि को नजरअंदाज किया जा सकता था। साठ के दशक के तीन बड़े और समकालीन सितारे-दिलीप कुमार, देवानंद और राजकुमार।
दोनों से अलग देवानंद ने एक भावुक रोमांटिक प्रेमी के तौर पर अपनी छवि बनाई। सितारों के लिए अपनी ही बनाई छवि को तोड़ना कई बार मुश्किल होता है। सो देव आनंद ने शहरी किरदार ही निभाए और जब सिर्फ एक फिल्म (इंसानियत) में धोती पहनी तो फिल्म फ्लाप हुई। देवानंद को धोती पहने देख लोगों ने खारिज कर दिया। वहीं दिलीप कुमार ने 'गंगा जमुना' समेत कई फिल्मों में ग्रामीण का किरदार बखूबी निभाया।
तो कहने का मतलब, ग्रामीण किरदारों को परदे पर उतारू सभी सितारों के बस की नहीं है। आज के सन्दर्भ में इसी बात को देखिये। शाहरुख, आमिर और सलमान में आमिर ने 'लगान' में धोती पहनी और ग्रामीण पृष्ठभूमि की बेहतरीन फिल्म बनाई। अब वे कुश्ती पर 'दंगल' बना रहे हैं। उम्मीद है, इसमें भी जचेंगे। अनुषा रिजवी (पीपली लाइव), अभिषेक चौबे (इश्किया, डेढ़ इश्किया), आमिर खान (लगन, दंगल), नागेश कुकूनूर (डोर, इकबाल) जैसे फिल्मकारों की छोटी जमात अभी भी गांव और कस्बों की कहानियां शहरी समुदाय को सुनाना चाहती है लेकिन ऐसे लोग गिने चुने हैं।
शहरीकरण ने हिंदी सिनेमा से गांव को लगभग गायब कर दिया है। जो गांव अब फिल्मों में दिखते भी हैं, वे भोले भाले लोगों के नहीं बल्कि षड्यंत्रकारियों से भरे हैं। जबकि शहर का एक काला डरावना पक्ष है लेकिन फिर भी यह रोमांस और संभावनाओं की जगह है!
अमिताभ पाराशर
कला और सिनेमा से जुड़े विषयों के गहन जानकार एवं विश्लेषक

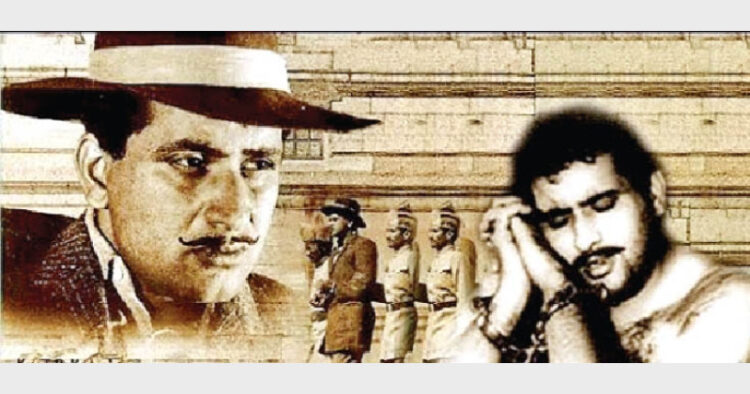










टिप्पणियाँ