|
.एस. पुरुषोत्तम
माना जाता है कि दुनिया में भारत हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश है, जो वैश्विक हथियार आयातों का 14 फीसदी हिस्सा आयात करता है। इससे वह देश में उत्पादन से जुड़े उन्नत पर्यावरण तंत्र, रोजगार और कौशल के अवसर गंवा देता है। वास्तव में, भारत व्यावहारिक तौर पर अपनी तमाम अत्याधुनिक आवश्यकता की चीजें आयात करता है, ये तथ्य इसे, मजाकिया तौर पर कहें तो, 'बनाना रिपब्लिक' नहीं, 'खरीदना रिपब्लिक' बनाता है।
हालांकि भारत ने कमाल के तकनीकी मुकाम हासिल किए हैं, पर यह अभी निर्माण की उन्नत तकनीकी विकसित करने की स्थिति में नहीं आया है। दुनिया औद्योगिकीकरण के बाद के युग में प्रवेश कर चुकी है, और वह उन्नत तकनीकी पर नियंत्रण जमाने की हरसंभव कोशिश कर रही है। एमआईटी और मैक्किंसी ने तो अभी से कह दिया है कि नई विध्वंसात्मक तकनीकें,जैसे-कृत्रिम गुप्तचरी, रोबोटिक्स, 3डी निर्माण, नैनोटेक्नोलोजी, एम्बेडिड टेक्नोलोजी और जीनोमिक्स-विकसित देशों की सालाना आर्थिक उन्नति में खरबों डालर का मुनाफा देंगी। इसीलिए 21वीं सदी में ताकत हासिल करने की दौड़ असल में तकनीकी में दूसरे से आगे निकलने की दौड़ है। इसीलिए चीन ने अनुसंधान और विकास में जबरदस्त पैसा लगाया है और वह इस क्षेत्र में अमरीका तक को पीछे छोड़ने की स्थिति में है। इसलिए जरूरी है कि भारत देश में ही अनुसंधान एवं विकास और तकनीकी विकास के क्षेत्र में सही माहौल पैदा करने पर ध्यान दे। हालांकि दुनिया भले अगले नए युग की तरफ बढ़ रही है, जिसके जरिए वह 'तकनीकशुदा' और 'तकनीक- रहित' देशों के बीच दरार चौड़ी कर रही है, लेकिन भारत अब भी लाइसेंसी उत्पादन में अटका है। नवम्बर, 2014 में समाधान की खोज में फोरम ऑन हाईटेक डिफेंस इन्नोवेशन की पांचवीं बैठक हुई थी। फोरम में हुई चर्चा का रक्षा एफडीआई में नीति निर्माताओं पर असर भी दिखा, और एयरोस्पेस तथा इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रों में काम आगे बढ़ा।
फोरम का मानना था कि भारत को अशोक के 4 खंभों पर आधारित उपरोक्त चार उद्देश्यों की पूर्ति के लिए रक्षा औद्योगिकीकरण अभियान शुरू करना चाहिए, जो हैं अनुसंधान और विकास, भारत का अपना उद्योग, 'साइंस स्टेट' और शिक्षा। दूसरे देशों ने भी आर्थिक उन्नति, रोजगार, उन्नत तकनीकी और उपकरण बढ़ाने के लिए डिफेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन स्ट्रेटेजीस का इस्तेमाल किया है।
1. शोध एवं अनुसंधान
अ) भारत की 2016 तक अनुसंधान और विकास की दर सकल घरेलू उत्पाद की दर के 1.75 फीसदी होना चाहिए।
ब) भारत को अनुसंधान और विकास को इस्रायल की तर्ज पर बढ़ाने के लिए विशेष अनुदान तैयार करने होंगे।
स) सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को अनुसंधान और विकास की गति बढ़ानी होगी और लाइसेंसशुदा उत्पादन की बजाय अनुसंधान और विकास पर आना होगा।
ग) नई सोच को बढ़ावा देने के लिए सरकारी खरीद के नियमों में सुधार करना होगा। सरकार/ रक्षा बलों द्वारा खरीदी जाने वाली तकनीकों की मान्यता, आकलन और सर्टीफिकेशन के लिए हाईर्टेक कंपनियों को एक नए, पारदर्शी, तकनीक-सुलभ सिंगल विंडो सिस्टम हो, जिसमें देरी के लिए जुर्माने का प्रावधान हो।
घ) भारत को कई सारे नए विज्ञान एवं औद्योगिक शहर/जोन्स बनाने चाहिएं जिनमें शिक्षा, तकनीकी अनुसंधान विश्वविद्यालय, अनुसंधान और विकास तथा निर्माण भी शामिल हों।
ड) भारत में दुनिया की 17 फीसदी आबादी होने के चलते हमें अपनी खुद की रक्षा, नौवहन, दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक्स की जरूरतें और मानक निर्धारित करने होंगे।
च) भारत को विज्ञान को लोकप्रिय बनाना होगा-वैज्ञानिकों और उन्नत तकनीकी के कामयाब निर्माताओं को राष्ट्रीय पुरस्कार, उन्नतियां और राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए ईनाम वगैरह देने होंगे।
2. अपने देश के उद्योग को बढ़ावा देना
फोरम ने रक्षा औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए दूसरे देशों की तरह रक्षा उद्योग समायोजन को मजबूत बनाने की पहचानी और परखी राह पर बढ़ने का सुझाव दिया था। जापान, कनाडा, पोलैंड और क्रोएशिया रक्षा उद्योगों का समायोजन लागू कर रहे हैं क्योंकि अगर ये ठीक से लागू हों तो उनसे औद्योगिक और तकनीकी क्षमताओं में इजाफा भी होता है।
इस्रायल में राष्ट्रीय समायोजन नीति लागू है जो रक्षा क्षेत्र में आगे तक प्रभाव डालती है। ऐसे बहुत से उदाहरण और बेहतरीन क्रियान्वयन हैं जिनका अध्ययन किया जा सकता है। अगले कुछ सालों में रक्षा निर्यात पर अनुमानत: 100-200 डालर का 100 फीसदी समायोजन भारतीय अर्थव्यवस्था में उतना ही बड़ा इजाफा करेगा। व्यापार घाटे पर दुखी होने की बजाय, मूलभूत सामर्थ्य के विकास में गजब की बढ़ोत्तरी होगी।
अत: रक्षा उद्योग का समायोजन भारत की प्रगति के लिए भी एक सही उपाय है। लेकिन दुनियाभर के देशों में समायोजन नीतियों की कामयाबी उन कुछ निहित स्वार्थ वालों ने भारतीय नीति निर्माताओं से छ़ुपाए रखी जो सैन्य उपकरणों के आयात पर फलते-फूलते हैं। साथ ही विदेश की हर चीज की नकल करने की चाह रखने वाले मानसिक और संस्थागत दबाव समूह अब भी उतने ही ताकतवर हैं। उनकी मानें तो भारतीय उद्योग में ऐसा करने की सामर्थ्य ही नहीं है।
समायोजन के पक्ष में सबसे बड़ी बात यह है कि अगर यह इतना नुकसानदेह होता तो इतने सारे देश अपने रक्षा औद्योगिकीकरण के लिए इसे लागू क्यों करते?
फोरम के सुझाव थे-
1. भारत को अपने समायोजन प्रावधानों को मजबूत करके लंबे-चौड़े रक्षा आयातों के अवसरों को थोड़ी जगह देनी होगी।
क. कोटा 30 फीसदी से 70 और 100 फीसदी के बीच बढ़ाकर
ख. कम से कम शुरुआत को 50 लाख डालर तक घटाकर
ग. निर्यात और उत्पादन के पूरे अधिकारों के साथ तकनीकी स्थानांतरण सुनिश्चित करके
घ. 100 फीसदी समायोजन के तहत, सम्पूर्ण पर्यावरण तंत्र विकसित करने के लिए अप्रत्यक्ष समायोजन की अनुमति दी जा सकती है।
2. रक्षा, विमान, दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक्स में जबरदस्त आयात को देखते हुए समायोजन नीति तय की जाए। राष्ट्रीय समायोजन नीति के तहत क्षेत्रवार समायोजन एजेंसियां स्थापित हों।
3. नागरिक उड्डयन में समायोजन को फिर से और ज्यादा पारदर्शिता के साथ क्रियान्वित किया जाए ताकि यह कहीं धुंधलके में न खो जाए।
4. सेवा क्षेत्र में बड़े हार्डवेयर उपकरण आयातों में समायोजन आवश्यक तौर पर लागू हो।
5. समायोजन देख रहे रक्षा मंत्रालय के अधिकरियों के लिए प्रशिक्षण आवश्यक किया जाए, क्योंकि समायोजन का प्रतिशत बढ़ाने में असली अड़चन बड़ी तादाद में परियोजनाओं को संभालने में संस्थागत अयोग्यता ही होती है।
6. इस पर कड़ी नजर, लेखा-जोखा रखा जाए।
भारतीय उद्योग को बढ़ावा देना
7. भारत वह एकमात्र बड़ी ताकत है जिसके पास इंटीग्रेटिड प्रोडक्शन मेन्युअल या आरडीए नहीं है। इसके पास बस एक डिफेंस प्रोडक्शन प्रोसीजर है जो सीधे खरीद की बात करता है, उत्पाद के विकास को अनदेखा करता है और इस तरह आयात का मुंह ताकने वाली संस्कृति को बढ़ावा देता है। जिन देशों में उन्नत रक्षा उत्पादन क्षेत्र हैं यानी स्वदेशी अनुसंधान से लेकर विकास, उत्पादन और आखिर में तैनाती और खरीद तक, वहां यह सारा आरडीए में लिखा होता है, इस तरह यह घरेलू उत्पादन में सहायक होता है। इसका न होना उत्पादक देशों, जैसे चीन और अमरीका तथा आयातक देशों, जैसे भारत के बीच बुनियादी फर्क रेखांकित करता है।
8. एक उलझन भरे डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर की बजाय एक स्पष्ट और सरल डिफेंस प्रोडक्शन अपनाना चाहिए, उन देशों की तर्ज पर जहां उन्नत रक्षा उत्पादन है।
9. हर क्षेत्र में एक प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस (पीएमए) नीति, जो मूलत: भारतीय कंपनियों को अपने ही देश में खरीद केआदेश पाने का मौका देने के लिए बनाई गई थी, पूरी तरह से बहाल की जानी चाहिए।
10. रक्षा खरीद आदेशों में भारतीय उद्योग को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, बाहरी कंपनियों की बजाय। भारतीय फर्म या क्रोएशिया को रक्षा समायोजनों और उत्पादन परियोजनाओं के लिए अग्रणी 'इंटीग्रेटर्स' तय करना चाहिए।
11. कर/आर्थिक नीतियों को भारतीय और बाहरी कंपनियों में भेद नहीं करना चाहिए।
12. 12वीं योजना में निर्माण परियोजनाएं शुरू की जानी चाहिएं जो 13वीं योजना में 100 फीसदी तक पहंुच जानी चाहिएं।
13. अमरीकी खरीद कानून की तर्ज पर भारतीय खरीद कानून अपनाया जाना चाहिए।
14. द्विपक्षीय समझौतों के तहत विमानों की सीटों को एकमुश्त देने की बजाय एमआरओ मार्केट का पूरा लाभ उठाना चाहिए।
3. 'साइंस स्टेट'
अमरीका की गजब की तकनीकी उपलब्धियां सरकार की सक्रिय दखल और अनुदान के बूते ही हो पाईं। तमाम विकसित देशों में सरकारें प्रमुख रक्षा सामथ्यों को बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाती हैं, जैसे अमरीका, रूस, चीन, यू.के., फ्रांस, जर्मनी, और अब तुर्की, यूएई तथा दक्षिण कोरिया भी अब अपनी रक्षा सामर्थ्यों पर खास ध्यान देते हैं। अगर भारत एक उपयुक्त रक्षा में नई तरह की अर्थव्यवस्था चाहता है, तो सरकार को वैसी ही तकनीकी खोजों, औद्योगिक नीति में सहायक की भूमिका निभानी होगी। इस तरह भारत एक उन्नत विज्ञान राष्ट्र बन सकता है।
4. शिक्षा में सुधार
रक्षा संबंधी औद्योगिकीकरण के लिए कुशल मानव संसाधन और शैक्षिक आधार तैयार करना होगा-
क. रक्षा संबंधी औद्योगिकीकरण के लिए बड़ी तादाद में वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, कुशल तकनीक विशेषज्ञों और वक्ताओं की आवश्यकता होगी। इस दिशा में बढ़ने के लिए शिक्षा/व्यावसायिक प्रशिक्षण क्षेत्र में सुधारों की तो जरूरत होगी ही।
ख. सुधारों का मकसद एक मजबूत प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र तैयार करना होना चाहिए ताकि बच्चे जटिल विषयों को समझ सकें, गहराई से सोच सकें और रोजगार के लिए तैयार हो सकें।
ग. शिक्षा क्षेत्र में अनुदान बड़े पैमाने पर बढ़ाना होगा।
घ. कौशल प्रशिक्षण के लिए सहूलियतों में इजाफा करना होगा। इस दिशा में एप्लाइड साइंस यूनिवर्सिटी की तर्ज पर काम किया जा सकता है जो इस हाईटेक औद्योगिक क्षेत्र को सीधे कौशल उपलब्ध कराती है।
ड. रक्षा तकनीकी और अनुसंधान आधारित विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने चाहिएं।
च. रक्षा समायोजन अनुदान या विनिवेश से होने वाले लाभ जैसे अनुदान के नए स्रोत खंगालने चाहिएं ताकि मौजूदा शिक्षा और प्रशिक्षण को बेहतर किया जा सके।
छ. शैक्षिक संस्थानों की मदद के लिए प्रावधान होने चाहिएं।
ज. भारत को अपने यहां विदेश के नामी विश्वविद्यालयों की शाखाएं खोलने की अनुमति देनी चाहिए जिससे शिक्षा में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रहे बेहतरीन कामों का लाभ हमारे यहां उपलब्ध हो।
झ. भारत में प्रादेशिक भाषाओं में छपा अच्छा अंतरराष्ट्रीय साहित्य उपलब्ध हो।
एक नया मंथन
किस्मत से आज, सरकार नए विचारों का स्वागत कर रही है और भरोसा बढ़ाने के उपाय लागू कर रही है। इससे दोहरे इस्तेमाल, हाईटेक, औद्योगिकीकरण के बाद की अर्थव्यवस्था तैयार करने में गति आएगी। इससे राष्ट्र की सुरक्षा और कल्याण का मार्ग खुलेगा।











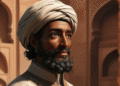
टिप्पणियाँ