दाना तो है पर पानी नहीं
|
प्रशांत महासागर में उभरा अल नीनो दिखा सकता है भारत पर अपना ताप
.आलोक गोस्वामी
मौसम विभाग इधर कुछ समय से मौसम के मिजाज के कुछ सही-सटीक आकलन करने लगा है। पहले से उलट, अब अगर मौसम विज्ञानी बूंदाबांदी के आसार बताते हैं तो रिमझिम हो ही जाती है, शाम को तेज हवाओं के कयास सूरज छिपते न छिपते आंधी चलने पर खरे उतरते हैं। गर्मियों की तपिश बढ़ने के साथ ही अप्रेल महीने में ही मौसम विभाग के निदेशक ने यह कहा था कि इस बार मानसून साधारण से कम रहने के आसार बन रहे हैं तो आगे के दो महीनों, मई और जून की झुलसाती गर्मी ने उस आसार के खरे उतरने के संकेत देते हुए देशवासियों, खासकर किसानों को सांसत में डाल दिया है। जिस देश की अर्थव्यवस्था खेती-किसानी पर टिकी हो उसमें मानसून क्या मायने रखता है, इसे समझना कोई मुश्किल नहीं है। सकल घरेलू उत्पाद का 17 से 20 प्रतिशत हिस्सा खेती-किसानी से आता है। देश के 75 फीसदी किसान प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से खेती पर आश्रित हैं। ऐसे में बारिश का साधारण से कम होना बेहद चिंताजनक स्थिति पैदा कर सकता है,क्योंकि भारत में आधे से ज्यादा खेत सिंचाई के लिए बारिश यानी मानसून के भरोसे होते हैं।
अप्रैल 2014 में मानसून की बढ़त के बारे में बताते हुए भारत के मौसम विभाग ने उत्तर की तरफ बढ़ते मानसून के कमजोर होने की भविष्यवाणी की थी। बताया था कि अगर दुनिया भर के ऋतु चक्र में हेर-फेर लाने वाला अल नीनो पश्चिमी कारकों को प्रभावित करता है तो बारिश साधारण से कम हो सकती है। अल नीनो के असर होने की 60 फीसदी संभावना जताई गई थी। यानी 60 फीसदी कम बारिश यानी सूखे के हालात।
मौसम की भौगोलिक स्थिति का आकलन करने के बाद पता चला है कि उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर क्षेत्र में भूगर्भीय तापमान उतने स्तर तक चढ़ गया है जो अल नीनो से पहले की स्थितियां बनाता है। दक्षिण-पश्चिम मानसून के मौसम के दौरान भूमध्यीय प्रशांत महासागर क्षेत्र में समुद्री सतह का तापमान भी बढ़ता देखा गया है। ये सब हालात अल नीनो प्र्रभाव की ओर संकेत करने वाले हैं। साधारणत: 100 सालों का रिकार्ड देखें तो सूखे की संभावना 17 फीसदी के आस-पास रहती है, जो इस साल 33 के स्तर तक पहंुच चुकी है। मौसम विभाग की मानें तो अगर यह 90 फीसदी तक पहुंच गई तो सूखा पड़ना निश्चित है।
उत्तर भारत में मई और जून के महीने बेहद झुलस भरे रहे। जून के आखिरी हफ्ते में बीच बीच में राहत के आसार नजर आए, बादल छाए, तेज धूल भरी हवाएं चलीं, कुछ इलाकों में हल्की तो कुछ में तेज बौछारें भी पड़ीं, लेकिन 5-10 मिनट की बारिश कुछ खास राहत न दे पाई। हालांकि मौसम विभाग ने यहां तक कह दिया था कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते उत्तर में मानसून आने के अच्छे आसार बनते दिखे हैं और अगले 48 घंटे में तेज बारिश आ सकती है। लेकिन बारिश वैसी नहीं आई जैसी उम्मीद बांधी गई थी। मौसम विभाग ने बताया कि अल नीनो प्रभाव के 60 फीसदी प्रभाव होने के बावजूद मानसून के अच्छे संकेत मिले हैं। मौसम विभाग प्रशान्त और हिन्द महासागर में समुद्री सतह पर होने वाले बदलावों पर बारीक नजर रख ही रहा था। विभाग के अनुसार साधारण मानसून अच्छा तब माना जाता है जब 96 से 104 फीसदी बारिश हो। अल नीनो के चलते 2002, 2004 और 2009 में भारत भयंकर सूखे के हालात झेल चुका है। लेकिन यह भी सच है कि पर्याप्त बारिश के चलते 2013 में अच्छी बारिश हुई थी और भारत के खलिहान 262 मिलियन टन अनाज की रिकार्ड पैदावार से भर-पूरे थे।
लेकिन इस साल चार माह के मानूसन में पहले माह यानी जून के दौरान पूरे भारत में साधारण से 43 फीसदी कम बारिश रिकार्ड की गई। महाराष्ट्र और गुजरात में तो 90 फसदी कम बारिश हुई। ये वे इलाके हैं जहां खासतौर पर कपास, सोयाबीन और गन्ने की खेती होती है। 2014 की फसल कैसी रहेगी? तस्वीर कोई खास उम्मीद नहीं जगाती, खासकर उत्तर भारत के खेतों को बारिश का अब भी इंतजार है। ऐसे में भारत के किसानों की चिंता कैसे दूर होगी?
मानसून के खराब रहने या कम होने को लेकर मोदी सरकार सचेत है। 26 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने मौसम और कृषि विशेषज्ञों की मौजूदगी में एक बैठक की। मौसम विभाग ने बैठक में माना कि अब तक मानसून उम्मीद से कम रहा है, लेकिन अल नीनो का असर अभी नहीं देखा गया है। विभाग ने एक बार फिर उम्मीद जगाई कि जुलाई और अगस्त में अच्छी बारिश हो सकती है। आसार खराब रहने के कयासों के बीच मोदी ने तमाम संबंधित मंत्रियों और अधिकारियों को कह दिया है कि मानसून पर 'एडवांस्ड एक्शन प्लान'को लागू करने में पर्याप्त सक्रियता और समन्वय से काम करना होगा।
मानसून के खराब रहने से सकल घरेलू उत्पाद पर सीधा असर तो पड़ेगा ही, मुद्रास्फीति भी 2 से 3 फीसदी बढ़ सकती है। सरकार ने इसीलिए जमाखोरों पर सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं और राज्यों से भी कहा है कि जमाखोरों और कालाबाजारियों से तेजी से निपटने के लिए विशेष अदालतों का गठन करें। मोदी ने मुद्रास्फीति को काबू करने के प्रयासों की भी जानकारी ली।
पिछले कई वर्षो से बारिश की लुका-छिपी और वैश्विक ताप के चलते धरती का जल स्तर लगातार नीचे जाना भी भू-वैज्ञानिकों और जल-संरक्षण में जुटे गैर सरकारी संगठनों की चिंता का विषय बना हुआ है। हर घर में लगे सब्मर्सीबल पंपों और पानी के अंधाधंुध दुरुपयोग ने जमीन में पानी को 150 फुट से भी नीचे पहुंचा दिया है। हर जगह सीमेंट से कच्ची जमीन को ढकने की भेड़चाल में लगे लोग यह नहीं जानते कि बरसात का पानी इसी कच्ची जगह से जमीन में समाकर उसे रीचार्ज करता है या आसपास के तालाबों,पोखरों को सींचता है। पर अपार्टमेंट्स और ऊंची अट्टालिकाओं के मकड़जाल पुराने तालाबों,बावडि़यों को लील चुके हैं। कहना न होगा कि शहरीकरण के नकारात्मक प्रभावों और नैसर्गिक पानी को संजोने की हमारी प्राचीन परंपराओं को हिकारत भरी नजरों देखने की वजह से आने वाला वक्त पानी को लेकर भीषण संघर्ष का साक्षी बन सकता है। वक्त रहते चेतना ही मानव हित में ही है।
अर्थव्यवस्था पर अल नीनो का असर
2002, 2004 और 2009 में भारत में अल नीनो का इतना जबरदस्त असर था कि तीनों साल भयंकर सूखा पड़ा, खेत पानी को तरस गए, फसल चौपट हो गई और किसान हताश। 2002 में तो अनाज की पैदावार मात्र 174.2 मिलियन टन रह गई थी। सकल घरेलू उत्पाद भी 3.9 फीसदी घटा था। 2004-05 में 2003-04 के मुकाबले अनाज की पैदावार कम होकर 204.6 मिलियन टन ही हुई। 2003-04 में यह 213.5 मिलियन टन थी। 2013 में रिकार्ड 262 मिलियन टन पैदावार हुई थी।
सरकार है तैयार
अल नीनो के असर में सूखे के हालात से निपटने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। अनाज गोदामों के स्टॉक लेने के साथ ही जमाखोरों और कालाबाजारियों के खिलाफ सख्ती बरती जा रही है। जगह-जगह छापे मारकर जमाखोरी रोकी जा रही है।
सालभर के लिए पर्याप्त अनाज
देश में गेहूं और चावल का पर्याप्त भण्डार है। इतना ही नहीं आलू और प्याज भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। इस वक्त 25.41 मिलियन टन चावल एफ.सी.आई गोदामों में सुसक्षित है। अनाज का कुल भण्डार (चावल और गेहूं मिलाकर) है 66.41 मिलियन टन।
बाजार विशेषज्ञों की राय
भारत के पास अनाज की फिलहाल कोई कमी नहीं है। जमाखोर और कालाबाजारिए फर्जी कमी दिखाकर अनाज का भण्डार कर रहे थे,जिनके खिलाफ सख्त कदम उठाकर सरकार ने अच्छे संकेत दिए हैं। इस कदम से मुद्रास्फीति पर लगाम लगेगी।
क्या है अल नीनो
दक्षिण अमरीका में प्रशान्त महासागर के तट के आसपास पानी का तापमान जब साधारण से ज्यादा हो जाता है तब मौसम में बेहद उतार-चढ़ाव देखने में आते हैं। इसे अल नीनो का असर कहते हैं। ऐसे में पूरा प्रशान्त क्षेत्र साधारण से ज्यादा गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से समुद्र की जो हवाएं एशिया में बारिश लाती हैं उनका बहाव घट जाता है। इसके चलते भारत में कम बारिश होती है। ऐसा होने पर सूखा पड़ता है। इस अल नीनो के बारे में पहले से बता पाना थोड़ा पेचीदा होता है।











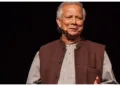
टिप्पणियाँ