|
धरती के स्वभाव में दिख रहे बदलाव, यानी बारिश के मौसम में सूखा, गर्मी में ठंडी, ठंडी में गर्म झोंके, आदि जनजीवन के लिए किस प्रकार घातक हैं?
यह पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि प्रकृति अपने स्वभाव में बदलाव कर ही रही है, क्योंकि इस संबंध में हमारा जो भी ज्ञान है वह 100 साल से ज्यादा पुराना नहीं है, जो प्रकृति के भंडार के सामने कहीं नहीं टिकता। आए दिन सुनने में आता है कि 25 साल का रिकार्ड टूट गया, 50 साल का रिकार्ड टूट गया कि इतनी बारिश हो गई, इतनी ठंड पड़ गई। ये सब100 साल के तराजू पर तोले गए आंकड़े होते हैं। इसलिए किसी को ऐसा घमंड नहीं करना चाहिए कि हम प्रकृति को बहुत अच्छे से जान गए हैं। उदाहरण के लिए, प्रकृति मदरडेयरी का बूथ नहीं है जो जितने टोकन डालो उतना दूध दे यानी उतनी ही बारिश करे। वह कहीं कम तो कहीं ज्यादा बारिश देती है। विवेकवान समाज का लक्षण है कि वह प्रकृति के छोटे-मोटे झोंकों को सहने लायक जीवन बनाए।
ल्ल आज कितनी ही जगह से बाढ़ की खबरें सुनाई देती हैं। ऐसा क्यों?
कुछ स्थानों पर पानी ज्यादा गिरने लगा है। पर गौर से देखें तो पानी का स्वभाव उतना नहीं बदला है जितना हमारा स्वभाव बदला है। जैसे, आज से 103 साल पहले जब दिल्ली को राजधानी बनाए जाने की तैयारी हुई थी उस वक्त यहां 800 तालाब थे। इन 100 सालों में हमने वे 800 तालाब पूर दिए, उन्हें पाट दिया। उन तालाबों की शायद जरूरत नहीं रही होगी या उस जमीन की ऊंची कीमत रही होगी कि हमें लगा क्या पानी रोकना, इससे तो इसे पाट दें।
ल्ल उन्हें पाटने से हमारे पेयजल में कमी आने का भी नहीं सोचा गया?
इसलिए क्योंकि लगा होगा कि हमारे पीने का पानी इन तालाबों से तो आ नहीं रहा है, यमुना से आ रहा है। फिर हमने यमुना खाली कर दी, तो गंगा से पानी लिया, भागीरथी से लिया। अब तो हिमाचल की रेणुका झील से पानी दिल्ली आने वाला है। ऐसे में सोचा गया होगा कि अगर हमारा पानी दिल्ली से 200-300 किलोमीटर दूर से आ रहा है तो हमें इन तालाबों की क्या जरूरत। लेकिन हमने इंद्र देवता को तो खबर नहीं दी कि 'हमारे यहां तालाब पाट दिए गए हैं, हमारा पानी बाहर से आता है, अब आप हमारी दिल्ली पर पानी मत बरसाना'। इंद्र पानी बरसाते रहे और यही वजह है कि कच्ची मिट्टी पर बने तालाब न रहने से घुटने-घुटने पानी इकट्ठा हो जाता है। अब बताइए, दोष प्रकृति का है या हमारा? दिल्ली में गिरा पानी 100-200 किलोमीटर दूर नदी में नहीं गिरने वाला, यहां की नदी खुद उफान पर है तो उसमें भी नहीं गिरेगा। जिन तालाबों में उसे भरना चाहिए था वे हम मिटा चुके हैं। पुराणों में देखें तो इंद्र का एक नाम है पुरंदर यानी किले तोड़ने वाला। शहर अव्यवस्थित होंगे तो इंद्र्र उन्हें पानी की मार यानी बाढ़ से तोड़ेंगे ही।
ल्ल उत्तराखण्ड में यही हुआ था?
उत्तराखण्ड में यही तो हुआ था। प्रकृति ये बताती है कि भई, हम तुम्हारे इन बिना सोचे बनाए शहरों को, टूरिस्ट केन्द्रों को बिल्कुल मान्यता नहीं देते। इसलिए शहर बनाते वक्त बहुत सावधानी रखनी चाहिए।
ल्ल दिल्ली में कंक्रीट का जंगल दिखता है, खेत उजड़ चुके हैं, ऊंची इमारतों का संजाल है। क्या इससे कुदरत नाराज हुई है?
हां, यहां जो पानी गिरेगा वह कहां जाएगा, सोखने को कच्ची जमीन कहां है, बाढ़ तो आएगी ही, इसलिए विकास जरूर करो पर प्रकृति को बिना भूले।
ल्ल शायद यही वजह है कि भूजल स्तर नीचे जा रहा है?
इसलिए क्योंकि उसको रीचार्ज करने की गुंजाइश नहीं है। एक तालाब में लाखों करोड़ों बाल्टी पानी आता था। उससे जमीन रीचार्ज होती थी। अब कहां हैं वे तालाब। ऊलजलूल विकास होगा तो उसकी कीमत चुकाने की तैयारी भी रखनी होगी।
ल्ल विकास के नाम पर विनाश न हो, इसका रास्ता क्या है?
कच्ची और पक्की जमीन के बीच संतुलन बना रहे। पानी रोकने के लिए तालाब हों। तालाब को पिछड़ा न मानें। मध्य प्रदेश में इंदौर के पास 20-25 साल पहले पीतम पुर नाम का शहर बसाया गया। वहां मोटर पार्ट्स बनाने वाली 600 औद्योगिक इकाइयां हैं। आज उस शहर में जमीन से पानी खत्म हो गया है। वहां आज टैंकरों से पानी आता है पास के गांवों से। कल उन गांवों का पानी भी सूख जाएगा। तो अच्छी दृष्टि ये होगी कि आप चाहे उद्योग नगरी बनाएं या रिहायशी नगरी, उसमें बड़े पैमाने पर पानी का प्रबंध रखा जाए, कच्ची जमीन छोड़ें, हरियाली छोड़ें।
ल्ल क्या दिल्ली की मिट्टी में जकड़े रहने की
गांधीवादी पर्यावरणविद् डॉ. अनुपम मिश्र लम्बे समय से जल संचयन की भारतीय संस्कृति का अध्ययन करते आ रहे हैं। वे प्रकृति में दिख रहे छिटपुट बदलावों को अनायास हुए बदलाव नहीं मानते। उनके अनुसार हमने बिना सोचे विकास की जैसी दौड़ लगाई है उसके दुष्परिणाम तो भोगने ही पड़ेंगे। वे विकास के विरुद्ध नहीं हैं, पर कच्ची और पक्की जमीन के बीच संतुलन बैठाने को बेहद जरूरी मानते हैं। पर्यावरण को लेकर आम लोगों में बढ़ रही चिंताओं के संदर्भ में प्रस्तुत हैं आलोक गोस्वामी की डॉ. मिश्र से हुई हुई बातचीत के प्रमुख अंश
ताकत खत्म हो रही है? आंधी में पुराने जमे पेड़ तक ढह जाते हैं?
वे इसलिए गिर जाते हैं क्योंकि उनको सांस लेने को जगह ही नहीं बची। जो पेड़ बाहर से 50 फुट का दिख रहा है उसकी जड़ें तो हमने 5 फुट नीचे भी नहीं जाने दीं। उसके आस-पास टाइलें लगा दीं। मिट्टी से नफरत की जाने लगी है, वह गंदगी दिखने लगी। पार्कों में टाइलें लगाकर 'जॉगिंग ट्रैक'बना दिए गए हैं। टाइलें भी मिट्टी की नहीं, बढि़या चमचमाती लगाएंगे। मिट्टी की टाइलों से बंगाल में कई मंदिर बने हैं। ऐसी टाइलें पानी को जमीन में जाने से नहीं रोकतीं। ऐसे बेसोचे-समझे विकास की कीमत चुकानी पड़ती है, हमारे गांव भी डूबते हैं और शहर भी। हमें मानना ही पड़ेगा कि तालाब के बिना जीवन नहीं है। नदियों की बात करें तो भूगोल ने हमें उनके अलग-अलग रास्तों पर रहने की बात समझाई है।











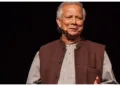
टिप्पणियाँ