|
22 मई अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस
– निर्भय कर्ण-
हमारी पृथ्वी काफी बेहतरीन व सुन्दर है जिसमें सभी जीव-जंतुओं का अपना-अपना अहम योगदान व महत्ता है। हरे-भरे पेड़-पौधे, विभिन्न प्रकार के जीव-जंतु, मिट्टी, हवा, पानी, पठार, नदियां, समुद्र, महासागर, आदि सब प्रकृति की देन हैं, जो हमारे अस्तित्व एवं विकास के लिए आवश्यक हैं। पृथ्वी हमें भोजन ही नहीं वरन् जिंदगी जीने के लिए हर जरूरी चीजें मुहैया कराती है। असल में सभी जीवों व पारिस्थितिकी तंत्रों की विभिन्नता एवं असमानता ही जैव विविधता कहलाती है। इसलिए यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जैव विविधता का मानव जीवन के अस्तित्व में अहम योगदान है।
जैव विविधता से जहां सजीवों के लिए भोजन तथा औषधियां मिलती हैं वहीं उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त होता है। वैज्ञानिकों की मानें तो विश्व की 25000 चिन्हित वनस्पति प्रजातियों में से महज 5000 प्रजातियों का ही औषधि प्रयोग हो रहा है जिसके एक छोटे से अंश से ही हमारी खाद्यान्न की आपूर्ति हो रही है। इनमें से लगभग 1700 वनस्पतियांे को खाद्य के रूप में उगाया जा सकता है लेकिन मात्र 30 से 40 वनस्पति फसलों से ही पूरे विश्व को भोजन उपलब्ध हो पा रहा है। इस भोजन में से भी हम हर साल एक-तिहाई तैयार भोजन बरबाद कर देते हैं। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक, दुनियाभर में 4 अरब टन सालाना खाद्यान्न का उत्पादन होता है जिसमें से करीब 1-2 अरब टन खाना बरबाद होता है। यह उप-सहारा क्षेत्र में सालभर में पैदा होने वाले कुल अनाज के बराबर है।
दुनिया के 17 महत्वपूर्ण जैव विविधता संपन्न देशों में भारत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस विविधता को बनाये रखने के लिए वन एवं वन्य जीवों की रक्षा जरूरी है। यदि वनों की बात की जाए तो पुर्वानुमानों के अनुसार वन विनाश की मौजूदा रफ्तार अगर जारी रहती है तो सन् 2020 तक दुनिया की लगभग 15 प्रतिशत प्रजातियां धरती से लुप्त हो जायेंगी। पेड़ों की अंधाधुध कटाई एवं सिमटते जंगलों की वजह से भूमि बंजर और रेगिस्तान मंे तब्दील होती जा रही है जिससे दुनियाभर में खाद्य संकट का खतरा मंडराने लगा है। यूएनईपी के मुताबिक, विश्व में 50-70 लाख हेक्टेयर भूमि प्रतिवर्ष बंजर हो रही है वहीं भारत में ही कृषि-योग्य भूमि का 60 प्रतिशत भाग तथा गैर कृषि भूमि का 75 प्रतिशत गुणात्मक ह्नास में परिवर्तित हो रहा है। भारत में पिछले नौ सालों में 2़79 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र विकास की भेंट चढ़ गए जबकि यहां पर कुल वन क्षेत्रफल 6,90,899 वर्ग किलोमीटर है। वन न केवल पृथ्वी पर मिट्टी की पकड़ बनाए रखता है बल्कि बाढ़ को भी रोकता और मृदा को उपजाऊ बनाए रखता है। वहीं पीने योग्य पानी की उपलब्धता में भी लगातार कमी आ रही है। धरती पर उपलब्ध 1़40 अरब घन किलोमीटर पानी में से 97़5 फीसदी खारा पानी समुद्र में है और 1़5 फीसदी पानी बर्फ के रूप में है। इसमें से ज्यादा ध्रुवों एवं ग्लेशियरों में है जो लोगांे की पहुंच से दूर है। बाकी एक फीसदी पानी ही नदियों, तालाबों एवं झीलों में है लेकिन इस पानी का भी एक बड़ा भाग जो 60-65 फीसदी तक है खेती और औद्योगिक क्रियाकलापों पर खर्च हो जाता है। आंकड़ों पर गौर करें तो 60 प्रतिशत तक पानी इस्तेमाल से पहले ही बर्बाद हो जाता है।
वनों एवं अन्य तरह की जैव विविधता में जीव-जंतुओं का योगदान उल्लेखनीय है। भिन्न-भिन्न प्रकार के जीव-जंतुओं की प्रजाति में लगातार कमी आ रही है। अपने स्वार्थ के चलते मानव द्वारा किए गए प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के कारण बीते 40 सालों में पशु-पक्षियों की संख्या घट कर एक तिहाई रह गई है। आंकड़ों पर गौर करें तो पाएंगे कि 52,017 प्रजातियों में से 18788 लुप्त होने के कगार पर हैं। दुनिया के 5490 स्तनधारियों में से 78 लुप्त हो चुके हैं तो 188 अधिक जोखिम की सूची में है वहीं 540 प्रजातियों पर खतरा मंडरा रहा है और 792 अतिसंवेदनशील सूची में शामिल है। दिलचस्प बात यह है कि जब भी जीवों के संरक्षण की योजनाएं बनती हैं तो बाघ, शेर और हाथी जैसे बड़े जीवों के संरक्षण पर खास ध्यान दिया जाता है लेकिन पक्षियों के संरक्षण को अपेक्षित महत्व नहीं मिल पाता।
जैव विविधता को कमजोर करने में कई कारकों का हाथ है जिसमें से ग्लोबल वार्मिंग भी प्रमुख है। ग्लोबल वार्मिंग ने मौसम को और भी मारक बना दिया है और आनेवाले वर्षों मंे मौसम में अहम बदलाव होने की पूरी संभावना है जिससे चक्रवात, लू, अतिवृष्टि और सूखे जैसी आपदाएं आम हो जाएंगी। धरती पर विद्यमान ग्लेशियर से पृथ्वी का तापमान संतुलित रहता है लेकिन बदलते परिवेश ने इसे असंतुलित कर दिया है।
लगातार तापमान में बढ़ोतरी ने जैव विविधता को संकट में ला खड़ा किया है। लगातार बढ़ते तापमान से ग्लेशियर पिघलने लगा है और वह दिन दूर नहीं जब पूरी पृथ्वी को जल प्रलय अपने आगोश में ले लेगा। दूसरी ओर हम अपने परिवेश को इतना दूषित करते जा रहे हैं कि जीना दूभर होता जा रहा है। ऐसा कोई तत्व शेष नहीं रहा जो प्रदूषित होने से बचा हो चाहे वायु, जल, भूमि प्रदूषण हो या फिर अन्य।
हम सभी जानते हैं कि पर्यावरण और प्राणी एक-दूसरे के पूरक हैं। पर्यावरण और प्रकृति के पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन से होने वाले दुष्प्रभावों से हमारी आबादी के मस्तिष्क पर चिंता की शिकन आना लाजिमी है जिसके लिए मानव जगत ही जिम्मेदार है। इतना सबके बावजूद मानव ने ही प्रकृति संरक्षण के प्रेरणादायी उदाहरण भी प्रस्तुत किये हैं, जिनसे जैव विविधता संरक्षण के प्रयासों को मजबूती मिली है। मानव का कर्तव्य बनता है कि अपने स्वार्थ को त्यागते हुए प्रकृति से निकटता बनाकर पृथ्वी को प्रदूषित होने से बचाए तथा विलुप्त होते जंगलों और उसमें रहने वाले पशु-पक्षियों की संपूर्ण सुरक्षा की जिम्मेदारी ले। वृक्षों की संख्या में इजाफा, जैविक खेती को प्रोत्साहन, माइक्रोवेव प्रदूषण में कमी करने जैसे अहम मुद्दों पर काम करने पर विशेष जोर देना होगा। मानव को अपनी गतिविधियों पर सोच-समझकर काम करना होगा जिससे कि इंसान प्रकृति से दुबारा जुड़कर उसका संरक्षण कर सके अन्यथा वह दिन अब ज्यादा दूर नहीं जब जैव विविधता पर मंडराता यह खतरा भविष्य में हमारे अस्तित्व पर भी प्रश्नचिह्न लगा दे। *








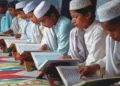



टिप्पणियाँ