|
भारत की संविधान सभा में इसके सदस्यों के बीच में सर्वाधिक विचार-विमर्श व टकराव भविष्य में ग्रामीण समुदायों तथा ग्राम पंचायतों की स्थिति के बारे में हुआ था। बारह खण्डों में प्रकाशित संविधान सभा की कार्यवाहियों को (9 दिसम्बर, 1946-26 जनवरी 1950) पढ़कर आसानी से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। वस्तुत: यह टकराव किसी एक मुद्दे पर न होकर दो चिंतन-धाराओं के बीच था। यह टकराव गांधी विचारकों तथा नेहरू समर्थकों के बीच था। यह मूलत: भारतीय चिंतन तथा पश्चात्य प्रभाव का टकराव था। यह अनुभव पर आधारित ग्राम स्वराज्य तथा देश के तेजी से शहरीकरण की कल्पना का टकराव था।
गांधी–नेहरू चिंतन में भेद
सर्वविदित है कि ब्रिटिश शासनकाल में भारत की ग्रामीण रचना, ग्रामीण समुदायों तथा ग्राम पंचायतों को समाप्त कर, भारतीय शासन प्रणाली को जड़ से उखाड़ने का प्रयत्न किया गया था। ग्रामों की आत्मनिर्भरता, स्वायत्तता तथा न्याय व्यवस्था खत्म कर दी थी। भूमि को व्यक्तिगत सम्पत्ति, कृषि का वाणिज्यकरण कर लोकमत का गला घोंट दिया था। गांधी जी ने 1909 में अपनी रचना 'हिन्द स्वराज्य' में जहां एक ओर तत्कालीन ब्रिटिश लोकतांत्रिक व्यवस्था की कटु आलोचना की वहीं भारत की प्रजा को चिंतन का आधार मानकर भारत के भविष्य के बारे में इसे 'ग्राम स्वराज्य' अथवा 'राम राज्य' का नाम दिया था। उन्होंने एक ओर ब्रिटिश संसद को 'वेश्या' तथा बांझ कहा तथा धन की बर्बादी कहा, दूसरी ओर रामराज्य को आदर्श राज्य की स्थापना कहा, जिसमें भारत के ग्रामीण समाज की पूरी भागीदारी हो। गांधीजी ग्राम केन्द्रित शासन व्यवस्था के प्रखर समर्थक थे। 1931 में जब वे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गये तब भी वहां उन्होंने ग्रामों को भारत की वास्तविक आत्मा बतलाया। इससे प्रेरित होकर ही लाखों ग्रामवासियों ने कांग्रेस के आन्दोलनों में बढ़ चढ़कर भाग लिया था।
इस संदर्भ में पं. नेहरू के विचार बिल्कुल भिन्न थे। वे पूरी तरह पाश्चात्य प्रभाव में रंगे थे। उन्होंने गांधीजी के 'हिन्द स्वराज्य' को पढ़ा था, पर वे उससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं थे। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार 1937 के चुनाव के समय भारतीय गांवों को निकट से देखा था। वस्तुत: वह उनके लिए 'भारत की खोज' थी। इसके बावजूद वे गांवों के प्रति आकर्षित नहीं हुए। उन्हें वे गन्दगी के ढेर लगते थे। इस सन्दर्भ में गांधी-नेहरू पत्र-व्यवहार अत्यन्त महत्वपूर्ण है। गांधी जी व नेहरू जी के पत्रों के अध्ययन से स्पष्ट है कि दोनों के विचारों में भारी अन्तर था। गांधी जी भारतीय संस्कृति तथा परम्पराओं के पोषक थे तथा नेहरू जी भारत के भविष्य में पूर्णत: पाश्चात्य रंग में रंगे हुए थे।
गांधीजी का संविधान
यहां यह उल्लेखनीय है कि 1944 में जेल से छूटने के पश्चात गांधीजी जी अपने को अकेला महसूस करने लगे थे। 2 अक्तूबर, 1947 को अपने जन्मदिवस पर प्रार्थना सभा में उन्होंने कहा था, 'अब तो मेरी कोई सुनता नहीं है। मैं कहूं कि तुम ऐसा करो तो कहते हैं नहीं, ऐसा हम नहीं करेंगे। ऐसे हालत में मेरे लिए जगह कहां है और मैं उसमें जिंदा रहकर क्या करूंगा?' इतना होने पर भी गांधी जी ने स्वतंत्र भारत के लिए स्वयं एक संविधान तैयार किया। यद्यपि यह वह समय था जब भारतीय संविधान सभा का भी कार्य करते हुए एक वर्ष से अधिक हो गया था। गांधी जी ने अपने संविधान में ग्राम स्वराज्य की बात कीं जिससे गांव आत्मनिर्भर तथा स्वायत्त हों तथा उसके प्रत्येक ग्रामीण की भागीदारी हो। उन्होंने सशक्त ग्राम पंचायतों की कल्पना की जिसमें संविधान का ढांचा नीचे से ऊपर की ओर हो, शासन शक्तियों का विकेन्द्रीयकरण हो। वे ग्राम स्वराज्य को रामराज्य कहते थे। उनके रामराज्य में गणतंत्रों की संघात्मक व्यवस्था थी जिसमें निचले स्तर पर प्रत्येक ग्रामीण जनसमूह एक स्वायत्तशासी इकाई का निर्माण करेगा। गांधीजी का मानना था कि लोकतंत्र तथा केन्द्रीयकरण की धाराओं में परस्पर अर्न्तविरोध है। गांधी जी ने एक बार लिखा था, 'केन्द्र में बैठे बीस व्यक्ति लोकतंत्र को कार्यान्वित नहीं कर सकते। लोकतंत्र का कार्यान्वयन नीचे से प्रत्येक ग्राम के लोगों द्वारा किया जायेगा। ऐसी व्यवस्था में ग्राम का प्रत्येक व्यक्ति जनसमूह के सार्वजनिक विषयों के प्रबंध में सक्रिय भाग लेगा। स्वराज्य थोड़े से जननेताओं के द्वारा राजनीतिक सत्ता के प्रयोग से नहीं मिलता, भले ही वे जनता द्वारा अपने प्रतिनिधि के रूप में चुने गये हो।' गांधी जी द्वारा निर्मित संविधान उनकी मृत्यु के पश्चात 7 फरवरी, 1948 को हरिजन में प्रकाशित हुआ।
संविधान सभा में गांव
दूसरी तरफ संविधान सभा में प्रत्येक मुद्दे पर कार्यान्वयन की दृष्टि से ड्राफ्ट कमेटी में ग्राम, ग्राम समुदाय, ग्राम पंचायत पर मुख्य चर्चा 4 नवम्बर, 1948 से हुई। इसमें संविधान सभा के सभी प्रमुख लोगों ने भाग किया। इस सन्दर्भ में भारतीय संविधान की ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष डा. बी.आर. अम्बेडकर ने तीन बातें कही। उन्होंने ब्रिटिश विद्वान मैटकाफ की इस टिप्पणी को बिल्कुल नकारा कि भारत के गांव छोटे-छोटे गणराज्य की भांति है। दूसरे, उन्होंने ग्राम को 'स्थानीय पिछड़ेपन, अज्ञानता की कोठरी, संकुचित मानसिकता तथा साम्प्रदायिकता से युक्त बतलाया तथा इसी कारण गांव को हटाकर व्यक्ति को इकाई मानने की बात कही (भाग सात पृ. 39, 4 नवम्बर 1948)। और तीसरे, उन्होंने कहा, 'वंश के बाद वंश लुढ़क गये। क्रांति के बाद क्रांति आई। हिन्दू, पठान, मुगल, मराठे, सिख, अंग्रेज- एक के बाद एक शासक रहे, पर ग्राम समुदाय वैसे ही रहे। कष्टों के दिनों में वे स्वयं सक्षम होने को तैयार होते, दुश्मन की सेना उनके गांव को लांघती होती, ग्राम समुदाय अपने पशुओं को ग्राम की दीवारों के अन्दर इकट्ठा रखते तथा दुश्मन सेना बिना व्यवस्था के पार चली जाती।'
उपरोक्त प्रश्न पर संविधान सभा के अधिकतर सदस्यों ने भाग लिया। इनमें से अधिकांश ने डा. अम्बेडकर के उपरोक्त तीनों तकर्ों में से किसी न किसी तर्क की आलोचना की। प्रो. शिव्वन लाल सक्सेना ने डा. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत चित्र को अस्वीकार करते हुए गांधीजी द्वारा प्रस्तुत रामराज्य की बात कही। अरुण चन्द्र गुहा ने गांधीजी के विचारों का समर्थन करते हुए मजबूत केन्द्र का भी समर्थन किया लेकिन उसके अंगों (ग्रामों) को कमजोर करने की आलोचना की। महावीर त्यागी ने अपनी व्यंग्यात्मक शैली में कहा आखिर गांवों को क्या मिला, केवल वोट का अधिकार। गोकुल सहाय भट्ट ने कटु भाषा में कहा कि 'यदि गांव को हटा दिया गया तो संविधान को ही हटा दिया जाना चाहिए।' टी. प्रकाशम का कथन था कि गांवों को भुलाकर हमने अनेक वर्षों के स्वतंत्रता संघर्ष को एक झटके में विस्मृत कर दिया।
क्यों है यह हाल?
एच.वी. कामथ ने उपरोक्त विषय पर विस्तृत चर्चा करते हुए कहा कि हमारा मैटकाफ के प्रति विश्वास नहीं है बल्कि गांधीजी के प्रति विश्वास है जिन्होंने हमें आजादी दिलवाई। एच. कृष्णास्वामी ने गांधीजी का उद्धरण देते हुए कहा कि 'भारत मर जायेगा यदि गांव समाप्त होते हैं। भारत तभी जीवित रह सकता है, यदि गांव जीवित रहते हैं।' श्री अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर तथा संविधान सभा के अध्यक्ष डा. राजेन्द्र प्रसाद जैसे विद्वानों ने भी ग्राम समुदायों तथा ग्रामों के विकास की ओर ध्यान देने को कहा।
इस सबके बावजूद संविधान सभा में गांधीजी के विचारों की हार हुई तथा नेहरू जी की जीत। यद्यपि अनेक सदस्यों – के. सन्थानम, ठाकुर दत्त भार्गव, सेठ गोविन्द दास आदि के प्रस्तावों तथा संशोधनों से ग्राम पंचायतों के गठन को राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कुछ स्थान दिया गया, परन्तु उनके पीछे कानूनों की वाध्यता न होने पर उनका महत्व कम ही रहा। सरकार की उदासीनता, उपेक्षा से स्थानीय संस्थाओं की चुनावी अनियमितताएं, लम्बे समय तक चुनाव न कराना, शक्ति न दिए जाने के कारण उपरोक्त नीति निर्देशक तत्वों का महत्व भी कम होता जा रहा है। स्वतंत्रता के 65 वर्ष बाद भी गांव गंदगी की ढेर बने हुए हैं। लोकसभा की अध्यक्षा श्रीमती मीरा कुमार के अनुसार देश के कुल 60,933 शहरों में सिर्फ 160 शहरों में 'सीवरेज' है, ग्रामीण क्षेत्रों में यह स्थिति शून्य है।
गांधीजी के नाम पर मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना) चलाई गई है, पर ग्राम विकास मंत्री जयराम रमेश के अनुसार भूमि सुधार का लाभ पाने लायक किसानों की संख्या देश में 80 फीसदी है, पर लाभ मात्र एक प्रतिशत का मिल रहा है। यहां तक कि 'मनरेगा दिवस' पर स्वयं सोनिया गांधी ने इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार को स्वीकार किया है। भारत के ग्राम आज भी वही खड़े हैं जहां 65 वर्ष पूर्व lÉä* डा. सतीश चन्द्र मित्तल








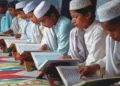



टिप्पणियाँ