|
भारत के सितारों की चमकद कन्हैया लाल चतुर्वेदीगत 12 से 27 नवम्बर तक चीन के ग्वांग्झू नगर में सम्पन्न हुए सोलहवें एशियाई खेलों में चीन ने फिर अपनी धाक जमा दी है। इस खेल-कुम्भ की आयोजन कुशलता और खेलों में श्रेष्ठ प्रदर्शन दोनों ही पक्षों में चीन ने अपनी छाप छोड़ी। रोमांचक उद्घाटन समारोह से लेकर नयनाभिराम समापन तक मेजबान देश ही पूरी तरह छाया रहा। जहां तक भारत का प्रश्न है, हमारे खिलाड़ियों ने भी अब तक का सर्वश्रे#ेष्ठ प्रदर्शन कर भविष्य के लिये आशा जगाई है। अक्तूबर माह में हुए राष्ट्रमण्डल खेलों में हमने पहली बार पदकों का शतक लगाते हुए 101 पदक जीते थे। एशियाई खेलों में भी पिछली उपलब्धियों को पीछे छोड़ते हुए हमने 64 पदक अपनी झोली में डाले, जिनमें 14 सोने के हैं।ग्वानडोंग चीन के दक्षिण-पूर्वी हिस्से का प्रांत है जो पहले क्वांटुंग नाम से जाना जाता था। इसकी राजधानी भी पहले केंटन के नाम से प्रसिद्ध थी, जो अब ग्वांग्झू हो गया है। इसी नगर में एशिया के 45 देशों का खेल-कुंभ आयोजित हुआ था। इससे पहले चीनी राजधानी बीजिंग में भी वर्ष 1990 में ग्यारहवें एशियाई खेल रखे गये थे। दक्षिण कोरिया, जापान और भारत भी दो-दो बार इन खेलों का आयोजन कर चुके हैं। सबसे पहले एशियाई खेल भारत में ही वर्ष 1951 में सम्पन्न हुए थे। वास्तव में एशिया के सभी देशों के बीच एक खेल प्रतियोगिता की कल्पना भारत ने ही की थी और इसी के परिणामस्वरूप “एशियन एथलेटिक फेडरेशन” का गठन दिल्ली में हुआ और पहले खेलों का दायित्व भारत को मिला। इसी के साथ एशियन गेम्स फेडरेशन भी बना, जो एशियाई खेलों की विधिवत् आयोजक बना। 1981 में “एशियाई ओलम्पिक परिषद” (ओलम्पिक कौंसिल ऑफ एशिया) बना। दिल्ली में अगले वर्ष हुए एशियाई खेल इसी परिषद के तत्वावधान में हुए और उस के बाद से यही इन खेलों का आयोजन कराती है।ग्वांग्झू में कुल 35 स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा दिखाने के लिये एशिया के 9704 खिलाड़ी एकत्रित हुए। दाव पर 477 स्वर्ण पदक सहित 1577 पदक थे, जिनमें से आधे से अधिक चीन, दक्षिण कोरिया तथा जापान ने ही झटक लिये। स्वर्ण पदकों में दोहरा शतक लगाने से चीन एक पदक से चूक गया। 199 स्वर्ण पदकों सहित अतिथेय देश ने 416 पदकों पर अधिकार जमाया, अर्थात् एक चौथाई से अधिक पदक अकेले चीन ने जीते । दक्षिण कोरिया ने 76 सुनहरे पदकों के साथ 232 और जापान ने 48 सोने के पदकों के साथ 216 पदक अपनी झोली में डाले। चीन की उपलब्धि का महत्व इसलिये और बढ़ जाता है कि पहले एशियाई खेलों में चीन ने भागीदारी ही नहीं की, जब कि मनीला (फिलीपींस) में 1956 के खेलों में इसने मात्र दो स्वर्ण पदक जीते थे।भारत ने इस बार चार-चार एशियाई खेलों के आयोजक थाईलैंण्ड ( बैंकाक में वर्ष 1966,70,74 तथा 98 में ये खेल हुए थे) को पीछे धकेल कर छठा स्थान प्राप्त किया। इस प्रकार नई दिल्ली में जीते 57 पदकों का आंकड़ा पार करते हुए हमारे खिलाड़ियों ने पहली बार 14 स्वर्ण पदक अपने नाम किये। एशियाड की 31 (कुल 35) स्पर्धाओं में चमक बिखेरने के लिये भारत से 843 प्रतिभागियों का भारी-भरकम दल गया था, जिसमें 609 खिलाड़ी तथा शेष उनके प्रशिक्षक व खेल अधिकारी थे। लेकिन चीन, कोरिया या जापान से यदि तुलना की जाये तो इस बार का हमारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी उनकी तुलना में कहीं नहीं ठहरता। कजाकिस्थान जैसा छोटा सा देश ही हम पर भारी पड़ा जिसकी जनसंख्या मात्र डेढ़ करोड़ है और जो बीस वर्ष पहले ही एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया है। फिर भी हमारी उपलब्धि इसलिये प्रशंसनीय है कि क्रिकेट के एकाधिकार व चकाचौंध, गर्हित राजनीति और भ्रष्ट तंत्र के बाद भी खिलाड़ियों ने अपने परिश्रम और समर्पण भाव से देश का नाम रोशन किया। राजनीति का एक उदाहरण महिला मुक्केबाज मैरी कॉम हैं। उनकी प्रतिभा में कोई संदेह नहीं है, किन्तु उनका वर्ग 48 किलो का है अर्थात् इस भार के वर्ग में वे विश्व चैम्पियन हैं। लेकिन उन्हें 51 किलो के वर्ग में ग्वांग्झू भेजा गया, इस वर्ग की प्रतिभावान मुक्केबाज सरिता का हक मार कर भेजा गया, केवल इसलिये कि मैरी कॉम को ही भेजना है। परिणाम यह हुआ कि यह विश्व चैम्पियन कांसे का पदक ही जीत सकी। ऐसे कई उदाहरण हैं और इन सब पक्षपातों और कठिनाइयों के बीच हमारे खिलाड़ी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, यह संतोष का विषय है। इसलिये सोलहवें एशियाई खेलों में भारत के प्रदर्शन के सम्बन्ध में दो -तीन विशेषतायें ध्यान में रखनी चाहिये। राष्ट्रमण्डल खेलों में हमें निशानेबाजी, कुश्ती तथा मुक्केबाजी में विशेष सफलता मिली थी, लेकिन एशियाई खेलों में हमारा प्रदर्शन तीनों में ही उतने उच्च स्तर का नहीं रहा। निशानेबाजी में रंजन सोढ़ी “डबल ट्रेप” में एकमात्र स्वर्ण जीत पाये और कुश्ती में कांसे के पदक ही हमें मिल पाये। मुक्केबाजी में अवश्य विजेन्द्र कुमार राष्ट्रमण्डल खेलों की निराशा को भूल कर चोटी पर पहुंचे और विकास कृष्णन ने भी अपने मुक्कों से सुनहरा जौहर दिखाया। हमारे खिलाड़ियों ने जिस स्पर्धा में विशेष प्रतिभा दिखाई वे हैं-दौड़-कूद अर्थात् “एथलेटिक्स” की स्पर्धायें। दोहा और उससे पहले बूसान (द.कोरिया) के खेलों में हमें दौड़-कूद प्रतियोगिताओं में मात्र एक-एक सोने का पदक मिला था, पर इस बार हमें पांच स्वर्ण सहित 11 पदक प्राप्त हुए।इन स्पर्धाओं में भी महिलाओं ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। पांच में से चार स्वर्ण तो महिलाओं ने ही जीत लिये। प्रीजा श्रीधरन ने दस हजार मीटर की दौड़ में स्वर्ण तथा पांच हजार में रजत पदक प्राप्त किया। ऐसे ही कर्नाटक की अश्विनी ने 400 मीटर की बाधा दौड़ में प्रथम स्थान पर आकर इतिहास रच दिया। 4न्400 की रिले में भी भारत की उड़न परियों ने धाक जमाई, वहीं अनेक बाधाओं वाली “स्टीपलचेज” (3000 मीटर) में सुधा सिंह की स्वर्णिम दौड़ भी ऐतिहासिक रही। पुरुषों में जोसेफ अब्राहम ही बाधा दौड़ (400 मी.) में सुनहरा तमगा बटोर सके। इसका संदेश स्पष्ट है, कि एथलेटिक्स में हमारे पास प्रतिभाएं हैं, ये ग्रामीण क्षेत्रों में है, देश की लड़कियों में समर्पण और सफलता की ललक अधिक है और यदि इन प्रतिभाओं को ठीक से तराशा जाये तो हम भी खेलों के क्षेत्र में महाशक्ति बन सकते हैं। लेकिन इसके लिये क्रिकेट के मोहपाश से निकलना आवश्यक है। इस उबाऊ खेल पर अरबों रुपया खर्च किया जाता है, क्रिकेट खिलाड़ियों पर करोड़ों रुपयों की बरसात होती है और मीडिया में भी इसी की चर्चा रहती है। इतना पैसा एथलीटों व अन्य खेलों में लगाया जाये तो इसके चमत्कारी परिणाम मिल सकते हैं। जहां एशियाई खेल हुए थे, चीन के उस ग्वानडोंग प्रांत की आधी आबादी विभिन्न खेलों में भाग लेती है। अकेले बेडमिण्टन खेलने वालों की संख्या वहां तीस लाख है। इसीलिये बीजिंग ओलम्पिक में चीन ने 51 स्वर्ण पदक जीत कर विश्व को चमत्कृत कर दिया था। निष्कर्ष यह है कि, कई दिनों तक चलने वाले खेल “क्रिकेट” पर जाया किया जाने वाला पैसा अन्य खेलों पर लगे, खेलों की सुविधाएं उपलब्ध कराने में व्यय हो, यह वर्तमान की आवश्यकता है। पदक विजेताओं पर दृष्टि डालने से पता चलता है, कि हरियाणा के अतिरिक्त केरल, कर्नाटक और राजस्थान की ग्रामीण प्रतिभाओं ने इन खेलों में देश का मस्तक ऊंचा किया है। सीकर जैसे दूर-दराज के क्षेत्र के बजरंग लाल ताखड़ ने नौकायन में जो स्वर्ण पदक जीता, वह भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। राजस्थान की ही कृष्णा पूनिया ने तश्तरी फैंक में यद्यपि कांस्य ही प्राप्त किया, फिर भी यह उपलब्धि प्रशंसनीय है। ऐसी प्रतिभाओं के प्रोत्साहन और प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था की आवश्यकता है। पर स्थिति इसके विपरीत है। पुरुष कबड्डी, वर्ष 1990 के एशियाई खेलों से इन प्रतियोगिताओं में शामिल है। ग्वांग्झू में महिलाओं की कबड्डी को भी पहली बार स्थान दिया गया था । भारत ने दोनों में स्वर्ण पदक जीते। पुरुष वर्ग में जयपुर के नवनीत गौतम सभी मुकाबलों में खेले और बहुत अच्छा खेले, लेकिन यह अन्तरर्#ाष्ट्रीय खिलाड़ी आज भी दूरसंचार विभाग में चपरासी है, जब कि एक टेस्ट मैच खेलने वाले क्रिकेट खिलाड़ी को कम से कम बीस लाख रु. मिल जाते हैं। कृष्णा पूनिया को भी अपने खर्चे से अमरीका में प्रशिक्षण लेना पड़ा था । यह भी उल्लेखनीय है कि ग्वांग्झू में बैडमिण्टन, टेबल टेनिस तथा टेनिस में भी हमें अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई। सोमदेव ने टेनिस में अकेले दम पर दो स्वर्ण जीते, वहीं मीडिया की लाड़ली सानिया मिर्जा मिश्रित युगल में ही पदक जीत सकी। शेष दो, बैडमिण्टन और टेबल टेनिस में इस बार हम पिछड़ गये। वस्तुत: राष्ट्रमण्डल, एशियाई तथा ओलम्पिक खेल जैसी प्रतियोगिताओं में हर बार नई-नई स्पर्धाएं जुड़ती हैं। ताकतवर खेल संगठन अपने स्थानीय खेलों को बड़ी प्रतियोगिताओं में किसी न किसी प्रकार सम्मिलित करवा ही लेते हैं। उदाहरण के लिये जूडो, कराटे और ताइक्वांडो लगभग एक जैसे खेल हैं, लेकिन तीनों एशियाई खेलों में भिन्न-भिन्न स्पर्धाएं हैं। “सेपक तकरा” मलयेशिया का खेल है जो “वालीबॉल” की तरह है। अन्तर इतना ही है कि इसमें गेंद को दूसरे पाले में पैर से मार कर भेजा जाता है, लेकिन मलेशिया ने इसे एशियाई खेलों में शामिल करवा लिया। “बॉलिंग” और “बीच-बालीबाल” जैसे गली-मौहल्ले के खेल भी एशियाई खेलों में स्थान बना चुके हैं। लेकिन भारत सिर्फ कबड्डी को पहचान दिला पाया है और वह भी केवल एशियाई खेलों में। खो-खो और मलखम्भ ऐसे खेल है, जिन्हें उक्त सभी खेल-कुम्भों में शमिल किया ही जाना चाहिये। इसी प्रकार मिट्टी की कुश्ती की भी पहचान बननी चाहिये। सतोलिया और गिल्ली-डण्डा जैसे खेलों को परिष्कृत कर इन्हें भी अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाया जा सकता है । हमारे अपने खेलों को प्रोत्साहन मिलेगा तो देश में खेल का वातावरण बनेगा और खेल-प्रतियोगिताओं में पदकों की संख्या भी बढ़ेगी। याद रहे कि इस बार एशियाई खेलों में क्रिकेट भी एक स्पर्धा के रूप में था, लेकिन फिर भी, चीन में क्रिकेट नहीं खेला जाता। अमरीका, रूस, जर्मनी, कोरिया और जापान जैसे उन्नत राष्ट्र भी इसे नहीं खेलते। द11



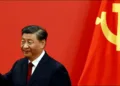








टिप्पणियाँ