पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक दार्शनिक, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री एवं अद्वितीय राजनीतिज्ञ थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी द्वारा प्रस्तुत दर्शन को ‘एकात्म मानववाद’ कहा जाता है, जिसका उद्देश्य एक ऐसा ‘स्वदेशी सामाजिक-आर्थिक मॉडल’ प्रस्तुत करना था जिसमें विकास के केंद्र में मानव हो। पंडित दीनदयाल उपाध्याय संपूर्ण राष्ट्र को एक परिवार के रूप में देखना चाहते थे। भारत को एक राष्ट्र के रूप में और यहाँ के निवासियों को नागरिक नहीं अपितु परिवार के सदस्यों के रूप में मानने वाला उनका विस्तृत दृष्टिकोण था। यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद का सिद्धांत है।
अपने एकात्म मानववाद को दीनदयाल जी सैद्धांतिक स्वरूप में नहीं, बल्कि आस्था के स्वरूप में स्वीकारते थे। उन्होंने इसे राजनीतिक सिद्धांत के रूप में नहीं; बल्कि हार्दिक भाव के रूप में जन्म दिया था। अपने एकात्म मानववाद के अर्थों को विस्तारित करते हुए उन्होंने कहा था कि- “हमारी आत्मा ने अंग्रेजी राज्य के प्रति विद्रोह केवल इसलिए नहीं किया कि दिल्ली में बैठकर राज करने वाले विदेशी थे, अपितु इसलिए भी कि हमारे दिन-प्रतिदिन के जीवन में, हमारे जीवन की गति में विदेशी पद्धतियाँ और रीति-रिवाज, विदेशी दृष्टिकोण और आदर्श अड़ंगा लगा रहे थे। हमारे संपूर्ण वातावरण को दूषित कर रहे थे, हमारे लिए साँस लेना भी दूभर हो गया था। आज यदि दिल्ली का शासनकर्त्ता अंग्रेज़ के स्थान पर हममें से ही एक, हमारे ही रक्त और मांस का एक अंश हो गया है तो हमको इसका हर्ष है, संतोष है; किंतु हम चाहते हैं कि उसकी भावनाएँ और कामनाएँ भी हमारी भावनाएँ और कामनाएँ जैसी ही हों। जिस देश की मिट्टी से उसका शरीर बना है, उसके प्रत्येक रजकण का इतिहास उसके शरीर के कण-कण से प्रतिध्वनित होना चाहिए।”
सर्वाधिक सूक्ष्म बोधवाक्य ‘जियो और जीने दो’ को ‘जीने दो और जियो’ के क्रम में रखने के देवत्वपूर्ण आचरण की सोच के कारण वे भारतीय राजनीति विज्ञान के उत्कर्ष का एक नया क्रम स्थापित कर गए। व्यक्ति की आत्मा को सर्वोपरि स्थान पर रखने वाले उनके सिद्धांत में आत्मबोध करने वाले व्यक्ति को समाज का शीर्ष माना गया। “आत्मबोध के भाव से उत्कर्ष करता हुआ व्यक्ति ‘सर्वे भवन्तु सुखिनः’ के भाव से जब अपनी रचनाधर्मिता और उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग करे तब ही एकात्म मानववाद का उदय होता है”- ऐसा वे मानते थे। देश और नागरिकता जैसे अधिकारिक शब्दों के संदर्भ में यह तथ्य पुनः मुखरित होता है कि उपरोक्त वर्णित व्यक्ति देश का नागरिक नहीं, बल्कि राष्ट्र का सेवक होता है।
पश्चिमी देशों का भौतिकवादी विचार जब अपने चरम की ओर बढ़ने की पूर्व दशा में था, तब उन्होंने इस प्रकार के विचार को सामने रखकर वस्तुतः पश्चिम से वैचारिक युद्ध का शंखनाद कर दिया था। उनके दौर में द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद वैश्विक स्तर पर विचारों और अभिव्यंजनाओं की स्थापना, मंडन-खंडन और भंजन की परस्पर होड़ चल रही थी। संपूर्ण विश्व- मार्क्सवाद, फासीवाद तथा अति उत्पादकता का दौर देख चुका था और महामंदी के दुष्परिणामों को भी भोग चुका था। वैश्विक सिद्धांतों और विचारों में अभिजात्य और नवअभिजात्य वर्ग की सीमाएं आकार ले चुकी थीं, तब संपूर्ण विश्व में भारत की ओर से किसी राजनीतिक सिद्धांत के जन्म की बात को किंचित असंभव और इससे भी बढ़कर हास्यास्पद ही माना जाता था। अपनी संकुचित सोच के कारण लोग यह मानने को तैयार ही नहीं होते थे कि भारत से कोई प्रगतिशील सोच जन्म ले सकती है।
औपनिवेशिक काल और औपनिवेशिक काल के बाद भी हम वैश्विक मंचों पर हेय दृष्टि और विचारहीन दृष्टि से देखे और माने जाते थे, यहाँ यह कहना गलत न होगा कि हमारा स्वातंत्रय्तोत्तर शासक वर्ग या राजनीतिक नेतृत्व जिस प्रकार पाश्चात्य शैलियों, पद्धतियों, नीतियों में डूबा, फँसा और मोहित रहा उससे हमारे प्रति यह हास्य और हेय भाव का दृष्टिकोण और भी बड़ा आकार लेता चला गया था। उस दौर में दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानवता के सिद्धांत की गौरवपूर्ण रचना और उद्घोषणा की थी।
1940 और 1950 के दशकों में विश्व में मार्क्सवाद से प्रभावित और लेनिन के साम्राज्यवाद से जनित ‘निर्भरता का सिद्धांत’ राजनीतिक शैली हो चला था। ‘निर्भरता का सिद्धांत’ यह है कि संसाधन निर्धन या अविकसित देशों से विकसित देशों की ओर प्रवाहित होते हैं और यह प्रवाह निर्धन देशों को और अधिक निर्धन करते हुए धनवान देशों को और अधिक धनवान बनाता है। इस सिद्धांत से यह तथ्य जन्म ले चुका था कि राजनीति में अर्थनीति का व्यापक समावेश होना ही चाहिए। संभवतः पंडित दीनदयाल जी ने इस सिद्धांत के उस मर्म को समझा, जिसे पश्चिमी जगत कभी समझ नहीं पाया। पंडित जी ने निर्भरता के इस शब्दों वाले कोरे सिद्धांत में में मानववाद नामक आत्मा की स्थापना की और इसमें से भौतिकवाद के राक्षस को बाहर ला फेंका।
राजनीति को अर्थनीति के साथ महीन रेशों से गूँथ देना और इसके समन्वय से एक नवसमाज के नवांकुर को रोपना और सींचना यही उनका मानववाद था। वे चाहते थे भौतिकता से दूर; किंतु मानव का श्रेष्ठतम उपयोग और उससे सर्वाधिक उत्पादन, फिर उत्पादन का राष्ट्रहित में उपयोग और राष्ट्रहित से अंत्योदय का ईश्वरीय कार्य, यही एकात्म मानववाद का सर्वोत्कृष्ट हितकारी रूप है। इस परिप्रेक्ष्य का अग्रिम रूप देखें तो स्पष्ट होता है कि उनके अर्थ के प्रभाव के माध्यम से वे विश्व की राजनीति में किस महत्त्वपूर्ण तत्त्व का प्रवेश करा देना चाहते थे।
‘एकात्म मानववाद’ और जनजातीय समाज
‘एकात्म मानववाद’ का यह विचार व्यक्ति बनाम समाज का नहीं है, बल्कि सामाजिक एकीकरण का विचार है। यह मनुष्य बनाम प्रकृति का विचार नहीं है, बल्कि मनुष्य और प्रकृति के बीच एकीकरण का विचार है। हमारे भारत में इसे ही ‘धर्म’ कहा जाता है – ‘यतो अभ्युदयनिः श्रेयससिद्धिः स धर्मः’। अर्थात धर्म वह है जो व्यक्ति को लौकिक उन्नति तथा आध्यात्मिक उन्नति (मोक्ष) दोनों प्रदान करने में मदद करता है। एकात्म मानववाद में यही व्यष्टि, समष्टि व परमेष्टि के बीच एकीकरण का विचार है।
जब हम जनजातीय समाज को केंद्र में रखकर इसका विचार करते हैं तो यह और भी प्रासंगिक हो जाता है, जनजातीय समाज भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपराओं का जीवंत उदाहरण है। जनजातीय समाज की जीवनशैली, परंपराएं, और प्रकृति के साथ सहजीवन निश्चित ही भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मूल हैं। जनजातीय समुदायों की अपनी भाषाएं, लोककथाएं, नृत्य, गीत और उत्सव उनकी सांस्कृतिक पहचान को दर्शाते हैं, जो एकात्म मानववाद की ‘सांस्कृतिक एकता’ की सोच के अनुरूप हैं।
हम सभी जानते हैं कि जनजातीय समाज में कोई भी सोच, कोई भी निर्णय व्यक्तिवादी नहीं होता जनजातीय समाज में सामूहिकता और सामुदायिक जीवन व्यवस्था को ही प्राथमिकता दी जाती है, जो पश्चिमी व्यक्तिवाद के विपरीत है, जनजातीय समाज में व्यक्ति परिवार, गोत्र और समुदाय के साथ अटूट रूप से जुड़ा होता है। और गहराई से देखने पर यह एकात्म मानववाद के सामाजिक एकीकरण के सिद्धांत को मजबूत करता है। जनजातियों की पंचायत व्यवस्था और सामुदायिक निर्णय प्रक्रिया भारतीय परंपरा की सामाजिक एकता को दर्शाती है, जो एकात्म मानववाद के विचार को ही प्रमाणित करती हैं।
जहाँ पश्चिमी विचार मनुष्य को प्रकृति, समाज और अध्यात्म से अलग करते हैं, वहीं एकात्म मानववाद इनके बीच एकीकरण की बात करता है, जनजातीय समाज की परम्पराओं में भी प्रकृति और मनुष्य के बीच कोई द्वंद्व नहीं है। वे प्रकृति को माता, नदियों को देवी, और पर्वतों को देवता मानते हैं। जनजातियों की जीवनशैली में सामुदायिकता और प्रकृति के प्रति सम्मान गहराई से समाया हुआ है। जनजातीय समाज में धर्मनिरपेक्षता का पश्चिमी रूप नहीं है बल्कि उनकी आध्यात्मिकता प्रकृति और सामुदायिक जीवन में ही निहित है, जो एकात्म मानववाद के धर्म के सिद्धांतों के अनुरूप है। जनजातीय समाज में धर्म का अर्थ मंदिर-पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रकृति, समुदाय और नैतिकता के साथ सामंजस्य है।
नागरिकता से परे होकर ‘राष्ट्र एक परिवार’ के भाव को आत्मा में स्थापित करना और तब परमात्मा की ओर आशा से देखना यह उनकी एकात्मता का शब्दार्थ है। इस रूप में हम राष्ट्रनिर्माण ही नहीं, अपितु उस परम वैभव की ओर भी जाएँ- यह भाव उनके सिद्धांत के एक शब्द ‘एकात्मता’ में प्राण स्थापित करता है। मानववाद वह है, जो ऐसी प्राणवान आत्मा से निस्सृत होकर एक शक्तिपुंज के रूप में सर्वत्र राष्ट्रभर में मुक्तभाव से बहे अर्थात अपनी क्षमता से और और प्राणपण से उत्पादन करे और राष्ट्र को समर्पित भाव से अर्पित कर दे एवं स्वयं भी सामंजस्य और परिवार बोध से उपभोग करता हुआ विकास-पथ की ओर अग्रसर रहे। एकात्मता में सराबोर होकर मानववाद की ओर बढ़ता यह एकात्म मानववाद-अपने इस ईश्वरीय भाव के कारण ही अंत्योदय जैसे परोपकारी राज्य के भाव को जन्म दे पाया।
इसके साथ ही संसाधनों को मानवीय आधार पर वितरण की न्यायसंगत व्यवस्थाओं को समर्पित करते हुए आगे बढें, यह अंत्योदय का प्रारंभिक बिंदु है, जबकि अंत्योदय का चरम वह है, जिसमें व्यक्ति एकदूसरे जुड़ा हुआ हो और निर्भर भी अवश्य हो किंतु उसमें न तो निर्भरता का भाव हो, न कभी हेय दृष्टि का भाव आए और न ही कभी देय दृष्टि का। इस प्रकार “अंत्योदय” पं. दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद के सहउत्पाद के रूप में जन्मा, इसे सहउत्पाद के स्थान पर एकात्म मानववाद के सिद्धांत का पुण्यप्रसाद कहना अधिक उपयुक्त होगा। इसी एकात्मता के फलस्वरूप जनजातीय समाज सुदूर वनक्षेत्रों में रहने के बाद भी भारतीयता से जुड़ा हुआ महसूस करता है और अन्त्योदय की इसी भावना के साथ हमारी केंद्र सरकार समर्पित भाव से उनके विकास को अपना दायित्त्व मानकर उनकी सेवा कर रही है।










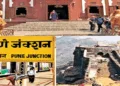







टिप्पणियाँ