अभी कुछ दिन पहले माननीय सरसंघचालक डाॅ मोहन भागवत ने कार्यकर्ता विकास वर्ग के समापन के अवसर पर एक भाषण दिया, जिसकी सर्वत्र चर्चा हो रही है। दरअसल यह भाषण अपने आपमें भारतीय राजनीति को भविष्य में किस दिशा में जाना चाहिए, इसकी कार्ययोजना का प्रारूप है। वर्तमान समय में राजनीतिक विद्वेष जिस निम्नतम स्तर पर पहुंचा है वह सभी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। सरसंघचालक जी ने अपने भाषण के माध्यम से उन सभी बातों के लिए सकारात्मक समाधान सुझाए हैं जो भारतीय लोकतंत्र के लिए चिंतनीय विषय हैं।
इसी भाषण में उन्होंने एक जगह कहा है कि ‘‘हम लोकमत का परिष्कार पहले भी करते आए हैं वैसा ही हमने इस चुनाव में भी किया।’’ लोकमत का परिष्कार विषय पर दीनदयाल उपाध्याय जी ने आज से लगभग 60 वर्ष से पहले एक लेख लिखा था। लेख के प्रारंभ में उन्होंने इस विषय का मंतव्य बताते हुए जवाहरलाल नेहरू का उल्लेख किया था क्योंकि राज्य पुनर्गठन के प्रश्न पर अलग-अलग जगह से अलग तरह की मांग उठने पर उनके सामने प्रश्न उपस्थित हुआ था कि जनता की इच्छा कौन सी समझी जाए।
दीनदयाल उपाध्याय जी लिखते हैं, ‘‘पंडित जी ने जो प्रश्न उपस्थित किया वह लोक राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, कारण लोकतंत्र राज्य जनता की इच्छाओं से चलता है किंतु किन्हीं दो व्यक्तियों की इच्छाएं एक सी नहीं हो सकतीं। फिर जहां करोड़ों मानवों का प्रश्न हो वहां राष्ट्र के सभी जन एक ही इच्छा करेंगे, यह सामान्यतया संभव नहीं।’’
‘‘वाद’’ की परंपरा:
इसी लेख में दीनदयाल उपाध्याय जी ने इच्छाओं, मान्यताओं और विश्वासों को ही सर्वोपरि मानकर अड़ने की प्रवृत्ति का विरोध किया है। उन्होंने हमारे शास्त्र की पुरानी उक्ति ‘‘वादे वादे जायते तत्व बोधः’’ का संदर्भ देते हुए कहा कि यदि हम दूसरे की बात ध्यानपूर्वक न सुनकर अपने ही दृष्टिकोण का आग्रह करेंगे तो ‘‘वादे वादे जायते कंठ शोषः’’ की उक्ति ही चरितार्थ होगी।
दीनदयाल जी ने लिखा है, ‘‘भारतीय संस्कृति इससे आगे बढ़कर वाद विवाद को तत्वबोध के साधन के रूप में देखती है। हमारी मान्यता है कि सत्य एकांगी नहीं होता, विविध कोणों से एक ही सत्य को देखा, परखा और अनुभव किया जा सकता है।’’ भारतीय संस्कृति वाद की परंपरा शाश्वत है और इसकी कई हजार वर्षों की ऐतिहासिक एवं शास्त्रीय साक्ष्य है। वाद का परिष्कृत और अभिजात्य स्वरूप शास्त्रार्थ है।
वाद-विवाद-वितंडावाद:
इस दृष्टि से दीनदयाल उपाध्याय जी ने लिखा है कि दूसरे की बात सुनना या उसके मत का आदर करना यानी उसके सामने झुक जाना नहीं है। वाद की परंपरा का किंचित विकृत स्वरूप विवाद है जो कि आज से कुछ वर्ष पूर्व तक हमारे देश की राजनीति पर हावी था। कई विवाद स्वयमेव थे कई विवाद पैदा किये गये थे। लेकिन अब हम विवाद से भी आगे बढ़ गये हैं और वितंडा के विकृृत स्वरूप में आ गये हैं। लोकतंत्र में अपनी बात को बलपूर्वक अथवा वितंडा खड़ा कर मनवा लेना तथा सामान्यजन में उसके प्रति गलत भाव पैदा करना, यह प्रवृति आज निरंतर बढ़ती नजर आ रही है। जिस लोकतांत्रिक तरीके से हमारे देश में आम चुनाव होते हैं उस प्रक्रिया को झुठला कर अथवा बहुमत का अपमान करके जनता में कैसे विभ्रम पैदा किया जा सकता है, इसके दृश्य आज सामान्य हो चले हैं।
वितंडा खड़ा करने के लिये आपको तथ्य और तर्कों की अधिक आवश्यकता नहीं होती। यह मायाजाल झूठ की बुनियाद पर रचा जाता है जो अतिनाटकीयता से प्रभावकारी हो जाता है। जमीनी सच्चाई से कोसों दूर सिर्फ अपने भ्रम में जीकर बिना वैचारिक आधार के वितंडा खड़ा करने वाले व्यक्ति राजनैतिक क्षेत्र में निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। विभिन्न सोशल मीडिया माध्यम जिसके अधिकांश उपभोक्ता युवा हैं ऐसे वितंडा दृश्यों को शुरुआत में मनोरंजन के लिये देखते सुनते पढ़ते हैं, लेकिन धीरे-धीरे वे उसी को सत्य मानने की भूल कर बैठते हैं। रील और मीम से बुना मनोरंजन का जाल कब राजनैतिक यथार्थ का रूप ले लेता है, समझ में ही नहीं आता। खेल खेल में रची गई चीजें ऐसे में राष्ट्र के विनाश का कारण बनने लगती हैं।
बहुमत का निरादर:
2024 के चुनाव परिणामों में पूर्ण बहुमत प्राप्त होने के बाद भी किस तरह एक गठबंधन को भ्रम फैला कर लगातार निहित स्वार्थ एवं दुराग्रह के कारण तिरोहित किया जा रहा है, यह देखना दुखदायी है। दीनदयाल उपाध्याय जी ने लोकमत के परिष्कार की व्यवस्था का उल्लेख करते हुए लिखा था कि लोकमत परिष्कार का कार्य वही कर सकता है जो लोकेषणाओं से ऊपर उठ चुका हो। इसके लिए उन्होंने भारत के वीतरागी द्वंद्वातीत संन्यासियों का उदाहरण दिया है। जिस समय दीनदयाल उपाध्याय जी ने यह लिखा उस समय का परिदृश्य अलग रहा होगा। आज जिस तरह की भाषा एवं अभिव्यक्ति का प्रयोग विभिन्न माध्यमों में अपना विरोध जताने के लिए किया जा रहा है वह निश्चित तौर पर हमारी संस्कृति के अनुरूप नहीं है। सोशल मीडिया पर जिस तरह की अभद्र भाषा तथा वाक्य प्रचारों का प्रयोग चुने हुए सम्मानित जनप्रतिनिधियों के लिए होता है वह संभवतः लोकमत के तिरस्कार को ही दिखाता है।
विरोध या वितंडा का यह भ्रम ऐसे लोग फैला रहे हैं जो लगातार संविधान की दुहाई देते हैं। ‘‘संविधान खतरे में है’’ के सहारे रचे गये झूठ का प्रपंच जब नहीं चला तो उन्होंने चुने हुये जनप्रतिनिधियों और बहुमत से चुनी गई सरकार को गढ़े गये झूठ के सहारे अपमानित करने का प्रपंच रचा है। सारी मर्यादायें लांघते हुये सीधे सीधे बहुमत का निरादर करते रहना दर्शाता है कि संविधान की दुहाई देने वालों में संवैधानिक परंपराओं के सम्मान की मानसिकता है ही नहीं।
विपक्ष या प्रतिपक्ष:
ऐसे में यह प्रश्न भी उठना स्वाभाविक है कि बहुमत का इस तरह निरादर करने का अधिकार इन्हें कौन देता है। यदि चुनावी प्रक्रिया को खेल भावना से लिया जाकर निकलने वाले परिणामों को सहज स्वीकारा जाता तो ऐसे दृश्य देखने को नहीं मिलते जो आज संसद के अंदर अथवा संसद के बाहर देखने को मिल रहे हैं।
सरसंघचालक डाॅ. मोहन भागवत जी ने अपने उद्बोधन में एक और महत्वपूर्ण बात कही थी और वह थी विपक्ष की जगह प्रतिपक्ष शब्द का प्रयोग। हमारे यहां प्रतिपक्ष विपक्ष कब हो गया, पता ही नहीं चला। हम ऐसी परंपरा से आते हैं जहां सभी के विचारों का आदर किया जाता है।
ऋग्वेद में कहा भी गया है, ‘‘समानो मंत्रः समिति समानी, समानं मनः सहचित्त मेषाम’’। हमारी न्यायालीन प्रक्रिया में दो पक्ष वादी और प्रतिवादी होते हैं। इसका आशय यही है कि पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों ही किसी भी विषय के न्यायपूर्ण एवं लोकहित की अवधारणा के अनुरूप समाधान के लिए काम करते हैं। सरसंघचालक जी ने विनोबाजी के संदर्भ से ‘सहचित्त मेषाम’’ शब्द की व्याख्या करते हुए भी सार रूप में यही कहा है कि .व्यक्ति व्यक्ति की प्रवृत्ति और प्रकृति अलग होने के बावजूद उनके चित्तों का मिलना एक स्वस्थ सामाजिक व्यवस्था का प्रतीक है।
प्रतिपक्ष या प्रतिवादी के माध्यम से सकारात्मक, तथ्यात्मक और विचार आधारित विरोध की अपेक्षा की जाती है। लेकिन जहां विरोध का आशय प्रतिरोध न होकर गतिरोध हो और जो विरोध केवल विरोध प्रकट करने या वितंडा खड़ा करने की नीयत से किया गया हो तो उसका सैद्धांतिक आधार ढूंढ़ना तो बेमानी है।
प्रतिद्वंदी या शत्रु:
विरोध प्रकट करने का जो तरीका इन दिनों दृष्टिगोचर हो रहा है वह दिखाता है कि यह उपक्रम प्रतिद्वंदिता का नहीं, शत्रुता का है। चुनाव प्रक्रिया में भी आमने सामने खड़े दो उम्मीदवारों का प्रतिद्वंदी कहा जाता है। हमारे देश की महान लोकतांत्रिक परंपरा में एक दूसरे के विचारों का आदर करना तथा एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करना शामिल रहा है। इसलिये चुनाव में जीत-हार का निर्णय हो जाने के बाद अपेक्षा की जाती है कि प्रतिद्वंदी आपस में मिलकर देश हित और समाज हित के कार्यों में साथ आगे बढ़ें। लेकिन देखा यह जा रहा है कि प्रतिद्वंदिता शत्रुता में परिणित होती जा रही है और सार्वजनिक माध्यमों पर निहायत व्यक्तिगत कटाक्षों और आरोपों के माध्यम से पूरे वातावरण को कलुषित करने का प्रयास किया जा रहा है।
इस सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में जब हम बेहद कटुतापूर्ण संवादों को अथवा लज्जास्पद भंगिमाओं को देखते हैं तो कहीं कहीं यह शंका भी हो उठती है कि ऐसा कहीं किसी और संस्कृति अथवा सभ्यता के इशारों पर तो नहीं हो रहा है। दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने लेख में लिखा है, ‘‘लोक राज्य तभी सफल हो सकता है जब एक एक नागरिक अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे और उसका निर्वाह करने के लिए क्रियाशील रहेंगे। जिस दल को लगता है कि आज नहीं तो कल हमारे कंधों पर राज्य संचालन का भार आ सकता है वह कभी अपने वादों में और व्यवहार में गैरजिम्मेदार एवं असंयत नहीं होगा।’’
हिंसा और भय की सृष्टि:
अभी तक यह विरोध विचारधारा और राजनैतिक कार्यकर्ताओं तक ही सीमित था। पिछले चुनावों तक राजनैतिक दलों पर हमला या उनके कार्यालयों पर हमला होते देखा गया।
लेकिन अभी देखने में आ रहा है कि इस प्रवृत्ति की चपेट में मतदाता भी आ गये हैं। पश्चिम बंगाल में किसी निश्चित पार्टी को वोट देने वाले मतदाताओं को जिस तरह हिंसा का शिकार बनाया जा रहा है और उनसे आजीविका छीनी जा रही है वह बेहद अमानवीय और अलोकतांत्रिक है। यह प्रतिशोध तो किसी भी सभ्य समाज में शोभा नहीं देता फिर भारत तो लोकतंत्र की जननी है, वहां ऐसा पाशविक व्यवहार कैसे संभव है। आश्चर्य की बात यह है कि संविधान की बात करने वाले और वैचारिक स्वतंत्रता की दुहाई देने वाले सभी लोग इस पाशविक व्यवहार पर चुप हैं।
आश्चर्य तो यह भी है कि पूरे भारत का बौद्धिक नेतृत्व करने का दंभ भरने वाले पश्चिम बंगाल में ऐसा हो रहा है और वहां का ‘‘भद्र समाज’’ यह सब चुपचाप देख रहा है। यदि यह सब ऐसे ही चला तो भविष्य में मतदाता मतदान करने के लिये कैसे प्रेरित होंगे।
दुख तो इस बात का भी है कि राजनैतिक शत्रुता और अपनी निष्कृष्ट सोच को सिर्फ राजनैतिक व्यक्तियों तक ही सीमित न किया जाकर उनके ऐसे परिवारजनों को भी निशाना बनाया जा रहा है, जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि हम सोच के धरातल पर इतने गिर जायें कि परिवारजनों पर अनर्गल आरोप लगाकर आसुरी आनंद लेते रहें।
विरोध और गतिरोध की प्रवृति एक बेहद खतरनाक दिशा में आगे बढ़ रही है। ऐसा न हो कि ये सारी बातें हम सबको एक ऐसे मार्ग पर ले जाये जहां से वापिस लौटने का रास्ता ही न हो यानि हमें च्वपदज व िछव त्मजनतद की ओर ले जाये। एक ऐसे बिंदु पर ले जाये जहां संवाद की संभावनायें शून्य हो जाये और शत्रुता चरमसीमा पर पहंुच जाये। बेहतर होगा कि चाहे पक्ष हो या प्रतिपक्ष, सभी इस खतरे को भांपते हुये कोई कारगर उपाय सोचें जिससे इस स्थिति से बचा जा सकते हैं और लोकतंत्र में आस्था तथा विश्वास को पुनः स्थापित किया जा सके।
आज आवश्यकता इस बात की है कि सिर्फ राजनैतिक दल ही नहीं बल्कि जनता भी इस बारे में गंभीर विचार करे तथा लोकमत के परिष्कार के लिए कोई न कोई ठोस कदम उठाए। अभी जिस तरह से वर्तमान दृश्य दिखाई दे रहा है उसमें लोकमत के तिरस्कार की प्रवृत्ति का ही बढ़ना संभव है, और यह भारत जैसे लोकतंत्र के लिए तो बिल्कुल भी लाभकारी नहीं है।




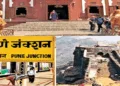












टिप्पणियाँ