किसी भी राष्ट्र का भविष्य शिक्षा पर निर्भर करता है। शिक्षा के अभाव में विकास की सारी बातें बेमानी हैं। पिछले 10 वर्षों में देश ने लगभग हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की, परंतु शिक्षा के क्षेत्र में उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना दिया जाना चाहिए था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रचार-प्रसार तो खूब हुआ, परंतु धरातल पर उसका क्रियान्वयन, प्रभाव और परिणाम दिखाई नहीं देता। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव-प्रचार के दौरान छोटे-बड़े सभी चैनलों पर दिए गए साक्षात्कार में राष्ट्रीय जीवन के अधिकांश विषयों एवं पहलुओं पर खुलकर बातें कीं। परंतु इसे विडंबना ही कहेंगे कि लोकतंत्र में प्रहरी की भूमिका का दावा करने वाले तमाम चैनलों में से किसी ने भी उनसे शिक्षा में सुधारों से जुड़े प्रश्न नहीं पूछे!
यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भावी पीढ़ी के भविष्य व निर्माण से जुड़ा विषय – समाज और सरकार की प्राथमिकता-सूची में सबसे निचले क्रम पर दिखाई देता है। राजनीतिक दलों के लिए जब सत्ता-प्राप्ति का सीमित और तात्कालिक लक्ष्य सर्वोपरि हो जाता है, तब विचारों के गठन और व्यक्ति-निर्माण का प्रश्न पीछे छूट जाता है। निःसंदेह मोदी सरकार ने पिछली सरकारों की तुलना में अधिक आईआईटी, आईआईएम, मेडिकल कॉलेज एवं केंद्रीय विश्वविद्यालय आदि खोले हैं। परंतु क्या केवल उतने भर से संतुष्ट हुआ जा सकता है? क्या हमारे विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों की शिक्षा की स्थिति, शिक्षण का स्तर, पाठ्यक्रम की गुणवत्ता, विश्व में उसकी साख एवं विश्वसनीयता, वर्षों से लंबित एवं रिक्त पदों पर नई नियुक्ति, मौलिक शोध एवं नवोन्मेष, कौशल एवं तकनीक की दक्षता, अध्यापकों के प्रशिक्षण, नियमित सत्र, अनुशासित एवं रचनात्मक शैक्षिक वातावरण, रोजगारपरक शिक्षा, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, पारदर्शी एवं कदाचारमुक्त परीक्षा तथा भारी धन खर्च कर भी विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने की बढ़ती लालसा आदि पर समाधानपरक काम नहीं किया जाना चाहिए?
पाठ्यक्रम में सुधार की दृष्टि से ठोस एवं निर्णायक पहल की जाना चाहिए। जहाँ बुनियाद बदलने की शर्त्त हो, क्या वहाँ केवल रंग-रोगन अथवा साज-सज्जा से काम चलाया जा सकता है? आवश्यकता संशोधन-संक्षिप्तीकरण की नहीं, अपितु राष्ट्र की चिर-प्रतीक्षित आकांक्षा के अनुरूप पाठ्यक्रम में आमूल-चूल परिवर्तन किए जाने की थी और है। क्या यह माना जाय कि सरकार, एनसीईआरटी एवं विभिन्न स्तरों पर पाठ्यक्रम का निर्धारण करने वाली समितियां और संस्थाएं योगेंद्र यादव, सुहास पल्शीकर एवं उन जैसे तमाम एजेंडाधारी-वामपंथी बुद्धिजीवियों के दबाव में परिवर्तन से हिचकिचा रही हैं? इन वामपंथी एवं तथाकथित बुद्धिजीवियों का तो काम ही विचारधारा विशेष का समर्थन और भारत की मूल प्रकृति, प्रवृत्ति, स्व और संस्कृति की उपेक्षा करना है।
समय की माँग और परिवर्तन को स्वीकार करना तो दूर, ये तो उसकी हर पदचाप पर हाय-तौबा मचाना प्रारंभ कर देते हैं। इन्होंने 8 जून, 2023 को भी नाम हटाने की धमकी देकर एनसीईआरटी पर दबाव बनाने की कोशिश की थी और अभी 17 जून, 2024 को नई सरकार के गठन के तुरंत बाद से ही इन्होंने पुस्तकों से अपना नाम हटाए जाने की राजनीति प्रारंभ कर दी। इनके विरोध और पुरस्कार वापसी गैंग के विरोध की प्रकृति व प्रवृत्ति में समानता देखी जा सकती है। इस बार तो योगेंद्र यादव व पल्शीकर ने धौंसपट्टी दिखाते हुए एनसीईआरटी के निदेशक पर मानहानि का मुकदमा दायर करने की धमकी तक दे डाली। वस्तुतः ये सभी प्रयत्न किसी भी कीमत पर पाठ्यक्रम में परिवर्तन न होने देने का राजनीतिक-रणनीतिक उपक्रम है। अब नेपथ्य में बैठे इनके ‘आका’ संसद से लेकर अन्य शैक्षिक-सार्वजनिक मंचों पर इनके सुर-में-सुर मिलाते हुए एक राग अलापेंगे।
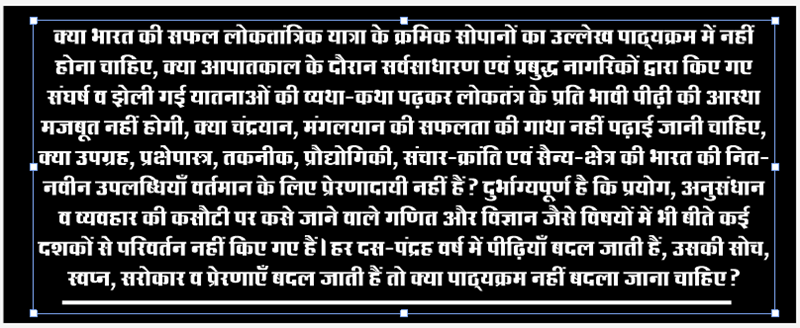
दरअसल, योगेंद्र यादव व सुहास पल्शीकर जैसे वामपंथी विद्वानों का व्यवस्था के कार्य में विघ्न डालना तथा सरकार के कामकाज में रोड़े अटकाना स्वभाव व अतीत है। इन्हें पाठ्यक्रम परामर्शदात्री समिति में सम्मिलित किए जाने की एनसीईआरटी की विवशता समझ से परे है। ऐसा भी नहीं है कि ये सामाजिक विज्ञान विषय के एकमेव मूर्द्धन्य विद्वान अथवा विशेषज्ञ हों कि समिति में इनके न होने से अनर्थ हो जाएगा या देश मौलिक एवं महानतम ज्ञान व चिंतन से वंचित रह जाएगा! अच्छा तो यह होगा कि एनसीईआरटी को ऐसे बौद्धिक ‘खेमेबाजों’ एवं ‘गिरोहों के सरगनाओं’ से स्वतःप्रेरणा से मुक्त हो जाना चाहिए, अन्यथा ऐसे पूर्वाग्रही, हठधर्मी, परिवर्तन-विरोधी ‘खेमेबाज’ उसके विरुद्ध नकारात्मक अभियान चलाते रहेंगे। इनके दोहरेपन की पराकाष्ठा यह है कि ये सांप्रदायिकता के प्रति विद्यार्थियों को सजग करने के नाम पर अबोध-अपरिपक्व बच्चों को जहां गोधरा कांड एवं अयोध्या के विवादित ढाँचे का ध्वंस पढ़ाए जाने की पैरवी करते हैं, वहीं 1984 के सिख विरोधी दंगे, विभाजन काल में मुस्लिम लीग और उसके अनुयायियों द्वारा किए गए भीषण नरसंहार, इस्लामिक आक्रांताओं द्वारा तोड़े गए असंख्य मंदिर, जलाए गए तमाम पुस्तकालय और तलवार के बल पर चलाए गए मतांतरण-अभियान पर नितांत मौन साध जाते हैं।
जहाँ तक पाठ्यक्रम परिवर्तन की बात है तो क्या इसमें भी कोई दो राय हो सकती है कि भाषा, साहित्य, इतिहास, राजनीति शास्त्र, दर्शन जैसे मानविकी के विभिन्न विषयों के माध्यम से सांस्कृतिक एकता एवं अखंडता को मजबूती मिलनी चाहिए, भारतीय ज्ञान-परंपरा को पोषण मिलना चाहिए, अस्तित्ववादी विमर्श एवं विभाजनकारी प्रवृत्तियों पर विराम लगना चाहिए, सहयोग, समन्वय, संतुलन, सामाजिकता, संवेदनशीलता एवं देशभक्ति जैसे मूल्यों को प्रश्रय एवं प्रोत्साहन मिलना चाहिए, भारतीय संस्कृति में व्याप्त बहुलता, शांति एवं सह-अस्तित्व के मूल स्रोत की खोज व पहचान की जानी चाहिए? कैसी विचित्र विडंबना है कि हमारे बौद्धिक-राजनीतिक-अकादमिक विमर्श में ‘ भारत वर्ष में व्याप्त विविधता में एकता’ का उल्लेख तो भरपूर किया जाता है, पर उस एकत्व को पोषण देने वाले मूल्यों, मान्यताओं, परंपराओं, प्रमुख घटकों, मंदिरों, मठों, तीर्थों, त्योहारों आदि की कोई चर्चा नहीं होती?
क्या पाठ्यक्रम में इन्हें यथोचित स्थान नहीं मिलना चाहिए? कौन नहीं जानता कि इतिहास की हमारी पाठ्यपुस्तकों में विदेशी आक्रांताओं की अतिरंजित विवेचना की गई है, भारतीयों के साहस, संघर्ष एवं प्रतिरोध को अपेक्षाकृत कम महत्त्व दिया गया है, संपूर्ण देश के वैशिष्ट्य एवं गौरवशाली अध्यायों की अपेक्षा केवल दिल्ली-केंद्रित इतिहास को केंद्र में रखा गया है तथा देश के अमर सपूतों, बलिदानी धर्मरक्षकों, महान संतों, समन्वयवादी समाज-सुधारकों, साहसी क्रांतिकारियों, राष्ट्रनिष्ठ स्वतंत्रता सेनानियों को नेपथ्य में रख, दो-चार का महिमामंडन किया गया है! क्या यह सत्य नहीं कि हमारी शिक्षा-व्यवस्था व पाठ्य-सामग्रियों में श्रद्धा, आस्था एवं विश्वास पर संदेह, अनास्था एवं अविश्वास को वरीयता दी गई है। उसमें अधिकार भाव की प्रबलता है, कर्त्तव्य-भावना गौण है, नैतिक मूल्यों एवं संस्कारों का अभाव है तथा सफलता एवं प्रतिस्पर्द्धा का प्राधान्य है?
औपनिवेशिक मानसिकता, अस्मितावादी विमर्श एवं वर्गीय चेतना के नाम पर हीन भावनाओं, अलगाववादी वृत्तियों तथा पारस्परिक मतभेद, असहमति एवं संघर्ष को शिक्षा के माध्यम से पाला-पोसा-बढ़ाया गया है। मूल बनाम बाहरी, उत्तर बनाम दक्षिण, राष्ट्रभाषा बनाम क्षेत्रीय भाषा, स्त्री बनाम पुरुष, व्यक्ति बनाम समाज, वर्गीय/जातीय/सामुदायिक अस्मिता बनाम राष्ट्रीय अस्मिता, परंपरा बनाम आधुनिकता, नगरीय बनाम ग्रामीण, मजदूर बनाम किसान, गरीब बनाम अमीर, उपभोक्ता बनाम उत्पादक, उद्योगपति बनाम सर्वहारा, मनुष्य बनाम प्रकृति, विकास बनाम पर्यावरण जैसी मिथ्या एवं कृत्रिम लड़ाइयाँ शिक्षा, साहित्य, कला व संस्कृति के माध्यम से खड़ी की गईं हैं।
परिवार, समाज एवं राष्ट्र की विभिन्न इकाइयों को परस्पर विरोधी मानने वाली ऐसी खंडित एवं विभेदकारी दृष्टि के स्थान पर, क्या शिक्षा-व्यवस्था में समन्वय और समग्रता पर आधारित सनातन दृष्टि को स्थान नहीं मिलना चाहिए? सच तो यह है कि हमारी पूरी शिक्षा-व्यवस्था व पाठ्य-सामग्रियों में जोड़ने वाले तत्त्वों का अभाव है और तोड़ने वाले तर्कों, कारकों, धारणाओं, पूर्वाग्रहों का प्रभाव है। इतना ही नहीं, हमारी आधुनिक शिक्षा की दृष्टि में रामायण-महाभारत गल्प हैं, वेद-वेदांग-गीता-उपनिषद-षड्दर्शन वायवीय एवं पारलौकिक हैं, भारत विभिन्न राष्ट्रीयताओं एवं अनेक संस्कृतियों का गठजोड़ है। अब कोई बताए कि ऐसे पाठ्यक्रमों को पढ़कर कैसे नागरिक, कैसे मतदाता, कैसे नौकरशाह, कैसे राजनेता, कैसे न्यायाधीश तैयार होंगें? पराए राग-रंग व सोच में आकंठ डूबे लोगों से स्व के साक्षात्कार व भारत के बोध की भला क्या और कितनी उम्मीद की जा सकती है? क्या यह भी बताने की आवश्यकता है कि स्वतंत्र भारत की अनेक गौरवशाली उपलब्धियाँ पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए जाने की बाट जोह रही हैं?
क्या भारत की सफल लोकतांत्रिक यात्रा के क्रमिक सोपानों का उल्लेख पाठ्यक्रम में नहीं होना चाहिए, क्या आपातकाल के दौरान सर्वसाधारण एवं प्रबुद्ध नागरिकों द्वारा किए गए संघर्ष व झेली गई यातनाओं की व्यथा-कथा पढ़कर लोकतंत्र के प्रति भावी पीढ़ी की आस्था मजबूत नहीं होगी, क्या चंद्रयान, मंगलयान की सफलता की गाथा नहीं पढ़ाई जानी चाहिए, क्या उपग्रह, प्रक्षेपास्त्र, तकनीक, प्रौद्योगिकी, संचार-क्रांति एवं सैन्य-क्षेत्र की भारत की नित-नवीन उपलब्धियाँ वर्तमान के लिए प्रेरणादायी नहीं हैं? दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रयोग, अनुसंधान व व्यवहार की कसौटी पर कसे जाने वाले गणित और विज्ञान जैसे विषयों में भी बीते कई दशकों से परिवर्तन नहीं किए गए हैं। हर दस-पंद्रह वर्ष में पीढ़ियाँ बदल जाती हैं, उसकी सोच, स्वप्न, सरोकार व प्रेरणाएँ बदल जाती हैं तो क्या पाठ्यक्रम नहीं बदला जाना चाहिए?
उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अध्ययन-अध्यापन की भाषा के रूप में मातृभाषा एवं भारतीय भाषाओं की पुरजोर पैरवी की गई है। शिक्षाविदों ने इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आत्मा के रूप में चिह्नित-प्रतिपादित किया है। परंतु अभी तक इस दिशा में किसी स्तर पर कोई ठोस काम नहीं हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 में प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने तथा माध्यमिक स्तर पर दो राष्ट्रीय (नैटिव) एवं एक विदेशी (फॉरेन) और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर एक भारतीय (नैटिव) एवं एक विदेशी (फॉरेन) भाषा पढ़ाए जाने की संस्तुति की गई है, परंतु विभिन्न बोर्डों की ओर से इस दिशा में अभी तक कोई दिशानिर्देश (गाइडलाइंस) नहीं जारी किए गए हैं।
यथार्थ यह है कि हिंदी भाषी राज्यों में कुकरमुत्ते की तरह अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खुलते चले जा रहे हैं। कई निजी विद्यालयों में तो स्थिति इतनी भयावह है कि वहाँ न केवल हिंदी बोलने पर प्रतिबंध है, अपितु दंड का भी प्रावधान है। उच्च शिक्षा की कौन कहे, ग्यारहवीं-बारहवीं में भी अधिकांश छात्र हिंदी को एक विषय के रूप में नहीं चुनते हैं, क्योंकि उनके पास हिंदी के विकल्प के रूप में अधिक अंक दिलाने वाले अनेक विषयों के विकल्प उपलब्ध हैं। उन्हें हिंदी का पाठ्यक्रम रोचक, ज्ञानवर्द्धक, रोजगारोनुकूल एवं परिवेशगत नहीं लगता। चूँकि हिंदी भाषा व साहित्य को छोड़कर शेष सभी विषयों की पढ़ाई अंग्रेजी में कराई जाती है, इसलिए हिंदी लिखना भी उन्हें कठिन जान पड़ता है।
वहीं जेईई, नीट, यूपीएससी, क्लेट, कैट, सीडीएस, एनडीए जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में पाठ्य-सामग्रियों का अभाव और प्रश्नपत्रों का प्रारूप भी नई पीढ़ी को उनसे दूर ले जाता है। घिसी-पिटी परिपाटी, नौकरशाही एवं राजनीतिक दलों के निहित स्वार्थ तथा सरकार की इच्छाशक्ति की कमी के कारण भारतीय भाषाओं की उपेक्षा का क्रम यथावत जारी है। हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं की स्थिति में तब तक अपेक्षित सुधार नहीं लाया जा सकता, जब तक कि उन्हें विद्यालयी शिक्षा में अनिवार्यतः लागू नहीं किया जाता। विभिन्न स्तरों की परीक्षा-पद्धत्ति, प्रश्नपत्र के प्रारूप, मूल्यांकन की प्रक्रिया आदि में अनेक सुधार अपेक्षित एवं अत्यावश्यक हैं।
प्रश्नपत्र लीक होने की समस्या दिन-प्रतिदिन विकराल रूप धारण करती जा रही है। नीट और नेट का ज्वलंत उदाहरण हमारे सम्मुख है। इस प्रकार की घटनाओं के कारण विद्यार्थियों एवं अभिभावकों में व्यवस्था के प्रति अनावश्यक असंतोष पनपता है। चाहे वह राज्यों की सरकार हो या केंद्र की, उन्हें विद्यार्थियों-परीक्षार्थियों के प्रति अतिरिक्त संवेदना दर्शानी होगी और व्यवस्था में व्याप्त ऐसे सभी छिद्रों को अनिवार्यतः बंद करना होगा। संयोग से कुछ दिनों पूर्व ही किए गए मंत्रिमंडल के गठन में निरंतरता का विशेष ध्यान रखा गया है। निःसंदेह इससे शिक्षा-क्षेत्र में भी सुधारों को गति एवं दिशा मिलेगी, नीतियों के क्रियान्वयन में सुविधा होगी तथा समाधान को बल मिलेगा।


















टिप्पणियाँ