ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्नल जोसेफ बोडेन ने भारतीय शास्त्रों के विकृतिकरण के लिए भारी भरकम धनराशि की व्यवस्था की थी। साथ ही, संस्कृत अध्ययन पीठ की स्थापना के लिए अपनी वसीयत में स्पष्ट लिखा था-

पैसिफिक विश्वविद्यालय समूह (उदयपुर) के अध्यक्ष-आयोजना व नियंत्रण
प्राचीन भारतीय संस्कृत ग्रंथों के विकृतिकरण के घोषित लक्ष्य से गठित आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की बोडेन अध्ययन पीठ को 200 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जोसेफ बोडेन की 15 अगस्त, 1811 की वसीयत से 1827 में आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की यह संस्कृत अध्ययन पीठ अस्तित्व में आई थी। इसका उद्देश्य संस्कृत शास्त्रों के प्रति भारतीय समाज में अश्रद्धा निर्माण एवं उसके जरिये देश में जातीय, भाषायी व क्षेत्रीय विद्वेष उत्पन्न करने के लिए वेद सहित संस्कृत साहित्य का व्यापक रूपांतर और विकृतिकरण करना था। आक्सफोर्ड के स्नातकों के मतदान से इस अध्ययन पीठ के अध्यक्ष का चुनाव भी ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा ही किया जाता था, जो इन उद्देश्यों के प्रति प्रतिबद्धता जताते थे। प्रथम दृष्टया यह बात अविश्वसनीय लगती है, पर कर्नल जोसेफ बोडेन की वसीयत, तत्संबंधी आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के 1827 के अध्यादेश के प्रावधान एवं बोडेन पीठ के अभ्यर्थियों की इस पद की दावेदारी के लिए जारी घोषणापत्रों के उद्धरण इसके प्रमाण हैं।
क्या थी बोडेन की वसीयत?
ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्नल जोसेफ बोडेन ने भारतीय शास्त्रों के विकृतिकरण के लिए भारी भरकम धनराशि की व्यवस्था की थी। साथ ही, संस्कृत अध्ययन पीठ की स्थापना के लिए अपनी वसीयत में स्पष्ट लिखा था, ‘‘मैं अपनी समस्त संपदा और उसकी निष्पत्तियां, उनका अब तक का संग्रह, यदि कोई हो, तथा स्टॉक्स, निधियां, प्रतिभूतियां आदि आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को देता हूं और वसीयत करता हूं कि इसे उस निकाय द्वारा उक्त विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज में शांस्क्रीट (संस्कृत) भाषा में एक प्रोफेसरशिप के निर्माण और बंदोबस्ती के लिए निवेशित और विनियोजित की जाए, (क्योंकि यह मेरी) राय है कि उस भाषा का अधिक सामान्य और महत्वपूर्ण ज्ञान मेरे देशवासियों को भारत के मूल निवासियों को, उनके बीच पवित्र ग्रंथों के ज्ञान का प्रसार करके, अन्य सभी तरीकों से अधिक प्रभावशाली ढंग से, ईसाई मत में कन्वर्ट कराने में सक्षम बनाने का एक साधन होगी।’’
वसीयत में स्पष्ट लिखा है कि भारत के लोगों के बीच संस्कृत के पवित्र ग्रंथों का भ्रामक ज्ञान फैलाकर उन्हें ईसाई मत में परिवर्तित करना था। विश्वविद्यालय ने नवंबर 1827 में बोडेन की वसीयत को स्वीकार किया और 1832 में हैमेन विल्सन उसका पहला अध्यक्ष चुना गया। उसकी मृत्यु के बाद 1860 में एक कड़े मुकाबले में मैक्समूलर को पराजित कर मोनियर विलियम्स इस अध्ययन पीठ का दूसरा अध्यक्ष बना था। मोनियर ने अपने चुनावी घोषणापत्र में कहा था, ‘‘यदि मैं बोडेन संस्कृत अध्ययन पीठ का अध्यक्ष चुना गया, तो अपनी पूरी ऊर्जा उस एक उद्देश्य में लगाऊंगा, जिससे भारतीयों के कन्वर्जन में अंग्रेजों को सक्षम बनाने के साधन के रूप में संस्कृत साहित्य का उपयोग किया जा सके और समग्र संस्कृत साहित्य ईसाई मत को बढ़ावा देने योग्य बने।’’ इसके बाद वह 200 मतों से विजयी हुआ था।
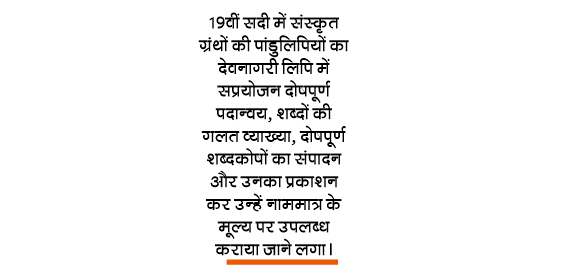 वहीं, मैक्समूलर ने अपने घोषणापत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्वयं को ऋग्वेद के संपादन का काम सौंपे जाने का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके अध्ययन व भाष्य के संपादन के बिना मिशनरी हिंदू धर्म की शिक्षाओं के बारे में पूरी तरह से नहीं जान सकती, जिससे उनके काम में बाधा आती है। मेरे विचार से वैदिक ज्ञान व ब्राह्मण ही मिशनरी प्रयासों में गंभीर बाधा साबित हुए हैं। इस बाधा को दूर करने के लिए मेरे द्वारा संपादित ऋग्वेद संस्करण तीन खंडों में प्रकाशित हो चुके हैं और तीन प्रकाशित होने हैं। मेरी दृष्टि में उस देश (भारत) में अभी भी प्रचलित मूर्ति पूजा की प्राचीन प्रणालियों को उखाड़ फेंकने और वैदिक मान्यताओं के बीच ईसायत को स्थापित करने के प्रयासों में मेरे प्रकाशनों से सभी मिशनरियों को अपूर्व सहायता मिलेगी।
वहीं, मैक्समूलर ने अपने घोषणापत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्वयं को ऋग्वेद के संपादन का काम सौंपे जाने का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके अध्ययन व भाष्य के संपादन के बिना मिशनरी हिंदू धर्म की शिक्षाओं के बारे में पूरी तरह से नहीं जान सकती, जिससे उनके काम में बाधा आती है। मेरे विचार से वैदिक ज्ञान व ब्राह्मण ही मिशनरी प्रयासों में गंभीर बाधा साबित हुए हैं। इस बाधा को दूर करने के लिए मेरे द्वारा संपादित ऋग्वेद संस्करण तीन खंडों में प्रकाशित हो चुके हैं और तीन प्रकाशित होने हैं। मेरी दृष्टि में उस देश (भारत) में अभी भी प्रचलित मूर्ति पूजा की प्राचीन प्रणालियों को उखाड़ फेंकने और वैदिक मान्यताओं के बीच ईसायत को स्थापित करने के प्रयासों में मेरे प्रकाशनों से सभी मिशनरियों को अपूर्व सहायता मिलेगी।
हिंदुत्व के प्रति मोनियर विलियम्स के मन में कितना जहर था, इसका पता उसकी पुस्तक ‘मॉडर्न इंडिया एंड द इंडियंस’ से लगता है।यहां उसकी पुस्तक के 1979 के तीसरे संस्करण के पृष्ठ 261 और 262 के उद्धरण पठनीय हैं। बोडेन चेयर की स्थापना के वास्तविक उद्देश्य के बारे में पृष्ठ 261 पर उसने लिखा है- ‘‘… इसलिए ब्राह्मणवाद समाप्त होना चाहिए। यह सिद्ध करना होगा कि सामान्य वैज्ञानिक विषयों पर भी इन हिंदुओं के विचार इतने गलत हैं कि ईसाई मत की सहायता के बिना सामान्य शिक्षा-भूगोल की पढ़ाई भी अधूरी है। अंतत: यही इनकी नींव को नष्ट करेगा।’’ इसी पुस्तक में अगले पृष्ठ पर वह लिखता है जब ब्राह्मणवाद के शक्तिशाली किले की दीवारों को घेर लिया जाएगा (यानी उनके शास्त्रों में अनर्गल तथ्यों को जोड़ कर व उन्हें कलुषित करके) और नष्ट कर दिया जाएगा, तब अंत में क्रॉस के सैनिकों द्वारा उन पर हमला किया जाएगा। फिर ईसाई मत की समग्र और पूर्ण विजय होगी।
विकृत व्याख्याओं का दौर
19वीं सदी में संस्कृत ग्रंथों का देवनागरी लिपि में मुद्रण प्रारंभ हुआ। इससे पहले संस्कृत विद्वानों के पास हस्तलिखित पांडुलिपियां श्लोक-बद्ध मूल संस्कृत में रहती थीं। गुरुकुलों और आश्रमों में इन्हीं हस्तलिखित प्रतिलिपियों से पढ़ाया जाता रहा है। लेकिन प्रकाशन शुरू होने के बाद लाखों रुपये खर्च कर शास्त्रों की मूल पांडुलिपियों का प्रकाशन, सप्रयोजन दोषपूर्ण पदान्वय, शब्दों की गलत व्याख्या, दोषपूर्ण शब्दकोषों का संपादन और उनका प्रकाशन कर उन्हें कम या नाममात्र के मूल्य पर उपलब्ध कराया जाने लगा। मनुस्मृति सहित विविध स्मृतियों, विष्णु पुराण सहित विविध पुराणों और अनेक संस्कृत ग्रंथों में व्यापक प्रक्षेप, निरुपण व उनकी भ्रामक व्याख्या व्यापक स्तर पर की गई।
चूंकि स्मृतियां एवं पुराण लौकिक संस्कृत में थे, इसलिए उनमें कूट रचित श्लोकों को जोड़ना सरल था। वेद मंत्रों में प्रक्षेप संभव नहीं होने से उनका मूल पाठ यथावत रख कर उनकी दोषपूर्ण व्याख्याएं की गईं इसके लिए निघंटुओं व निरुक्त से विपरीत तथा दोषपूर्ण अर्थ के शब्दकोष भी संकलित किए गए। कम कीमत पर इन ग्रंथों को सर्वसुलभ करवाने से प्रामाणिक पांडुलिपियां अप्रचलित व लुप्त होती गईं या विनष्ट भी कर दी गईं। धन लुटा कर असंख्य यूरोपीय विद्वानों एवं तारानाथ शास्त्री जैसे कुछ भारतीय विद्वानों ने भी अनेक विकृतिपूर्ण संपादन किए। ग्रंथवार विविध तथाकथित विद्वानों द्वारा किए गए इन विकृतिपूर्ण प्रक्षेपों अर्थात् उनमें विकृत श्लोकों को जोड़ने व भ्रामक व्याख्याओं पर कई ग्रंथ बन सकते हैं। लेकिन इस लेख में केवल दो विकृत व्याख्याओं को उदाहरण के तौर पर लिया जा रहा है।
भारतीय शास्त्रों में ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश शासकों और कई यूरोपीय लेखकों द्वारा किए प्रक्षेपों एवं दुष्प्रेरणाजनित व्याख्याओं का संशोधन और परिष्कार अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसे एक राष्ट्रीय अभियान के रूप में लेने की आवश्यकता है। भारतीय इतिहास, काल गणना सहित संपूर्ण भारतीय ज्ञान परंपरा का पुनर्व्याख्यान आवश्यक है।
पशुबलि और अश्लील व्याख्याओं को ही लें तो अश्वमेध यज्ञ में घोड़े को काट-काट कर उसकी बलि की व्याख्या की गई, जिससे अधिकांश विद्वानों के मानस में यह भ्रांति घर कर गई कि अश्वमेध का अर्थ घोड़े की बलि से है। जबकि अमरकोष आदि के अनुसार इसकी सही व्याख्या है-अश्वं वै वीर्यम् यानी वीर्य, शौर्य बल और पराक्रम को अश्व कहते हैं। तैत्तिरीय संहिता और शतपथ ब्राह्मण में इसे और स्पष्ट कर कहा गया है- राष्ट्रम् अश्वमेध:। इसका अर्थ होता है- राष्ट्र का गठन और जागरण ही अश्वमेध है अर्थात् राष्ट्र के प्रजाजनों को एकजुट कर संगठित करना अश्वमेध है। स्पष्टतया, राष्ट्र के सभी लोगों की मेधा अर्थात् बुद्धि के मतैक्य से राष्ट्रजनों को एकजुट करना एवं उनका पराक्रम जाग्रत करना अवश्मेध की श्रेणी में माना जाता था।
शतपथ ब्राह्मण 21/1/2/9/3 में अश्वमेध के इसी स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा गया है- ‘‘श्री वै राष्ट्रं। राष्ट्रं वै अश्वमेध: तस्मात् राष्ट्री अश्वमेधेन् यजेत्। सर्षा: वै देवता:। अश्वमेधे अवयता:। तस्मात् अश्वमेधे थाजी सर्व दिशों अभिजयन्ति।’’ अर्थात् समृद्धि पूर्ण वर्चस्व ही राष्ट्र है। राष्ट्र संगठन ही अश्वमेध है। सभी दिशाओं में विजयी राष्ट्र-परायण अश्वमेध का केंद्रीय शासक व संयोजक ही सर्व विजयी तथा मर्यादाओं का संस्थापक होता है। वस्तुत: शतपथ और गोपथ जैसे ब्राह्मण ग्रंथ ही कर्मकांडों और वैदिक कर्मों को व्याख्यायित करते हैं।
यजुर्वेद संहिता के 18वें अध्याय के 22वें मंत्र ‘अ॒ग्निश्च॑ मे घ॒र्मश्च॑ मे॒ऽर्कश्च॑ मे॒ सूर्यश्च॑ मे प्रा॒णश्च॑ मेऽश्वमे॒धश्च॑ मे पृथि॒वी च॒ मेऽदि॑तिश्च॑ मे॒ दिति॑श्च॑ मे॒ द्यौश्च॑॑ मे॒ऽङ्गुल॑य:- शक्व॑रयो॒ दिश॑श्च मे य॒ज्ञेन॑ कल्पन्ताम्॥’ में राष्ट्र को अखंडित रहने की बात कही गई है। पूरा मंत्र इसके अनुसार अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान राष्ट्र की अखंडता व एकता के लिए किया जाता था। यजुर्वेद के इस मंत्र की राष्ट्र के लिए बलवर्द्धक कई व्याख्याएं मिलती हैं।
जयदेव की व्याख्यानुसार इस मंत्र का भावार्थ है-(अग्नि: च) अग्नि रूप अग्रणी और ज्ञानी नेता पुरुष और अग्निष्टोम यज्ञ, (धर्म: च) तेज, प्रताप, धर्म नामक प्रवर्ग्य इष्टि, (अर्क : च) अर्चनायोग्य सामग्री, अर्चनीय पुरुष और याग, (सूर्य: च) प्राण, (अश्वमेध: च) अश्वमेध यज्ञ और राष्ट्र (पृथ्वी च) पृथ्वी, (अदिति: च) अखंड राजनीति और राष्ट्रभूमि, (दिति: च) विभक्त भूमि अथवा शत्रु को खंड-खंड करने वाली शक्ति, (द्यौ: च) धर्म की प्रकाशक राजसभा, (अङ्गुलय:) अङ्गुलियों के समान परराष्ट्र को पकड़ने और वश करने वाली अग्रगामिनी सेनाएं अथवा राष्ट्र के अङ्ग, (शक्करय:) शक्तिशाली सेनाएं, (दिश: च) दिशाएं और उनमें रहने वाली प्रजाएं, ये सब (मे) मेरे (यज्ञेन) परस्पर संग और राष्ट्र-पालन द्वारा (कल्पन्ताम्) हों।
मंत्र का एक अन्य भावार्थ है- ‘‘मेरे राष्ट्र की अग्नि अर्थात् ऊर्जा में वृद्धि हो और उसके धर्म अर्थात् नीति युक्त आचरण में संवृद्धि हो, मेरे राष्ट्र की तेजस्विता में संवृद्धि हो, मेरा राष्ट्र कीर्तिमान हो, उसकी सत्कार करने योग्य विशेष सामग्री, उसकी प्रखरता व बल में वृद्धि हो, उसकी शुद्धि करने के व्यवहार में वृद्धि हो और जीविका के हेतुओं मे वृद्धि हो, मेरा राज्य रूपी यह देश/राष्ट्र बल-समृद्धिपूर्ण हो और राजनीति में मेरी पृथिवी से द्युलोक तक अक्षय व स्थिर कीर्ति हो, इस देश के सब पदार्थों में वृद्धि हो, मेरी नीतिमत्ता व कीर्ति अखंड हो और मेरे प्रजाजनों की इंद्रियों का बल अक्षुण्ण हो, मेरे धर्म का प्रकाश दिन व रात में निरंतर बढ़े और परमात्मा यज्ञ रूपी मेरे अक्षय अभियानों से मुझे समर्थ बनाए।

अश्वमेध यानी राष्ट्र उपासना
देश की प्राचीन स्वर्णयुगीन परिस्थितियों के पीछे राष्ट्र के राजा एवं प्रजा की यही भावना थी। विख्यात इतिहासकार ए.एल. बाशम ने अपनी पुस्तक ‘द वंडर दैट वाज इंडिया’ में लिखा है, ‘‘यदि कहीं के निवासियों ने अपने राष्ट्र को जीवंत, जाग्रत और उपास्य माना है, तो वह भारत है।’’ उनके अनुसार ‘अश्वमेध’ राष्ट्र उपासना की सर्वाधिक प्रचलित प्रक्रिया थी, जिसका अनुष्ठान शासक श्रोत्रिय (मनीषी) एवं जन समूह सभी मिलजुल कर करते थे। इसी के द्वारा न केवल राजनीतिक क्षितिज पर, बल्कि आर्थिक, बौद्धिक और सामाजिक दायरों में विकास के मापदंड स्थापित किए गए थे। इस संबंध में शतपथ ब्राह्मण का एक संपूर्ण मंत्र निम्नानुसार है-
राष्ट्रं वा अश्वमेध: राष्ट्र एते व्यायच्छन्ते येऽश्वं रक्षन्ति तेषां य उदृचं गच्छन्ति राष्ट्रेणैव ते राष्ट्रं भवन्त्यथ ये नोदृचं गच्छन्ति राष्ट्रात्ते व्यवच्छिद्यन्ते तस्माद्रार्ष्ट्यश्वमेधेन यजेत परा वा एष सिच्यते योऽबलोऽश्वमेधेन यजते यद्यमित्रा अश्वं विन्देरन्यज्ञोऽस्य विच्छिद्येत पापीयान्त्स्याच्छतं कवचिनो रक्षन्ति यज्ञस्य संतत्या अव्यवच्छेदाय
न पापीयान्भवत्यथान्यमानीय प्रोक्षेयु: सैव तत्र प्रायश्चित्ति:। (शतपथ ब्राह्मण 13/1/6/3)
इसका संक्षिप्त भावार्थ है कि राष्ट्र का पराक्रमपूर्वक सुचारू रूप से संगठन एवं संचालन करना ही अश्वमेध यज्ञ है। ऊपर के कथनानुसार अश्व ही बल और पराक्रम है। यह अश्वमेध यज्ञ यानी अश्व रूपी पराक्रम ही राष्ट्र के सुदृढ़ संगम का प्रतीक है। यहां मेध शब्द का अर्थ वध नहीं है। ‘मेध’ शब्द के कई अर्थ हैं, लेकिन उसका अर्थ वध या बलि कदापि नहीं है। यह शब्द मेधृ धातु से बना है, जिसे धातुपाठ में इस प्रकार परिभाषित किया है- मेधृ – मेधासंगमनयोर्हिनसायां च। मुख्य रूप से मेध का संबंध मेधा से है तथा मेधा का मंथन से। मेध का अर्थ सत् (सत्य, सार, जीवनी शक्ति) है। इस आधार पर श्री विष्णु का एक नाम मेधज है, जो मेध या मेधा अर्थात् बुद्धि को उत्पन्न करते हैं। विष्णुसहस्रनाम में भी मेधा शब्द बुद्धि का प्रतीक है, वध का नहीं। जैसे-
अमानी मानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक्।
सुमेधा मेधजो धन्य: सत्यमेधा धराधर:।।
(विष्णुसहस्राम स्तोत्रम्- 80)
इस मंत्र के अनुसार, मेध ज्ञान, बुद्धि तथा समझ का स्रोत है। मेध का अर्थ समागम या साथ आना भी है। मेध का अर्थ पुष्टिकर भी है, अर्थात् राष्ट्र की पुष्टि। शब्दों के अर्थ को लेकर सायण व महीधर के भाष्यों के प्रकाशन में भी विकृतियों के अनगिनत प्रक्षेप किए गए हैं। निघंटु, जो वैदिक शब्दों के पर्यायवाची कोष अर्थात् अंग्रेजी थिसोरस की श्रेणी में होते हैं, उनमें व अमरकोष में ऐसे शब्दों के और भी अनेक अर्थ मिल जाते हैं।

चार पुरुषार्थों की दूषित व्याख्या
अश्वमेध की तरह चार पुरुषार्थों की भी दूषित व्याख्या की गई है। यजुर्वेद के मंत्र में ‘ते उभे चतुर्पदे सम्प्रसारयाव’ का वास्तविक अर्थ होता है- वे दो अर्थात् राजा व प्रजा दोनों मिलकर चारों प्रकार के पुरुषार्थों- धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष का प्रसार करें। कई व्याख्याकारों ने इसकी व्याख्या पुरुष व स्त्री के संदर्भ में तथा उन दोनों के चार पैरों की अनर्गल व्याख्या कर दी।
वर्णभेद व ऊंच-नीच परक श्लोकों के प्रक्षेप व दोषपूर्ण व्याख्याएं : श्रम के स्वेद अर्थात् परिश्रम पूर्वक पसीना बहाकर मूल्यवान वस्तु के उत्पादक वर्ग (श्रमस्य स्वेदेन उत्पादनरत एव शूद्र:) की शब्द निरुक्ति के स्थान पर क्षुद्र शब्द से शूद्र शब्द की रचना के अनेक भेद मूलक विवरण गढ़ कर समाज को बांटने के षड्यंत्रों में भी बोडेन पीठ प्रेरित लेखकों ने कोई कसर नहीं छोड़ी।
आर्य-द्रविड़ विभेद का मिथक : संपूर्ण वृहत्तर पौराणिक भारत के निवासी अर्थात् इंडोनेशिया से पूर्वी ईरान तक के लोग 1200 वर्ष पूर्व एक अविच्छिन्न हिंदू संस्कृति के अंग थे। उनमें आर्य-द्रविड़ जैसा कोई भेद कभी नहीं था। इस भेद को तो 1858 से केवल काल्डवेल और मैक्समुलर जैसे यूरोपीय लेखकों ने ही योजनापूर्वक गढ़ा था। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की सभी भाषाओं को 1858 से पहले एक ही भाषा समूह में रखा-समझा जाता था। दक्षिण भारत की भाषाओं को शेष भारतीय भाषाओं से अलग भाषाओं के रूप में प्रथम बार 1858 में यूरोपीय मिशनरी पादरी रॉबर्ट कॉल्डवेल द्वारा षड्यंत्रपूर्वक भेद मूलक वर्गीकरण कर अलग दिखाने का प्रयास किया गया था। इसके पूर्व आर्य और द्रविड़ जैसा कृत्रिम विभाजन न हो कर सारी भारतीय भाषाओं को एक समूह की भाषाओें के रूप में ही विवेचित किया जाता रहा है।
1858 में प्रकाशित कॉल्डवेल की भेदमूलक पुस्तक ‘अ कम्पेरेटिव ग्रामर आफ द्राविड़ियन आर साऊथ इंडियन लैंग्वेजेज’ के पूर्व की भाषा विज्ञान की सभी पुस्तकें भारतीय भाषाओं का समेकित एवं साझा विवेचन ही करती रही हैं। उदाहरण के लिए, कॉल्डवेल से 300 वर्ष पूर्व 1560-65 के बीच मार्कण्डेय रचित ‘प्राकृत सर्वस्वम्’ नामक ग्रंथ में, जो एक प्रकार से भारतवर्ष की सभी भाषाओं का सर्वेक्षण कहा जा सकता है, ऐसा कोई भेद नहीं है। मार्कण्डेय रचित सर्वेक्षण पियर्सन व कॉल्डवेल के भेदमूलक व षड्यंत्रकारी ग्रंथों से बहुत पहले का है। इसमें भारतवर्ष की भाषाओं का कोई पारिवारिक भेद नहीं है। आर्य, द्रविड़ भाषा परिवार जैसा कोई विभाजन उसमें नहीं है। आर्यों के विदेश से आगमन के मिथक का भी कोई वैज्ञानिक, तथ्यात्मक व ऐतिहासिक आधार नहीं होकर, सिर्फ भारतीय व यूरोपीय भाषाओं के भारोपीय समूह के नाम से ही कॉल्डवेल, मैक्स मुलर आदि द्वारा गढ़ा गया था।
इस संपूर्ण विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय शास्त्रों में ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश शासकों और कई यूरोपीय लेखकों द्वारा किए प्रक्षेपों एवं दुष्प्रेरणाजनित व्याख्याओं का संशोधन और परिष्कार अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसे एक राष्ट्रीय अभियान के रूप में लेने की आवश्यकता है। भारतीय इतिहास, काल गणना सहित संपूर्ण भारतीय ज्ञान परंपरा का पुनर्व्याख्यान आवश्यक है।
(लेखक : पैसिफिक विश्वविद्यालय समूह (उदयपुर) के अध्यक्ष-आयोजना व नियंत्रण)


















टिप्पणियाँ