अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैंसी पैलोसी के ताइवान पहुंचते ही चीनी सेना ने ताइवान के इर्द-गिर्द मिसाइल निशानेबाजी शुरू कर दी। सवाल यह है कि क्या ड्रैगन की यह उछल-कूद अंकल सैम को डरा पाएगी?
मगर इससे जुड़े हुए कुछ सवाल और भी हैं।
ताइवान क्या है? ड्रैगन क्या है? और अंकल सैम यानी अमेरिका चाहता क्या है? इन दोनों की रस्साकशी में भारत के हित कहा हैं?
हर दिन जटिल होते हुए भू-राजनीतिक समीकरणों को सरल करने के लिए कई बार रूपक और उपमाएं आवश्यक हो जाती हैं।
यह समझना पड़ेगा कि ताइवानी राष्ट्रपति त्साई इंग वेन, किम जोंग उन नहीं हैं और नैन्सी पैलोशी अमरीकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं हैं।
चीन को यह भी समझना होगा कि एशियाई बाघ कहा जाने वाला यह द्विपीय देश, ड्रैगन का बगल बच्चा नहीं है। यह यूक्रेन भी नहीं है। यह प्रभुसत्ता की ताल ठोकता ताइवान है जो एक चीन की नीति नहीं मानता।
चीनी नेतृत्व को अगर किसी विचारधारा के खांचे में समझने की कोशिश करेंगे तो गच्चा खा जाएंगे। खुद चीनी मानते हैं कि यह माओ का मुखौटा लगाए मनमानी पर उतरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना (सीपीसी) की वर्गीय कोटरी ही है।
वह विचारधारा जो वामपंथ जपते-जपते पूरी तरह दामपंथी यानी पूंजीवादी हो चुकी है। यह वास्तव में चंद लोगों की झोलियां भरने का खेल भर है।
जिसने पहले देश के भीतर स्वीकार्यता जुटाने के लिए छल, बल का खेल खेला और फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कदम बढ़ाते हुए निर्यात, निवेश और निर्भरता का जाल बुना गया जिसमें अलग-अलग देशों को फांसा गया। जो चीन के साथ लगते थे, उनको दबाया या भरमाया गया और, जिनके प्रति चीन शत्रुता का भाव रखता है, उनके इर्द-गिर्द भी बड़ी सूक्ष्मता से सैन्य कूटनीति आधारित जाल बुना गया।
प्रश्न है कि अंकल सैम क्या चाहता है?
अमेरिका में राज चाहे रिपब्लिकन पार्टी का हो या डेमोक्रेट, यह देश अपने मूल चरित्र में विशुद्ध पूंजीवादी है। डेमोक्रेट वहां की जनता के बीच कुछ भी छवि बनाएं किन्तु अपनी मंशाओं में वे पूरी तरह से पूंजीवादी ही हैं। समय- समय पर इनके बाजारवादी हितों से जुड़ी चर्चाएं उठती रही हैं।
राजनीति में विचारधारा का पल्लू पकड़ अपने दल के लिए अकेले और अमेरिका के वर्चस्व के लिए बारी-बारी से डेमोक्रेट और रिपब्लिकन काम करते रहे हैं। लगातार अपना हित विस्तार करते रहने की आदत ही अमेरिकी- चीनी टकराहट का वास्तविक कारण है।
दोनों की इस रस्साकशी में भारत?
नेहरू और चाऊ एन लाई के बीच पंचशील समझौता संदेह के कुहासे में हुआ था। समझौता होने के बाद जल्दी ही दरारें दिखने लगीं थीं और अंतत: चीन ने भरोसे के उस भ्रम को भी चकनाचूर कर दिया। तिब्बत के मसले को लेकर चीन की जो आक्रामकता और अड़ियल रुख था, उसने भारत को चिंतित कर दिया था। सरदार पटेल ने तब इस पर चिंता जताई थी। और 1962 के भारत-चीन युद्ध में यह साफ हो गया कि चीन की मौजूदा मंशाओं के साथ रहना या मित्र के तौर पर आगे बढ़ना भारत के लिए संभव नहीं है।
भारत की सीमा कभी भी चीन से नहीं लगती थी। उसने जब तिब्बत को हड़पा, उसके बाद हमारी एक और सीमा पर ध्यान केंद्रित किया। पाकिस्तान और चीन, दोनों भारत के प्रति प्रारंभ से शत्रु भाव रखते थे। सो, इन्होंने अपने साझे शत्रु, यानी भारत के विरुद्ध षड्यंत्र का जाल बुनना शुरू किया ताकि अलग-अलग मोर्चों पर बार-बार भारत को चुनौती दी जा सके। यह उनकी दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा था कि अगर भारत को पटखनी देना संभव नहीं, तो लगातार चुनौती दी जाए। उसे लगातार आहत किया जाए। पाकिस्तान पोषित आतंकवाद पर चीन मौन रहा और चीन में उइगुर मुसलमानों के दमन पर पाकिस्तान मौन रहा। दोनों मिलकर चल रहे थे। 1963 में दोनों ने आपस में एक संधि कर ली। यह संधि उनमें आपस में थी, मगर प्रकारांतर से यह भारत के विरुद्ध ही थी। भारत का एक क्षेत्र ट्रांस काराकोरम ट्रैक यानी, जिसे शक्सगाम घाटी कहते थे, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा था, वह पाकिस्तान ने चीन को दे दिया।
ड्रैगन कैसे पंजे गड़ाता है ?
ड्रैगन नेपाल में भी दोस्ती की आड़ में वहां की जगहों पर कब्जा करने की मंशा से आया। नेपाल के साथ चीन ने बुनियादी ढांचा समझौते की बात की और फिर गोरखा, रुई, हुमला जैसे नेपाली इलाकों में नेपालियों का जाना ही रोक दिया।
पाकिस्तान में भी ड्रैगन की मंशा यही है। बलूच विद्रोहियों ने जब चीन के कर्मचारियों को मारा तो चीन ने अपनी सेना भेजने की बात कही। कोई पूछे, चीन आ जाएगा तो क्या पाकिस्तान अपनी जगह बचा पाएगा? चीन ने पाकिस्तान को जो पहले सुनहरे ख्वाब दिखाये थे, वह फौजी जरनलों की जेबों में भले उतरे हों, जमीन पर नहीं उतरे।
चीन किसी देश को अपने ऊपर पूरी तरह निर्भर कैसे बनाता है। पहला, आधारभूत ढांचे में निवेश करना, दूसरा, सैन्य उपक्रमों के आयात में निर्भरता बनाना और अपनी बढ़त बनाना।
स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के आर्म्स ट्रांसफर डेटाबेस के अनुसार, 2010 से पूर्व के दशक के आंकड़ों की तुलना में 2010 और 2020 के बीच चीन से पाकिस्तान के हथियारों का आयात दोगुने से भी अधिक हो गया है। चीन अब पाकिस्तान का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भी है। |ब्जर्वेटरी | ऑफ इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी के आंकड़ों के अनुसार, 2009 और 2019 के बीच, पाकिस्तान से चीन को निर्यात में 87 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि आयात में 183 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
चीन की कमजोर नस क्या है?
दुनिया को यह समझना होगा कि चीन किसी एक का मसला नहीं है। नेपाल, श्रीलंका, से लेकर और सुदूर अफ्रीका तक विस्तारवादी मंशाओं को पूरा करने के लिए लुभावना जाल फैला है।
अमेरिका चीन से टकराया, ठीक! मगर पूरी दुनिया को सिर्फ अपने हित देखने के अलावा यह समझना पड़ेगा कि हनक और विस्तारवादी मंसूबों से कैसे निबटना है। बारीकी से देखेंगे तो पाएंगे कि ड्रैगन की कमजोरी को मापने का त्रिसूत्री फार्मूला उपलब्ध है।
इसे ऐसे देखें कि एक बहुत दमदार बादशाह है मगर वह तुतलाता है, तो उसकी हनक, हेकड़ी, उसका रसूख खत्म हो जाता है। ऐसे ही ड्रेगन तीन चीजों पर तुतलाता है। संयोग से तीनों शब्द ‘त’ से ही शुरू होते हैं।
जिस तरह भारत में कुछ लोगों को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किए गए आह्वान, तिरंगे और इसकी डीपी से डर लगता है, उसी तरह ड्रैगन को ताइवान की डीपीटी यानी डेमोक्रेटिक पार्टी से डर लगता है। वजह यह कि ताइवान में द्वि-दलीय व्यवस्था है और चीनी झुकाव रखने वाली पार्टी से उलट डीपीटी प्रबल राष्ट्रीय आग्रह रखने वाली पार्टी है। ताइवान की वर्तमान राष्ट्रपति पूर्व में दल की मुखिया रही हैं, इससे भी दिलचस्प और चीन को डराने वाला तथ्य यह है कि उनकी पीएचडी का विषय ‘अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस एंड सेफगार्ड एक्शन’ रहा है। तो चीन के असली भय की वजह कौन है, विश्व को समझना पड़ेगा। ताइवान की इच्छाओं को भी समझना पड़ेगा।
इनमें पहला तिआनमेन (चौक) है, जहां चीनी छात्र-छात्राओं द्वारा 14 मई,1989 को सरकार विराधी प्रदर्शन हुआ और सरकार ने अपने ही 10 हजार से ज्यादा नागरिकों की जान ले ली।
दूसरा तिब्बत है जिसकी सांस्कृतिक पहचान को कम्युनिस्ट सरकार ने मानो पूरी तरह नष्ट करने की कसम खा रखी है। परंतु दलाई लामा की सूझ और तिब्बती युवाओं के प्रखर प्रतिरोध के कारण अब तक वह अपने इरादे में सफल नहीं हो पाई।
तीसरा ताइवान है। ताइवान विश्व की जरूरतों को सकारात्मक ढंग से पूरा करने वाला प्रमुख औद्योगिक केन्द्र है। याद है ! कोविड संकट के दौरान जब सेमीकंडक्टर की आपूर्ति रुकी थी तो पूरी दुनिया में ऑटो मोबाइल सेक्टर अटक गया था। यह भारत के तमिलनाडु जितना छोटा सा देश है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद उसका आधार है। दिलचस्प बात यह है कि ताइवान वामपंथी विचार को नहीं मानता। वह मानता है कि चीन पर वामपंथियों ने कब्जा कर लिया है और चीन के एक सांस्कृतिक शास्त्रीय राष्ट्र का प्रतिनिधित्व असल में ताइवान करता है।
जिस तरह भारत में कुछ लोगों को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किए गए आह्वान, तिरंगे और इसकी डीपी से डर लगता है, उसी तरह ड्रैगन को ताइवान की डीपीटी यानी डेमोक्रेटिक पार्टी से डर लगता है। वजह यह कि ताइवान में द्वि-दलीय व्यवस्था है और चीनी झुकाव रखने वाली पार्टी से उलट डीपीटी प्रबल राष्ट्रीय आग्रह रखने वाली पार्टी है। ताइवान की वर्तमान राष्ट्रपति पूर्व में दल की मुखिया रही हैं, इससे भी दिलचस्प और चीन को डराने वाला तथ्य यह है कि उनकी पीएचडी का विषय ‘अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस एंड सेफगार्ड एक्शन’ रहा है। तो चीन के असली भय की वजह कौन है, विश्व को समझना पड़ेगा। ताइवान की इच्छाओं को भी समझना पड़ेगा।
तिब्बत की सांस्कृतिक पहचान से जुड़ी आकांक्षाओं को भी समझना पड़ेगा। तिएनआनमन के बलिदान को भी याद रखना पड़ेगा।
विश्व के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि उसका ताइवान के प्रति झुकाव, तिब्बत के प्रति प्रेम या तिएनआनन के प्रति संवेदना- यह चीन से नफरत के कारण नहीं, बल्कि मानवीयता के साथ खड़े होने के आग्रह के कारण हो।
यह इसलिए क्योंकि नफरत के आधार पर कोई भी यात्रा बहुत लंबी नहीं चलती। लगता तो यह भी है कि सीपीसी से इतर चीनी समाज भी इन, या इन जैसे अन्य मुद्दों पर वर्तमान कम्युनिस्ट नेतृत्व के साथ नहीं है।
@hiteshshankar

















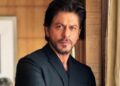

टिप्पणियाँ