|
आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, आपके पास मेल एकाउंट है, सोशल साइट्स पर एकाउंट है, मोबाइल में एप्स हैं- तो समझिए कि आप घर की चाहारदीवारी में रहते हुए भी सड़क पर ही खुले में ही गुजर-बसर कर रहे हैं
प्रशांत बाजपेई
आप गूगल पर 'सर्च' करते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि गूगल भी आपको सर्च करता है? एकाउंट बनाते समय मांगी गई जानकारियां आपने दी होंगी, पर यदि फेसबुक के पास वे जानकारियां भी हों जो आपने नहीं दी थीं, तो? आपके मेल आपकी प्रेषण सूची तक ही पहुंचते हैं या उसके और भी ठिकाने हैं? आपके व्हाट्सअप संदेश कौन-कौन पढ़ सकता है आपके मित्रों के अलावा? स्मार्टफोन में डाउनलोड एप्स क्या आपकी निजता के लिहाज से सुरक्षित हैं? क्या बड़ी-बड़ी इंटरनेट कंपनियां आपको मंजे हुए खुराफाती हैकरों से बचा सकती हैं… आखिर करोड़ों लोग साइबर अपराधों के शिकार हुए हैं। खतरे की संभावनाएं बहुत लंबी-चौड़ी हैं। पर डरिए मत, सजग रहिए। सजगता ही बचाव है।
खेल के नाम पर
कुछ ही महीने पहले 'पोकेमॉन गो' नामक मोबाइल खेल ने सुर्खियां बनाईं। पोकेमॉन नाम संक्षिप्त रूप है 'पॉकेट मॉन्स्टर' का। अर्थात् जेब में रखा हुआ दैत्य। इस मोबाइल खेल में खेलने वाले मिलकर एक काल्पनिक दैत्य से लड़ते हैं। इस दैत्य का आपके शहर में एक काल्पनिक रहवास होता है जिसे आपको सड़क पर निकलकर ढूंढना होता है, जबकि आपका मोबाइल एप आपको उसके पते-ठिकाने के संकेत देता रहता है।
अब मोबाइल स्क्रीन पर नजर जमाए गाडि़यां चलाते अथवा सड़क पर चलते पोकेमॉन खिलाड़ी दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। अपराधी भी 'पोकेमॉन गो' की मदद से इन खिलाडि़यों पर घात लगाए बैठे हैं। अमेरिका के रिवरटन की 19 वर्षीया लड़की शायला विगिन्स काल्पनिक 'पॉकेट मॉन्स्टर' को खोजते हुए झील में तैरती एक सचमुच की लाश तक जा पहुंची और तबसे सदमे में है। पुलिस को भी कहीं भी पहुंचने वाले लोगों की शिकायतें आ रही हैं। बच्चों का यौन शोषण करने वाले अपने शिकार को इस एप की मदद से किसी सुनसान या असुरक्षित स्थान पर बुलाकर फांस सकते हैं। हद तब हो गई जब पोकेमॉन को ढूंढ़ते बच्चे 'सेक्स शॉप्स' और वेश्यालयों तक जा पहुंचे।
साइटें कितनी सुरक्षित
पिछले साल दुनिया (विशेष रूप से पश्चिम) के लाखों लोगों की जिंदगी में भूचाल आया। आपकी पहचान गुप्त रख वयस्क मित्र बनाने और उनसे ऑनलाइन वीडियो चैट वाली वेबसाइट 'एडल्ट फ्रेंड फाइंडर' पर हैकरों ने हमला बोला और 39 लाख लोगों की अत्यंत गोपनीय जानकारी, अंतरंग फोटो, उनके संबंध आदि इंटरनेट पर सार्वजनिक कर दिए। इनमें वे लोग भी थे जो इस साइट का कुछ समय उपयोग करने के बाद अपने अकाउंट डिलीट कर चुके थे। शिकार हुए उपयोगकर्ताओं में दुनिया के कई बड़े सरकारी, सैन्य अधिकारी भी थे जिस कारण यह घटना एक सुरक्षा चुनौती भी बन गई। ऑनलाइन दुनिया में ऐसी हजारों साइट्स हैं।
हर गली, चेहरे पर नजर
गूगल स्ट्रीट व्यू एप दुनिया भर की सड़कों और सार्वजनिक स्थानों, गली-मुहल्लों के वास्तविक चित्र उपलब्ध करवाता है। इसे बहुत पसंद किया गया लेकिन तमाम लोगों ने अपनी निजता के उल्लंघन को लेकर गूगल के खिलाफ अदालत के दरवाजे खटखटाने शुरू कर दिए। इस 'सेवा' को उपलब्ध कराने के लिए विशेष कैमरों से लैस गूगल की गाडि़यां दुनियाभर में सड़कों पर चित्र उतारते घूमती रहती हैं। इसमें बहुत से ऐसे लोगों की फोटो रिकॉर्ड में आती हैं जो ऐसा नहीं चाहते। अलग-अलग देशों के चलन और रहन-सहन के हिसाब से अलग-अलग आपत्तियां दर्ज हो रही हैं। स्ट्रीट व्यू कार में लगा विशेष सेंसर वाई-फाई नेटवर्कांे को भी पकड़ कर उनकी जानकारी रिकॉर्ड करता है। लोगों के यूजर नेम और पासवर्ड भी गूगल के पास पहुंच जाते हैं। मुकदमे चल रहे हैं। गूगल का कहना है कि ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में गड़बड़ी से हो रहा था। अब वाई-फाई डेटा जुटाना बंद कर दिया गया है। गूगल की डायरेक्टर ऑफ प्राइवेसी एल्मा व्हिटेन ने बयान दिया, ''इस डेटा का कभी उपयोग नहीं किया जाएगा। हम इसे नष्ट करने जा रहे हैं।'' जानकारों का कहना है कि तकनीक निरंतर बदल रही है और इसलिए निगरानी की निरंतरता आवश्यक है।
ब्रिटेन में व्यक्तिगत निजता और नागरिक अधिकार के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था बिग ब्रदर वॉच के निदेशक निक पिकल्स कहते हैं, ''लोगों के घरों, जानकारी और गाडि़यों के नंबरों का सार्वजनिक होना एक बड़ा सुरक्षा मुद्दा है। गूगल उसकी सुविधाओं का उपयोग करने वालों को आर्थिक उपयोग की वस्तु के रूप में देखता है।'' इससे आतंकी भी लाभान्वित हो रहे हैं। 26/11 के हमले के लिए मुंबई की रेकी करने के लिए जिहादियों ने इंटरनेट द्वारा प्रदत्त इस सुविधा का भी उपयोग किया था।
सवाल है कि गूगल या अन्य कोई सर्च इंजन अपने उपयोगकर्ताओं के बारे में क्या-क्या जानता है? यदि आप नियमित उपयोगकर्ता हैं तो आमतौर पर गूगल को आपका नाम, लिंग, आयुवर्ग, भाषा, रुचियां, कंप्यूटर मॉडल, कितने ईमेल प्राप्त हुए, कंप्यूटर पर बैठने का समय, इंटरनेट पर क्या देखते-पढ़ते हैं, आज तक यूट्यूब पर कितने वीडियो देखे, सब पता है। हालांकि 2009 में गूगल ने पारदर्शिता डैशबोर्ड नामक टूल दिया जिससे आप यह पता कर सकते हैं कि आपकी किस प्रकार की जानकारी कंपनी के पास रिकॉर्ड में आ रही है। गूगल आपकी गतिविधियों पर नियमित शोध करता है।
महानगर का एक युवा गुरुवार को अपने कार्यालय में भोजन अवकाश के समय शनिवार को किसी के साथ कहीं घूमने जाने की योजना बना रहा है। मित्र को गूगल चैट पर सन्देश भेजकर पूछता है कि क्या वह शनिवार को अमुक समय पर खाली है। फिर गूगल पर रेस्तरां ढूंढ़ता है, मेन्यू पर नजर दौड़ाता है और एक रेस्तरां तय करता है। वह मित्र को इसके बारे में ईमेल करता है। शनिवार को रेस्तरां पहुंचने के लिए दोनों मित्र गूगल मैप का प्रयोग करते हैं। ये सारी गतिविधियां गूगल को दोनों व्यक्तियों और संबंधित स्थानों के बारे में कई जानकारियां उपलब्ध करवा देती हैं। लाखों लोग प्रतिदिन गूगल का डेटा समृद्ध करने में योगदान देते हैं। आपके इंटरनेट सर्च की निजता को बनाए रखने के लिए कुछ प्राइवेट ब्राउजिंग मॉड उपलब्ध करवाए गए हैं जैसे गूगल क्रोम, पर ये भी शत प्रतिशत सुरक्षा नहीं देते। वीपीएंस और द टोर नेटवर्क जैसे उन्नत विकल्प हैं। मगर इनके बारे में जानकारी और पहुंच कितने लोगों के पास है।
आजकल ज्यादातर लोगों के ईमेल एकाउंट जीमेल पर बने हुए हैं। इन पर जो कुछ भी लिखा जाता है, गूगल उसे स्कैन करता है, ताकि व्यक्ति की रुचि के आधार पर संबंधित विज्ञापनों को उस एकाउंट को भेजा जा सके। जब आप कोई ईमेल मिटा देते हैं तब भी वह गूगल के दस्तावेज में 60 दिनों तक सुरक्षित रहता है। ये जानकारियां विज्ञापन जगत के लिए अमूल्य हैं जिन्हें और किसी माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता। गूगल अकेला नहीं है। फेसबुक भी डाटा जुटाता है। सौ करोड़ से ज्यादा लोग उस पर हैं। इनमें आधे प्रतिदिन अपने फेसबुक एकाउंट से कुछ न कुछ गतिविधि करते हैं। फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग का बयान है, ''मैं दुनिया को अधिक खुली (ओपन) जगह बनाने की कोशिश कर रहा हूं।'' और जैसा कि हम जानते हैं कि इक्कीसवीं सदी में 'डेटा' सोने की खान है।
मोबाइल एप्स
'एप इंस्टॉल' होते समय कुछ ऐसी अनुमतियां मांगता है कि वह आपकी किन-किन जानकारियों तक पहुंच सकेगा। जल्दी में हम प्राय: इस पक्ष की उपेक्षा कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। एप निर्माताओं को भी एप बनाते समय पहले चरण से ही निजता और सुरक्षा को अपनी प्राथमिकताओं में रखना चाहिए। हालांकि ऐसा भी है कि अगर आप किसी एप को अनुमति नहीं देते हैं तो वह ठीक से इंस्टॉल ही नहीं होता।
जानकारी जरूरी
बड़े व्यावसायिक और औद्योगिक संस्थान विशेषज्ञों और तकनीशियनों की सेवा लेते हैं। सरकारी और सुरक्षा एजेंसियां अपने स्वतंत्र तंत्र विकसित करती हैं। पर आम आदमी का हथियार मूलभूत ज्ञान, जानकारियों के आदान-प्रदान और कानून की समझ में ही है। देश में मोबाइल और इंटरनेट की पहुंच जिस तेजी से बढ़ रही है उस तेजी से सुरक्षा और उपयोग की समझ नहीं बढ़ रही। जागरूकता आवश्यकता है। इन माध्यमों पर नजर रखने वाले जनमंचों का निर्माण शहर-दर-शहर आवश्यक है। जहां पर आम व्यक्ति और तकनीकी विशेषज्ञ परस्पर संवाद कर सकें।
वे कैसे फंसाते हैं, आप कैसे बचें
मनीष शर्मा (सॉफ्टवेयर और साइबर विशेषज्ञ)
हम सब सोशल नेटवर्किंग साइट, ईमेल/ व्हाट्सएप, ऑनलाइन पोर्टल का इस्तेमाल करते ही हैं। इसका साइबर जगत की बड़ी कंपनियां वांछित अथवा अवांछित फायदा उठा सकती हैं।
क्लाउड कंप्यूटिंग
हम क्लाउड कंप्यूटिंग के युग में प्रवेश कर रहे हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग का तात्पर्य है सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर/डिवाइस में इनस्टॉल न कर उसे ऑनलाइन एक्सेस करना अथवा अपना डेटा इंटरनेट में किसी कंप्यूटर अथवा सर्वर में सेव करना, जहां से आप उसे कभी भी, कहीं भी, किसी भी डिवाइस जैसे लैपटॉप/मोबाइल से पा सकें। सामग्री अपने पास रखने के बजाय 'ऑनलाइन सेव' करने से उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है।
डेटा बिकता है
क्लाउड में स्टोर सामग्री की मदद से कंपनियों को व्यापारिक निर्णय लेने में मदद मिलती है और इसके लिए 'बिग डेटा' का उपयोग किया जाता है। 'बिग डेटा' का तात्पर्य है भिन्न-भिन्न स्रोतों से अधिक से अधिक मात्रा में संरचित (स्ट्रच्कर्ड) अथवा असंरचित डेटा एकत्रित करना जिससे व्यक्ति अथवा समूह अथवा समाज की आदतों, रुझानों आदि का पता किया जा सके। जैसे किसी कंपनी को कार का नया मॉडल लांच करना हो तो वह यह जानना चाहेगी कि
वर्तमान कारों में कौन से फीचर्स लोगों को पसंद हैं?
वर्तमान कारों में लोगों के अनुसार क्या कमियां हैं?
लोग किस कीमत की कार खरीदना
पसंद करेंगे?
ब्राउजिंग आदतें
अगर कुछ लोग दिसंबर में घूमने की योजना बनाते हैं तो सितम्बर-अक्टूबर से ही उन साइट्स पर जाने लगते हैं जो अलग-अलग पर्यटन स्थलों की जानकारी प्रदान करती हैं? गूगल अथवा याहू आपकी ब्राउजिंग आदतों से आपकी जरूरत को समझ जाते हैं और उसके अनुसार विज्ञापन दिखाने लगते हैं। तो बात एकदम सीधी है :
आपका डाटा, व्यवहार इत्यादि सब कुछ क्लाउड में है।
इस डेटा/ व्यवहार का 'बिग डेटा सिस्टम्स' द्वार उपयोग अथवा दुरुपयोग किया जा सकता है
व्यक्तिगत सामग्री और साइबर अपराध
अगर आपका व्यक्तिगत डेटा साइबर अपराधियों के हाथ लग जाए तो लेने के देने पड़ सकते हैं। 'पर्सनल इन्फॉर्मेशन इज द करेंसी ऑफ द अंडरग्राउंड इकॉनमी।' हैकर्स आपकी महत्वपूर्ण जानकारी को घोटालेबाजों को बेच सकते हैं और घोटालेबाज प्रलोभन देकर आपको धन हानि अथवा अन्य नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपका ईमेल ज्ञात होने पर स्पैमर्स आपको विषय से सम्बद्ध लुभावने मेल भेज सकते हैं। आपके क्रेडिट कार्ड के अंतिम चार अंक ज्ञात होने पर हैकर्स आपके के्रडिट कार्ड का पासवर्ड रिसेट (बदल) कर सकते हैं। इसके बाद उनके लिए आपके क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना आसान हो जाता है।
धोखाधड़ी से ऐसे बचें
ईमेल का पासवर्ड संख्या के साथ जटिल रखें और समय-समय पर इसे बदलते रहें
ब्राउजिंग करने के बाद लॉगआउट करें
ब्राउजर से कुकी/कैश साफ करते रहें
स्थान की जानकारी की अनुमति न दें
फायरवॉल का उपयोग करें
कौन ज्यादा जरूरी: हमारी निजताया देशहित
जब लोगों की निजता खतरे में पड़ती है तब भी विवाद होता है और जब उसे हद से ज्यादा सुरक्षित कर दिया जाता है तब भी हल्ला मचता है। आखिर माजरा क्या है?
बालेन्दु शर्मा दाधीच
साल 2013 में एडवर्ड स्नोडेन ने अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (एनएसए) द्वारा आम लोगों के निजी संदेशों की जासूसी का रहस्योद्घाटन कर दुनिया भर में तहलका मचा दिया था। सिर्फ अमेरिका क्यों, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की एजेंसियां भी इंटरनेट कंपनियों पर कानूनी दबाव डालकर आम लोगों के ईमेल, चैट संदेशों और दूसरी निजी सामग्री को खंगाल रही थीं। इस घटना पर भारत समेत दुनिया भर में जबरदस्त रोष पैदा हुआ और खुफिया एजेंसियों के साथ-साथ निशाने पर आईं फेसबुक, याहू और गूगल जैसी कंपनियां। वैश्विक बहस और आक्रोश के बीच तमाम तरह के तकनीकी रास्ते निकाले गए जिनके जरिए आम लोग अपनी निजता की हिफाजत कर सकते थे। सरकारी एजेंसियों के अलावा अपराधियों और हैकरों के हाथों भी लोगों की निजी सूचनाएं चुरा लिए जाने की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। हाल ही में हमने भारतीय बैंकों के लाखों ग्राहकों के एटीएम कार्ड संबंधी डेटा चुरा लिए जाने की खबरें पढ़ी हैं।
निजी डेटा में घात भले ही सरकार की तरफ से हो या अपराधी तत्वों की तरफ से, तकनीकी कंपनियों के व्यवसाय और भविष्य के लिए यह खतरे की घंटी थी और उन्होंने गलती सुधारते हुए अपने संदेशों को एनक्रिप्ट (कूट भाषा में परिवर्तित) करना शुरू कर दिया। क्या फेसबुक और क्या व्हाट्सएप सबने ऐसी एनक्रिप्शन तकनीकों को अपना लिया जिनके माध्यम से भेजे गए संदेशों को या तो सिर्फ भेजने वाला पढ़, सुन या देख सकता था, या फिर पाने वाला। रास्ते में किसी और के इन संदेशों को देख-सुन लेने की कोई संभावना नहीं बची। तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि कुछ महीने बाद एनक्रिप्शन के जरिए आपकी निजता को सुरक्षित करने की यह प्रक्रिया भी नई चिंताओं को जन्म दे देगी। लेकिन हर चीज के दो पहलू होते ही हैं, सो एनक्रिप्शन की इस सुविधा के भी हैं। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने सुधीर यादव नामक याचिकाकर्ता की वह जनहित याचिका खारिज है जिसमें उन्होंने व्हाट्सएप, वाइबर और बाइक जैसे मैसेंजर एप्स पर यह कहते हुए पाबंदी लगाने की मांग की थी कि उनकी एनक्रिप्शन सुविधा आतंकवाद से जुड़े मामलों में जांच की प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाएगी। आतंकवादियों या दूसरे राष्ट्रविरोधी तत्वों के बीच भेजे जाने वाले संदेशो को पढ़ना सुरक्षा या जांच एजेंसियों के लिए संभव नहीं रह जाएगा। एनक्रिप्टेड संदेशों को पढ़ने में एक सुपर कंप्यूटर को भी सौ साल लग जाएंगे। न्यायालय ने हालांकि इस याचिका को उसके गुण-दोष के आधार पर खारिज नहीं किया बल्कि याचिकाकर्ता को शिकायत का निबटारा करने के लिए दूरसंचार विवाद निबटान के समक्ष अर्जी लगाने की सलाह दी।
क्या हमारी निजता देश की सुरक्षा से भी अधिक कीमती है? इन दिनों अनेक देशों में यह बहस चल रही है। जहां भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने एनक्रिप्शन के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज कर दी वहीं ब्राजील में एक अदालत ने वहां के बैंकों में मौजूद फेसबुक की धनराशि को फ्ऱीज कर दिया है क्योंकि उसने स्थानीय अपराधियों के एनक्रिप्टेड व्हाट्सएप संदेशों को पढ़ने का ब्राजील पुलिस का आग्रह अस्वीकार कर दिया। इस्रायल के गृह मंत्री ने फेसबुक को एक दैत्य की संज्ञा दी है क्योंकि उसने एक इस्रायली किशोरी पर हमला करने वाले फिलस्तीनी हमलावर के फेसबुक संदेशों तक पहुंच मुहैया कराने से इनकार कर दिया। आयरलैंड और रूस की सरकारें इस बात पर अड़ी हुई हैं कि फेसबुक को अपने एनक्रिप्टेड संदेशों को पढ़ने के लिए पिछले दरवाजे से एक रास्ता जरूर उपलब्ध कराना होगा, यानी बैकडोर एन्ट्री।
अजीब बहस है जिसमें दोनों ही पक्ष अपने-अपने दायित्व का जिम्मेदारी से पालन करते दिखाई देते हैं। आम लोगों के संदेशों और सामग्री के संरक्षक के रूप में फेसबुक, गूगल, व्हाट्सएप, वाइबर, टेलीग्राम, हाइक और वाइन आदि की जिम्मेदारी है कि उनकी निजता की हरसंभव सुरक्षा करें। लेकिन सरकार और कानून-व्यवस्था लागू करने वाली एजेंसियों का यह दायित्व है कि राष्ट्रहित तथा नागरिकों के जीवन को सुरक्षित करने के लिए वे हर जरूरी कदम उठाएं, भले ही इसमें उन्हीं के कुछ अधिकारों का हनन होता हो। यहां यह सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि सरकारें अपने इस अधिकार का दुरुपयोग नहीं कर रही हों। राष्ट्रविरोधी तत्वों, आतंकवादियों, अपराधियों और शत्रु देशों के जासूसों के नाम पर वे अपने राजनैतिक विरोधियों या आम लोगों की निजता का अतिक्रमण नहीं कर रही हों। ऐसे में एक लक्ष्मण रेखा खींचने की जरूरत है जिसका पालन सरकार के साथ-साथ इंटरनेट, दूरसंचार तथा मैसेन्जर एप्स के निमार्ताओं के लिए भी अनिवार्य हो।
एपल और अमेरिकी खुफिया एजेंसी एफबीआई के बीच लंबा टकराव चला। सान बर्नार्दिनो (कैलिफोर्निया) में पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी आतंकवादी रिजवान फारूक और उसकी पत्नी तशफीन मलिक ने 14 लोगों को मार डाला। एफबीआई ने दोनों का एक आइफोन बरामद किया था। वह इस नरसंहार की जांच के लिए आइफोन के जरिए भेजे संदेशों को पढ़ना चाहती थी। एपल ने इन एनक्रिप्टेड संदेशों को पढ़ने में मदद करने से साफ इनकार कर दिया। लंबे समय तक दबाव डालने के बाद आखिरकार एफबीआई ने बात वहीं रोक दी क्योंकि उसे इन्हें पढ़ने का कोई 'वैकल्पिक रास्ता' मिल गया था।
गारलैंड (टेक्सास, अमेरिका) में आतंकवादी वारदात की जांच के दौरान एफबीआई को एक अमेरिकी और आतंकवादी संगठन आइएसआइएस के बीच व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे मैसेंजर एप्स पर भेजे गए 109 संदेशों के लेनदेन का पता चला था। वह उनकी जांच नहीं कर सकी क्योंकि ये एनक्रिप्टेड संदेश थे और मैसेंजर कंपनियों ने उन्हें पढ़ने की सुविधा नहीं दी। व्हाट्सएप का कहना है कि उसके सभी संदेश (टेक्स्ट, चित्र, ऑडियो, वीडियो) स्वचालित ढंग से एनक्रिप्ट किए जाते हैं और हैकरों, अपराधियों, साइबर जासूसों और सरकारी एजेंसियों तो क्या, खुद व्हाट्सएप के लिए भी उन्हें पढ़ना संभव नहीं है। इस दावे पर संदेह का कोई कारण नजर नहीं आता क्योंकि ऐसी अभेद्य तकनीकों का विकास हो चुका है जो 128 बिट और 256 बिट एनक्रिप्शन के जरिए यह काम असंभव बना देती हैं।
सरकारों की चिंताएं नाजायज नहीं हैं। इंटरनेट, दूरसंचार और मैसेंजर कंपनियों के भी अपने दायित्व, नैतिकता और व्यावसायिक हित हैं। लेकिन अपवाद के लिए रास्ता बंद नहीं किया जा सकता, खासकर तब जब चिंता लोगों की जिंदगियां बचाने की हो या फिर देश को सुरक्षित रखने की।











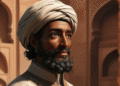
टिप्पणियाँ